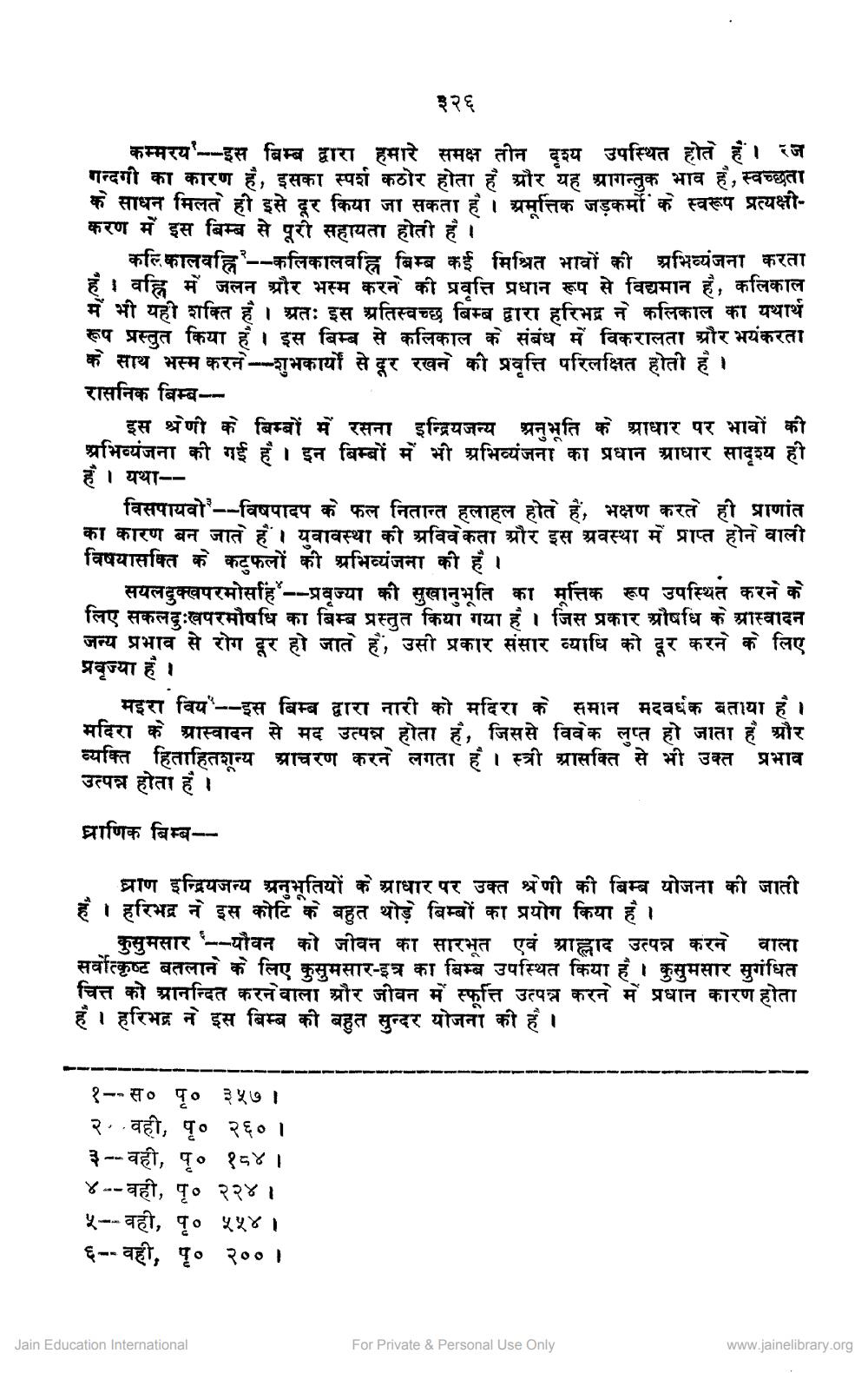________________
३२६
कम्मरय' -- इस बिम्ब द्वारा हमारे समक्ष तीन दृश्य उपस्थित होते हैं । रज गन्दगी का कारण है, इसका स्पर्श कठोर होता है और यह श्रागन्तुक भाव है, स्वच्छता के साधन मिलते ही इसे दूर किया जा सकता है । अमूत्तिक जड़कर्मों के स्वरूप प्रत्यक्षीकरण में इस बिम्ब से पूरी सहायता होती है ।
कलिकालवह्नि -- कलिकालवह्नि बिम्ब कई मिश्रित भावों की अभिव्यंजना करता हूँ । ह्नि में जलन और भस्म करने की प्रवृत्ति प्रधान रूप से विद्यमान है, कलिकाल मैं भी यही शक्ति है । अतः इस प्रतिस्वच्छ बिम्ब द्वारा हरिभद्र ने कलिकाल का यथार्थ रूप प्रस्तुत किया है । इस बिम्ब से कलिकाल के संबंध में विकरालता और भयंकरता के साथ भस्म करने -- शुभकार्यों से दूर रखने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है । रासनिक बिम्ब
इस श्रेणी के बिम्बों में रसना इन्द्रियजन्य अनुभूति के आधार पर भावों की श्रभिव्यंजना की गई हैं । इन बिम्बों में भी अभिव्यंजना का प्रधान आधार सादृश्य ही हैं। यथा-
विसायवो -- विषपादप के फल नितान्त हलाहल होते हैं, भक्षण करते ही प्राणांत का कारण बन जाते हैं । युवावस्था की अविवेकता और इस अवस्था में प्राप्त होने वाली विषयासक्ति के कटुफलों की अभिव्यंजना की है ।
सयल दुक्खपरमोसहि* -- प्रवृज्या को सुखानुभूति का मूत्तिक रूप उपस्थित करने के लिए सकलदुःखपरमौषधि का बिम्ब प्रस्तुत किया गया है । जिस प्रकार औषधि के आस्वादन जन्य प्रभाव से रोग दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार संसार व्याधि को दूर करने के लिए प्रवृज्या है ।
मइरा विय' - - इस बिम्ब द्वारा नारी को मदिरा के समान मदवर्धक बताया है । मदिरा के आस्वादन से मद उत्पन्न होता है, जिससे विवेक लुप्त हो जाता है और व्यक्ति हिताहितशून्य आचरण करने लगता है । स्त्री प्रासक्ति से भी उक्त उत्पन्न होता है ।
प्रभाव
प्राणिक बिम्ब-
प्राण इन्द्रियजन्य अनुभूतियों के आधार पर उक्त श्रेणी की बिम्ब योजना की जाती हैं । हरिभद्र ने इस कोटि के बहुत थोड़े बिम्बों का प्रयोग किया है ।
वाला
कुसुमसार यौवन को जीवन का सारभूत एवं प्रह्लाद उत्पन्न करने सर्वोत्कृष्ट बतलाने के लिए कुसुमसार इत्र का बिम्ब उपस्थित किया है । कुसुमसार सुगंधित चित्त को प्रानन्दित करने वाला और जीवन में स्फूर्ति उत्पन्न करने में प्रधान कारण होता है । हरिभद्र ने इस बिम्ब को बहुत सुन्दर योजना की हैं ।
१- स० पृ०
२. वही, पृ० ३ -- वही,
पृ०
४ -- वही, पृ० ५ -- वही, पृ० ६-- वही, पृ०
Jain Education International
३५७ ॥
२६० ।
१८४ ।
२२४ ॥
५५४।
२०० ।
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org