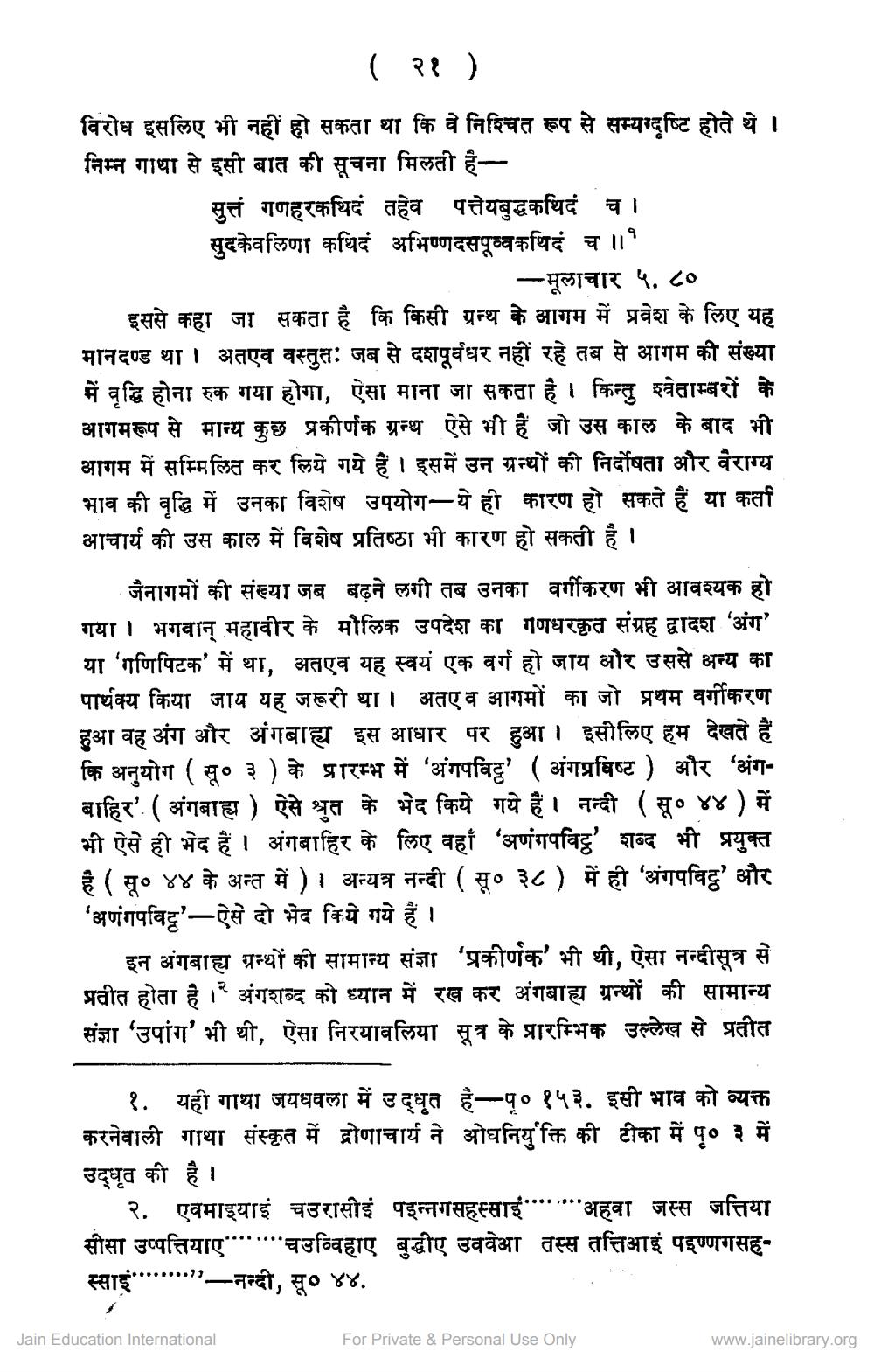________________
( २१ ) विरोध इसलिए भी नहीं हो सकता था कि वे निश्चित रूप से सम्यग्दृष्टि होते थे । निम्न गाथा से इसी बात की सूचना मिलती है
सुत्तं गणहरकथिदं तहेव पत्तेयबुद्धकथिदं च । सुदकेवलिणा कथिदं अभिण्णदसपूवकथिदं च ॥'
-मूलाचार ५. ८० इससे कहा जा सकता है कि किसी ग्रन्थ के आगम में प्रवेश के लिए यह मानदण्ड था। अतएव वस्तुतः जब से दशपूर्वधर नहीं रहे तब से आगम की संख्या में वृद्धि होना रुक गया होगा, ऐसा माना जा सकता है। किन्तु श्वेताम्बरों के आगमरूप से मान्य कुछ प्रकीर्णक ग्रन्थ ऐसे भी हैं जो उस काल के बाद भी आगम में सम्मिलित कर लिये गये हैं। इसमें उन ग्रन्थों की निर्दोषता और वैराग्य भाव की वृद्धि में उनका विशेष उपयोग-ये ही कारण हो सकते हैं या कर्ता आचार्य की उस काल में विशेष प्रतिष्ठा भी कारण हो सकती है।
जैनागमों की संख्या जब बढ़ने लगी तब उनका वर्गीकरण भी आवश्यक हो गया। भगवान महावीर के मौलिक उपदेश का गणधरकृत संग्रह द्वादश 'अंग' या 'गणिपिटक' में था, अतएव यह स्वयं एक वर्ग हो जाय और उससे अन्य का पार्थक्य किया जाय यह जरूरी था। अतए व आगमों का जो प्रथम वर्गीकरण हुआ वह अंग और अंगबाह्य इस आधार पर हुआ। इसीलिए हम देखते है कि अनुयोग ( सू० ३ ) के प्रारम्भ में 'अंगपविट्ट' ( अंगप्रविष्ट ) और 'अंगबाहिर' ( अंगबाह्य ) ऐसे श्रुत के भेद किये गये हैं। नन्दी ( सू० ४४ ) में भी ऐसे ही भेद हैं । अंगबाहिर के लिए वहाँ 'अणंगपविट्ठ' शब्द भी प्रयुक्त है ( सू० ४४ के अन्त में )। अन्यत्र नन्दी ( सू० ३८ ) में ही 'अंगपविट्ठ' और 'अणंगपविट्ठ'-ऐसे दो भेद किये गये हैं।
इन अंगबाह्य ग्रन्थों की सामान्य संज्ञा 'प्रकीर्णक' भी थी, ऐसा नन्दीसूत्र से प्रतीत होता है । अंगशब्द को ध्यान में रख कर अंगबाह्य ग्रन्थों की सामान्य संज्ञा 'उपांग' भी थी, ऐसा निरयावलिया सूत्र के प्रारम्भिक उल्लेख से प्रतीत
१. यही गाथा जयधवला में उद्धृत है-१० १५३. इसी भाव को व्यक्त करनेवाली गाथा संस्कृत में द्रोणाचार्य ने ओघनियुक्ति की टीका में पृ० ३ में उद्धृत की है।
२. एवमाइयाइं चउरासीइं पइन्नगसहस्साई......."अहवा जस्स जत्तिया सीसा उप्पत्तियाए..."चउन्विहाए बुद्धीए उववेआ तस्स तत्तिआइं पइण्णगसहस्साई......."-नन्दी, सू० ४४.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org