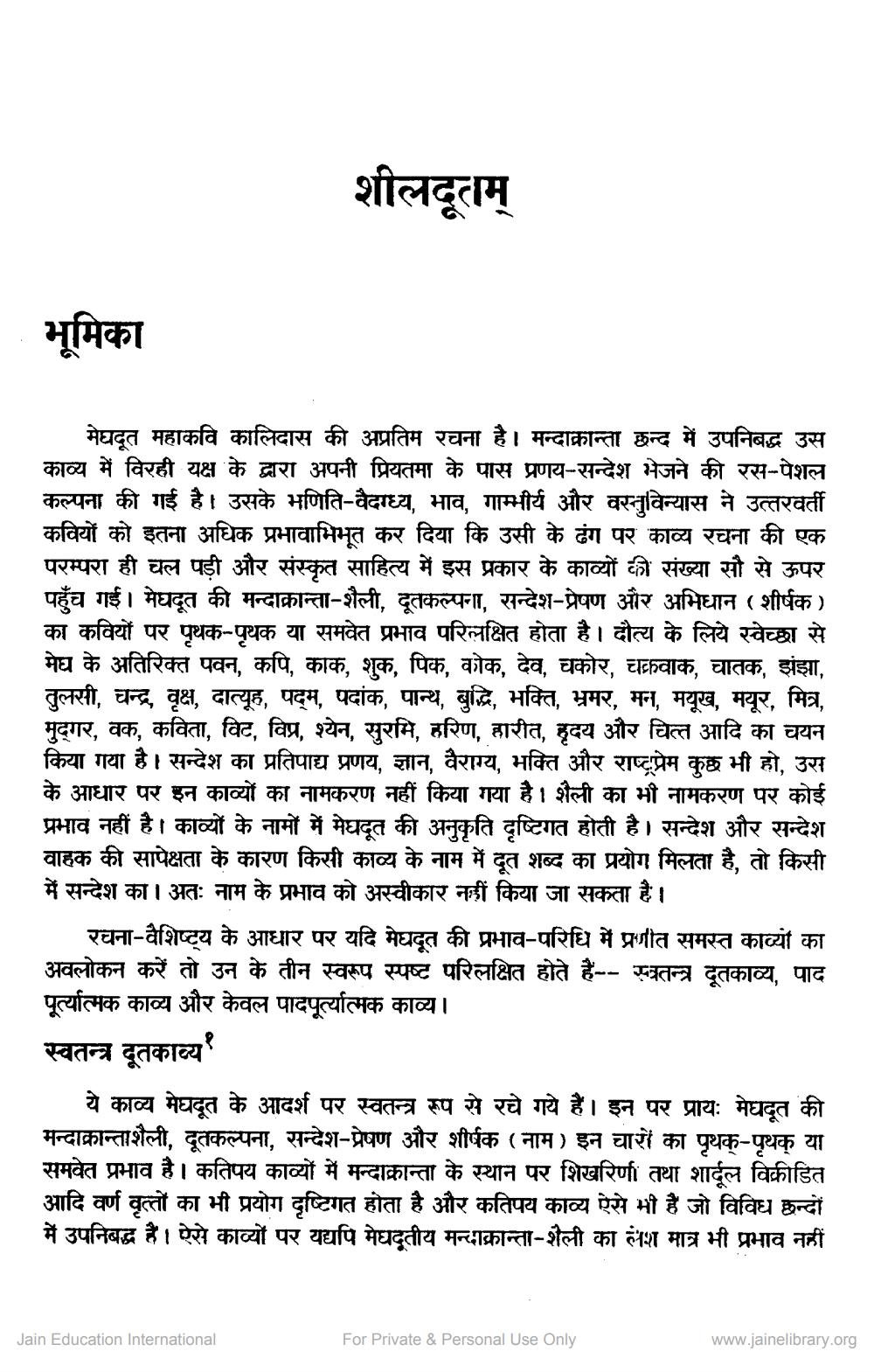________________
शीलदूतम्
भूमिका
मेघदूत महाकवि कालिदास की अप्रतिम रचना है। मन्दाक्रान्ता छन्द में उपनिबद्ध उस काव्य में विरही यक्ष के द्वारा अपनी प्रियतमा के पास प्रणय-सन्देश भेजने की रस-पेशल कल्पना की गई है। उसके भणिति-वैदग्ध्य, भाव, गाम्भीर्य और वस्तुविन्यास ने उत्तरवर्ती कवियों को इतना अधिक प्रभावाभिभूत कर दिया कि उसी के ढंग पर काव्य रचना की एक परम्परा ही चल पड़ी और संस्कृत साहित्य में इस प्रकार के काव्यों की संख्या सौ से ऊपर पहुँच गई। मेघदूत की मन्दाक्रान्ता-शैली, दूतकल्पना, सन्देश-प्रेषण और अभिधान (शीर्षक) का कवियों पर पृथक-पृथक या समवेत प्रभाव परिलक्षित होता है। दौत्य के लिये स्वेच्छा से मेघ के अतिरिक्त पवन, कपि, काक, शुक, पिक, कोक, देव, चकोर, चक्रवाक, चातक, झंझा, तुलसी, चन्द्र, वृक्ष, दात्यूह, पद्म, पदांक, पान्थ, बुद्धि, भक्ति, भ्रमर, मन, मयूख, मयूर, मित्र, मुद्गर, वक, कविता, विट, विप्र, श्येन, सुरमि, हरिण, हारीत, हृदय और चित्त आदि का चयन किया गया है। सन्देश का प्रतिपाद्य प्रणय, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और राष्ट्रप्रेम कुछ भी हो, उस के आधार पर इन काव्यों का नामकरण नहीं किया गया है। शैली का भी नामकरण पर कोई प्रभाव नहीं है। काव्यों के नामों में मेघदूत की अनुकृति दृष्टिगत होती है। सन्देश और सन्देश वाहक की सापेक्षता के कारण किसी काव्य के नाम में दूत शब्द का प्रयोग मिलता है, तो किसी में सन्देश का। अतः नाम के प्रभाव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।
रचना-वैशिष्ट्य के आधार पर यदि मेघदूत की प्रभाव-परिधि में प्रणीत समस्त काव्यों का अवलोकन करें तो उन के तीन स्वरूप स्पष्ट परिलक्षित होते हैं-- स्वतन्त्र दूतकाव्य, पाद पूात्मक काव्य और केवल पादपूर्त्यात्मक काव्य। स्वतन्त्र दूतकाव्य
ये काव्य मेघदूत के आदर्श पर स्वतन्त्र रूप से रचे गये हैं। इन पर प्रायः मेघदूत की मन्दाक्रान्ताशैली, दूतकल्पना, सन्देश-प्रेषण और शीर्षक (नाम ) इन चारों का पृथक्-पृथक् या समवेत प्रभाव है। कतिपय काव्यों में मन्दाक्रान्ता के स्थान पर शिखरिणी तथा शार्दूल विक्रीडित आदि वर्ण वृत्तों का भी प्रयोग दृष्टिगत होता है और कतिपय काव्य ऐसे भी है जो विविध छन्दों में उपनिबद्ध हैं। ऐसे काव्यों पर यद्यपि मेघदूतीय मन्दाक्रान्ता-शैली का लश मात्र भी प्रभाव नहीं
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org