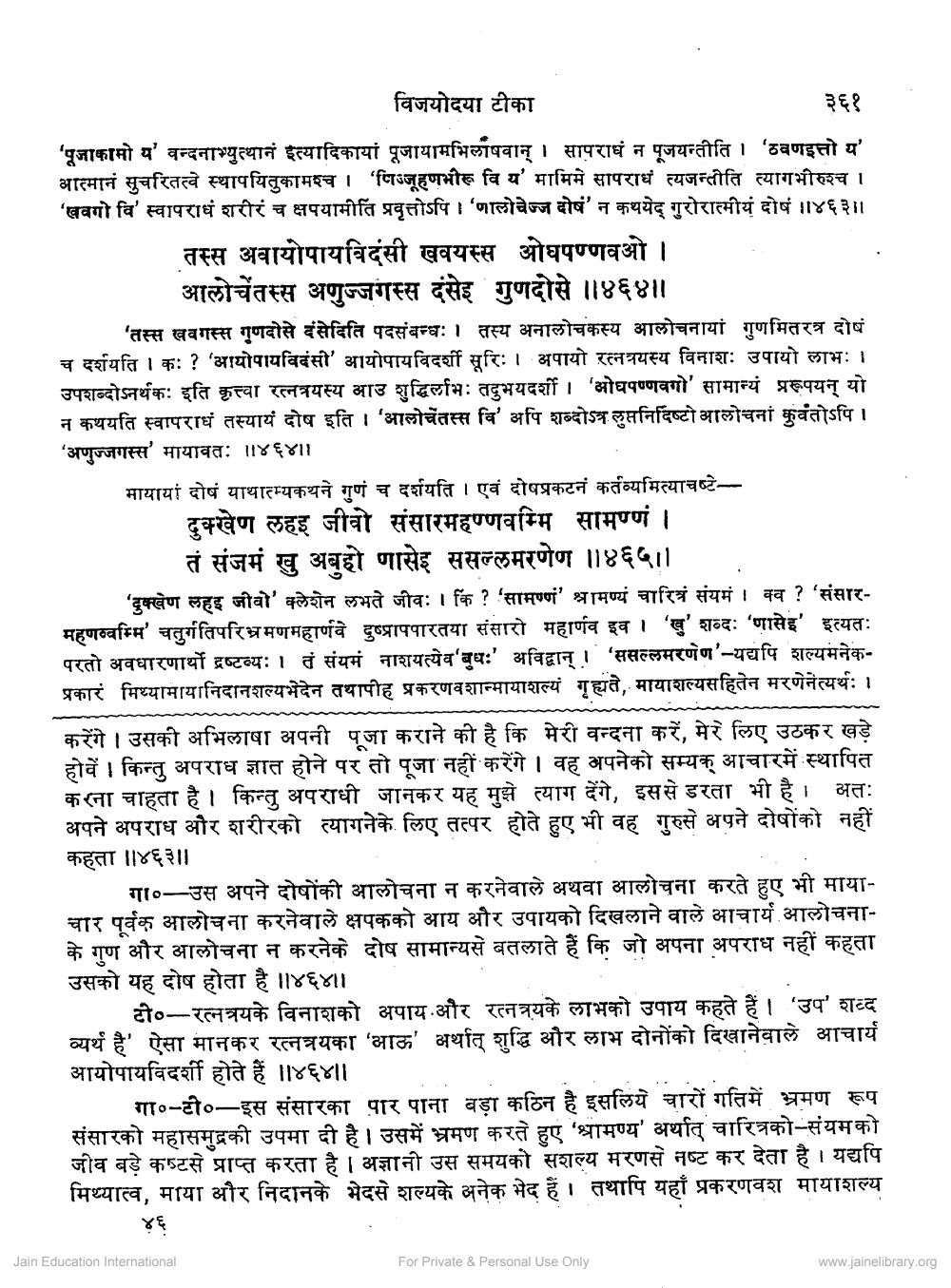________________
विजयोदया टीका 'पूजाकामो य' वन्दनाभ्युत्थानं इत्यादिकायां पूजायामभिलाषवान् । सापराधं न पूजयन्तीति । 'ठवणइत्तो य' आत्मानं सुचरितत्वे स्थापयितुकामश्च । “णिज्जूहणभीरू वि य' मामिमे सापराधं त्यजन्तीति त्यागभीरुश्च । 'खवगो वि' स्वापराधं शरीरं च क्षपयामीति प्रवृत्तोऽपि । 'गालोचेज्ज दोषं' न कथयेद् गुरोरात्मीयं दोषं ।।४६३।।
तस्स अवायोपायविदंसी खवयस्स ओघपण्णवओ ।
आलोचंतस्स अणुज्जगस्स दंसेइ गुणदोसे ॥४६४॥ 'तस्स खवगस्स गुणदोसे दंसेदिति पदसंबन्धः । तस्य अनालोचकस्य आलोचनायां गुणमितरत्र दोषं च दर्शयति । कः ? 'आयोपायविवंसी' आयोपायविदर्शी सूरिः । अपायो रत्नत्रयस्य विनाशः उपायो लाभः । उपशब्दोऽनर्थकः इति कृत्वा रत्नत्रयस्य आउ शुद्धिाभः तदुभयदर्शी । 'ओघपण्णवगो' सामान्यं प्ररूपयन यो न कथयति स्वापराधं तस्यायं दोष इति । 'आलोचेंतस्स वि' अपि शब्दोऽत्रलप्तनिर्दिष्टोआलोचनां कुर्वतोऽपि । 'अणुज्जगस्स' मायावतः ॥४६४॥ मायायां दोषं याथात्म्यकथने गुणं च दर्शयति । एवं दोषप्रकटनं कर्तव्यमित्याचष्टे
दुक्खेण लहइ जीवो संसारमहण्णवम्मि सामण्णं ।
तं संजमं खु अबुहो णासेइ ससल्लमरणेण ॥४६५।। 'दुक्खेण लहइ जीवो' क्लेशेन लभते जीवः । किं ? 'सामण्णं' श्रामण्यं चारित्रं संयमं । क्व ? 'संसारमहणवम्मि' चतुर्गतिपरिभ्रमणमहार्णवे दुष्प्रापपारतया संसारो महार्णव इव । 'खु' शब्दः ‘णासेइ' इत्यतः परतो अवधारणाओं द्रष्टव्यः । तं संयमं नाशयत्येव'बुधः' अविद्वान् । 'ससल्लमरणेण'-यद्यपि शल्यमनेकप्रकारं मिथ्यामायानिदानशल्यभेदेन तथापीह प्रकरणवशान्मायाशल्यं गृह्यते, मायाशल्यसहितेन मरणेनेत्यर्थः । करेंगे । उसकी अभिलाषा अपनी पूजा कराने की है कि मेरी वन्दना करें, मेरे लिए उठकर खड़े होवें । किन्तु अपराध ज्ञात होने पर तो पूजा नहीं करेंगे । वह अपनेको सम्यक् आचारमें स्थापित करना चाहता है। किन्तु अपराधी जानकर यह मुझे त्याग देंगे, इससे डरता भी है। अतः अपने अपराध और शरीरको त्यागनेके लिए तत्पर होते हुए भी वह गुरुसे अपने दोषोंको नहीं कहता ॥४६३||
गा०—उस अपने दोषोंकी आलोचना न करनेवाले अथवा आलोचना करते हुए भी मायाचार पूर्वक आलोचना करनेवाले क्षपकको आय और उपायको दिखलाने वाले आचार्य आलोचनाके गुण और आलोचना न करनेके दोष सामान्यसे बतलाते हैं कि जो अपना अपराध नहीं कहता उसको यह दोष होता है ।।४६४।।
टो०-रत्नत्रयके विनाशको अपाय और रत्नत्रयके लाभको उपाय कहते हैं। 'उप' शब्द व्यर्थ है' ऐसा मानकर रत्नत्रयका 'आऊ' अर्थात् शुद्धि और लाभ दोनोंको दिखानेवाले आचार्य आयोपायविदर्शी होते हैं ॥४६४||
गा०-टी०-इस संसारका पार पाना बड़ा कठिन है इसलिये चारों गतिमें भ्रमण रूप संसारको महासमुद्रकी उपमा दी है। उसमें भ्रमण करते हुए 'श्रामण्य' अर्थात् चारित्रको-संयमको जीव बड़े कष्टसे प्राप्त करता है । अज्ञानी उस समयको सशल्य मरणसे नष्ट कर देता है । यद्यपि मिथ्यात्व, माया और निदानके भेदसे शल्यके अनेक भेद हैं। तथापि यहाँ प्रकरणवश मायाशल्य
४६
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org