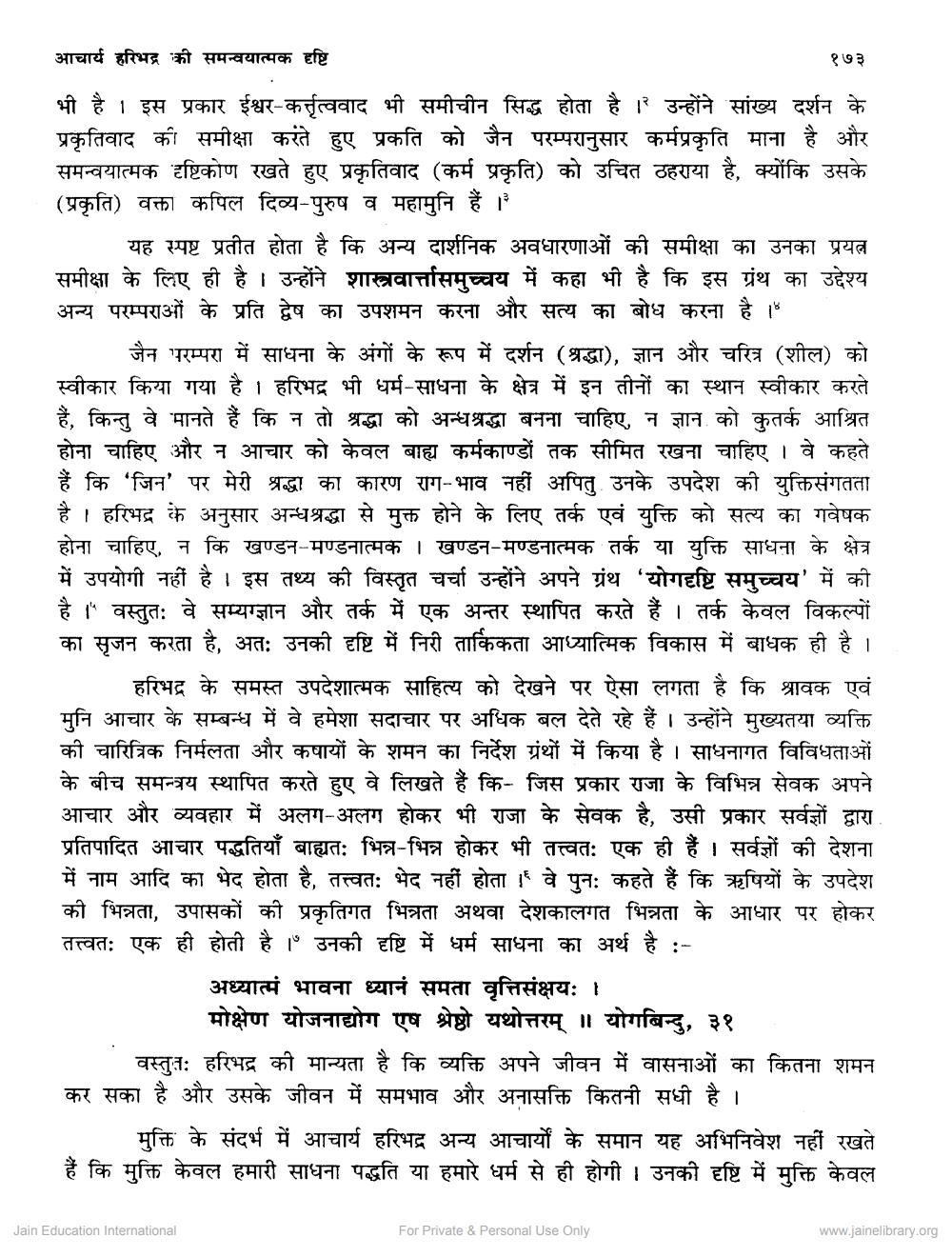________________
आचार्य हरिभद्र की समन्वयात्मक दृष्टि
१७३
भी है । इस प्रकार ईश्वर-कर्तृत्ववाद भी समीचीन सिद्ध होता है । उन्होंने सांख्य दर्शन के प्रकृतिवाद की समीक्षा करते हुए प्रकति को जैन परम्परानुसार कर्मप्रकृति माना है और समन्वयात्मक दृष्टिकोण रखते हुए प्रकृतिवाद (कर्म प्रकृति) को उचित ठहराया है, क्योंकि उसके (प्रकृति) वक्ता कपिल दिव्य-पुरुष व महामुनि हैं ।'
यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अन्य दार्शनिक अवधारणाओं की समीक्षा का उनका प्रयत्न समीक्षा के लिए ही है । उन्होंने शास्त्रवार्तासमुच्चय में कहा भी है कि इस ग्रंथ का उद्देश्य अन्य परम्पराओं के प्रति द्वेष का उपशमन करना और सत्य का बोध करना है ।
जैन परम्परा में साधना के अंगों के रूप में दर्शन (श्रद्धा), ज्ञान और चरित्र (शील) को स्वीकार किया गया है । हरिभद्र भी धर्म-साधना के क्षेत्र में इन तीनों का स्थान स्वीकार करते हैं. किन्त वे मानते हैं कि न तो श्रद्धा को अन्धश्रद्धा बनना चाहिए, न ज्ञान को कतर्क आश्रित होना चाहिए और न आचार को केवल बाह्य कर्मकाण्डों तक सीमित रखना चाहिए । वे कहते हैं कि 'जिन' पर मेरी श्रद्धा का कारण राग-भाव नहीं अपितु उनके उपदेश की युक्तिसंगतता है । हरिभद्र के अनुसार अन्धश्रद्धा से मुक्त होने के लिए तर्क एवं युक्ति को सत्य का गवेषक होना चाहिए, न कि खण्डन-मण्डनात्मक । खण्डन-मण्डनात्मक तर्क या युक्ति साधना के क्षेत्र में उपयोगी नहीं है । इस तथ्य की विस्तृत चर्चा उन्होंने अपने ग्रंथ 'योगदृष्टि समुच्चय' में की है । वस्तुतः वे सम्यग्ज्ञान और तर्क में एक अन्तर स्थापित करते हैं । तर्क केवल विकल्पों का सृजन करता है, अत: उनकी दृष्टि में निरी तार्किकता आध्यात्मिक विकास में बाधक ही है ।
हरिभद्र के समस्त उपदेशात्मक साहित्य को देखने पर ऐसा लगता है कि श्रावक एवं मुनि आचार के सम्बन्ध में वे हमेशा सदाचार पर अधिक बल देते रहे हैं। उन्होंने मुख्यतया व्यक्ति की चारित्रिक निर्मलता और कषायों के शमन का निर्देश ग्रंथों में किया है। साधनागत विविधताओं के बीच समन्वय स्थापित करते हुए वे लिखते हैं कि- जिस प्रकार राजा के विभिन्न सेवक अपने आचार और व्यवहार में अलग-अलग होकर भी राजा के सेवक है, उसी प्रकार सर्वज्ञों द्वारा प्रतिपादित आचार पद्धतियाँ बाह्यत: भिन्न-भिन्न होकर भी तत्त्वत: एक ही हैं । सर्वज्ञों की देशना में नाम आदि का भेद होता है, तत्त्वतः भेद नहीं होता । वे पुनः कहते हैं कि ऋषियों के उपदेश की भिन्नता, उपासकों की प्रकृतिगत भिन्नता अथवा देशकालगत भिन्नता के आधार पर होकर तत्त्वतः एक ही होती है। उनकी दृष्टि में धर्म साधना का अर्थ है :
अध्यात्म भावना ध्यानं समता वृत्तिसंक्षयः ।
मोक्षेण योजनाद्योग एष श्रेष्ठो यथोत्तरम् ॥ योगबिन्दु, ३१ वस्तुतः हरिभद्र की मान्यता है कि व्यक्ति अपने जीवन में वासनाओं का कितना शमन कर सका है और उसके जीवन में समभाव और अनासक्ति कितनी सधी है ।
__ मुक्ति के संदर्भ में आचार्य हरिभद्र अन्य आचार्यों के समान यह अभिनिवेश नहीं रखते हैं कि मुक्ति केवल हमारी साधना पद्धति या हमारे धर्म से ही होगी । उनकी दृष्टि में मुक्ति केवल
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org