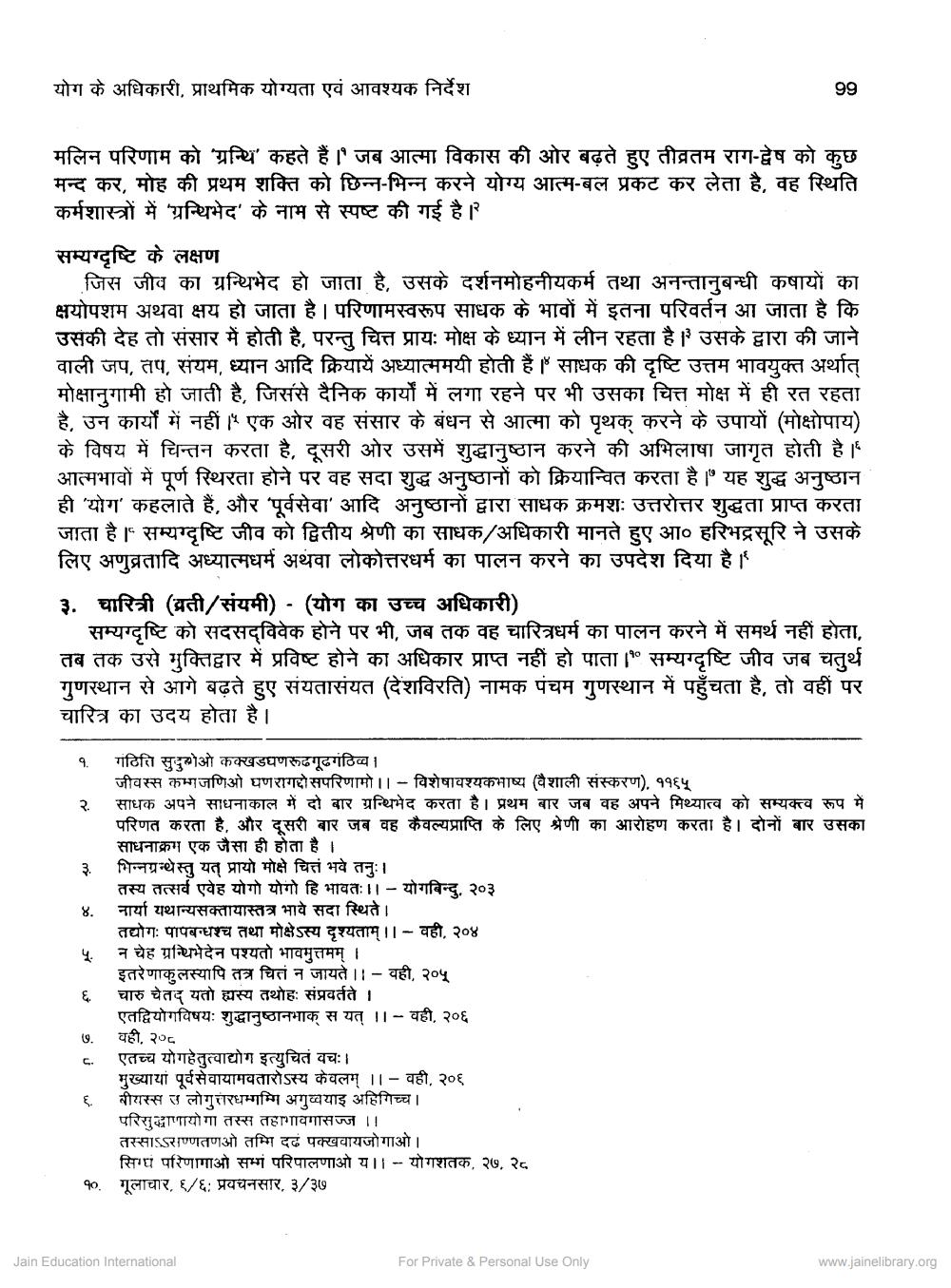________________
योग के अधिकारी, प्राथमिक योग्यता एवं आवश्यक निर्देश
99
मन्दिक परिणाम को प्रथमिथ
मलिन परिणाम को 'ग्रन्थि' कहते हैं। जब आत्मा विकास की ओर बढ़ते हुए तीव्रतम राग-द्वेष को कुछ मन्द कर, मोह की प्रथम शक्ति को छिन्न-भिन्न करने योग्य आत्म-बल प्रकट कर लेता है, वह स्थिति कर्मशास्त्रों में 'ग्रन्थिभेद' के नाम से स्पष्ट की गई है।
सम्यग्दृष्टि के लक्षण
जिस जीव का ग्रन्थिभेद हो जाता है, उसके दर्शनमोहनीयकर्म तथा अनन्तानुबन्धी कषायों का क्षयोपशम अथवा क्षय हो जाता है। परिणामस्वरूप साधक के भावों में इतना परिवर्तन आ जाता है कि उसकी देह तो संसार में होती है, परन्तु चित्त प्रायः मोक्ष के ध्यान में लीन रहता है। उसके द्वारा की जाने वाली जप, तप, संयम, ध्यान आदि क्रियायें अध्यात्ममयी होती हैं। साधक की दृष्टि उत्तम भावयुक्त अर्थात् मोक्षानुगामी हो जाती है, जिससे दैनिक कार्यों में लगा रहने पर भी उसका चित्त मोक्ष में ही रत रहता है, उन कार्यों में नहीं। एक ओर वह संसार के बंधन से आत्मा को पृथक् करने के उपायों (मोक्षोपाय) के विषय में चिन्तन करता है, दूसरी ओर उसमें शुद्धानुष्ठान करने की अभिलाषा जागृत होती है। आत्मभावों में पूर्ण स्थिरता होने पर वह सदा शुद्ध अनुष्ठानों को क्रियान्वित करता है। यह शुद्ध अनुष्ठान ही 'योग' कहलाते हैं, और पूर्वसेवा' आदि अनुष्ठानों द्वारा साधक क्रमशः उत्तरोत्तर शुद्धता प्राप्त करता जाता है। सम्यग्दृष्टि जीव को द्वितीय श्रेणी का साधक/अधिकारी मानते हुए आ० हरिभद्रसूरि ने उसके लिए अणुव्रतादि अध्यात्मधर्म अथवा लोकोत्तरधर्म का पालन करने का उपदेश दिया है।
३. चारित्री (व्रती/संयमी) - (योग का उच्च अधिकारी)
सम्यग्दृष्टि को सदसद्विवेक होने पर भी, जब तक वह चारित्रधर्म का पालन करने में समर्थ नहीं होता, तब तक उसे मुक्तिद्वार में प्रविष्ट होने का अधिकार प्राप्त नहीं हो पाता। सम्यग्दृष्टि जीव जब चतुर्थ गुणस्थान से आगे बढ़ते हुए संयतासंयत (देशविरति) नामक पंचम गुणस्थान में पहुँचता है, तो वहीं पर चारित्र का उदय होता है।
१. गठिति सुदुखोओ कक्खडपणरूढगूढगठिव्व।।
जीवस्स काजणिओ घणरागदो सपरिणामो।। -विशेषावश्यकभाष्य (वैशाली संस्करण). ११६५ साधक अपने साधनाकाल में दो बार ग्रन्थिभेद करता है। प्रथम बार जब वह अपने मिथ्यात्व को सम्यक्त्व रूप में परिणत करता है, और दूसरी बार जब वह कैवल्यप्राप्ति के लिए श्रेणी का आरोहण करता है। दोनों बार उसका साधनाक्रम एक जैसा ही होता है । भिन्नग्रन्थेस्तु यत् प्रायो मोक्षे चित्तं भवे तनुः ।
तस्य तत्सर्व एवेह योगो योगो हि भावतः।। -योगबिन्दु. २०३ ४. नार्या यथान्यसक्तायास्तत्र भावे सदा स्थिते।
तद्योगः पापबन्धश्च तथा मोक्षेऽस्य दृश्यताम् ।। - वही, २०४ ५. न चेह ग्रन्थिभेदेन पश्यतो भावमुत्तमम् ।
इतरेणाकुलस्यापि तत्र चितं न जायते ।। - वही, २०५ चारु चेतद् यतो ह्यस्य तथोहः संप्रवर्तते ।
एतद्वियोगविषयः शुद्धानुष्ठानभाक स यत् ।। - वही, २०६ ७. वही, २०८
एतच्च योगहेतुत्वाद्योग इत्युचितं वचः। मुख्यायां पूर्वसेवायामवतारोऽस्य केवलम् ।। - वही, २०६ बीयस्स उ लोगुत्तरधम्गम्गि अगुव्वयाइ अहिगिच्च । परिसुद्धाणायोगा तस्स तहागावगासज्ज ।। तरसाऽऽसण्णतणओ तम्मि ददं पक्खवायजोगाओ।
सिप परिणागाओ सग परिपालणाओ य।। - योगशतक, २७.२८ १०. गूलाचार, ६/६: प्रवचनसार, ३/३७
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org