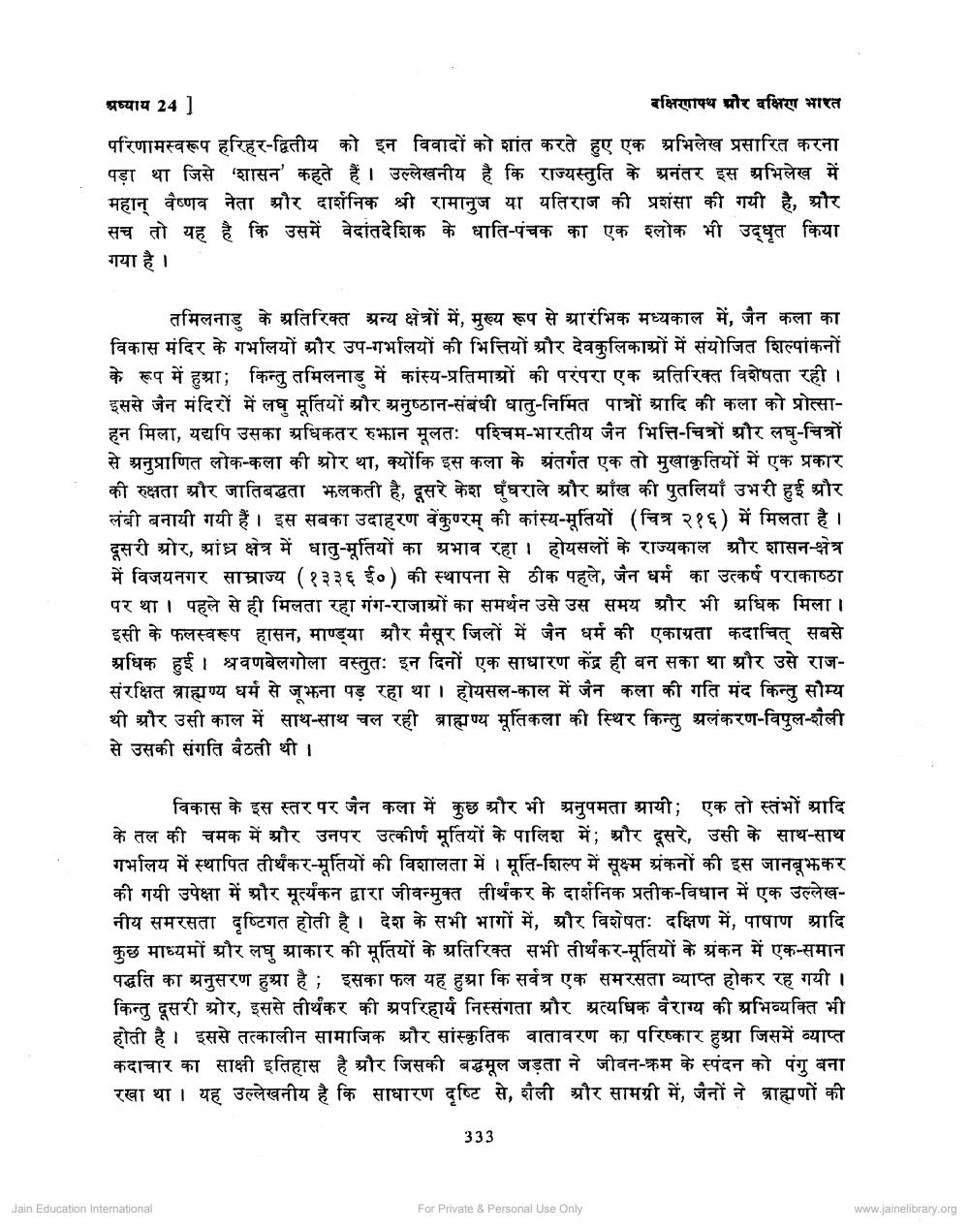________________
अध्याय 24]
दक्षिणापथ और दक्षिण भारत
परिणामस्वरूप हरिहर-द्वितीय को इन विवादों को शांत करते हुए एक अभिलेख प्रसारित करना पड़ा था जिसे 'शासन' कहते हैं। उल्लेखनीय है कि राज्यस्तुति के अनंतर इस अभिलेख में महान वैष्णव नेता और दार्शनिक श्री रामानुज या यतिराज की प्रशंसा की गयी है, और सच तो यह है कि उसमें वेदांतदेशिक के धाति-पंचक का एक श्लोक भी उद्धृत किया गया है।
तमिलनाडु के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में, मुख्य रूप से प्रारंभिक मध्यकाल में, जैन कला का विकास मंदिर के गर्भालयों और उप-गर्भालयों की भित्तियों और देवकुलिकाओं में संयोजित शिल्पांकनों के रूप में हुआ; किन्तु तमिलनाडु में कांस्य-प्रतिमाओं की परंपरा एक अतिरिक्त विशेषता रही। इससे जैन मंदिरों में लघु मूर्तियों और अनुष्ठान-संबंधी धातु-निर्मित पात्रों आदि की कला को प्रोत्साहन मिला, यद्यपि उसका अधिकतर रुझान मूलतः पश्चिम-भारतीय जैन भित्ति-चित्रों और लघु-चित्रों से अनुप्राणित लोक-कला की ओर था, क्योंकि इस कला के अंतर्गत एक तो मुखाकृतियों में एक प्रकार की रुक्षता और जातिबद्धता झलकती है, दूसरे केश धुंघराले और आँख की पुतलियाँ उभरी हुई और लंबी बनायी गयी हैं। इस सबका उदाहरण वेंकरम की कांस्य-मतियों (चित्र २१६) में मिलता है। दूसरी ओर, अांध्र क्षेत्र में धातु-मूर्तियों का प्रभाव रहा। होयसलों के राज्यकाल और शासन-क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य (१३३६ ई०) की स्थापना से ठीक पहले, जैन धर्म का उत्कर्ष पराकाष्ठा पर था। पहले से ही मिलता रहा गंग-राजाओं का समर्थन उसे उस समय और भी अधिक मिला। इसी के फलस्वरूप हासन, माण्ड्या और मैसूर जिलों में जैन धर्म की एकाग्रता कदाचित् सबसे अधिक हुई। श्रवणबेलगोला वस्तुतः इन दिनों एक साधारण केंद्र ही बन सका था और उसे राजसंरक्षित ब्राह्मण्य धर्म से जूझना पड़ रहा था। होयसल-काल में जैन कला की गति मंद किन्तु सौम्य थी और उसी काल में साथ-साथ चल रही ब्राह्मण्य मूर्तिकला की स्थिर किन्तु अलंकरण-विपुल-शैली से उसकी संगति बैठती थी।
विकास के इस स्तर पर जैन कला में कुछ और भी अनुपमता आयी; एक तो स्तंभों आदि के तल की चमक में और उनपर उत्कीर्ण मूर्तियों के पालिश में; और दूसरे, उसी के साथ-साथ गर्भालय में स्थापित तीर्थंकर-मूर्तियों की विशालता में । मूर्ति-शिल्प में सूक्ष्म अंकनों की इस जानबूझकर की गयी उपेक्षा में और मूर्यंकन द्वारा जीवन्मुक्त तीर्थंकर के दार्शनिक प्रतीक-विधान में एक उल्लेखनीय समरसता दृष्टिगत होती है। देश के सभी भागों में, और विशेषतः दक्षिण में, पाषाण आदि कुछ माध्यमों और लघु आकार की मूर्तियों के अतिरिक्त सभी तीर्थंकर-मूर्तियों के अंकन में एक-समान पद्धति का अनुसरण हुआ है ; इसका फल यह हुआ कि सर्वत्र एक समरसता व्याप्त होकर रह गयी। किन्तु दूसरी ओर, इससे तीर्थकर की अपरिहार्य निस्संगता और अत्यधिक वैराग्य की अभिव्यक्ति भी होती है। इससे तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का परिष्कार हा जिसमें व्याप्त कदाचार का साक्षी इतिहास है और जिसकी बद्धमूल जड़ता ने जीवन-क्रम के स्पंदन को पंगु बना रखा था। यह उल्लेखनीय है कि साधारण दृष्टि से, शैली और सामग्री में, जैनों ने ब्राह्मणों की
333
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org