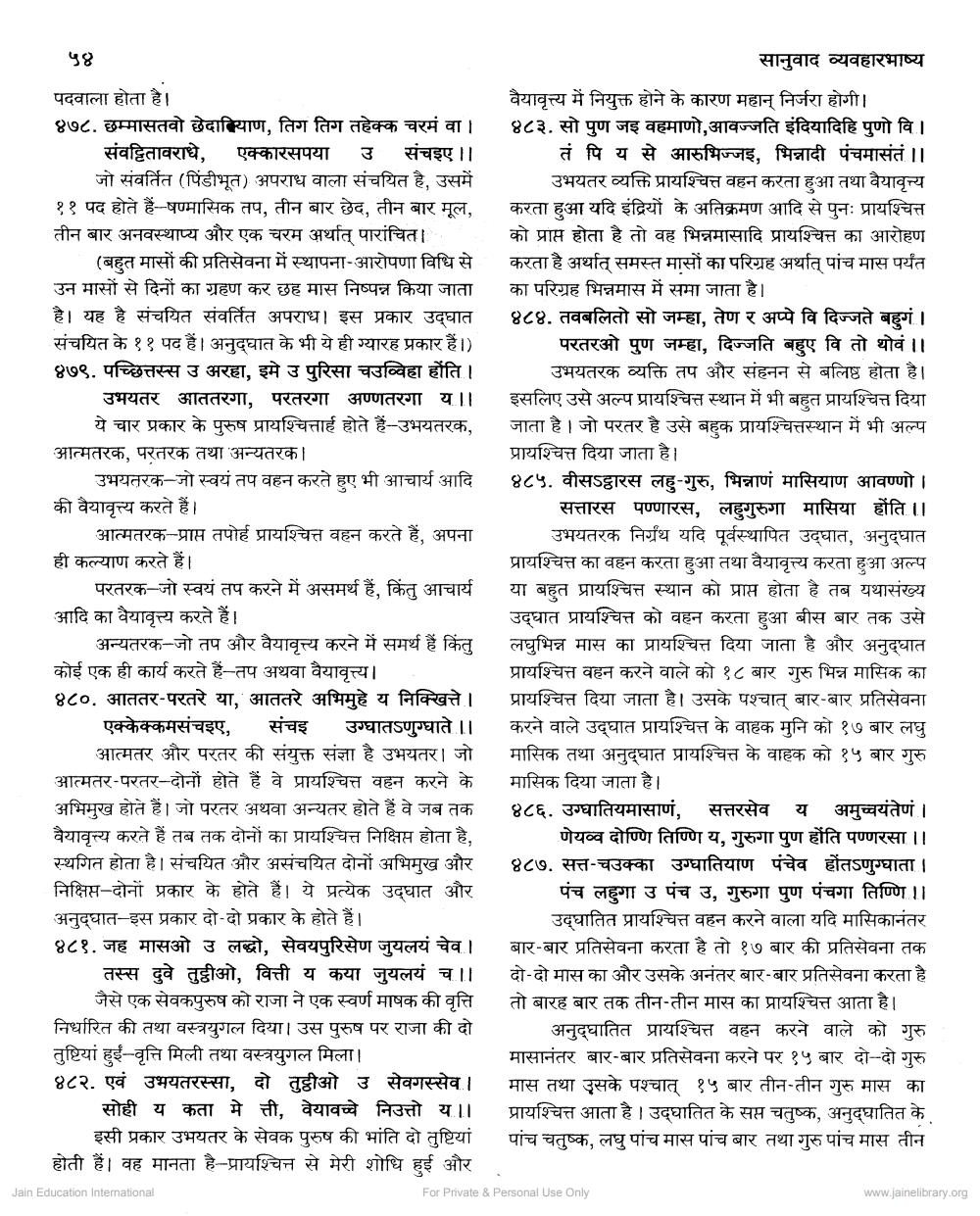________________
५४
सानुवाद व्यवहारभाष्य पदवाला होता है।
वैयावृत्त्य में नियुक्त होने के कारण महान् निर्जरा होगी। ४७८. छम्मासतवो छेदाबियाण, तिग तिग तहेक्क चरमं वा। ४८३. सो पुण जइ वमाणो,आवज्जति इंदियादिहि पुणो वि ।
संवट्टितावराधे, एक्कारसपया उ संचइए ।। तं पि य से आरुभिज्जइ, भिन्नादी पंचमासंतं ।।
जो संवर्तित (पिंडीभूत) अपराध वाला संचयित है, उसमें उभयतर व्यक्ति प्रायश्चित्त वहन करता हुआ तथा वैयावृत्त्य ११ पद होते हैं--षण्मासिक तप, तीन बार छेद, तीन बार मूल, करता हुआ यदि इंद्रियों के अतिक्रमण आदि से पुनः प्रायश्चित्त तीन बार अनवस्थाप्य और एक चरम अर्थात् पारांचित। को प्राप्त होता है तो वह भिन्नमासादि प्रायश्चित्त का आरोहण
(बहुत मासों की प्रतिसेवना में स्थापना-आरोपणा विधि से करता है अर्थात् समस्त मासों का परिग्रह अर्थात् पांच मास पर्यंत उन मासों से दिनों का ग्रहण कर छह मास निष्पन्न किया जाता का परिग्रह भिन्नमास में समा जाता है। है। यह है संचयित संवर्तित अपराध। इस प्रकार उद्घात ४८४. तवबलितो सो जम्हा, तेण र अप्पे वि दिज्जते बहुगं । संचयित के ११ पद हैं। अनुद्घात के भी ये ही ग्यारह प्रकार हैं।) परतरओ पुण जम्हा, दिज्जति बहुए वि तो थोवं ।। ४७९. पच्छित्तस्स उ अरहा, इमे उ पुरिसा चउब्विहा होति । उभयतरक व्यक्ति तप और संहनन से बलिष्ठ होता है।
उभयतर आततरगा, परतरगा अण्णतरगा य ।। इसलिए उसे अल्प प्रायश्चित्त स्थान में भी बहुत प्रायश्चित्त दिया
ये चार प्रकार के पुरुष प्रायश्चित्ताह होते हैं-उभयतरक, जाता है। जो परतर है उसे बहुक प्रायश्चित्तस्थान में भी अल्प आत्मतरक, परतरक तथा अन्यतरक।
प्रायश्चित्त दिया जाता है। उभयतरक-जो स्वयं तप वहन करते हए भी आचार्य आदि ४८५. वीसऽट्ठारस लहु-गुरु, भिन्नाणं मासियाण आवण्णो। की वैयावृत्त्य करते हैं।
सत्तारस पण्णारस, लहुगुरुगा मासिया होति ।। आत्मतरक-प्राप्त तपोर्ह प्रायश्चित्त वहन करते हैं, अपना उभयतरक निग्रंथ यदि पूर्वस्थापित उद्घात, अनुद्घात ही कल्याण करते हैं।
प्रायश्चित्त का वहन करता हुआ तथा वैयावृत्त्य करता हुआ अल्प परतरक-जो स्वयं तप करने में असमर्थ हैं, किंतु आचार्य या बहुत प्रायश्चित्त स्थान को प्राप्त होता है तब यथासंख्य आदि का वैयावृत्त्य करते हैं।
उद्धात प्रायश्चित्त को वहन करता हुआ बीस बार तक उसे अन्यतरक-जो तप और वैयावृत्त्य करने में समर्थ हैं किंतु लघुभिन्न मास का प्रायश्चित्त दिया जाता है और अनुयात कोई एक ही कार्य करते हैं-तप अथवा वैयावृत्त्य।
प्रायश्चित्त वहन करने वाले को १८ बार गुरु भिन्न मासिक का ४८०. आततर-परतरे या, आततरे अभिमुहे य निक्खित्ते। प्रायश्चित्त दिया जाता है। उसके पश्चात् बार-बार प्रतिसेवना
एक्केक्कमसंचइए, संचइ उग्घातऽणुग्घाते ।। करने वाले उद्घात प्रायश्चित्त के वाहक मुनि को १७ बार लघु
आत्मतर और परतर की संयुक्त संज्ञा है उभयतर। जो मासिक तथा अनुद्घात प्रायश्चित्त के वाहक को १५ बार गुरु आत्मतर-परतर-दोनों होते हैं वे प्रायश्चित्त वहन करने के मासिक दिया जाता है। अभिमुख होते हैं। जो परतर अथवा अन्यतर होते हैं वे जब तक ४८६. उग्घातियमासाणं, सत्तरसेव य अमुच्चयंतेणं । वैयावृत्त्य करते हैं तब तक दोनों का प्रायश्चित्त निक्षिप्त होता है, णेयव्व दोण्णि तिण्णि य, गुरुगा पुण होति पण्णरसा ।। स्थगित होता है। संचयित और असंचयित दोनों अभिमुख और ४८७. सत्त-चउक्का उग्धातियाण पंचेव होतऽणुग्घाता। निक्षिप्त-दोनों प्रकार के होते हैं। ये प्रत्येक उद्घात और पंच लहुगा उ पंच उ, गुरुगा पुण पंचगा तिणि ।। अनुद्घात-इस प्रकार दो-दो प्रकार के होते हैं।
उद्घातित प्रायश्चित्त वहन करने वाला यदि मासिकानंतर ४८१. जह मासओ उ लद्धो, सेवयपुरिसेण जुयलयं चेव। बार-बार प्रतिसेवना करता है तो १७ बार की प्रतिसेवना तक
तस्स दुवे तुट्ठीओ, वित्ती य कया जुयलयं च ।।। दो-दो मास का और उसके अनंतर बार-बार प्रतिसेवना करता है
जैसे एक सेवकपुरुष को राजा ने एक स्वर्ण माषक की वृत्ति। तो बारह बार तक तीन-तीन मास का प्रायश्चित्त आता है। निर्धारित की तथा वस्त्रयुगल दिया। उस पुरुष पर राजा की दो ___अनुद्घातित प्रायश्चित्त वहन करने वाले को गुरु तुष्टियां हुईं-वृत्ति मिली तथा वस्त्रयुगल मिला।
मासानंतर बार-बार प्रतिसेवना करने पर १५ बार दो-दो गुरु ४८२. एवं उभयतरस्सा, दो तुट्ठीओ उ सेवगस्सेव।। मास तथा उसके पश्चात् १५ बार तीन-तीन गुरु मास का
सोही य कता मे त्ती, वेयावच्चे निउत्तो य ।। प्रायश्चित्त आता है। उद्घातित के सप्त चतुष्क, अनुद्घातित के.
इसी प्रकार उभयतर के सेवक पुरुष की भांति दो तुष्टियां पांच चतुष्क, लघु पांच मास पांच बार तथा गुरु पांच मास तीन होती हैं। वह मानता है-प्रायश्चित्त से मेरी शोधि हुई और .
www.jainelibrary.org
Jain Education International
For Private & Personal Use Only