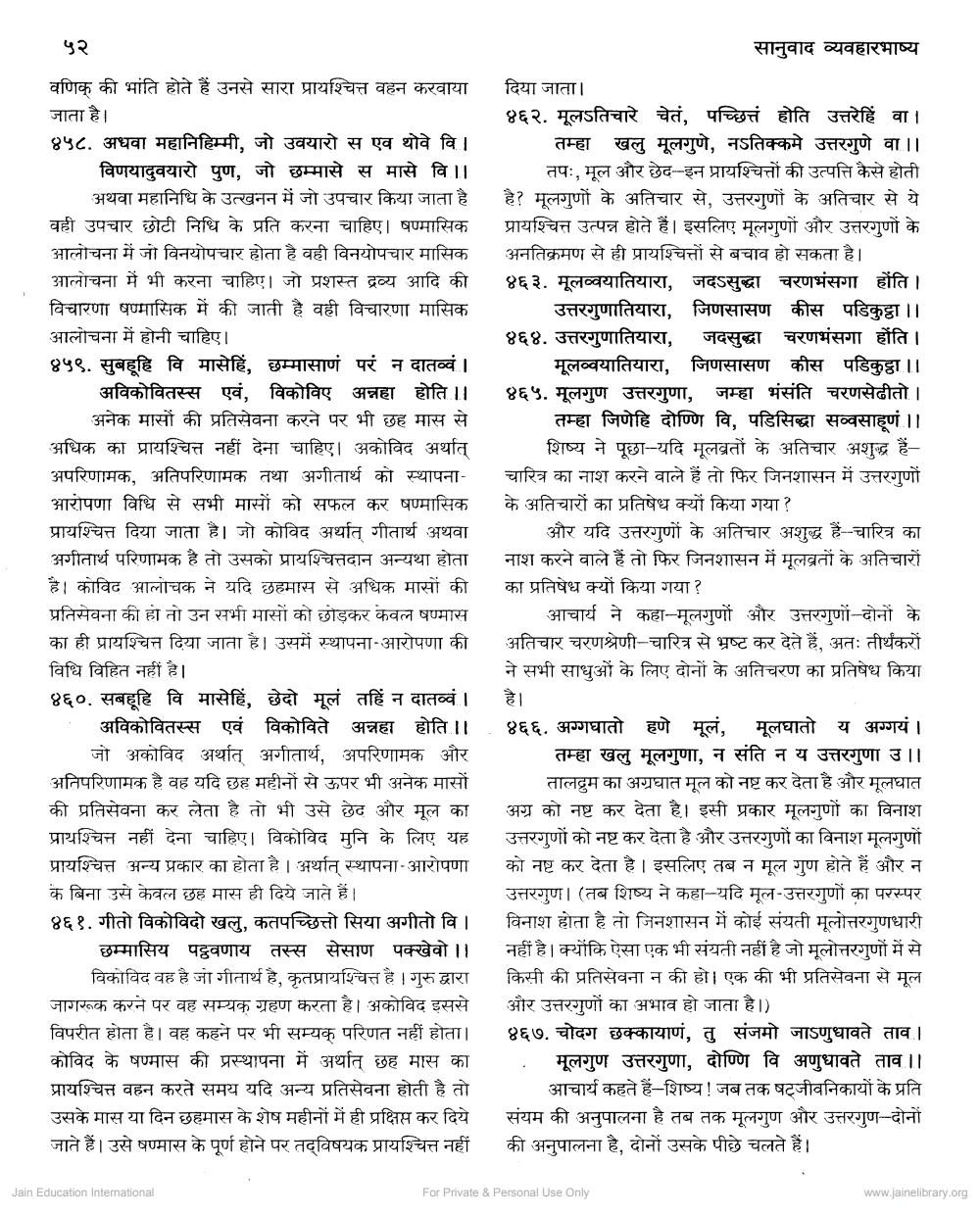________________
५२
सानुवाद व्यवहारभाष्य
वणिक की भांति होते हैं उनसे सारा प्रायश्चित्त वहन करवाया दिया जाता। जाता है।
४६२. मूलऽतिचारे चेतं, पच्छित्तं होति उत्तरेहिं वा। ४५८. अधवा महानिहिम्मी, जो उवयारो स एव थोवे वि। तम्हा खलु मूलगुणे, नऽतिक्कमे उत्तरगुणे वा ।।
विणयादुवयारो पुण, जो छम्मासे स मासे वि ।। तपः, मूल और छेद-इन प्रायश्चित्तों की उत्पत्ति कैसे होती
अथवा महानिधि के उत्खनन में जो उपचार किया जाता है है? मूलगुणों के अतिचार से, उत्तरगुणों के अतिचार से ये वही उपचार छोटी निधि के प्रति करना चाहिए। षण्मासिक प्रायश्चित्त उत्पन्न होते हैं। इसलिए मूलगुणों और उत्तरगुणों के आलोचना में जो विनयोपचार होता है वही विनयोपचार मासिक अनतिक्रमण से ही प्रायश्चित्तों से बचाव हो सकता है। आलोचना में भी करना चाहिए। जो प्रशस्त द्रव्य आदि की ४६३. मूलव्वयातियारा, जदऽसुद्धा चरणभंसगा होति। विचारणा षण्मासिक में की जाती है वही विचारणा मासिक
उत्तरगुणातियारा, जिणसासण कीस पडिकुट्ठा ।। आलोचना में होनी चाहिए।
४६४. उत्तरगुणातियारा, जदसुद्धा चरणभंसगा होति । ४५९. सुबहूहि वि मासेहिं, छम्मासाणं परं न दातव्वं । मूलव्वयातियारा, जिणसासण कीस पडिकुट्ठा ।।
अविकोवितस्स एवं, विकोविए अन्नहा होति ।। ४६५. मूलगुण उत्तरगुणा, जम्हा भंसंति चरणसेढीतो।
अनेक मासों की प्रतिसेवना करने पर भी छह मास से तम्हा जिणेहि दोण्णि वि, पडिसिद्धा सव्वसाहूणं ।। अधिक का प्रायश्चित्त नहीं देना चाहिए। अकोविद अर्थात् शिष्य ने पूछा-यदि मूलव्रतों के अतिचार अशुद्ध हैंअपरिणामक, अतिपरिणामक तथा अगीतार्थ को स्थापना- चारित्र का नाश करने वाले हैं तो फिर जिनशासन में उत्तरगुणों आरोपणा विधि से सभी मासों को सफल कर षण्मासिक के अतिचारों का प्रतिषेध क्यों किया गया? प्रायश्चित्त दिया जाता है। जो कोविद अर्थात् गीतार्थ अथवा
और यदि उत्तरगुणों के अतिचार अशुद्ध हैं-चारित्र का अगीतार्थ परिणामक है तो उसको प्रायश्चित्तदान अन्यथा होता नाश करने वाले हैं तो फिर जिनशासन में मूलव्रतों के अतिचारों है। कोविट आलोचक ने यदि छहमास से अधिक मासों की का प्रतिषेध क्यों किया गया? प्रतिसेवना की हो तो उन सभी मासों को छोड़कर केवल षण्मास आचार्य ने कहा-मूलगुणों और उत्तरगुणों-दोनों के का ही प्रायश्चित्त दिया जाता है। उसमें स्थापना-आरोपणा की अतिचार चरणश्रेणी-चारित्र से भ्रष्ट कर देते हैं, अतः तीर्थंकरों विधि विहित नहीं है।
ने सभी साधुओं के लिए दोनों के अतिचरण का प्रतिषेध किया ४६०. सबहूहि वि मासेहिं, छेदो मूलं तहिं न दातव्वं । है।
अविकोवितस्स एवं विकोविते अन्नहा होति ।। ४६६. अग्गघातो हणे मूलं, मूलघातो य अग्गयं ।
जो अकोविद अर्थात् अगीतार्थ, अपरिणामक और तम्हा खलु मूलगुणा, न संति न य उत्तरगुणा उ ।। अतिपरिणामक है वह यदि छह महीनों से ऊपर भी अनेक मासों तालद्रुम का अग्रघात मूल को नष्ट कर देता है और मूलधात की प्रतिसेवना कर लेता है तो भी उसे छेद और मूल का अग्र को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार मूलगुणों का विनाश प्रायश्चित्त नहीं देना चाहिए। विकोविद मुनि के लिए यह उत्तरगुणों को नष्ट कर देता है और उत्तरगुणों का विनाश मूलगुणों प्रायश्चित्त अन्य प्रकार का होता है । अर्थात् स्थापना-आरोपणा को नष्ट कर देता है। इसलिए तब न मूल गुण होते हैं और न क बिना उसे केवल छह मास ही दिये जाते हैं।
उत्तरगुण। (तब शिष्य ने कहा-यदि मूल-उत्तरगुणों का परस्पर ४६१. गीतो विकोविदो खलु, कतपच्छित्तो सिया अगीतो वि।। विनाश होता है तो जिनशासन में कोई संयती मूलोत्तरगुणधारी
छम्मासिय पट्ठवणाय तस्स सेसाण पक्खेवो।। नहीं है। क्योंकि ऐसा एक भी संयती नहीं है जो मूलोत्तरगणों में से
विकोविद वह है जो गीतार्थ है, कृतप्रायश्चित्त है । गुरु द्वारा किसी की प्रतिसेवना न की हो। एक की भी प्रतिसेवना से मूल जागरूक करने पर वह सम्यक ग्रहण करता है। अकोविद इससे और उत्तरगुणों का अभाव हो जाता है।) विपरीत होता है। वह कहने पर भी सम्यक् परिणत नहीं होता। ४६७. चोदग छक्कायाणं, तु संजमो जाऽणुधावते ताव । कोविद के षण्मास की प्रस्थापना में अर्थात् छह मास का मूलगुण उत्तरगुणा, दोण्णि वि अणुधावते ताव ।। प्रायश्चित्त वहन करते समय यदि अन्य प्रतिसेवना होती है तो आचार्य कहते हैं-शिष्य ! जब तक षट्जीवनिकायों के प्रति उसके मास या दिन छहमास के शेष महीनों में ही प्रक्षिप्त कर दिये संयम की अनुपालना है तब तक मूलगुण और उत्तरगुण-दोनों जाते हैं। उसे षण्मास के पूर्ण होने पर तद्विषयक प्रायश्चित्त नहीं की अनुपालना है, दोनों उसके पीछे चलते हैं।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org