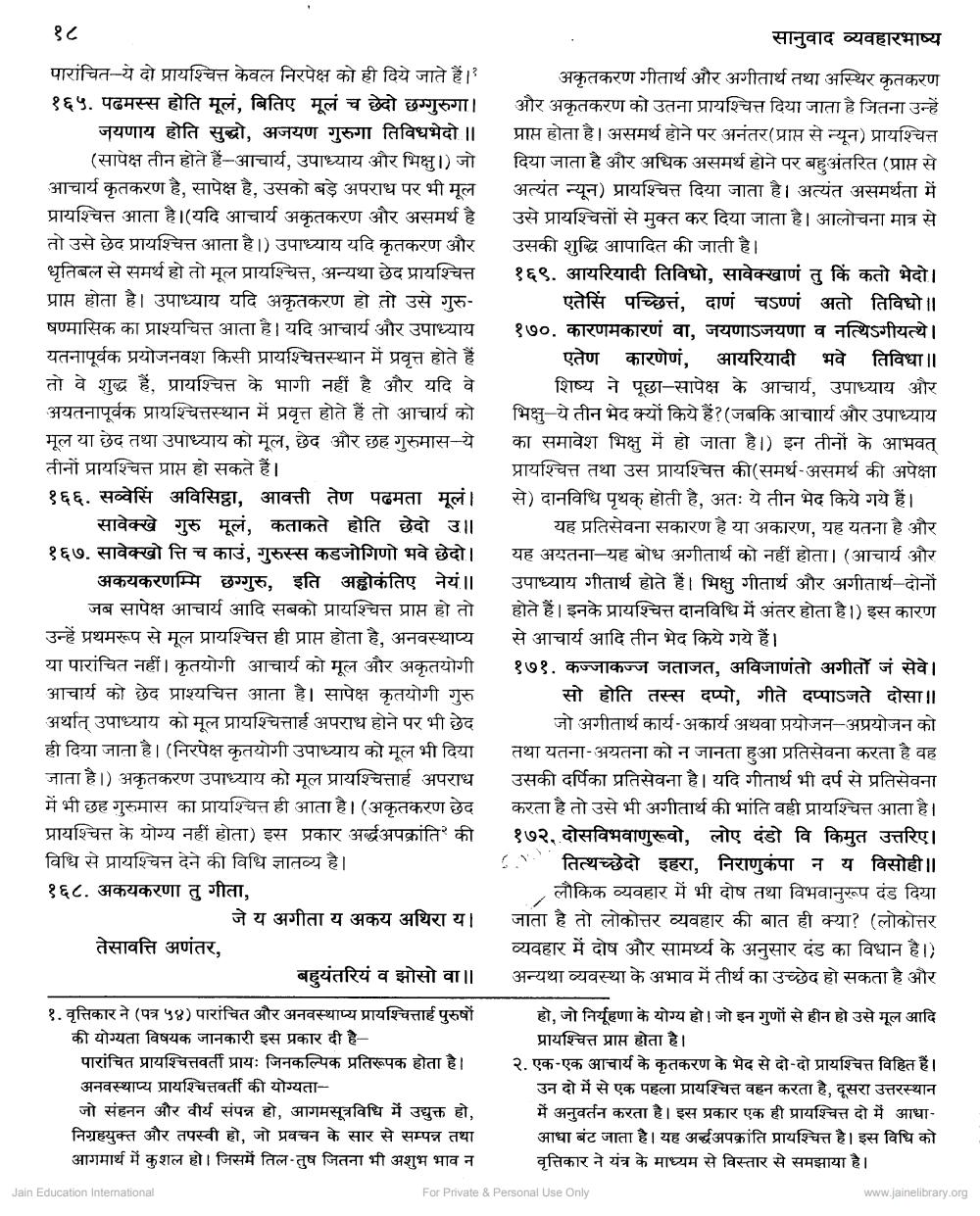________________
सावन
१८
सानुवाद व्यवहारभाष्य पारांचित-ये दो प्रायश्चित्त केवल निरपेक्ष को ही दिये जाते हैं। अकृतकरण गीतार्थ और अगीतार्थ तथा अस्थिर कृतकरण १६५. पढमस्स होति मूलं, बितिए मूलं च छेदो छग्गुरुगा। और अकृतकरण को उतना प्रायश्चित्त दिया जाता है जितना उन्हें
जयणाय होति सुद्धो, अजयण गुरुगा तिविधभेदो ॥ प्राप्त होता है। असमर्थ होने पर अनंतर(प्राप्त से न्यून) प्रायश्चित्त
(सापेक्ष तीन होते हैं-आचार्य, उपाध्याय और भिक्षु।) जो दिया जाता है और अधिक असमर्थ होने पर बहुअंतरित (प्राप्त से आचार्य कृतकरण है, सापेक्ष है, उसको बड़े अपराध पर भी मूल अत्यंत न्यून) प्रायश्चित्त दिया जाता है। अत्यंत असमर्थता में प्रायश्चित्त आता है।(यदि आचार्य अकृतकरण और असमर्थ है उसे प्रायश्चित्तों से मुक्त कर दिया जाता है। आलोचना मात्र से तो उसे छेद प्रायश्चित्त आता है।) उपाध्याय यदि कृतकरण और उसकी शुद्धि आपादित की जाती है। धृतिबल से समर्थ हो तो मूल प्रायश्चित्त, अन्यथा छेद प्रायश्चित्त १६९. आयरियादी तिविधो, सावेक्खाणं तु किं कतो भेदो। प्राप्त होता है। उपाध्याय यदि अकृतकरण हो तो उसे गुरु- एतेसिं पच्छित्तं, दाणं चऽण्णं अतो तिविधो॥ षण्मासिक का प्राश्यचित्त आता है। यदि आचार्य और उपाध्याय १७०. कारणमकारणं वा, जयणाऽजयणा व नत्थिडगीयत्थे। यतनापूर्वक प्रयोजनवश किसी प्रायश्चित्तस्थान में प्रवृत्त होते हैं
एतेण कारणेणं, आयरियादी भवे तिविधा। तो वे शुद्ध हैं, प्रायश्चित्त के भागी नहीं है और यदि वे शिष्य ने पूछा-सापेक्ष के आचार्य, उपाध्याय और अयतनापूर्वक प्रायश्चित्तस्थान में प्रवृत्त होते हैं तो आचार्य को भिक्षु-ये तीन भेद क्यों किये हैं?(जबकि आचार्य और उपाध्याय मूल या छेद तथा उपाध्याय को मूल, छेद और छह गुरुमास-ये। का समावेश भिक्षु में हो जाता है। इन तीनों के आभवत् तीनों प्रायश्चित्त प्रास हो सकते हैं।
प्रायश्चित्त तथा उस प्रायश्चित्त की(समर्थ-असमर्थ की अपेक्षा १६६. सव्वेसिं अविसिट्ठा, आवत्ती तेण पढमता मूलं। से) दानविधि पृथक् होती है, अतः ये तीन भेद किये गये हैं।
सावेक्खे गुरु मूलं, कताकते होति छेदो उ॥ यह प्रतिसेवना सकारण है या अकारण, यह यतना है और १६७. सावेक्खो त्ति च काउं, गुरुस्स कडजोगिणो भवे छेदो। यह अयतना-यह बोध अगीतार्थ को नहीं होता। (आचार्य और
अकयकरणम्मि छग्गुरु, इति अढोकंतिए नेयं ।। उपाध्याय गीतार्थ होते हैं। भिक्षु गीतार्थ और अगीतार्थ-दोनों
जब सापेक्ष आचार्य आदि सबको प्रायश्चित्त प्राप्त हो तो होते हैं। इनके प्रायश्चित्त दानविधि में अंतर होता है।) इस कारण उन्हें प्रथमरूप से मूल प्रायश्चित्त ही प्राप्त होता है, अनवस्थाप्य से आचार्य आदि तीन भेद किये गये हैं। या पारांचित नहीं। कृतयोगी आचार्य को मूल और अकृतयोगी १७१. कज्जाकज्ज जताजत, अविजाणतो अगीतों जं सेवे। आचार्य को छेद प्राश्यचित्त आता है। सापेक्ष कृतयोगी गुरु
सो होति तस्स दप्पो, गीते दप्पाऽजते दोसा।। अर्थात् उपाध्याय को मूल प्रायश्चित्तार्ह अपराध होने पर भी छेद जो अगीतार्थ कार्य-अकार्य अथवा प्रयोजन-अप्रयोजन को ही दिया जाता है। (निरपेक्ष कृतयोगी उपाध्याय को मूल भी दिया तथा यतना-अयतना को न जानता हुआ प्रतिसेवना करता है वह जाता है।) अकृतकरण उपाध्याय को मूल प्रायश्चित्ताह अपराध उसकी दर्पिका प्रतिसेवना है। यदि गीतार्थ भी दर्प से प्रतिसेवना में भी छह गुरुमास का प्रायश्चित्त ही आता है। (अकृतकरण छेद करता है तो उसे भी अगीतार्थ की भांति वही प्रायश्चित्त आता है। प्रायश्चित्त के योग्य नहीं होता) इस प्रकार अर्द्धअपक्रांति की १७२. दोसविभवाणुरूवो, लोए दंडो वि किमुत उत्तरिए। विधि से प्रायश्चित्त देने की विधि ज्ञातव्य है।
..' तित्थच्छेदो इहरा, निराणुकंपा न य विसोही॥ १६८. अकयकरणा तु गीता,
लौकिक व्यवहार में भी दोष तथा विभवानुरूप दंड दिया जे य अगीता य अकय अथिरा य।। जाता है तो लोकोत्तर व्यवहार की बात ही क्या? (लोकोत्तर तेसावत्ति अणंतर,
व्यवहार में दोष और सामर्थ्य के अनुसार दंड का विधान है।
बहुयंतरियं व झोसो वा॥ अन्यथा व्यवस्था के अभाव में तीर्थ का उच्छेद हो सकता है और १. वृत्तिकार ने (पत्र ५४) पारांचित और अनवस्थाप्य प्रायश्चित्ताह पुरुषों हो, जो नि!हणा के योग्य हो। जो इन गुणों से हीन हो उसे मूल आदि की योग्यता विषयक जानकारी इस प्रकार दी है
प्रायश्चित्त प्राप्त होता है। पारांचित प्रायश्चित्तवर्ती प्रायः जिनकल्पिक प्रतिरूपक होता है। २. एक-एक आचार्य के कृतकरण के भेद से दो-दो प्रायश्चित्त विहित हैं। अनवस्थाप्य प्रायश्चित्तवर्ती की योग्यता
उन दो में से एक पहला प्रायश्चित्त वहन करता है, दूसरा उत्तरस्थान जो संहनन और वीर्य संपन्न हो, आगमसूत्रविधि में उद्युक्त हो, में अनुवर्तन करता है। इस प्रकार एक ही प्रायश्चित्त दो में आधानिग्रहयुक्त और तपस्वी हो, जो प्रवचन के सार से सम्पन्न तथा आधा बंट जाता है। यह अर्द्धअपक्रांति प्रायश्चित्त है। इस विधि को आगमार्थ में कुशल हो। जिसमें तिल-तुष जितना भी अशुभ भाव न वृत्तिकार ने यंत्र के माध्यम से विस्तार से समझाया है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org