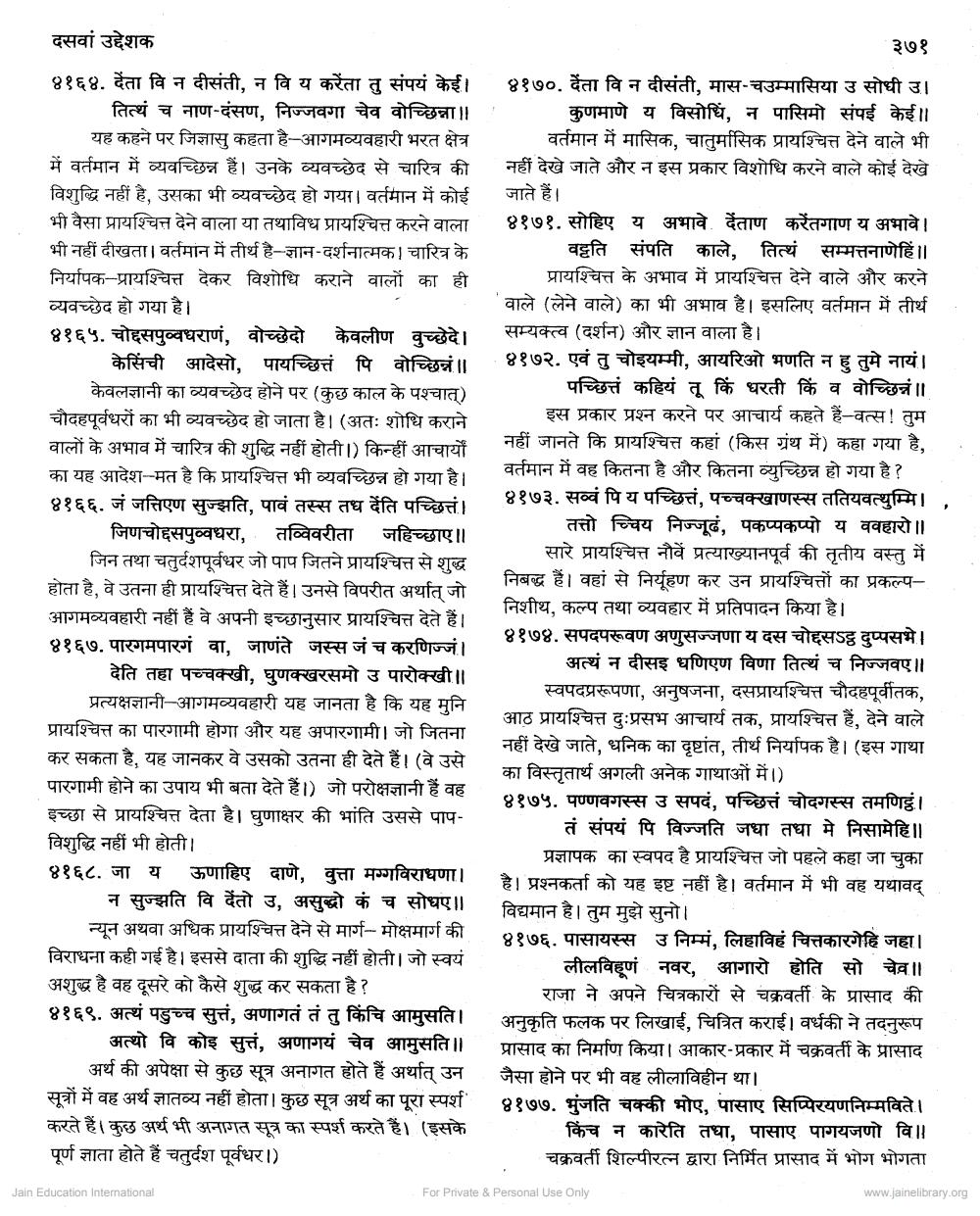________________
दसवां उद्देशक
४१६४. देता वि न दीसंती, न वि य करेंता तु संपयं केई । तित्थं च नाण- दंसण, निज्जवगा चेव वोच्छिन्ना ॥ यह कहने पर जिज्ञासु कहता है-आगमव्यवहारी भरत क्षेत्र में वर्तमान में व्यवच्छिन्न हैं। उनके व्यवच्छेद से चारित्र की विशुद्धि नहीं है, उसका भी व्यवच्छेद हो गया। वर्तमान में कोई भी वैसा प्रायश्चित्त देने वाला या तथाविध प्रायश्चित्त करने वाला भी नहीं दीखता । वर्तमान में तीर्थ है-ज्ञान-दर्शनात्मक । चारित्र के निर्यापक-प्रायश्चित्त देकर विशोधि कराने वालों का ही व्यवच्छेद हो गया है।
४१६५. चोद्दसपुव्वधराणं, वोच्छेदो केवलीण
वुच्छेदे । केसिंची आदेसो, पायच्छित्तं पि वोच्छिन्नं ॥ केवलज्ञानी का व्यवच्छेद होने पर (कुछ काल के पश्चात् ) चौदहपूर्वधरों का भी व्यवच्छेद हो जाता है। (अतः शोधि कराने वालों के अभाव में चारित्र की शुद्धि नहीं होती ।) किन्हीं आचार्यों का यह आदेश - मत है कि प्रायश्चित्त भी व्यवच्छिन्न हो गया है। ४१६६. जं जत्तिएण सुज्झति, पावं तस्स तध देंति पच्छित्तं । जिणचोद्दसपुव्वधरा, तव्विवरीता जहिच्छाए ॥ जिन तथा चतुर्दशपूर्वधर जो पाप जितने प्रायश्चित्त से शुद्ध होता है, वे उतना ही प्रायश्चित्त देते हैं। उनसे विपरीत अर्थात् जो आगमव्यवहारी नहीं हैं वे अपनी इच्छानुसार प्रायश्चित्त देते हैं। ४१६७. पारगमपारगं वा, जाणंते जस्स जं च करणिज्जं ।
देति तहा पच्चक्खी, घुणक्खरसमो उ पारोक्खी ॥ प्रत्यक्षज्ञानी- आगमव्यवहारी यह जानता है कि यह मुनि प्रायश्चित्त का पारगामी होगा और यह अपारगामी । जो जितना कर सकता है, यह जानकर वे उसको उतना ही देते हैं। (वे उसे पारगामी होने का उपाय भी बता देते हैं।) जो परोक्षज्ञानी हैं वह इच्छा से प्रायश्चित्त देता है। घुणाक्षर की भांति उससे पापविशुद्धि नहीं भी होती ।
४१६८. जा य ऊणाहिए दाणे, वुत्ता मग्गविराधणा | न सुज्झति वि देंतो उ, असुद्धो कं च सोधए ।। न्यून अथवा अधिक प्रायश्चित्त देने से मार्ग- मोक्षमार्ग की विराधना कही गई है। इससे दाता की शुद्धि नहीं होती। जो स्वयं अशुद्ध है वह दूसरे को कैसे शुद्ध कर सकता है ? ४१६९. अत्थं पडुच्च सुत्तं, अणागतं तं तु किंचि आमुसति ।
अत्यो वि कोइ सुत्तं, अणागयं चेव आमुसति ॥ अर्थ की अपेक्षा से कुछ सूत्र अनागत होते हैं अर्थात् उन सूत्रों में वह अर्थ ज्ञातव्य नहीं होता। कुछ सूत्र अर्थ का पूरा स्पर्श करते हैं। कुछ अर्थ भी अनागत सूत्र का स्पर्श करते हैं। (इसके पूर्ण ज्ञाता होते हैं चतुर्दश पूर्वधर 1)
Jain Education International
३७१ ४१७०. देता विन दीसंती, मास- चउम्मासिया उ सोधी उ । कुणमाणे य विसोधिं, न पासिमो संपई केई ॥ वर्तमान में मासिक, चातुर्मासिक प्रायश्चित्त देने वाले भी नहीं देखे जाते और न इस प्रकार विशोधि करने वाले कोई देखे जाते हैं।
४१७१. सोहिए य अभावे देताण करेंतगाण य अभावे । वट्टति संपति काले, तित्थं सम्मत्तनाणेहिं ॥ प्रायश्चित्त के अभाव में प्रायश्चित्त देने वाले और करने वाले (लेने वाले) का भी अभाव है। इसलिए वर्तमान में तीर्थ सम्यक्त्व (दर्शन) और ज्ञान वाला है।
४१७२. एवं तु चोइयम्मी, आयरिओ भणति न हु तुमे नायं । पच्छित्तं कहियं तू किं धरती किं व वोच्छिन्नं ॥
इस प्रकार प्रश्न करने पर आचार्य कहते हैं-वत्स ! तुम नहीं जानते कि प्रायश्चित्त कहां (किस ग्रंथ में) कहा गया है, वर्तमान में वह कितना है और कितना व्युच्छिन्न हो गया है ? ४१७३. सव्वं पि य पच्छित्तं, पच्चक्खाणस्स ततियवत्थुम्मि ।
तत्तो च्चिय निज्जूढं, पकप्पकप्पो य ववहारो ॥ सारे प्रायश्चित्त नौवें प्रत्याख्यानपूर्व की तृतीय वस्तु में निबद्ध हैं। वहां से निर्यूहण कर उन प्रायश्चित्तों का प्रकल्प - निशीथ, कल्प तथा व्यवहार में प्रतिपादन किया है। ४१७४. सपदपरूवण अणुसज्जणा य दस चोद्दसऽट्ठ दुप्पसभे ।
अत्थं न दीसइ धणिएण विणा तित्थं च निज्जवए ॥ स्वपदप्ररूपणा, अनुषजना, दसप्रायश्चित्त चौदहपूर्वीतक, आठ प्रायश्चित्त दुःप्रसभ आचार्य तक, प्रायश्चित्त हैं, देने वाले नहीं देखे जाते, धनिक का दृष्टांत, तीर्थ निर्यापक है। (इस गाथा
विस्तृतार्थ अगली अनेक गाथाओं में ।)
४१७५. पण्णवगस्स उ सपदं, पच्छित्तं चोदगस्स तमणिद्वं ।
तं संपयं पि विज्जति जधा तथा मे निसामेहि ॥ प्रज्ञापक का स्वपद है प्रायश्चित्त जो पहले कहा जा चुका है। प्रश्नकर्ता को यह इष्ट नहीं है। वर्तमान में भी वह यथावद् विद्यमान है। तुम मुझे सुनो।
४१७६. पासायस्स उ निम्मं, लिहाविहं चित्तकारगेहि जहा ।
लीलविहूणं नवर, आगारो होति सो चेव ॥ राजा ने अपने चित्रकारों से चक्रवर्ती के प्रासाद की अनुकृति फलक पर लिखाई, चित्रित कराई। वर्धकी ने तदनुरूप प्रासाद का निर्माण किया। आकार-प्रकार में चक्रवर्ती के प्रासाद जैसा होने पर भी वह लीलाविहीन था ।
४१७७. भुंजति चक्की भोए, पासाए सिप्पिरयणनिम्मविते । किंच न कारेति तधा, पासाए पागयजणो वि ॥ चक्रवर्ती शिल्पीरत्न द्वारा निर्मित प्रासाद में भोग भोगता
www.jainelibrary.org
For Private & Personal Use Only