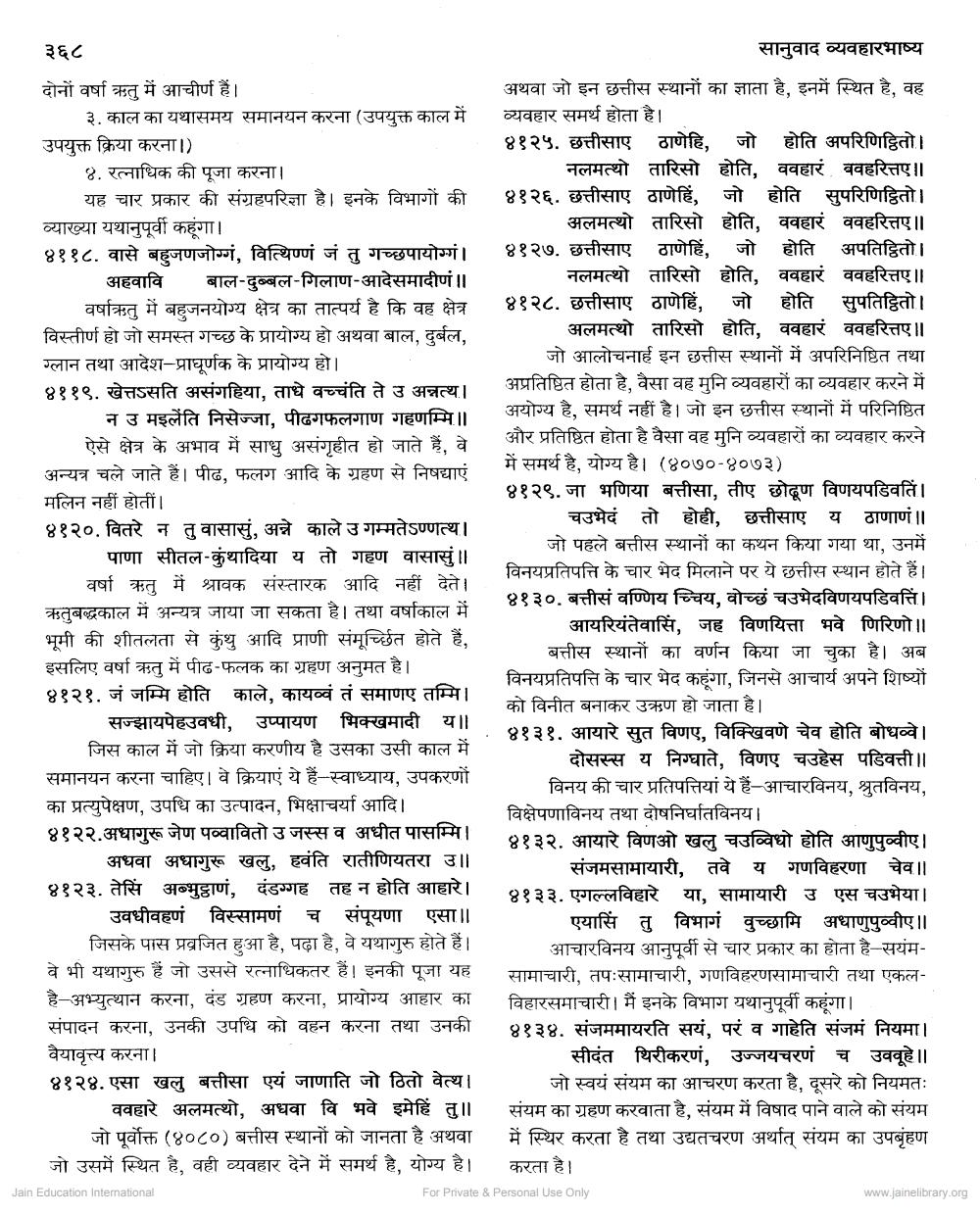________________
३६८
दोनों वर्षा ऋतु में आचीर्ण हैं।
३. काल का यथासमय समानयन करना ( उपयुक्त काल में उपयुक्त क्रिया करना । )
४. रत्नाधिक की पूजा करना ।
यह चार प्रकार की संग्रहपरिज्ञा है। इनके विभागों की व्याख्या यथानुपूर्वी कहूंगा।
४११८. वासे बहुजणजोग्गं, वित्थिण्णं जं तु गच्छपायोग्गं । अहवावि बाल-दुब्बल - गिलाण - आदेसमादीणं ॥ वर्षाऋतु में बहुजनयोग्य क्षेत्र का तात्पर्य है कि वह क्षेत्र विस्तीर्ण हो जो समस्त गच्छ के प्रायोग्य हो अथवा बाल, दुर्बल, ग्लान तथा आदेश - प्राघूर्णक के प्रायोग्य हो । ४११९. खेत्तऽसति असंगहिया, ताधे वच्चंति ते उ अन्नत्थ । न उ मइलेंति निसेज्जा, पीढगफलगाण गहणम्मि | ऐसे क्षेत्र के अभाव में साधु असंगृहीत हो जाते हैं, वे अन्यत्र चले जाते हैं। पीढ़, फलग आदि के ग्रहण से निषद्याएं मलिन नहीं होतीं ।
४१२०. वितरे न तु वासासुं, अन्ने काले उ गम्मतेऽण्णत्थ ।
पाणा सीतल- कुंथादिया य तो गहण वासासुं ॥ वर्षा ऋतु में श्रावक संस्तारक आदि नहीं देते। ऋतुबद्धकाल में अन्यत्र जाया जा सकता है। तथा वर्षाकाल में भूमी की शीतलता से कुंथु आदि प्राणी संमूर्च्छित होते हैं, इसलिए वर्षा ऋतु में पीढ - फलक का ग्रहण अनुमत है। ४१२१. जं जम्मि होति काले, कायव्वं तं समाणए तम्मि । सज्झायपेहउवधी, उप्पायण भिक्खमादी य॥
जिस काल में जो क्रिया करणीय है उसका उसी काल में समानयन करना चाहिए। वे क्रियाएं ये हैं- स्वाध्याय, उपकरणों का प्रत्युपेक्षण, उपधि का उत्पादन, भिक्षाचर्या आदि । ४१२२. अधागुरू जेण पव्वावितो उ जस्स व अधीत पासम्मि ।
अधवा अधागुरू खलु हवंति रातीणियतरा उ ॥ ४१२३. तेसिं अब्भुट्ठाणं, दंडग्गह तह न होति आहारे ।
उवधीवहणं विस्सामणं च संपूयणा एसा || जिसके पास प्रव्रजित हुआ है, पढ़ा है, वे यथागुरु होते हैं। वे भी यथागुरु हैं जो उससे रत्नाधिकतर हैं। इनकी पूजा यह है - अभ्युत्थान करना, दंड ग्रहण करना, प्रायोग्य आहार का संपादन करना, उनकी उपधि को वहन करना तथा उनकी वैयावृत्त्य करना ।
४१२४. एसा खलु बत्तीसा एयं जाणाति जो ठितो वेत्थ ।
ववहारे अलमत्थो, अधवा वि भवे इमेहिं तु ॥ जो पूर्वोक्त (४०८०) बत्तीस स्थानों को जानता है अथवा जो उसमें स्थित है, वही व्यवहार देने में समर्थ है, योग्य है ।
Jain Education International
सानुवाद व्यवहारभाष्य
अथवा जो इन छत्तीस स्थानों का ज्ञाता है, इनमें स्थित है, वह व्यवहार समर्थ होता है।
ववहरित्तए ।
अपतिट्ठितो ।
ववहरित्तए ।
होति
सुपतिट्ठितो ।
४१२५. छत्तीसाए ठाणेहि, जो होति अपरिणिद्वितो । लमत्थो तारिसो होति, ववहारं बवहरित्तए । ४१२६. छत्तीसाए ठाणेहिं, जो होति सुपरिणिद्वितो । अलमत्थो तारिसो होति, ववहारं ४१२७. छत्तीसाए ठाणेहिं, जो होति नलमत्थो तारिसो होति, ववहारं ४१२८. छत्तीसाए ठाणेहिं, जो अलमत्यो तारसो होति, ववहारं ववहरित्तए । जो आलोचनार्ह इन छत्तीस स्थानों में अपरिनिष्ठित तथा अप्रतिष्ठित होता है, वैसा वह मुनि व्यवहारों का व्यवहार करने में अयोग्य है, समर्थ नहीं है। जो इन छत्तीस स्थानों में परिनिष्ठित और प्रतिष्ठित होता है वैसा वह मुनि व्यवहारों का व्यवहार करने में समर्थ है, योग्य है। (४०७०-४०७३) ४१२९. जा भणिया बत्तीसा, तीए छोढूण विणयपडिवतिं ।
चउभेदं तो होही, छत्तीसाए य ठाणाणं ।। जो पहले बत्तीस स्थानों का कथन किया गया था, उनमें विनयप्रतिपत्ति के चार भेद मिलाने पर ये छत्तीस स्थान होते हैं। ४१३०. बत्तीसं वण्णिय च्चिय, वोच्छं चउभेदविणयपडिवत्तिं ।
आयरियंतेवासिं, जह विणयित्ता भवे णिरिणो ॥ बत्तीस स्थानों का वर्णन किया जा चुका है। अब विनयप्रतिपत्ति के चार भेद कहूंगा, जिनसे आचार्य अपने शिष्यों को विनीत बनाकर उऋण हो जाता है।
४१३१. आयारे सुत विणए, विक्खिवणे चेव होति बोधव्वे |
दोसस्स य निग्घाते, विणए चउहेस पडिवत्ती ॥ विनय की चार प्रतिपत्तियां ये हैं- आचारविनय, श्रुतविनय, विक्षेपणाविनय तथा दोषनिर्घातविनय ।
४१३२. आयारे विणओ खलु चउव्विधो होति आणुपुव्वीए । संजमसामायारी, तवे य गणविहरणा चेव ॥ ४१३३. एगल्लविहारे या, सामायारी उ एस चउभेया ।
एयासिं तु विभागं वुच्छामि अधाणुपुव्वीए । आचारविनय आनुपूर्वी से चार प्रकार का होता है-सयमसामाचारी, तपः सामाचारी, गणविहरणसामाचारी तथा एकलविहारसमाचारी | मैं इनके विभाग यथानुपूर्वी कहूंगा। ४१३४. संजममायरति सयं, परं व गाहेति संजमं नियमा ।
सीदंत थिरीकरणं, उज्जयचरणं च उववूहे ॥ जो स्वयं संयम का आचरण करता है, दूसरे को नियमतः संयम का ग्रहण करवाता है, संयम में विषाद पाने वाले को संयम में स्थिर करता है तथा उद्यतचरण अर्थात् संयम का उपबृंहण
करता है। For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org