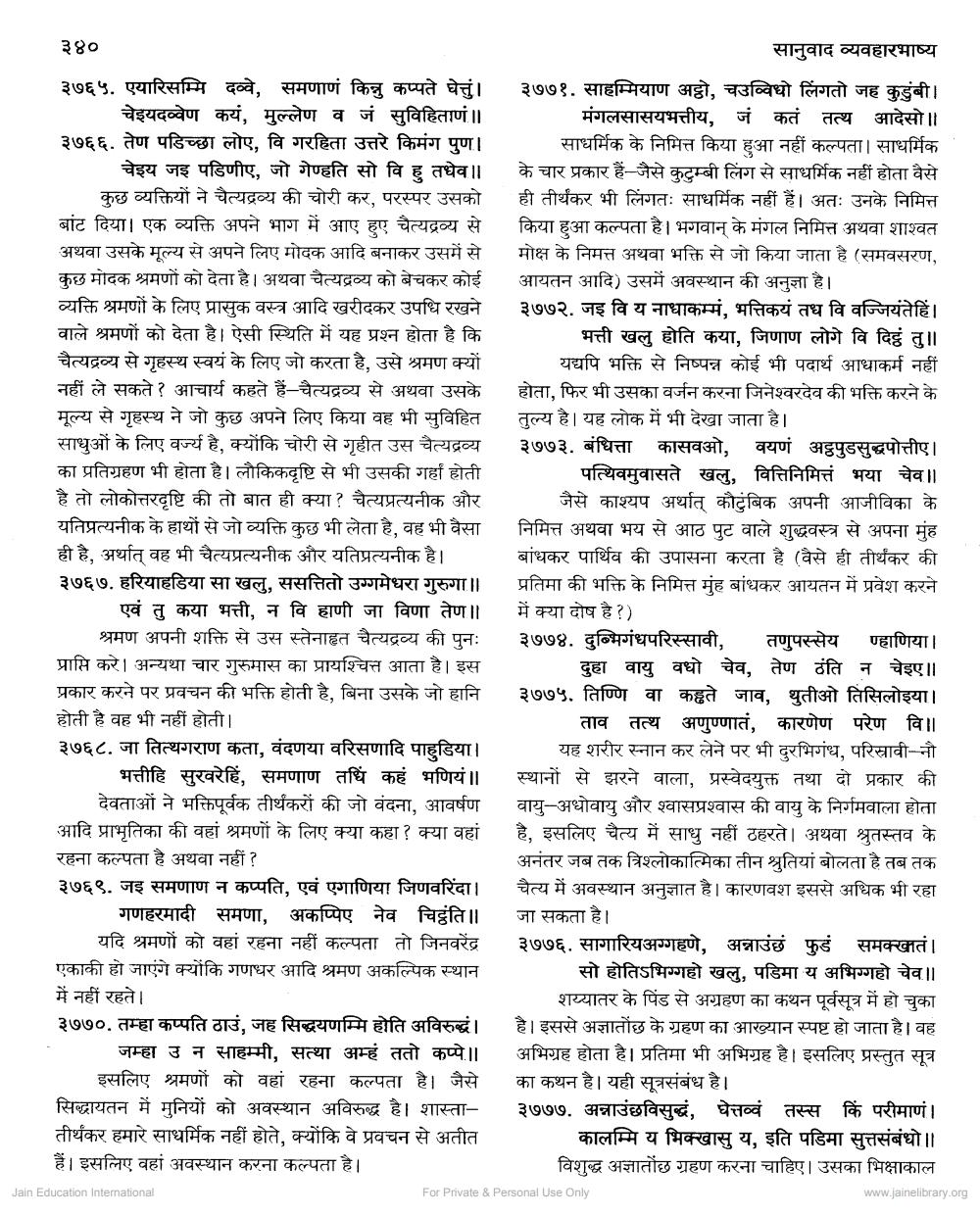________________
३४०
सानुवाद व्यवहारभाष्य
३७६५. एयारिसम्मि दव्वे, समणाणं किन्नु कप्पते घेत्तुं। ३७७१. साहम्मियाण अट्ठो, चउव्विधो लिंगतो जह कुटुंबी। चेइयदव्वेण कयं, मुल्लेण व जं सुविहिताणं ।।
मंगलसासयभत्तीय, जं कतं तत्थ आदेसो॥ ३७६६. तेण पडिच्छा लोए, वि गरहिता उत्तरे किमंग पुण। साधर्मिक के निमित्त किया हुआ नहीं कल्पता। साधर्मिक
चेइय जइ पडिणीए, जो गेण्हति सो वि हु तधेव॥ के चार प्रकार हैं-जैसे कुटुम्बी लिंग से साधर्मिक नहीं होता वैसे कुछ व्यक्तियों ने चैत्यद्रव्य की चोरी कर, परस्पर उसको ही तीर्थंकर भी लिंगतः साधर्मिक नहीं हैं। अतः उनके निमित्त बांट दिया। एक व्यक्ति अपने भाग में आए हुए चैत्यद्रव्य से किया हुआ कल्पता है। भगवान् के मंगल निमित्त अथवा शाश्वत अथवा उसके मूल्य से अपने लिए मोदक आदि बनाकर उसमें से मोक्ष के निमत्त अथवा भक्ति से जो किया जाता है (समवसरण, कुछ मोदक श्रमणों को देता है। अथवा चैत्यद्रव्य को बेचकर कोई आयतन आदि) उसमें अवस्थान की अनुज्ञा है। व्यक्ति श्रमणों के लिए प्रासुक वस्त्र आदि खरीदकर उपधि रखने ३७७२. जइ वि य नाधाकम्म, भत्तिकयं तध वि वज्जियंतेहिं। वाले श्रमणों को देता है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न होता है कि
भत्ती खलु होति कया, जिणाण लोगे वि दिटुं तु॥ चैत्यद्रव्य से गृहस्थ स्वयं के लिए जो करता है, उसे श्रमण क्यों यद्यपि भक्ति से निष्पन्न कोई भी पदार्थ आधाकर्म नहीं नहीं ले सकते? आचार्य कहते हैं-चैत्यद्रव्य से अथवा उसके होता, फिर भी उसका वर्जन करना जिनेश्वरदेव की भक्ति करने के मूल्य से गृहस्थ ने जो कुछ अपने लिए किया वह भी सुविहित तुल्य है। यह लोक में भी देखा जाता है। साधुओं के लिए वर्त्य है, क्योंकि चोरी से गृहीत उस चैत्यद्रव्य ३७७३. बंधित्ता कासवओ, वयणं अट्ठपुडसुद्धपोत्तीए। का प्रतिग्रहण भी होता है। लौकिकदृष्टि से भी उसकी गहाँ होती __ पत्थिवमुवासते खलु, वित्तिनिमित्तं भया चेव॥ है तो लोकोत्तरदृष्टि की तो बात ही क्या? चैत्यप्रत्यनीक और जैसे काश्यप अर्थात् कौटुंबिक अपनी आजीविका के यतिप्रत्यनीक के हाथों से जो व्यक्ति कुछ भी लेता है, वह भी वैसा निमित्त अथवा भय से आठ पुट वाले शुद्धवस्त्र से अपना मुंह ही है, अर्थात् वह भी चैत्यप्रत्यनीक और यतिप्रत्यनीक है। बांधकर पार्थिव की उपासना करता है (वैसे ही तीर्थंकर की ३७६७. हरियाहडिया सा खलु, ससत्तितो उग्गमेधरा गुरुगा॥ प्रतिमा की भक्ति के निमित्त मुंह बांधकर आयतन में प्रवेश करने ____एवं तु कया भत्ती, न वि हाणी जा विणा तेण॥ में क्या दोष है ?)
श्रमण अपनी शक्ति से उस स्तेनाहृत चैत्यद्रव्य की पुनः ३७७४. दुन्भिगंधपरिस्सावी, तणुपस्सेय हाणिया। प्राप्ति करे। अन्यथा चार गुरुमास का प्रायश्चित्त आता है। इस
दुहा वायु वधो चेव, तेण ठंति न चेइए। प्रकार करने पर प्रवचन की भक्ति होती है, बिना उसके जो हानि ३७७५. तिण्णि वा कहते जाव, थुतीओ तिसिलोइया। होती है वह भी नहीं होती।
ताव तत्थ अणुण्णातं, कारणेण परेण वि॥ ३७६८. जा तित्थगराण कता, वंदणया वरिसणादि पाहुडिया। यह शरीर स्नान कर लेने पर भी दुरभिगंध, परिस्रावी-नौ
भत्तीहि सुरवरेहिं, समणाण तधिं कहं भणियं॥ स्थानों से झरने वाला, प्रस्वेदयुक्त तथा दो प्रकार की देवताओं ने भक्तिपूर्वक तीर्थंकरों की जो वंदना, आवर्षण वायु-अधोवायु और श्वासप्रश्वास की वायु के निर्गमवाला होता आदि प्राभृतिका की वहां श्रमणों के लिए क्या कहा? क्या वहां है, इसलिए चैत्य में साधु नहीं ठहरते। अथवा श्रुतस्तव के रहना कल्पता है अथवा नहीं?
अनंतर जब तक त्रिश्लोकात्मिका तीन श्रुतियां बोलता है तब तक ३७६९. जइ समणाण न कप्पति, एवं एगाणिया जिणवरिंदा। चैत्य में अवस्थान अनुज्ञात है। कारणवश इससे अधिक भी रहा
गणहरमादी समणा, अकप्पिए नेव चिट्ठति॥ जा सकता है।
यदि श्रमणों को वहां रहना नहीं कल्पता तो जिनवरेंद्र ३७७६. सागारियअग्गहणे, अन्नाउंछं फुडं समक्खातं। एकाकी हो जाएंगे क्योंकि गणधर आदि श्रमण अकल्पिक स्थान
सो होतिऽभिग्गहो खलु, पडिमा य अभिग्गहो चेव।। में नहीं रहते।
शय्यातर के पिंड से अग्रहण का कथन पूर्वसूत्र में हो चुका ३७७०. तम्हा कप्पति ठाउं, जह सिद्धयणम्मि होति अविरुद्धं। है। इससे अज्ञातोंछ के ग्रहण का आख्यान स्पष्ट हो जाता है। वह
जम्हा उ न साहम्मी, सत्था अम्हं ततो कप्पे॥ अभिग्रह होता है। प्रतिमा भी अभिग्रह है। इसलिए प्रस्तुत सूत्र
इसलिए श्रमणों को वहां रहना कल्पता है। जैसे का कथन है। यही सूत्रसंबंध है। सिद्धायतन में मुनियों को अवस्थान अविरुद्ध है। शास्ता- ३७७७. अन्नाउंछविसुद्धं, घेत्तव्वं तस्स किं परीमाणं। तीर्थंकर हमारे साधर्मिक नहीं होते, क्योंकि वे प्रवचन से अतीत
कालम्मि य भिक्खासु य, इति पडिमा सुत्तसंबंधो।। हैं। इसलिए वहां अवस्थान करना कल्पता है।
विशुद्ध अज्ञातोंछ ग्रहण करना चाहिए। उसका भिक्षाकाल Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org