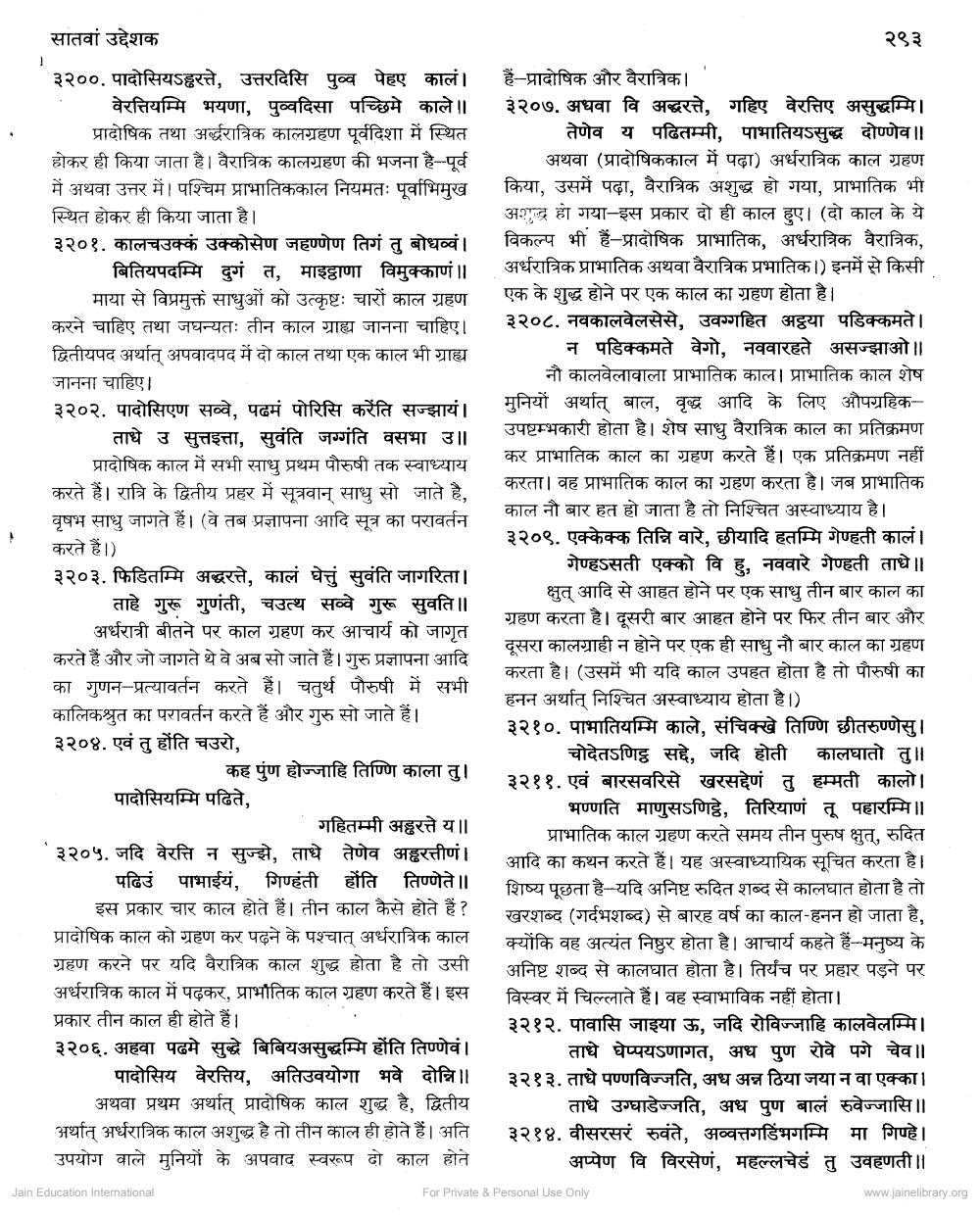________________
२९३
सातवां उद्देशक ३२००. पादोसियऽडरते, उत्तरदिसि पुव्व पेहए कालं।
वेरत्तियम्मि भयणा, पुव्वदिसा पच्छिमे काले॥ प्रादोषिक तथा अर्द्धरात्रिक कालग्रहण पूर्वदिशा में स्थित होकर ही किया जाता है। वैरात्रिक कालग्रहण की भजना है-पूर्व में अथवा उत्तर में। पश्चिम प्राभातिककाल नियमतः पूर्वाभिमख स्थित होकर ही किया जाता है। ३२०१. कालचउक्कं उक्कोसेण जहण्णेण तिगं तु बोधव्वं ।
बितियपदम्मि दुगं त, माइट्ठाणा विमुक्काणं॥ माया से विप्रमुक्तं साधुओं को उत्कृष्टः चारों काल ग्रहण करने चाहिए तथा जघन्यतः तीन काल ग्राह्य जानना चाहिए। द्वितीयपद अर्थात् अपवादपद में दो काल तथा एक काल भी ग्राह्य जानना चाहिए। ३२०२. पादोसिएण सव्वे, पढमं पोरिसि करेंति सज्झायं।
ताधे उ सुत्तइत्ता, सुवंति जग्गंति वसभा उ॥ प्रादोषिक काल में सभी साधु प्रथम पौरुषी तक स्वाध्याय करते हैं। रात्रि के द्वितीय प्रहर में सूत्रवान् साधु सो जाते है, वृषभ साधु जागते हैं। (वे तब प्रज्ञापना आदि सूत्र का परावर्तन करते हैं।) ३२०३. फिडितम्मि अद्धरत्ते, कालं घेत्तुं सुवंति जागरिता।
ताहे गुरू गुणंती, चउत्थ सव्वे गुरू सुवति।।
अर्धरात्री बीतने पर काल ग्रहण कर आचार्य को जागृत करते हैं और जो जागते थे वे अब सो जाते हैं। गुरु प्रज्ञापना आदि का गुणन-प्रत्यावर्तन करते हैं। चतुर्थ पौरुषी में सभी कालिकश्रुत का परावर्तन करते हैं और गुरु सो जाते हैं। ३२०४. एवं तु होति चउरो,
कह पुंण होज्जाहि तिण्णि काला तु। पादोसियम्मि पढिते,
गहितम्मी अडरत्ते य॥ '३२०५. जदि वेरत्ति न सुज्झे, ताधे तेणेव अडरत्तीणं।
पढिउं पाभाईयं, गिण्हती होति तिण्णेते॥ इस प्रकार चार काल होते हैं। तीन काल कैसे होते हैं ? प्रादोषिक काल को ग्रहण कर पढ़ने के पश्चात् अर्धरात्रिक काल ग्रहण करने पर यदि वैरात्रिक काल शुद्ध होता है तो उसी अर्धरात्रिक काल में पढ़कर, प्रार्भातिक काल ग्रहण करते है। इस प्रकार तीन काल ही होते हैं। ३२०६. अहवा पढमे सुद्धे बिबियअसुद्धम्मि होति तिण्णेवं।
पादोसिय वेरत्तिय, अतिउवयोगा भवे दोन्नि॥
अथवा प्रथम अर्थात् प्रादोषिक काल शुद्ध है, द्वितीय अर्थात् अर्धरात्रिक काल अशुद्ध है तो तीन काल ही होते हैं। अति उपयोग वाले मुनियों के अपवाद स्वरूप दो काल होते
हैं-प्रादोषिक और वैरात्रिक। ' ३२०७. अधवा वि अद्धरत्ते, गहिए वेरत्तिए असुद्धम्मि।
तेणेव य पढितम्मी, पाभातियऽसुद्ध दोण्णेव॥
अथवा (प्रादोषिककाल में पढ़ा) अर्धरात्रिक काल ग्रहण किया, उसमें पढ़ा, वैरात्रिक अशुद्ध हो गया, प्राभातिक भी अशुद्ध हो गया-इस प्रकार दो ही काल हुए। (दो काल के ये विकल्प भी हैं-प्रादोषिक प्राभातिक, अर्धरात्रिक वैरात्रिक, अर्धरात्रिक प्राभातिक अथवा वैरात्रिक प्रभातिक।) इनमें से किसी एक के शुद्ध होने पर एक काल का ग्रहण होता है। ३२०८. नवकालवलसस, उवग्गाहत अट्ठया पाडक्कमत।
न पडिक्कमते वेगो, नववारहते असज्झाओ॥
नौ कालवेलावाला प्राभातिक काल। प्राभातिक काल शेष मुनियों अर्थात् बाल, वृद्ध आदि के लिए औपग्रहिकउपष्टम्भकारी होता है। शेष साधु वैरात्रिक काल का प्रतिक्रमण कर प्राभातिक काल का ग्रहण करते हैं। एक प्रतिक्रमण नहीं करता। वह प्राभातिक काल का ग्रहण करता है। जब प्राभातिक काल नौ बार हत हो जाता है तो निश्चित अस्वाध्याय है। ३२०९. एक्केक्क तिन्नि वारे, छीयादि हतम्मि गेण्हती कालं।
गेण्हऽसती एक्को वि हु, नववारे गेण्हती ताधे॥
क्षुत् आदि से आहत होने पर एक साधु तीन बार काल का ग्रहण करता है। दूसरी बार आहत होने पर फिर तीन बार और दूसरा कालग्राही न होने पर एक ही साधु नौ बार काल का ग्रहण करता है। (उसमें भी यदि काल उपहत होता है तो पौरुषी का हनन अर्थात् निश्चित अस्वाध्याय होता है।) ३२१०. पाभातियम्मि काले, संचिक्खे तिण्णि छीतरुण्णेसु।
चोदेतऽणिट्ठ सद्दे, जदि होती कालघातो तु॥ ३२११. एवं बारसवरिसे खरसद्देणं तु हम्मती कालो।
___ भण्णति माणुसऽणिढे, तिरियाणं तू पहारम्मि॥
प्राभातिक काल ग्रहण करते समय तीन पुरुष क्षुत्, रुदित आदि का कथन करते हैं। यह अस्वाध्यायिक सूचित करता है। शिष्य पूछता है-यदि अनिष्ट रुदित शब्द से कालघात होता है तो खरशब्द (गर्दभशब्द) से बारह वर्ष का काल-हनन हो जाता है, क्योंकि वह अत्यंत निष्ठुर होता है। आचार्य कहते हैं-मनुष्य के अनिष्ट शब्द से कालघात होता है। तिर्यंच पर प्रहार पड़ने पर विस्वर में चिल्लाते हैं। वह स्वाभाविक नहीं होता। ३२१२. पावासि जाइया ऊ, जदि रोविज्जाहि कालवेलम्मि।
ताधे घेप्पयऽणागत, अध पुण रोवे पगे चेव॥ ३२१३. ताधे पण्णविज्जति, अध अन्न ठिया जया न वा एक्का।
ताधे उग्घाडेज्जति, अध पुण बालं रुवेज्जासि॥ ३२१४. वीसरसरं रुवंते, अव्वत्तगडिंभगम्मि मा गिण्हे।
अप्पेण वि विरसेणं, महल्लचेडं तु उवहणती।।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org