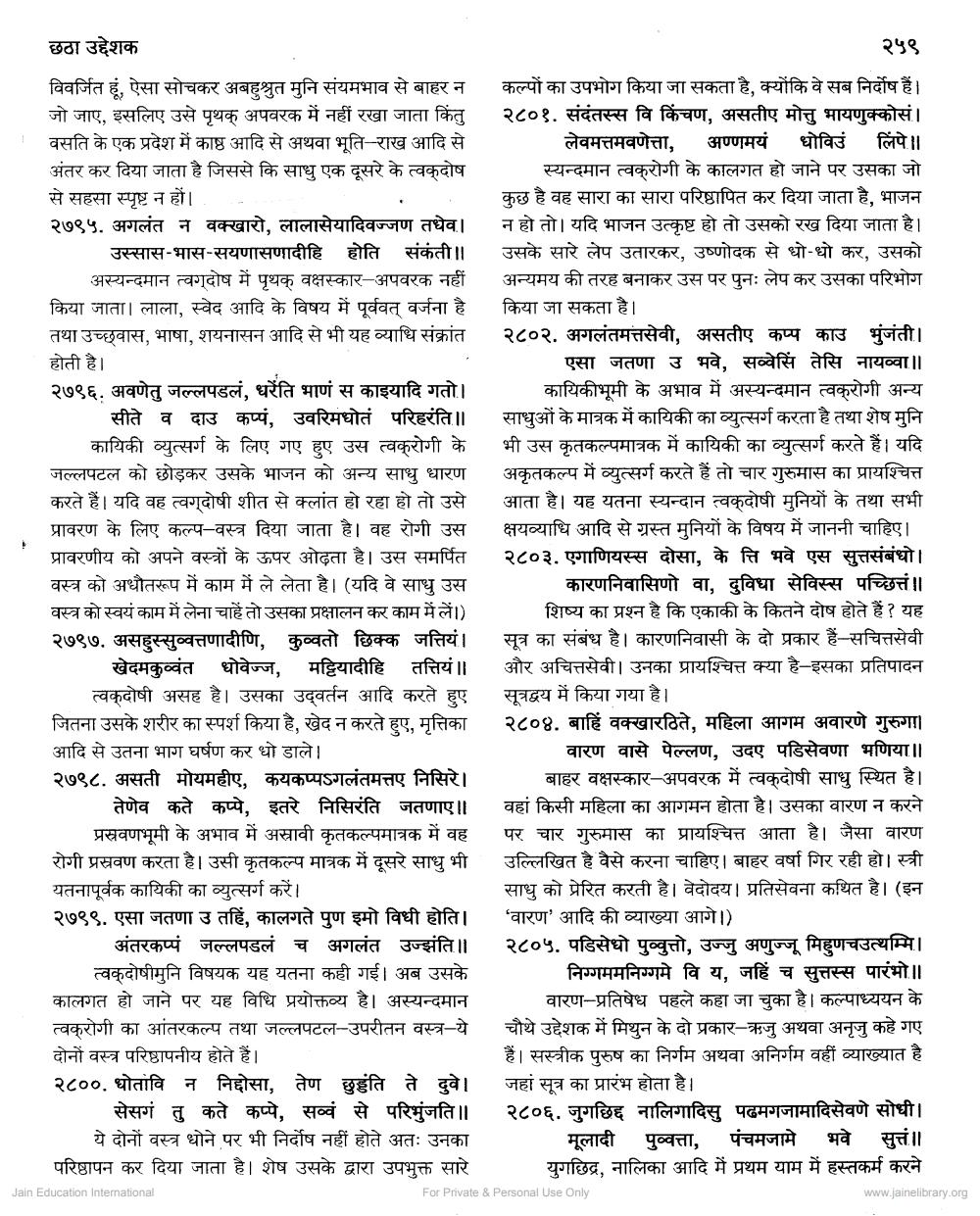________________
छठा उद्देशक
विवर्जित हूं, ऐसा सोचकर अबहुश्रुत मुनि संयमभाव से बाहर न जो जाए, इसलिए उसे पृथक् अपवरक में नहीं रखा जाता किंतु वसति के एक प्रदेश में काष्ठ आदि से अथवा भूति - राख आदि से अंतर कर दिया जाता है जिससे कि साधु एक दूसरे के त्वक्दोष से सहसा स्पृष्ट न हों।
२७९५. अगलंत न वक्खारो, लालासेयादिवज्जण तधेव ।
उस्सास भास-सयणासणादीहि होति संकंती ॥ अस्यन्दमान त्वग्दोष में पृथक् वक्षस्कार - अपवरक नहीं किया जाता। लाला, स्वेद आदि के विषय में पूर्ववत् वर्जना है तथा उच्छ्वास, भाषा, शयनासन आदि से भी यह व्याधि संक्रांत होती है।
२७९६ :
. अवणेतु जल्लपडलं, धरेंति भाणं स काइयादि गतो । सीते व दाउ कप्पं, उवरिमधोतं परिहरति । कायिकी व्युत्सर्ग के लिए गए हुए उस त्वक्रोगी के जल्लपटल को छोड़कर उसके भाजन को अन्य साधु धारण करते हैं। यदि वह त्वग्दोषी शीत से क्लांत हो रहा हो तो उसे प्रावरण के लिए कल्प - वस्त्र दिया जाता है। वह रोगी उस प्रावरणीय को अपने वस्त्रों के ऊपर ओढ़ता है। उस समर्पित वस्त्र को अधौतरूप में काम में ले लेता है। (यदि वे साधु उस वस्त्र को स्वयं काम में लेना चाहें तो उसका प्रक्षालन कर काम में लें ।) २७९७. असहुस्सुव्वत्तणादीणि, कुव्वतो छिक्क जत्तियं ।
खेदमकुव्वंत धोवेज्ज, मट्टियादीहि तत्तियं ॥ त्वदोषी असह है। उसका उद्वर्तन आदि करते हुए जितना उसके शरीर का स्पर्श किया है, खेद न करते हुए, मृत्तिका आदि से उतना भाग घर्षण कर धो डाले। २७९८. असती मोयमहीए, कयकप्पऽगलंतमत्तए निसिरे ।
तेणेव कते कप्पे, इतरे निसिरंति जतणाए । प्रस्रवणभूमी के अभाव में अस्रावी कृतकल्पमात्रक में वह रोगी प्रस्रवण करता है। उसी कृतकल्प मात्रक में दूसरे साधु भी यतनापूर्वक कायिकी का व्युत्सर्ग करें।
२७९९. एसा जतणा उ तहिं कालगते पुण इमो विधी होति ।
अंतरकप्पं जल्लपडलं च अगलंत उज्झति ॥ त्वदोषीमुनि विषयक यह यतना कही गई। अब उसके कालगत हो जाने पर यह विधि प्रयोक्तव्य है। अस्यन्दमान त्वक्रोगी का आंतरकल्प तथा जल्लपटल - उपरीतन वस्त्र- ये दोनों वस्त्र परिष्ठापनीय होते हैं।
२८००. धोतांवि न निद्दोसा, तेण छुडुंति ते दुवे । सेसगं तु कते कप्पे, सव्वं से परिभुंजति ॥ ये दोनों वस्त्र धोने पर भी निर्दोष नहीं होते अतः उनका परिष्ठापन कर दिया जाता है। शेष उसके द्वारा उपभुक्त सारे
Jain Education International
२५९
कल्पों का उपभोग किया जा सकता है, क्योंकि वे सब निर्दोष हैं। २८०१. संदंतस्स वि किंचण, असतीए मोत्तु भायणुक्कोसं । लेवमत्तमवणेत्ता, अण्णमयं धोविउं लिपे ॥
स्यन्दमान त्वक्रोगी के कालगत हो जाने पर उसका जो कुछ है वह सारा का सारा परिष्ठापित कर दिया जाता है, भाजन न हो तो। यदि भाजन उत्कृष्ट हो तो उसको रख दिया जाता है। उसके सारे लेप उतारकर, उष्णोदक से धो-धो कर, उसको अन्यमय की तरह बनाकर उस पर पुनः लेप कर उसका परिभोग किया जा सकता है।
२८०२. अगलंतमत्तसेवी असतीए कप्प काउ भुंजंती ।
एसा जतणा उ भवे, सव्वेसिं तेसि नायव्वा ॥ कायिकीभूमी के अभाव में अस्यन्दमान त्वक्ररोगी अन्य साधुओं के मात्रक में कायिकी का व्युत्सर्ग करता है तथा शेष मुनि भी उस कृतकल्पमात्रक में कायिकी का व्युत्सर्ग करते हैं। यदि अकृतकल्प में व्युत्सर्ग करते हैं तो चार गुरुमास का प्रायश्चित्त आता है। यह यतना स्यन्दान त्वक्दोषी मुनियों के तथा सभी क्षयव्याधि आदि से ग्रस्त मुनियों के विषय में जाननी चाहिए। २८०३. एगाणिस्स दोसा, के त्ति भवे एस सुत्तसंबंधो।
कारणनिवासिणो वा, दुविधा सेविस्स पच्छित्तं ॥ शिष्य का प्रश्न है कि एकाकी के कितने दोष होते हैं ? यह सूत्र का संबंध है। कारणनिवासी के दो प्रकार हैं-सचित्तसेवी और अचित्तसेवी । उनका प्रायश्चित्त क्या है-इसका प्रतिपादन सूत्रद्वय में किया गया है।
२८०४. बाहिं वक्खारठिते, महिला आगम अवारणे गुरुगा।
वारण वासे पेल्लण, उदए पडिसेवणा भणिया ।। बाहर वक्षस्कार- अपवरक में त्वक्दोषी साधु स्थित है। वहां किसी महिला का आगमन होता है। उसका वारण न करने पर चार गुरुमास का प्रायश्चित्त आता है। जैसा वारण उल्लिखित है वैसे करना चाहिए। बाहर वर्षा गिर रही हो । स्त्री साधु को प्रेरित करती है। वेदोदय । प्रतिसेवना कथित है। (इन 'वारण' आदि की व्याख्या आगे ।)
२८०५. पडिसेधो पुव्वुत्तो, उज्जु अणुज्जू मिहुणचउत्थम्मि ।
निग्गममनिग्गमे विय, जहिं च सुत्तस्स पारंभो ॥ वारण-प्रतिषेध पहले कहा जा चुका है। कल्पाध्ययन के चौथे उद्देशक में मिथुन के दो प्रकार - ऋजु अथवा अनृजु कहे गए हैं । सस्त्रीक पुरुष का निर्गम अथवा अनिर्गम वहीं व्याख्यात है। जहां सूत्र का प्रारंभ होता है।
२८०६. जुगछिद्द नालिगादिसु पढमगजामादिसेवणे सोधी । मूलादी पुव्वत्ता, पंचमजामे भवे सुत्तं ॥ युगछिद्र, नालिका आदि में प्रथम याम में हस्तकर्म करने
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org