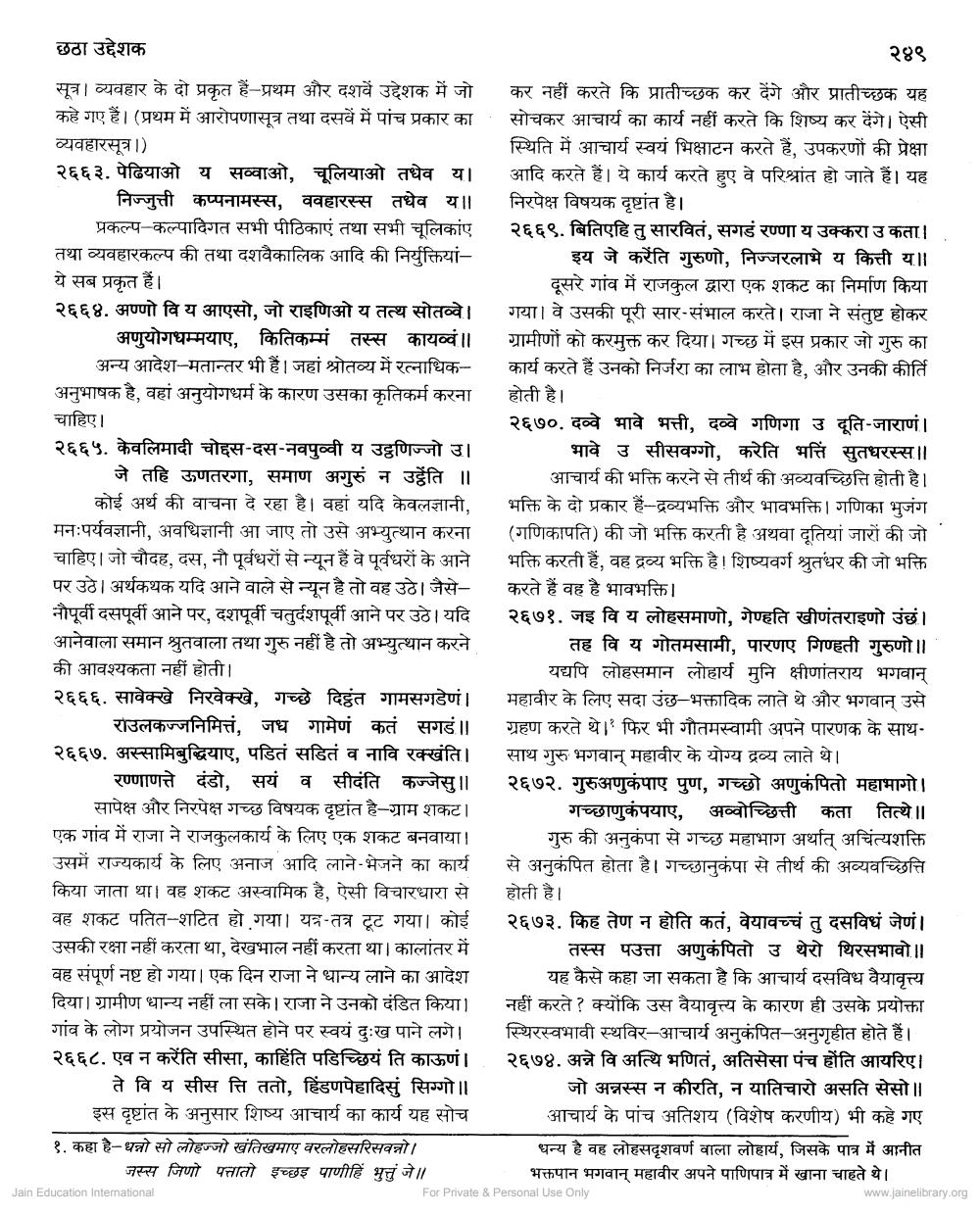________________
छठा उद्देशक
सूत्र । व्यवहार के दो प्रकृत हैं-प्रथम और दशवें उद्देशक में जो कहे गए हैं। (प्रथम में आरोपणासूत्र तथा दसवें में पांच प्रकार का व्यवहारसूत्र ।)
२६६३. पेढियाओ य सव्वाओ, चूलियाओ तधेव य । निज्जुत्ती कप्पनामस्स, ववहारस्स तधेव य ।। प्रकल्प-कल्पादिगत सभी पीठिकाएं तथा सभी चूलिकांए तथा व्यवहारकल्प की तथा दशवैकालिक आदि की नियुक्तियांये सब प्रकृत हैं।
२६६४. अण्णो विय आएसो, जो राइणिओ य तत्थ सोतव्वे । अयोगधम्मयाए, कितिकम्मं तस्स कायव्वं ॥ अन्य आदेश-मतान्तर भी हैं। जहां श्रोतव्य में रत्नाधिकअनुभाषक है, वहां अनुयोगधर्म के कारण उसका कृतिकर्म करना चाहिए।
२६६५. केवलिमादी चोद्दस-दस नवपुव्वी य उट्ठणिज्जो उ । जे तहि ऊणतरगा, समाण अगुरुं न उट्ठेति ॥ कोई अर्थ की वाचना दे रहा है। वहां यदि केवलज्ञानी, मनः पर्यवज्ञानी, अवधिज्ञानी आ जाए तो उसे अभ्युत्थान करना चाहिए। जो चौदह, दस, नौ पूर्वधरों से न्यून हैं वे पूर्वधरों के आने पर उठे । अर्थकथक यदि आने वाले से न्यून है तो वह उठे। जैसे
पूर्वी दसपूर्वी आने पर, दशपूर्वी चतुर्दशपूर्वी आने पर उठे । यदि आनेवाला समान श्रुतवाला तथा गुरु नहीं है तो अभ्युत्थान करने की आवश्यकता नहीं होती।
२६६६. सावेक्खे निरवेक्खे, गच्छे दिट्ठत गामसगडेणं । राउलकज्जनिमित्तं, जध गामेणं कतं सगडं ॥ २६६७. अस्सामिबुद्धियाए, पडितं सडितं व नावि रक्खति ।
रण्णाणत्ते दंडो, सयं व सीदंति कज्जेसु ॥ सापेक्ष और निरपेक्ष गच्छ विषयक दृष्टांत है-ग्राम शकट । एक गांव में राजा ने राजकुलकार्य के लिए एक शकट बनवाया। उसमें राज्यकार्य के लिए अनाज आदि लाने भेजने का कार्य किया जाता था। वह शकट अस्वामिक है, ऐसी विचारधारा से वह शकट पतित-शटित हो गया । यत्र तत्र टूट गया। कोई उसकी रक्षा नहीं करता था, देखभाल नहीं करता था। कालांतर में वह संपूर्ण नष्ट हो गया। एक दिन राजा ने धान्य लाने का आदेश दिया। ग्रामीण धान्य नहीं ला सके। राजा ने उनको दंडित किया। गांव के लोग प्रयोजन उपस्थित होने पर स्वयं दुःख पाने लगे। २६६८. एव न करेंति सीसा, काहिंति पडिच्छियं ति काऊणं ।
ते वि य सीस त्ति ततो, हिंडणपेहादिसुं सिग्गो ॥ इस दृष्टांत के अनुसार शिष्य आचार्य का कार्य यह सोच १. कहा है- धन्नो सो लोहज्जो खंतिखमाए वरलोहसरिसवन्नो । जस्स जिणो पत्तातो इच्छइ पाणीहिं भुत्तुं जे ॥
Jain Education International
२४९
कर नहीं करते कि प्रातीच्छक कर देंगे और प्रातीच्छक यह सोचकर आचार्य का कार्य नहीं करते कि शिष्य कर देंगे। ऐसी स्थिति में आचार्य स्वयं भिक्षाटन करते हैं, उपकरणों की प्रेक्षा आदि करते हैं। ये कार्य करते हुए वे परिश्रांत हो जाते हैं। यह निरपेक्ष विषयक दृष्टांत है।
२६६९. बितिएहि तु सारवितं, सगडं रण्णा य उक्करा उ कता ।
इय जे करेंति गुरुणो, निज्जरलाभे य कित्ती य ॥ दूसरे गांव में राजकुल द्वारा एक शकट का निर्माण किया गया। वे उसकी पूरी सार-संभाल करते । राजा ने संतुष्ट होकर ग्रामीणों को करमुक्त कर दिया। गच्छ में इस प्रकार जो गुरु का कार्य करते हैं उनको निर्जरा का लाभ होता है, और उनकी कीर्ति होती है।
२६७०. दव्वे भावे भत्ती, दव्वे गणिगा उ दूति- जाराणं ।
भावे उ सीसवग्गो, करेति भत्तिं सुतधरस्स ॥ आचार्य की भक्ति करने से तीर्थ की अव्यवच्छित्ति होती है । भक्ति के दो प्रकार हैं- द्रव्यभक्ति और भावभक्ति । गणिका भुजंग (गणिकापति) की जो भक्ति करती है अथवा दूतियां जारों की जो भक्ति करती हैं, वह द्रव्य भक्ति है। शिष्यवर्ग श्रुतधर की जो भक्ति करते हैं वह है भावभक्ति ।
२६७१. जइ वि य लोहसमाणो, गेण्हति खीणंतराइणो उछं ।
तह वि य गोतमसामी, पारणए गिण्हती गुरुणो ॥ यद्यपि लोहसमान लोहार्य मुनि क्षीणांतराय भगवान् महावीर के लिए सदा उंछ-भक्तादिक लाते थे और भगवान् उसे ग्रहण करते थे। फिर भी गौतमस्वामी अपने पारणक के साथसाथ गुरु भगवान् महावीर के योग्य द्रव्य लाते थे। २६७२. गुरुअणुकंपाए पुण, गच्छो अणुकंपितो महाभागो ।
गच्छाणुकंपयाए, अव्वोच्छित्ती कता तित्थे ।
गुरु की अनुकंपा से गच्छ महाभाग अर्थात् अचिंत्यशक्ति से अनुकंपित होता है। गच्छानुकंपा से तीर्थ की अव्यवच्छित्ति होती है।
२६७३. किह तेण न होति कतं, वेयावच्चं तु दसविधं जेणं ।
तस्स पउत्ता अणुकंपितो उ थेरो थिरसभावो ॥ यह कैसे कहा जा सकता है कि आचार्य दसविध वैयावृत्त्य नहीं करते? क्योंकि उस वैयावृत्त्य के कारण ही उसके प्रयोक्ता स्थिरस्वभावी स्थविर - आचार्य अनुकंपित - अनुगृहीत होते हैं । २६७४. अन्ने वि अत्थि भणितं, अतिसेसा पंच होंति आयरिए ।
जो अन्नस्स न कीरति, न यातिचारो असति सेसो ॥ आचार्य के पांच अतिशय (विशेष करणीय) भी कहे गए धन्य है वह लोहसदृशवर्ण वाला लोहार्य, जिसके पात्र में आनीत भक्तपान भगवान् महावीर अपने पाणिपात्र में खाना चाहते थे ।
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org