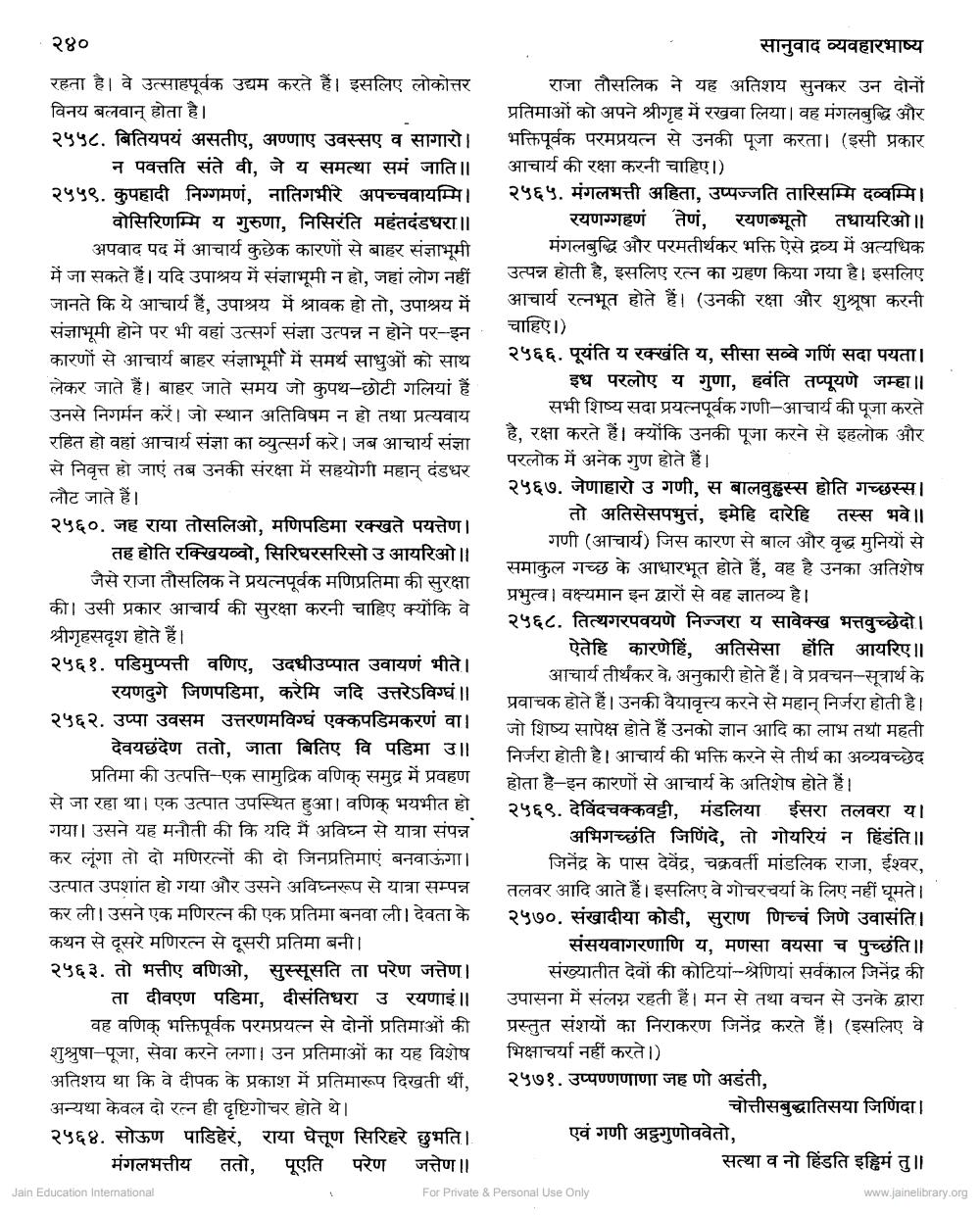________________
२४०
सानुवाद व्यवहारभाष्य रहता है। वे उत्साहपूर्वक उद्यम करते हैं। इसलिए लोकोत्तर राजा तौसलिक ने यह अतिशय सुनकर उन दोनों विनय बलवान् होता है।
प्रतिमाओं को अपने श्रीगृह में रखवा लिया। वह मंगलबुद्धि और २५५८. बितियपयं असतीए, अण्णाए उवस्सए व सागारो। भक्तिपूर्वक परमप्रयत्न से उनकी पूजा करता। (इसी प्रकार
न पवत्तति संते वी, जे य समत्था समं जाति॥ आचार्य की रक्षा करनी चाहिए।) २५५९. कुपहादी निग्गमणं, नातिगभीरे अपच्चवायम्मि। २५६५. मंगलभत्ती अहिता, उप्पज्जति तारिसम्मि दव्वम्मि। वोसिरिणम्मि य गुरुणा, निसिरंति महंतदंडधरा॥
रयणग्गहणं तेणं, रयणन्भूतो तधायरिओ॥ अपवाद पद में आचार्य कुछेक कारणों से बाहर संज्ञाभूमी
मंगलबुद्धि और परमतीर्थकर भक्ति ऐसे द्रव्य में अत्यधिक में जा सकते हैं। यदि उपाश्रय में संज्ञाभूमी न हो, जहां लोग नहीं
उत्पन्न होती है, इसलिए रत्न का ग्रहण किया गया है। इसलिए जानते कि ये आचार्य हैं, उपाश्रय में श्रावक हो तो, उपाश्रय में
आचार्य रत्नभूत होते हैं। (उनकी रक्षा और शुश्रूषा करनी संज्ञाभूमी होने पर भी वहां उत्सर्ग संज्ञा उत्पन्न न होने पर-इन ।
चाहिए।) कारणों से आचार्य बाहर संज्ञाभूमी में समर्थ साधुओं को साथ
२५६६. पूर्वति य रक्खंति य, सीसा सव्वे गणिं सदा पयता। लेकर जाते हैं। बाहर जाते समय जो कुपथ-छोटी गलियां हैं
इध परलोए य गुणा, हवंति तप्पूयणे जम्हा॥ उनसे निगमन करें। जो स्थान अतिविषम न हो तथा प्रत्यवाय
सभी शिष्य सदा प्रयत्नपूर्वक गणी-आचार्य की पूजा करते रहित हो वहां आचार्य संज्ञा का व्युत्सर्ग करे। जब आचार्य संज्ञा
है, रक्षा करते हैं। क्योंकि उनकी पूजा करने से इहलोक और
परलोक में अनेक गुण होते हैं। से निवृत्त हो जाएं तब उनकी संरक्षा में सहयोगी महान् दंडधर
२५६७. जेणाहारो उ गणी, स बालवुड्डस्स होति गच्छस्स। लौट जाते हैं।
तो अतिसेसपभुत्तं, इमेहि दारेहि तस्स भवे॥ २५६०. जह राया तोसलिओ, मणिपडिमा रक्खते पयत्तेण।
गणी (आचार्य) जिस कारण से बाल और वृद्ध मुनियों से तह होति रक्खियव्वो, सिरिघरसरिसोउ आयरिओ।।
समाकुल गच्छ के आधारभूत होते हैं, वह है उनका अतिशेष जैसे राजा तौसलिक ने प्रयत्नपूर्वक मणिप्रतिमा की सुरक्षा
प्रभुत्व। वक्ष्यमान इन द्वारों से वह ज्ञातव्य है। की। उसी प्रकार आचार्य की सुरक्षा करनी चाहिए क्योंकि वे
२५६८. तित्थगरपवयणे निज्जरा य सावेक्ख भत्तवुच्छेदो। श्रीगृहसदृश होते हैं।
ऐतेहि कारणेहिं, अतिसेसा होति आयरिए। २५६१. पडिमुप्पत्ती वणिए, उदधीउप्पात उवायणं भीते।
आचार्य तीर्थंकर के अनुकारी होते हैं। वे प्रवचन-सूत्रार्थ के रयणदुगे जिणपडिमा, करेमि जदि उत्तरेऽविग्घं ।।
प्रवाचक होते हैं। उनकी वैयावृत्त्य करने से महान् निर्जरा होती है। २५६२. उप्पा उवसम उत्तरणमविग्घं एक्कपडिमकरणं वा।
जो शिष्य सापेक्ष होते हैं उनको ज्ञान आदि का लाभ तथा महती देवयछंदेण ततो, जाता बितिए वि पडिमा उ॥
निर्जरा होती है। आचार्य की भक्ति करने से तीर्थ का अव्यवच्छेद प्रतिमा की उत्पत्ति-एक सामुद्रिक वणिक् समुद्र में प्रवहण ।
होता है-इन कारणों से आचार्य के अतिशेष होते हैं। से जा रहा था। एक उत्पात उपस्थित हुआ। वणिक् भयभीत हो २५६९. देविंदचक्कवट्टी, मंडलिया ईसरा तलवरा य। गया। उसने यह मनौती की कि यदि मैं अविघ्न से यात्रा संपन्न
__ अभिगच्छंति जिणिंदे, तो गोयरियं न हिंडंति॥ कर लूंगा तो दो मणिरत्नों की दो जिनप्रतिमाएं बनवाऊंगा।
जिनेंद्र के पास देवेंद्र, चक्रवर्ती मांडलिक राजा, ईश्वर, उत्पात उपशांत हो गया और उसने अविघ्नरूप से यात्रा सम्पन्न तलवर आदि आते हैं। इसलिए वे गोचरचर्या के लिए नहीं घूमते। कर ली। उसने एक मणिरत्न की एक प्रतिमा बनवा ली। देवता के २५७०. संखादीया कोडी, सुराण णिच्चं जिणे उवासंति। कथन से दूसरे मणिरत्न से दूसरी प्रतिमा बनी।
संसयवागरणाणि य, मणसा वयसा च पुच्छंति॥ २५६३. तो भत्तीए वणिओ, सुस्सूसति ता परेण जत्तेण। संख्यातीत देवों की कोटियां-श्रेणियां सर्वकाल जिनेंद्र की
ता दीवएण पडिमा, दीसंतिधरा उ रयणाई॥ उपासना में संलग्न रहती हैं। मन से तथा वचन से उनके द्वारा वह वणिक् भक्तिपूर्वक परमप्रयत्न से दोनों प्रतिमाओं की प्रस्तुत संशयों का निराकरण जिनेंद्र करते हैं। (इसलिए वे शुश्रुषा-पूजा, सेवा करने लगा। उन प्रतिमाओं का यह विशेष भिक्षाचर्या नहीं करते।) अतिशय था कि वे दीपक के प्रकाश में प्रतिमारूप दिखती थीं, २५७१. उप्पण्णणाणा जह णो अडंती, अन्यथा केवल दो रत्न ही दृष्टिगोचर होते थे।
चोत्तीसबुद्धातिसया जिणिंदा। २५६४. सोऊण पाडिहेरं, राया घेत्तूण सिरिहरे छुभति।
एवं गणी अट्ठगुणोववेतो, मंगलभत्तीय ततो, पूएति परेण जत्तेण ।।
सत्था व नो हिंडति इड्डिमं तु॥
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org