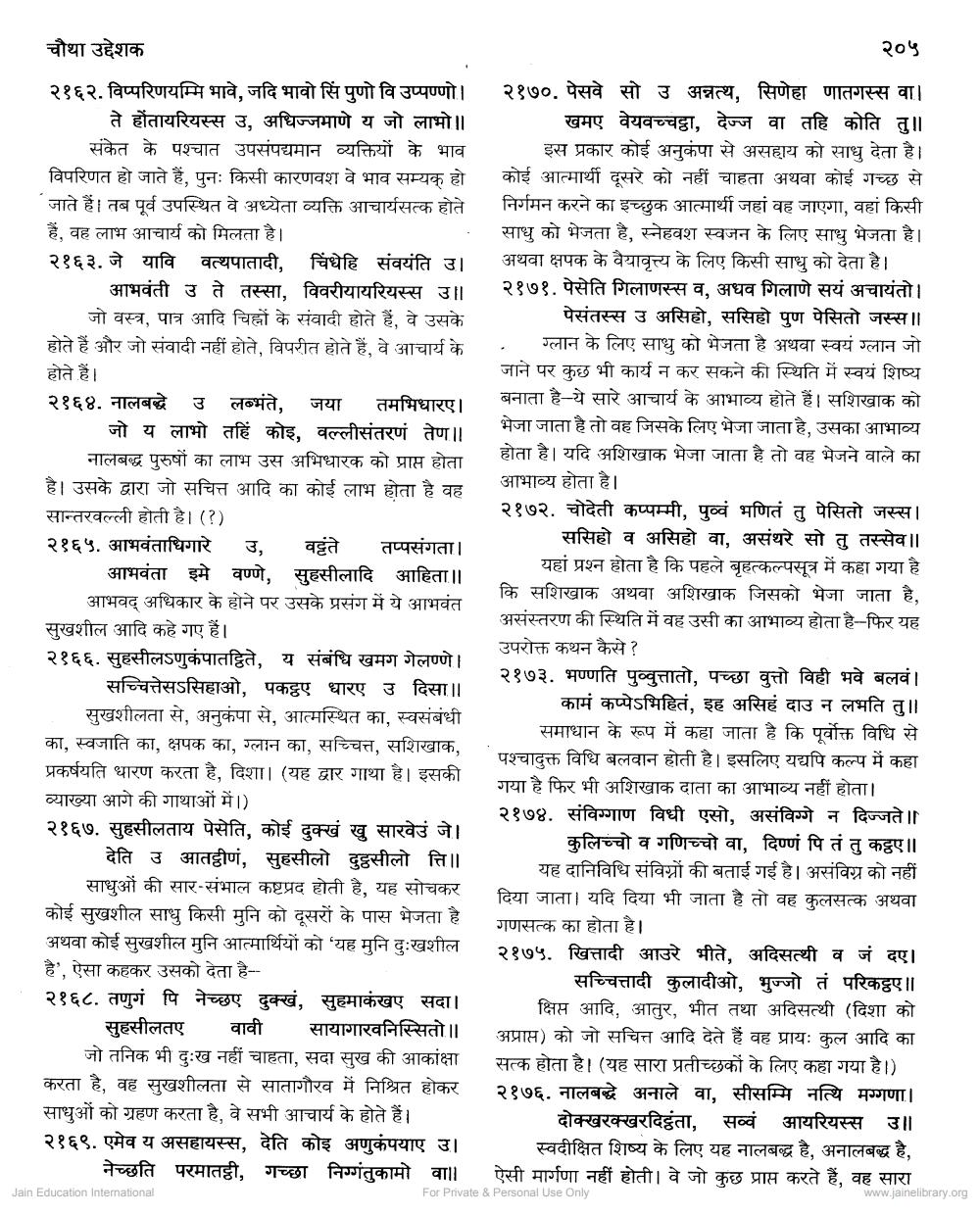________________
चौथा उद्देशक
२०५ २१६२. विप्परिणयम्मि भावे, जदि भावो सिं पुणो वि उप्पण्णो। २१७०. पेसवे सो उ अन्नत्थ, सिणेहा णातगस्स वा। ते होंतायरियस्स उ, अधिज्जमाणे य जो लाभो॥
खमए वेयवच्चट्ठा, देज्ज वा तहि कोति तु॥ संकेत के पश्चात उपसंपद्यमान व्यक्तियों के भाव इस प्रकार कोई अनुकंपा से असहाय को साधु देता है। विपरिणत हो जाते हैं, पुनः किसी कारणवश वे भाव सम्यक् हो कोई आत्मार्थी दूसरे को नहीं चाहता अथवा कोई गच्छ से जाते हैं। तब पूर्व उपस्थित वे अध्येता व्यक्ति आचार्यसत्क होते निर्गमन करने का इच्छुक आत्मार्थी जहां वह जाएगा, वहां किसी हैं, वह लाभ आचार्य को मिलता है।
साधु को भेजता है, स्नेहवश स्वजन के लिए साधु भेजता है। २१६३. जे यावि वत्थपातादी, चिंधेहि संवयंति उ। अथवा क्षपक के वैयावृत्त्य के लिए किसी साधु को देता है।
आभवंती उ ते तस्सा, विवरीयायरियस्स उ॥ २१७१. पेसेति गिलाणस्स व, अधव गिलाणे सयं अचायतो। जो वस्त्र, पात्र आदि चिह्नों के संवादी होते हैं, वे उसके
पेसंतस्स उ असिहो, ससिहो पुण पेसितो जस्स। होते हैं और जो संवादी नहीं होते, विपरीत होते हैं, वे आचार्य के . ग्लान के लिए साधु को भेजता है अथवा स्वयं ग्लान जो होते हैं।
जाने पर कुछ भी कार्य न कर सकने की स्थिति में स्वयं शिष्य २१६४. नालबद्धे उ लब्भंते, जया तमभिधारए।
बनाता है-ये सारे आचार्य के आभाव्य होते हैं। सशिखाक को जो य लाभो तहिं कोइ, वल्लीसंतरणं तेण।।
भेजा जाता है तो वह जिसके लिए भेजा जाता है, उसका आभाव्य नालबद्ध पुरुषों का लाभ उस अभिधारक को प्राप्त होता
होता है। यदि अशिखाक भेजा जाता है तो वह भेजने वाले का है। उसके द्वारा जो सचित्त आदि का कोई लाभ होता है वह
आभाव्य होता है। सान्तरवल्ली होती है। (?)
२१७२. चोदेती कप्पम्मी, पुव्वं भणितं तु पेसितो जस्स। २१६५. आभवंताधिगारे उ, वटुंते तप्पसंगता।
ससिहो व असिहो वा, असंथरे सो तु तस्सेव।। आभवंता इमे वण्णे, सुहसीलादि आहिता।।
यहां प्रश्न होता है कि पहले बृहत्कल्पसूत्र में कहा गया है आभवद् अधिकार के होने पर उसके प्रसंग में ये आभवंत
कि सशिखाक अथवा अशिखाक जिसको भेजा जाता है,
असंस्तरण की स्थिति में वह उसी का आभाव्य होता है-फिर यह सुखशील आदि कहे गए हैं।
उपरोक्त कथन कैसे? २१६६. सुहसीलऽणुकंपातट्टिते, य संबंधि खमग गेलण्णे।
२१७३. भण्णति पुव्वुत्तातो, पच्छा वुत्तो विही भवे बलवं। सच्चित्तेसऽसिहाओ, पकट्ठए धारए उ दिसा।।
__ कामं कप्पेऽभिहितं, इह असिहं दाउ न लभति तु॥ सुखशीलता से, अनुकंपा से, आत्मस्थित का, स्वसंबंधी
समाधान के रूप में कहा जाता है कि पूर्वोक्त विधि से का, स्वजाति का, क्षपक का, ग्लान का, सच्चित्त, सशिखाक,
पश्चादुक्त विधि बलवान होती है। इसलिए यद्यपि कल्प में कहा प्रकर्षयति धारण करता है, दिशा। (यह द्वार गाथा है। इसकी
गया है फिर भी अशिखाक दाता का आभाव्य नहीं होता। व्याख्या आगे की गाथाओं में।)
२१७४. संविग्गाण विधी एसो, असंविग्गे न दिज्जते।। २१६७. सुहसीलताय पेसेति, कोई दुक्खं खु सारवेउं जे।
कुलिच्चो व गणिच्चो वा, दिण्णं पि तं तु कट्ठए।। देति उ आतट्ठीणं, सुहसीलो दुट्ठसीलो ति॥
यह दानिविधि संविग्नों की बताई गई है। असंविग्न को नहीं साधुओं की सार-संभाल कष्टप्रद होती है, यह सोचकर
दिया जाता। यदि दिया भी जाता है तो वह कुलसत्क अथवा कोई सुखशील साधु किसी मुनि को दूसरों के पास भेजता है।
गणसत्क का होता है। अथवा कोई सुखशील मुनि आत्मार्थियों को 'यह मुनि दुःखशील
२१७५. खित्तादी आउरे भीते, अदिसत्थी व जं दए। है', ऐसा कहकर उसको देता है
सच्चित्तादी कुलादीओ, भुज्जो तं परिकट्ठए॥ २१६८. तणुगं पि नेच्छए दुक्खं, सुहमाकंखए सदा।
क्षिप्त आदि, आतुर, भीत तथा अदिसत्थी (दिशा को __सुहसीलतए वावी सायागारवनिस्सितो॥
अप्राप्त) को जो सचित्त आदि देते हैं वह प्रायः कुल आदि का जो तनिक भी दुःख नहीं चाहता, सदा सुख की आकांक्षा
सत्क होता है। (यह सारा प्रतीच्छकों के लिए कहा गया है।) करता है, वह सुखशीलता से सातागौरव में निश्रित होकर
२१७६. नालबद्धे अनाले वा, सीसम्मि नत्थि मग्गणा। साधुओं को ग्रहण करता है, वे सभी आचार्य के होते हैं।
दोक्खरक्खरदिटुंता, सव्वं आयरियस्स उ॥ २१६९. एमेव य असहायस्स, देति कोइ अणुकंपयाए उ। स्वदीक्षित शिष्य के लिए यह नालबद्ध है, अनालबद्ध है,
नेच्छति परमातट्ठी, गच्छा निग्गंतुकामो वा। ऐसी मार्गणा नहीं होती। वे जो कुछ प्राप्त करते हैं, वह सारा Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org