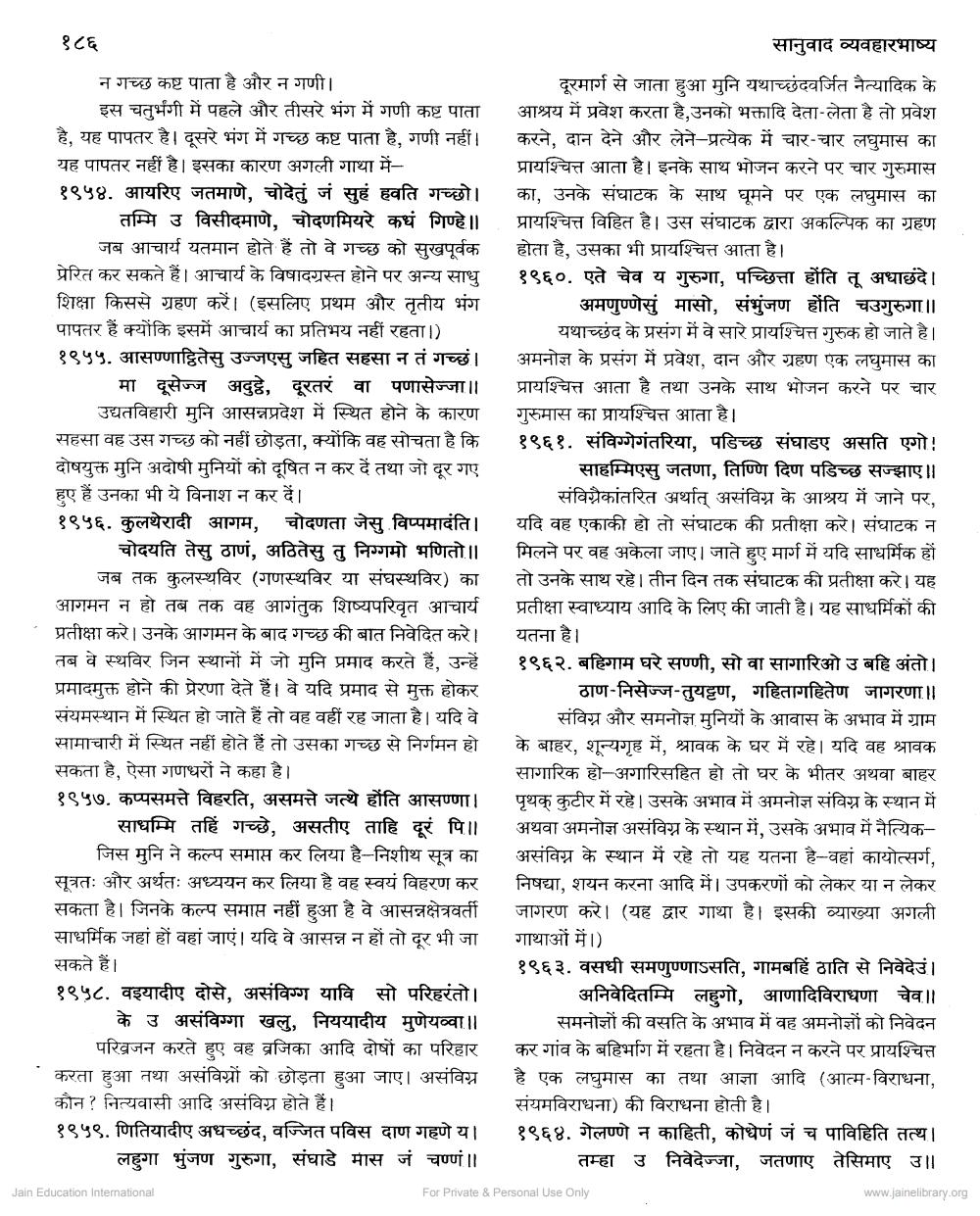________________
१८६
सानुवाद व्यवहारभाष्य
न गच्छ कष्ट पाता है और न गणी।
दूरमार्ग से जाता हुआ मुनि यथाच्छंदवर्जित नैत्यादिक के इस चतुर्भगी में पहले और तीसरे भंग में गणी कष्ट पाता आश्रय में प्रवेश करता है,उनको भक्तादि देता-लेता है तो प्रवेश है, यह पापतर है। दूसरे भंग में गच्छ कष्ट पाता है, गणी नहीं। करने, दान देने और लेने-प्रत्येक में चार-चार लघुमास का यह पापतर नहीं है। इसका कारण अगली गाथा में
प्रायश्चित्त आता है। इनके साथ भोजन करने पर चार गुरुमास १९५४. आयरिए जतमाणे, चोदेतुं जं सुहं हवति गच्छो।। का, उनके संघाटक के साथ घूमने पर एक लघुमास का
तम्मि उ विसीदमाणे, चोदणमियरे कधं गिण्हे॥ प्रायश्चित्त विहित है। उस संघाटक द्वारा अकल्पिक का ग्रहण जब आचार्य यतमान होते हैं तो वे गच्छ को सुखपूर्वक होता है, उसका भी प्रायश्चित्त आता है। प्रेरित कर सकते हैं। आचार्य के विषादग्रस्त होने पर अन्य साधु १९६०. एते चेव य गुरुगा, पच्छित्ता होति तू अधाछंदे। शिक्षा किससे ग्रहण करें। (इसलिए प्रथम और तृतीय भंग
अमणुण्णेसुं मासो, संभुंजण होति चउगुरुगा। पापतर हैं क्योंकि इसमें आचार्य का प्रतिभय नहीं रहता।) __ यथाच्छंद के प्रसंग में वे सारे प्रायश्चित्त गुरुक हो जाते है। १९५५. आसण्णाद्वितेसु उज्जएसु जहित सहसा न तं गच्छं। अमनोज्ञ के प्रसंग में प्रवेश, दान और ग्रहण एक लघुमास का
मा दूसेज्ज अदुढे, दूरतरं वा पणासेज्जा। प्रायश्चित्त आता है तथा उनके साथ भोजन करने पर चार उद्यतविहारी मुनि आसन्नप्रदेश में स्थित होने के कारण गुरुमास का प्रायश्चित्त आता है। सहसा वह उस गच्छ को नहीं छोड़ता, क्योंकि वह सोचता है कि १९६१. संविग्गेगंतरिया, पडिच्छ संघाडए असति एगो! दोषयुक्त मुनि अदोषी मुनियों को दूषित न कर दें तथा जो दूर गए
साहम्मिएसु जतणा, तिण्णि दिण पडिच्छ सज्झाए। हुए हैं उनका भी ये विनाश न कर दें।
संविग्नैकांतरित अर्थात् असंविग्न के आश्रय में जाने पर, १९५६. कुलथेरादी आगम, चोदणता जेसु विप्पमादंति। यदि वह एकाकी हो तो संघाटक की प्रतीक्षा करे। संघाटक न
चोदयति तेसु ठाणं, अठितेसु तु निग्गमो भणितो।। मिलने पर वह अकेला जाए। जाते हुए मार्ग में यदि साधर्मिक हों जब तक कुलस्थविर (गणस्थविर या संघस्थविर) का तो उनके साथ रहे। तीन दिन तक संघाटक की प्रतीक्षा करे। यह आगमन न हो तब तक वह आगंतुक शिष्यपरिवृत आचार्य प्रतीक्षा स्वाध्याय आदि के लिए की जाती है। यह साधर्मिकों की प्रतीक्षा करे। उनके आगमन के बाद गच्छ की बात निवेदित करे। यतना है। तब वे स्थविर जिन स्थानों में जो मुनि प्रमाद करते हैं, उन्हें १९६२. बहिगाम घरे सण्णी, सो वा सागारिओ उ बहि अंतो। प्रमादमुक्त होने की प्रेरणा देते हैं। वे यदि प्रमाद से मुक्त होकर
ठाण-निसेज्ज-तुयट्टण, गहितागहितेण जागरणा।। संयमस्थान में स्थित हो जाते हैं तो वह वहीं रह जाता है। यदि वे संविग्न और समनोज्ञ मुनियों के आवास के अभाव में ग्राम सामाचारी में स्थित नहीं होते हैं तो उसका गच्छ से निर्गमन हो के बाहर, शून्यगृह में, श्रावक के घर में रहे। यदि वह श्रावक सकता है, ऐसा गणधरों ने कहा है।
सागारिक हो-अगारिसहित हो तो घर के भीतर अथवा बाहर १९५७. कप्पसमत्ते विहरति, असमत्ते जत्थे होति आसण्णा। पृथक् कुटीर में रहे। उसके अभाव में अमनोज्ञ संविग्न के स्थान में
साधम्मि तहिं गच्छे, असतीए ताहि दूरं पि॥ अथवा अमनोज्ञ असंविग्न के स्थान में, उसके अभाव में नैत्यिकजिस मुनि ने कल्प समाप्त कर लिया है-निशीथ सूत्र का असंविग्न के स्थान में रहे तो यह यतना है-वहां कायोत्सर्ग, सूत्रतः और अर्थतः अध्ययन कर लिया है वह स्वयं विहरण कर निषद्या, शयन करना आदि में। उपकरणों को लेकर या न लेकर सकता है। जिनके कल्प समाप्त नहीं हुआ है वे आसन्नक्षेत्रवर्ती जागरण करे। (यह द्वार गाथा है। इसकी व्याख्या अगली साधर्मिक जहां हों वहां जाएं। यदि वे आसन्न न हो तो दूर भी जा गाथाओं में।) सकते हैं।
१९६३. वसधी समणुण्णाऽसति, गामबहिं ठाति से निवेदेउं। १९५८. वइयादीए दोसे, असंविग्ग यावि सो परिहरंतो।
अनिवेदितम्मि लहुगो, आणादिविराधणा चेव।। के उ असंविग्गा खलु, निययादीय मुणेयव्वा ।। समनोज्ञों की वसति के अभाव में वह अमनोज्ञों को निवेदन परिव्रजन करते हुए वह व्रजिका आदि दोषों का परिहार कर गांव के बहिर्भाग में रहता है। निवेदन न करने पर प्रायश्चित्त करता हुआ तथा असंविग्नों को छोड़ता हुआ जाए। असंविग्न है एक लघुमास का तथा आज्ञा आदि (आत्म-विराधना, कौन ? नित्यवासी आदि असंविग्न होते हैं।
संयमविराधना) की विराधना होती है। १९५९. णितियादीए अधच्छंद, वज्जित पविस दाण गहणे य। १९६४. गेलण्णे न काहिती, कोधेणं जं च पाविहिति तत्थ । लहुगा भुंजण गुरुगा, संघाडे मास जं चण्णं॥
तम्हा उ निवेदेज्जा, जतणाए तेसिमाए उ॥
आनवावतार
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org