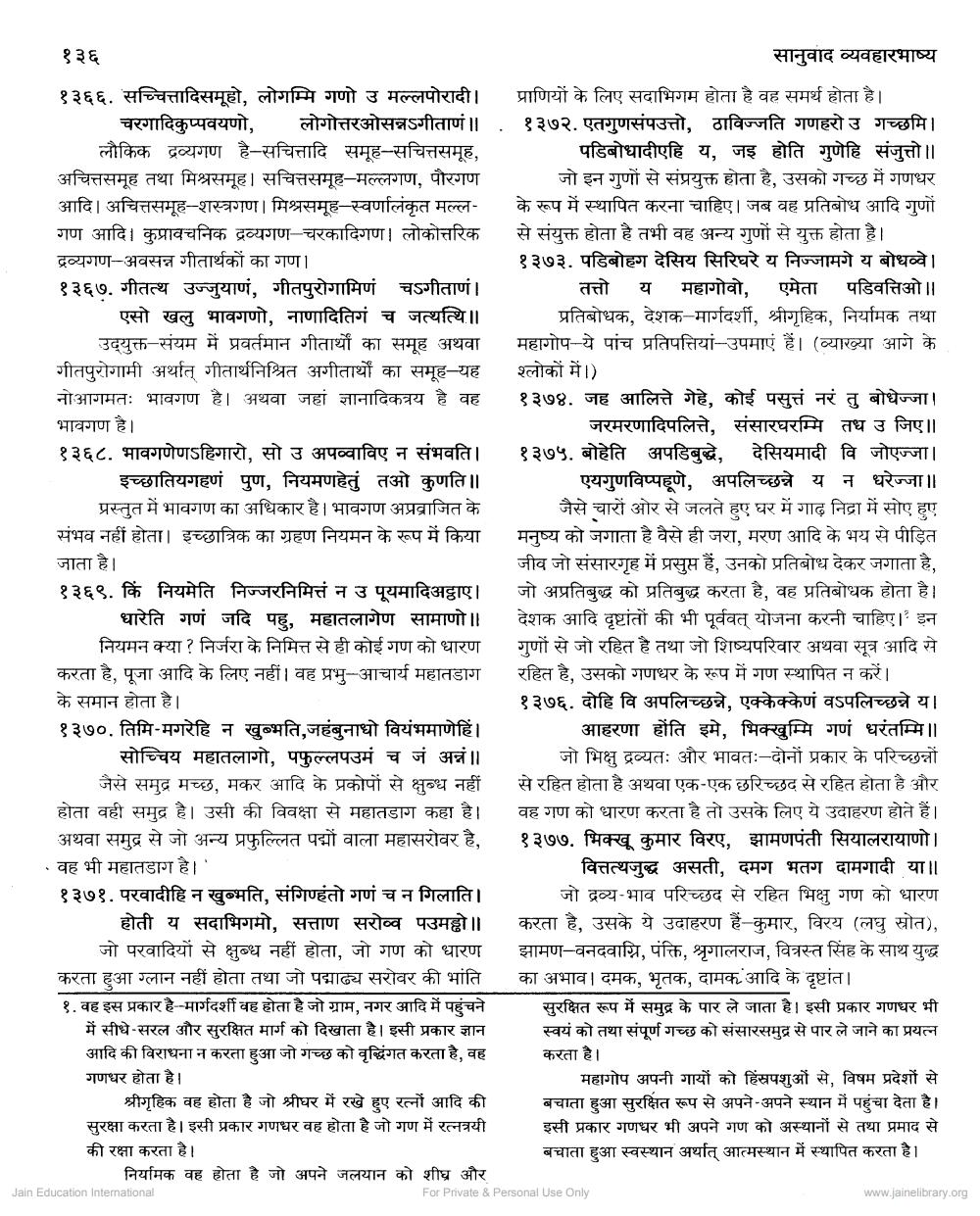________________
१३६
१३६६. सच्चित्तादिसमूहो, लोगम्मि गणो उ मल्लपोरादी। चरगादिकुप्पवयणो, लोगोत्तरओसन्नऽगीताणं ॥ लौकिक द्रव्यगण है- सचित्तादि समूह सचित्तसमूह, अचित्तसमूह तथा मिश्रसमूह सचित्तसमूह मल्लगण, पौरगण आदि । अचित्तसमूह-शस्त्रगण । मिश्रसमूह-स्वर्णालंकृत मल्लगण आदि। कुप्रावयनिक द्रव्यगण - चरकादिगण । लोकोत्तरिक द्रव्यगण - अवसन्न गीतार्थकों का गण |
१३६७. गीतत्थ उज्जुयाणं, गीतपुरोगामिणं चऽगीताणं ।
एसो खलु भावगणो, नाणादितिगं च जत्थत्थि ॥ उद्युक्त-संयम में प्रवर्तमान गीतार्थों का समूह अथवा गीतपुरोगामी अर्थात् गीतार्थनिश्रित अगीतार्थों का समूह यह नो आगमतः भावगण है। अथवा जहां ज्ञानादिकत्रय है वह भावगण है।
१३६८. भावगणेणऽहिगारो, सो उ अपव्वाविए न संभवति । इच्छातियहणं पुण, नियमणहेतुं तओ कुणति ॥ प्रस्तुत में भावगण का अधिकार है। भावगण अप्रव्राजित के संभव नहीं होता । इच्छात्रिक का ग्रहण नियमन के रूप में किया जाता है।
१३६९. किं नियमेति निज्जरनिमित्तं न उ पूयमादिअट्ठाए ।
धारेत गणं जदि पहु, महातलागेण सामाणो ॥ नियमन क्या ? निर्जरा के निमित्त से ही कोई गण को धारण करता है, पूजा आदि के लिए नहीं। वह प्रभु-आचार्य महातडाग के समान होता है ।
१३७०. तिमि - मगरेहि न खुब्भति, जहंबुनाधो वियंभमाणेहिं । सोच्चिय महातलागो, पफुल्लपउम च जं अनं ॥ जैसे समुद्र मच्छ, मकर आदि के प्रकोपों से क्षुब्ध नहीं होता वही समुद्र है। उसी की विवक्षा से महातडाग कहा है। अथवा समुद्र से जो अन्य प्रफुल्लित पद्मों वाला महासरोवर है, वह भी महातडाग है।
१३७१. परवादीहि न खुम्मति, संगिण्हंतो गणं च न गिलाति ।
होती य सदाभिगमो, सत्ताण सरोव्व पउमड्डो ॥ जो परवादियों से क्षुब्ध नहीं होता, जो गण को धारण करता हुआ ग्लान नहीं होता तथा जो पद्माढ्य सरोवर की भांति १. वह इस प्रकार है--मार्गदर्शी वह होता है जो ग्राम, नगर आदि में पहुंचने में सीधे सरल और सुरक्षित मार्ग को दिखाता है। इसी प्रकार ज्ञान आदि की विराधना न करता हुआ जो गच्छ को वृद्धिंगत करता है, वह गणधर होता है।
श्रीगृहिक वह होता है जो श्रीघर में रखे हुए रत्नों आदि की सुरक्षा करता है। इसी प्रकार गणधर वह होता है जो गण में रत्नत्रयी की रक्षा करता है ।
सानुवाद व्यवहारभाष्य प्राणियों के लिए सदाभिगम होता है वह समर्थ होता है। १३७२. एतगुणसंपउत्तो, ठाविज्जति गणहरो उ गच्छमि ।
पडिबोधादीएहि य, जइ होति गुणेहि संजुत्तो ॥ जो इन गुणों से संप्रयुक्त होता है, उसको गच्छ में गणधर के रूप में स्थापित करना चाहिए। जब वह प्रतिबोध आदि गुणों से संयुक्त होता है तभी वह अन्य गुणों से युक्त होता है। १३७३. पडिबोहग देसिय सिरिघरे व निज्जामगे य बोधव्वे ।
Jain Education International
तत्तो य महागोवो, एमेता पडिवत्तिओ ।। प्रतिबोधक, देशक-मार्गदर्शी, श्रीगृहिक, निर्यामक तथा महागोप- ये पांच प्रतिपत्तियां उपमाएं हैं (व्याख्या आगे के श्लोकों में।)
१३७४. जह आलित्ते गेहे, कोई पसुत्तं नरं तु बोधेज्जा | जरमरणादिपलित्ते, संसारपरम्मि तथ उ जिए । १३७५. बोहेति अपडिबुद्धे, देसियमादी वि जोएज्जा । एयगुणविप्पहूणे, अपलिच्छन्ने य न धरेज्जा ॥ जैसे चारों ओर से जलते हुए घर में गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य को जगाता है वैसे ही जरा, मरण आदि के भय से पीड़ित जीव जो संसारगृह में प्रसुप्त हैं, उनको प्रतिबोध देकर जगाता है, जो अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध करता है, वह प्रतिबोधक होता है। देशक आदि दृष्टांतों की भी पूर्ववत् योजना करनी चाहिए। इन गुणों से जो रहित है तथा जो शिष्यपरिवार अथवा सूत्र आदि से रहित है, उसको गणधर के रूप में गण स्थापित न करें। १३७६. दोहि वि अपलिच्छन्ने, एक्केक्केणं वऽपलिच्छन्ने य ।
आहरणा होंति इमे, भिक्खुम्मि गणं धरंतम्मि ॥ जो भिक्षु द्रव्यतः और भावतः दोनों प्रकार के परिच्छन्नों से रहित होता है अथवा एक-एक छरिच्छद से रहित होता है और वह गण को धारण करता है तो उसके लिए ये उदाहरण होते हैं। १३७७. भिक्खू कुमार विरए, झामणपंती सियालरायाणो ।
वित्तत्यजुद्ध असती, दमग मतग दामगादी या ॥ जो द्रव्य भाव परिच्छद से रहित भिक्षु गण को धारण करता है, उसके ये उदाहरण हैं- कुमार, विरय ( लघु स्रोत), झामण-वनदवाग्नि, पंक्ति, श्रृगालराज, वित्रस्त सिंह के साथ युद्ध का अभाव। दमक, भूतक, दामक आदि के वृष्टांत ।
सुरक्षित रूप में समुद्र के पार ले जाता है। इसी प्रकार गणधर भी स्वयं को तथा संपूर्ण गच्छ को संसारसमुद्र से पार ले जाने का प्रयत्न करता है।
महागोप अपनी गायों को हिंखपशुओं से विषम प्रदेशों से बचाता हुआ सुरक्षित रूप से अपने-अपने स्थान में पहुंचा देता है। इसी प्रकार गणधर भी अपने गण को अस्थानों से तथा प्रमाद से बचाता हुआ स्वस्थान अर्थात् आत्मस्थान में स्थापित करता है।
निर्यामक वह होता है जो अपने जलयान को शीघ्र और For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org