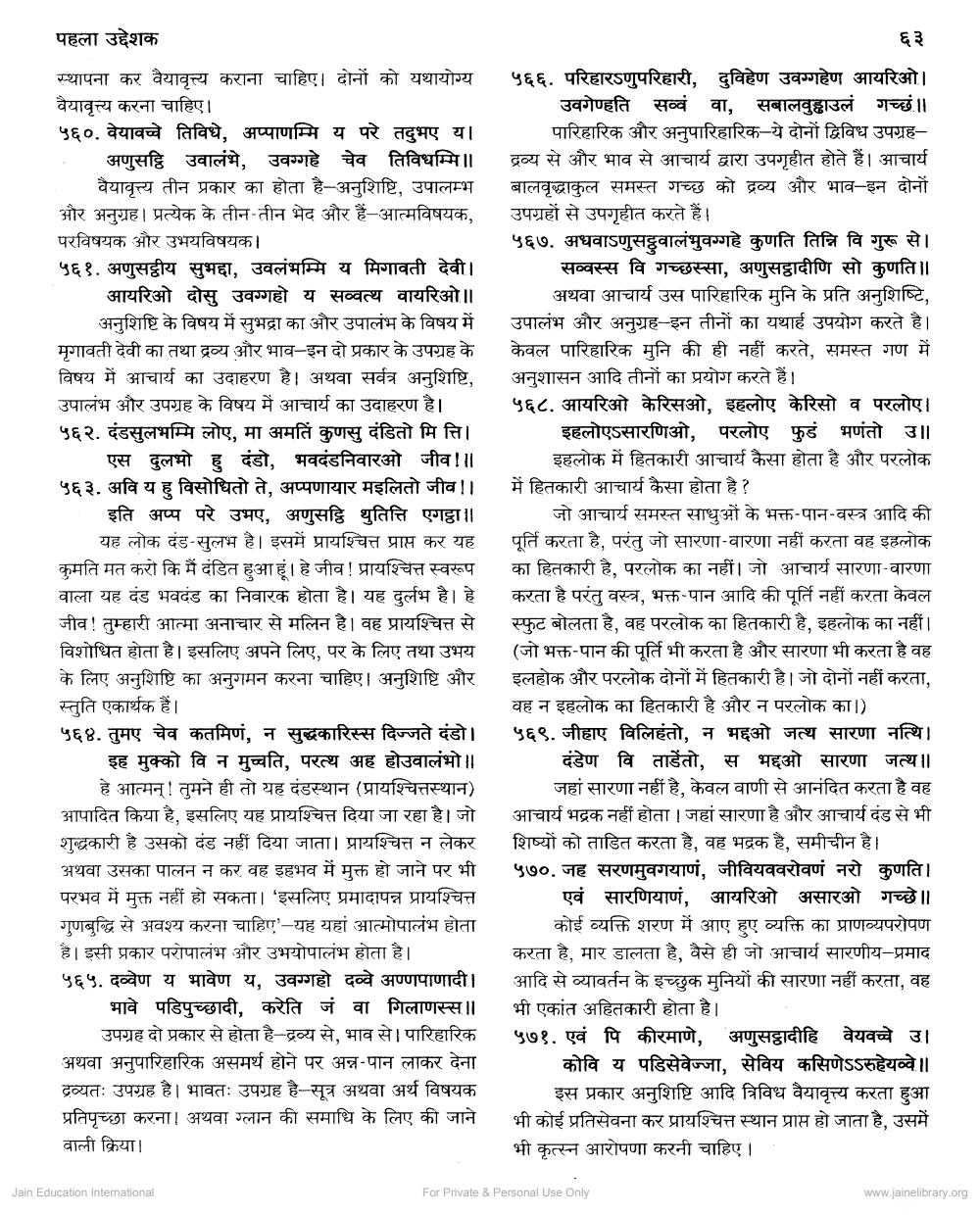________________
पहला उद्देशक
स्थापना कर वैयावृत्त्य कराना चाहिए। दोनों को यथायोग्य वैयावृत्य करना चाहिए।
५६०. वेयावच्चे तिविधे, अप्पाणम्मि य परे तदुभए य ।
अणुसट्ठि उवालंभे, उवग्गहे चेव तिविधम्मि ॥ वैयावृत्त्य तीन प्रकार का होता है-अनुशिष्टि, उपालम्भ और अनुग्रह प्रत्येक के तीन-तीन भेद और है-आत्मविषयक, परविषयक और उभयविषयक ।
|
५६१. अणुसद्वीय सुभद्दा, उवलंभम्मि य मिगावती देवी ।
आयरिओ दोसु उवग्गहो य सव्वत्य वायरिओ ॥ अनुशिष्टि के विषय में सुभद्रा का और उपालंभ के विषय में मृगावती देवी का तथा द्रव्य और भाव- इन दो प्रकार के उपग्रह के विषय में आचार्य का उदाहरण है। अथवा सर्वत्र अनुशिष्टि, उपालंभ और उपग्रह के विषय में आचार्य का उदाहरण है। ५६२. दंडसुलभम्मि लोए, मा अमर्ति कुणसु दंडितो मि ति ।
एस दुलभो हुदंडो, भवदंडनिवारओ जीव ! ॥ ५६३. अवि य हु विसोधितो ते, अप्पणायार मइलितो जीव ! । इति अप्प परे उभए, अणुसट्ठि थुतित्ति एगट्ठा || यह लोक दंड- सुलभ है। इसमें प्रायश्चित्त प्राप्त कर यह कुमति मत करो कि मैं दंडित हुआ हूं। हे जीव ! प्रायश्चित्त स्वरूप वाला यह दंड भवदंड का निवारक होता है। यह दुर्लभ है । है 1 जीव! तुम्हारी आत्मा अनाचार से मलिन है। वह प्रायश्चित्त से विशोधित होता है। इसलिए अपने लिए, पर के लिए तथा उभय के लिए अनुशिष्टि का अनुगमन करना चाहिए। अनुशिष्टि और स्तुति एकार्थक हैं।
५६४. तुमए चैव कतमिणं, न सुद्धकारिस्स दिज्जते दंडो
इह मुक्को वि न मुच्चति, परत्थ अह होउवालंभो ॥ हे आत्मन् ! तुमने ही तो यह दंडस्थान (प्रायश्चित्तस्थान) आपादित किया है, इसलिए यह प्रायश्चित्त दिया जा रहा है। जो शुद्धकारी है उसको दंड नहीं दिया जाता। प्रायश्चित्त न लेकर अथवा उसका पालन न कर वह इहभव में मुक्त हो जाने पर भी में मुक्त नहीं हो सकता। 'इसलिए प्रमादापन्न प्रायश्चित्त गुणबुद्धि से अवश्य करना चाहिए' यह यहां आत्मोपालंभ होता है। इसी प्रकार परोपालंभ और उभयोपालंभ होता है। ५६५. दव्वेण य भावेण य, उवग्गहो दव्वे अण्णपाणादी ।
परभव
भावे पढिपुच्छादी, करेति जं वा गिलाणस्स ॥ उपग्रह दो प्रकार से होता है-द्रव्य से, भाव से । पारिहारिक अथवा अनुपारिहारिक असमर्थ होने पर अन्न-पान लाकर देना द्रव्यतः उपग्रह है। भावतः उपग्रह है-सूत्र अथवा अर्थ विषयक प्रतिपृच्छा करना । अथवा ग्लान की समाधि के लिए की जाने वाली क्रिया।
Jain Education International
६३
५६६. परिहारऽणुपरिहारी, दुविहेण उवग्गहेण आयरिओ
उवगेण्हति सव्वं वा, सबालवुड्डाउलं गच्छं ॥ पारिहारिक और अनुपारिहारिक- ये दोनों द्विविध उपग्रहद्रव्य से और भाव से आचार्य द्वारा उपगृहीत होते हैं। आचार्य बालवृद्धाकुल समस्त गच्छ को द्रव्य और भाव- इन दोनों उपग्रहों से उपगृहीत करते हैं।
५६७. अथवाऽणुसङ्गवालंभुवम्गडे कुणति तिन्नि वि गुरू से ।
सव्वस्स वि गच्छस्सा, अणुसद्वादीणि सो कुणति ॥ अथवा आचार्य उस पारिहारिक मुनि के प्रति अनुशिष्टि, उपालंभ और अनुग्रह इन तीनों का यचाई उपयोग करते है। केवल पारिहारिक मुनि की ही नहीं करते, समस्त गण में अनुशासन आदि तीनों का प्रयोग करते हैं।
५६८. आयरिओ केरिसओ, इहलोए केरिसो व परलोए।
इहलोएऽसारणिओ, परलोए फुडं भणंतो उ ॥ इहलोक में हितकारी आचार्य कैसा होता है और परलोक में हितकारी आचार्य कैसा होता है ?
जो आचार्य समस्त साधुओं के भक्त-पान-वस्त्र आदि की पूर्ति करता है, परंतु जो सारणा वारणा नहीं करता वह इहलोक का हितकारी है, परलोक का नहीं जो आचार्य सारणा वारणा करता है परंतु वस्त्र, भक्त पान आदि की पूर्ति नहीं करता केवल स्फुट बोलता है, वह परलोक का हितकारी है, इहलोक का नहीं । (जो भक्त पान की पूर्ति भी करता है और सारणा भी करता है वह इलहोक और परलोक दोनों में हितकारी है। जो दोनों नहीं करता, वह न इहलोक का हितकारी है और न परलोक का ।) ५६९. जीहाए विलिहंतो न भद्दओ जत्थ सारणा नत्थि ।
दंडेण वि ताडेंतो, स भद्दओ सारणा जत्थ ॥ जहां सारणा नहीं है, केवल वाणी से आनंदित करता है वह आचार्य भद्रक नहीं होता। जहां सारणा है और आचार्य दंड से भी शिष्यों को ताडित करता है, वह भद्रक है, समीचीन है। ५७०. जह सरणमुवगयाणं, जीवियववरोवणं नरो कुणति ।
एवं सारणियाणं, आयरिओ असारओ गच्छे ॥ कोई व्यक्ति शरण में आए हुए व्यक्ति का प्राणव्यपरोपण करता है, मार डालता है, वैसे ही जो आचार्य सारणीय-प्रमाद आदि से व्यावर्तन के इच्छुक मुनियों की सारणा नहीं करता, वह भी एकांत अहितकारी होता है।
-
५७१. एवं पि कीरमाणे, अणुसट्ठादीहि वेयवच्चे उ ।
कोवि य पडिसेवेज्जा, सेविय कसिणेऽऽरुहेयब्वे ॥ इस प्रकार अनुशिष्टि आदि त्रिविध वैयावृत्त्य करता हुआ भी कोई प्रतिसेवना कर प्रायश्चित्त स्थान प्राप्त हो जाता है, भी कृत्स्न आरोपणा करनी चाहिए।
उसमें
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org