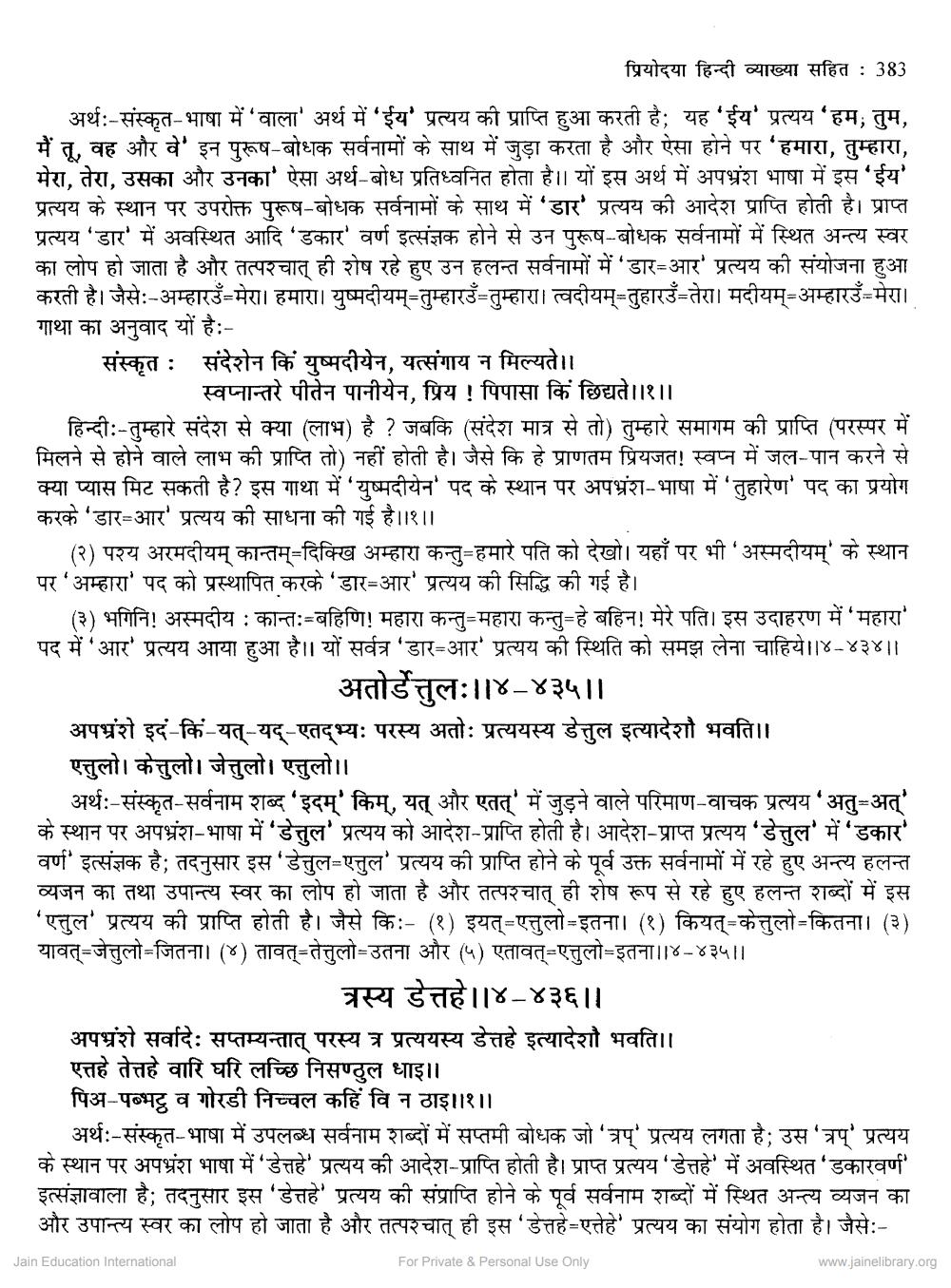________________
प्रियोदया हिन्दी व्याख्या सहित : 383 'हम तुम,
अर्थ:-संस्कृत-भाषा में 'वाला' अर्थ में 'ईय' प्रत्यय की प्राप्ति हुआ करती है; यह 'ईय' प्रत्यय ' मैं तू, वह और वे' इन पुरूष- बोधक सर्वनामों के साथ में जुड़ा करता है और ऐसा होने पर 'हमारा, तुम्हारा, मेरा, तेरा, उसका और उनका ऐसा अर्थ-बोध प्रतिध्वनित होता है । यों इस अर्थ में अपभ्रंश भाषा में इस 'ई' प्रत्यय के स्थान पर उपरोक्त पुरूष-बोधक सर्वनामों के साथ में 'डार' प्रत्यय की आदेश प्राप्ति होती है। प्राप्त प्रत्यय 'डार' में अवस्थित आदि 'डकार' वर्ण इत्संज्ञक होने से उन पुरूष - बोधक सर्वनामों में स्थित अन्त्य स्वर का लोप हो जाता है और तत्पश्चात् ही शेष रहे हुए उन हलन्त सर्वनामों में 'डार - आर' प्रत्यय की संयोजना हुआ करती है। जैसे:-अम्हारउँ- मेरा । हमारा । युष्मदीयम् - तुम्हारउँ = तुम्हारा । त्वदीयम् = तुहारउँ-तेरा। मदीयम्-अम्हारउँ-मेरा । गाथा का अनुवाद यों है:
-
संस्कृत :
संदेशेन किं युष्मदीयेन, यत्संगाय न मिल्यते ।
स्वप्नान्तरे पीतेन पानीयेन, प्रिय ! पिपासा किं छिद्यते ॥ १ ॥
हिन्दी:-तुम्हारे संदेश से क्या (लाभ) है ? जबकि (संदेश मात्र से तो) तुम्हारे समागम की प्राप्ति (परस्पर में मिलने से होने वाले लाभ की प्राप्ति तो) नहीं होती है। जैसे कि हे प्राणतम प्रियजत! स्वप्न में जल - पान करने से क्या प्यास मिट सकती है? इस गाथा में 'युष्मदीयेन' पद के स्थान पर अपभ्रंश भाषा में 'तुहारेण' पद का प्रयोग करके 'डार - आर' प्रत्यय की साधना की गई है || १ ||
(२) पश्य अरमदीयम् कान्तम् = दिक्खि अम्हारा कन्तु हमारे पति को देखो । यहाँ पर भी 'अस्मदीयम्' के स्थान पर 'अम्हारा' पद को प्रस्थापित करके 'डार - आर' प्रत्यय की सिद्धि की गई है।
(३) भगिनि! अस्मदीय : कान्तः - बहिणि ! महारा कन्तु - महारा कन्तु -हे बहिन ! मेरे पति । इस उदाहरण में 'महारा' पद में 'आर' प्रत्यय आया हुआ है । यों सर्वत्र 'डार-आर' प्रत्यय की स्थिति को समझ लेना चाहिये ।।४-४३४।।
अतोर्डेत्तुलः।।४-४३५ ।।
अपभ्रंशे इदं-किं-यत्-यद् - एतद्भ्यः परस्य अतोः प्रत्ययस्य डेत्तुल इत्यादेशौ भवति ।।
तुलो | केतुलो । जेत्तुलो। एत्तुलो ।।
अर्थः- संस्कृत- सर्वनाम शब्द 'इदम् ' किम्, यत् और एतत्' में जुड़ने वाले परिमाण - वाचक प्रत्यय 'अतु-अत्' के स्थान पर अपभ्रंश भाषा में 'डेत्तुल' प्रत्यय को आदेश प्राप्ति होती है। आदेश प्राप्त प्रत्यय 'डेत्तुल' में 'डकार' 'वर्ण' इत्संज्ञक है; तदनुसार इस 'डेत्तुल= एत्तुल' प्रत्यय की प्राप्ति होने के पूर्व उक्त सर्वनामों में रहे हुए अन्त्य हलन्त व्यजन का तथा उपान्त्य स्वर का लोप हो जाता है और तत्पश्चात् ही शेष रूप से रहे हुए हलन्त शब्दों में इस 'एतुल' प्रत्यय की प्राप्ति होती है। जैसे कि:- ( १ ) इयत् = एत्तुलो = इतना । (१) कियत् = केत्तुलो = कितना । (३) यावत्-जेत्तुलो=जितना। ( ४ ) तावत् - तेत्तुलो = उ - उतना और ( ५ ) एतावत् = एत्तुलो-इतना । । ४ - ४३५ ।। त्रस्य डेत्तहे ॥ ४-४३६।।
अपभ्रंशे सर्वादेः सप्तम्यन्तात् परस्य त्र प्रत्ययस्य डेत्तहे इत्यादेशौ भवति ।। एत तेत्त वारि घरि लच्छि निसण्ठुल धाइ ॥
पिअ - पब्भट्ट व गोरडी निच्चल कहिं वि न ठाइ ॥ १ ॥
अर्थः-संस्कृत-भाषा में उपलब्ध सर्वनाम शब्दों में सप्तमी बोधक जो 'त्रप्' प्रत्यय लगता है; उस 'त्रप्' प्रत्यय के स्थान पर अपभ्रंश भाषा में 'डेत्तहे' प्रत्यय की आदेश-प्राप्ति होती है। प्राप्त प्रत्यय 'डेत्तहे' में अवस्थित 'डकारवर्ण' इत्संज्ञावाला है; तदनुसार इस 'डेत्तहे' प्रत्यय की संप्राप्ति होने के पूर्व सर्वनाम शब्दों में स्थित अन्त्य व्यजन का और उपान्त्य स्वर का लोप हो जाता है और तत्पश्चात् ही इस 'डेत्तहे= एत्तेहे' प्रत्यय का संयोग होता है । जैसे:
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org