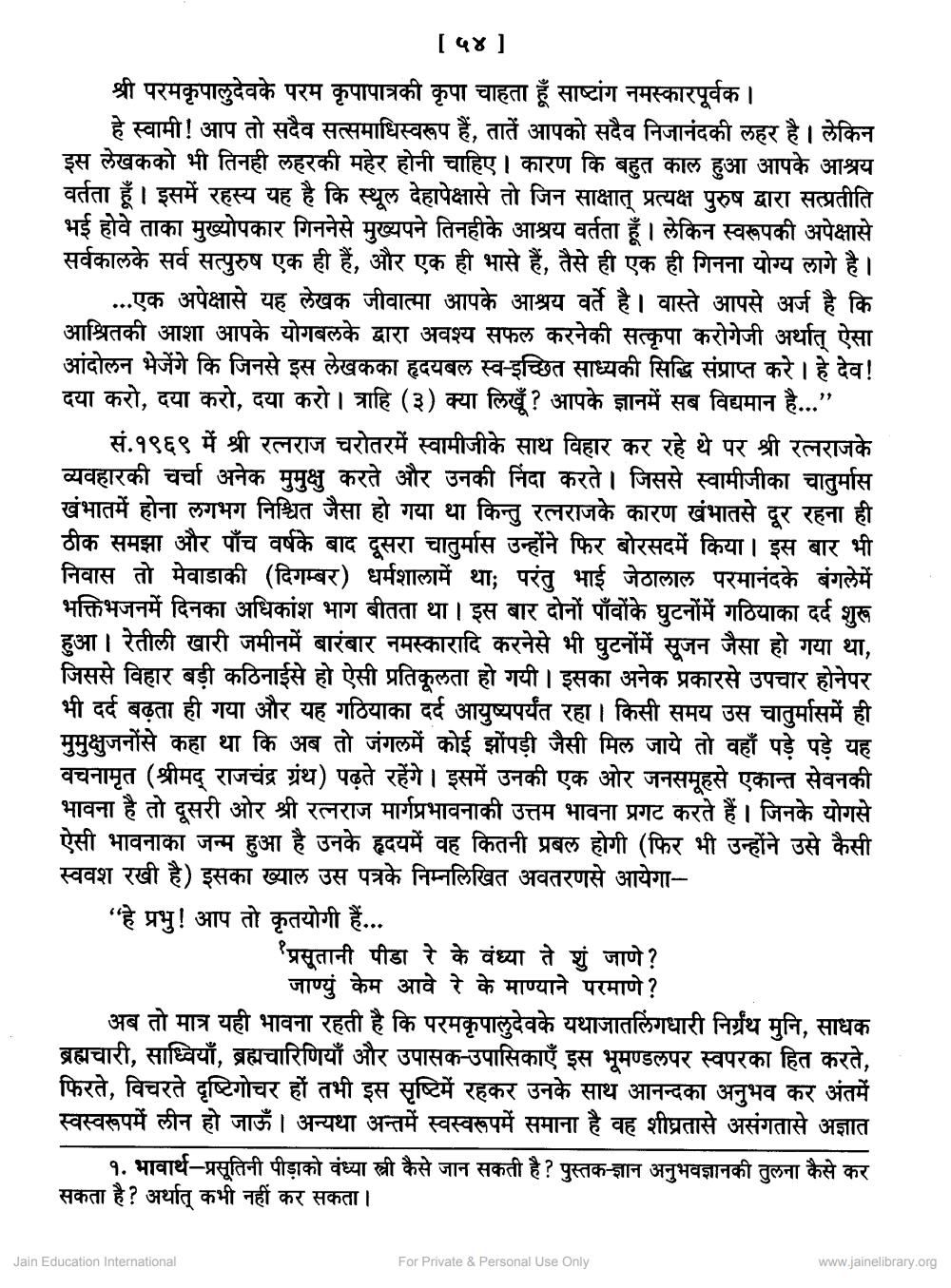________________
[ ५४] श्री परमकृपालुदेवके परम कृपापात्रकी कृपा चाहता हूँ साष्टांग नमस्कारपूर्वक ।
हे स्वामी! आप तो सदैव सत्समाधिस्वरूप हैं, तातें आपको सदैव निजानंदकी लहर है। लेकिन इस लेखकको भी तिनही लहरकी महेर होनी चाहिए। कारण कि बहुत काल हुआ आपके आश्रय वर्तता हूँ। इसमें रहस्य यह है कि स्थूल देहापेक्षासे तो जिन साक्षात् प्रत्यक्ष पुरुष द्वारा सत्प्रतीति भई होवे ताका मुख्योपकार गिननेसे मुख्यपने तिनहीके आश्रय वर्तता हूँ। लेकिन स्वरूपकी अपेक्षासे सर्वकालके सर्व सत्पुरुष एक ही हैं, और एक ही भासे हैं, तैसे ही एक ही गिनना योग्य लागे है।
...एक अपेक्षासे यह लेखक जीवात्मा आपके आश्रय वर्ते है। वास्ते आपसे अर्ज है कि आश्रितकी आशा आपके योगबलके द्वारा अवश्य सफल करनेकी सत्कृपा करोगेजी अर्थात् ऐसा आंदोलन भेजेंगे कि जिनसे इस लेखकका हृदयबल स्व-इच्छित साध्यकी सिद्धि संप्राप्त करे। हे देव! दया करो, दया करो, दया करो। त्राहि (३) क्या लिखू? आपके ज्ञानमें सब विद्यमान है..."
सं.१९६९ में श्री रत्नराज चरोतरमें स्वामीजीके साथ विहार कर रहे थे पर श्री रत्नराजके व्यवहारकी चर्चा अनेक मुमुक्षु करते और उनकी निंदा करते। जिससे स्वामीजीका चातुर्मास खंभातमें होना लगभग निश्चित जैसा हो गया था किन्तु रत्नराजके कारण खंभातसे दूर रहना ही ठीक समझा और पाँच वर्षके बाद दूसरा चातुर्मास उन्होंने फिर बोरसदमें किया। इस बार भी निवास तो मेवाडाकी (दिगम्बर) धर्मशालामें था; परंतु भाई जेठालाल परमानंदके बंगलेमें भक्तिभजनमें दिनका अधिकांश भाग बीतता था। इस बार दोनों पाँवोंके घुटनोंमें गठियाका दर्द शुरू हुआ। रेतीली खारी जमीनमें बारंबार नमस्कारादि करनेसे भी घुटनोंमें सूजन जैसा हो गया था, जिससे विहार बड़ी कठिनाईसे हो ऐसी प्रतिकूलता हो गयी। इसका अनेक प्रकारसे उपचार होनेपर भी दर्द बढ़ता ही गया और यह गठियाका दर्द आयुष्यपर्यंत रहा। किसी समय उस चातुर्मासमें ही मुमुक्षुजनोंसे कहा था कि अब तो जंगलमें कोई झोंपड़ी जैसी मिल जाये तो वहाँ पड़े पड़े यह वचनामृत (श्रीमद् राजचंद्र ग्रंथ) पढ़ते रहेंगे। इसमें उनकी एक ओर जनसमूहसे एकान्त सेवनकी भावना है तो दूसरी ओर श्री रत्नराज मार्गप्रभावनाकी उत्तम भावना प्रगट करते हैं। जिनके योगसे ऐसी भावनाका जन्म हुआ है उनके हृदयमें वह कितनी प्रबल होगी (फिर भी उन्होंने उसे कैसी स्ववश रखी है) इसका ख्याल उस पत्रके निम्नलिखित अवतरणसे आयेगा"हे प्रभु! आप तो कृतयोगी हैं...
'प्रसूतानी पीडा रे के वंध्या ते शुं जाणे?
जाण्यु केम आवे रे के माण्याने परमाणे? अब तो मात्र यही भावना रहती है कि परमकृपालुदेवके यथाजातलिंगधारी निग्रंथ मुनि, साधक ब्रह्मचारी, साध्वियाँ, ब्रह्मचारिणियाँ और उपासक-उपासिकाएँ इस भूमण्डलपर स्वपरका हित करते, फिरते, विचरते दृष्टिगोचर हों तभी इस सृष्टिमें रहकर उनके साथ आनन्दका अनुभव कर अंतमें स्वस्वरूपमें लीन हो जाऊँ । अन्यथा अन्तमें स्वस्वरूपमें समाना है वह शीघ्रतासे असंगतासे अज्ञात
१. भावार्थ-प्रसूतिनी पीडाको वंध्या स्त्री कैसे जान सकती है? पुस्तक ज्ञान अनुभवज्ञानकी तुलना कैसे कर सकता है? अर्थात् कभी नहीं कर सकता।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org