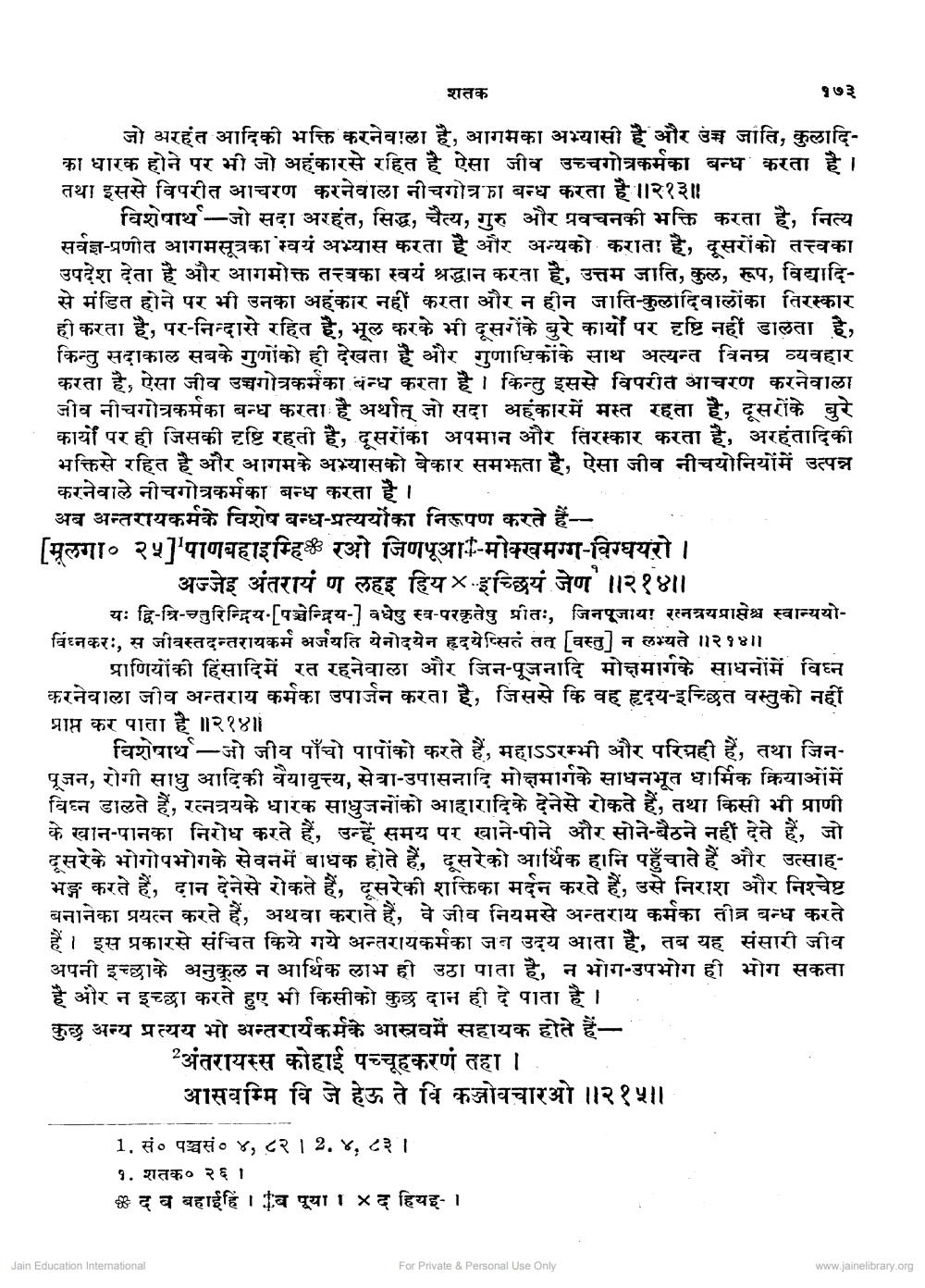________________
शतक
१७३
जो अरहंत आदिकी भक्ति करनेवाला है, आगमका अभ्यासी है और उन जाति, कुलादिका धारक होने पर भी जो अहंकारसे रहित है ऐसा जीव उच्चगोत्रकर्मका बन्ध करता है। तथा इससे विपरीत आचरण करनेवाला नीचगोत्रका बन्ध करता है ।।२१३॥
विशेषार्थ-जो सदा अरहंत, सिद्ध, चैत्य, गुरु और प्रवचनकी भक्ति करता है, नित्य सर्वज्ञ-प्रणीत आगमसूत्रका स्वयं अभ्यास करता है और अन्यको कराता है, दूसरोंको तत्त्वका उपदेश देता है और आगमोक्त तत्त्वका स्वयं श्रद्धान करता है, उत्तम जाति, कुल, रूप, विद्यादिसे मंडित होने पर भी उनका अहंकार नहीं करता और न हीन जाति-कुलादिवालोंका तिरस्कार ही करता है, पर-निन्दासे रहित है, भूल करके भी दूसरोंके बुरे कार्यों पर दृष्टि नहीं डालता है, किन्तु सदाकाल सबके गुणोंको ही देखता है और गुणाधिकोंके साथ अत्यन्त विनम्र व्यवहार करता है, ऐसा जीव उच्चगोत्रकर्मका बन्ध करता है। किन्तु इससे विपरीत आचरण करनेवाला जीव नीचगोत्रकर्मका बन्ध करता है अर्थात् जो सदा अहंकारमें मस्त रहता है, दूसरोंके बुरे कार्यों पर ही जिसकी दृष्टि रहती है, दूसरोका अपमान और तिरस्कार करता है, अरहतादिका भक्तिसे रहित है और आगमके अभ्यासको बेकार समझता है, ऐसा जीव नीचयोनियोंमें उत्पन्न करनेवाले नीचगोत्रकर्मका बन्ध करता है। अब अन्तरायकर्मके विशेष बन्ध-प्रत्ययोंका निरूपण करते हैं[मूलगा० २५] पाणबहाइम्हि के रओ जिणपूआ:-मोक्खमग्ग-विग्धयरो।
अज्जेइ अंतरायं ण लहइ हियx.इच्छियं जेण ॥२१४॥ यः द्वि-त्रि-चतुरिन्द्रिय [पञ्चेन्द्रिय-] वधेषु स्व-परकृतेषु प्रीतः, जिनपूजाया रत्नत्रयप्राप्तेश्च स्वान्ययोविघ्नकरः, स जीवस्तदन्तरायकर्म अर्जयति येनोदयेन हृदयेप्सितं तत् विस्तु न लभ्यते ॥२१४॥
प्राणियोंकी हिंसादिमें रत रहनेवाला और जिन-पूजनादि मोक्षमार्गके साधनोंमें विघ्न करनेवाला जीव अन्तराय कर्मका उपार्जन करता है, जिससे कि वह हृदय-इच्छित वस्तुको नहीं प्राप्त कर पाता है ॥२१४॥
विशेषार्थ-जो जीव पाँचो पापोंको करते हैं, महाऽऽरम्भी और परिग्रही हैं, तथा जिनपूजन, रोगी साधु आदिकी वैयावृत्त्य, सेवा-उपासनादि मोक्षमार्गके साधनभूत धार्मिक क्रियाओंमें विघ्न डालते हैं, रत्नत्रयके धारक साधुजनोंको आहारादिके देनेसे रोकते हैं, तथा किसी भी प्राणी के खान-पानका निरोध करते हैं, उन्हें समय पर खाने-पीने और सोने-बैठने नहीं देते हैं, जो दूसरेके भोगोपभोगके सेवनमें बाधक होते हैं, दूसरेको आर्थिक हानि पहुंचाते हैं और उत्साहभङ्ग करते हैं, दान देनेसे रोकते हैं, दूसरेकी शक्तिका मर्दन करते हैं, उसे निराश और निश्चेष्ट बनानेका प्रयत्न करते हैं, अथवा कराते हैं, वे जीव नियमसे अन्तराय कर्मका तीव्र बन्ध करते हैं। इस प्रकारसे संचित किये गये अन्तरायकर्मका जन उदय आता है, तब यह संसारी जीव अपनी इच्छाके अनुकूल न आर्थिक लाभ हो उठा पाता है, न भोग-उपभोग ही भोग सकता है और न इच्छा करते हुए भी किसीको कुछ दान ही दे पाता है। . कुछ अन्य प्रत्यय भो अन्तरार्यकर्मके आस्रवमें सहायक होते हैं
अंतरायस्स कोहाई पच्चूहकरणं तहा । आसवम्मि वि जे हेऊ ते वि कजोवचारओ ॥२१॥
1. सं० पञ्चसं० ४, ८२ | 2. ४, ८३ । १. शतक० २६ ।
दब बहाईहिं । ब पूया । द हियइ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org