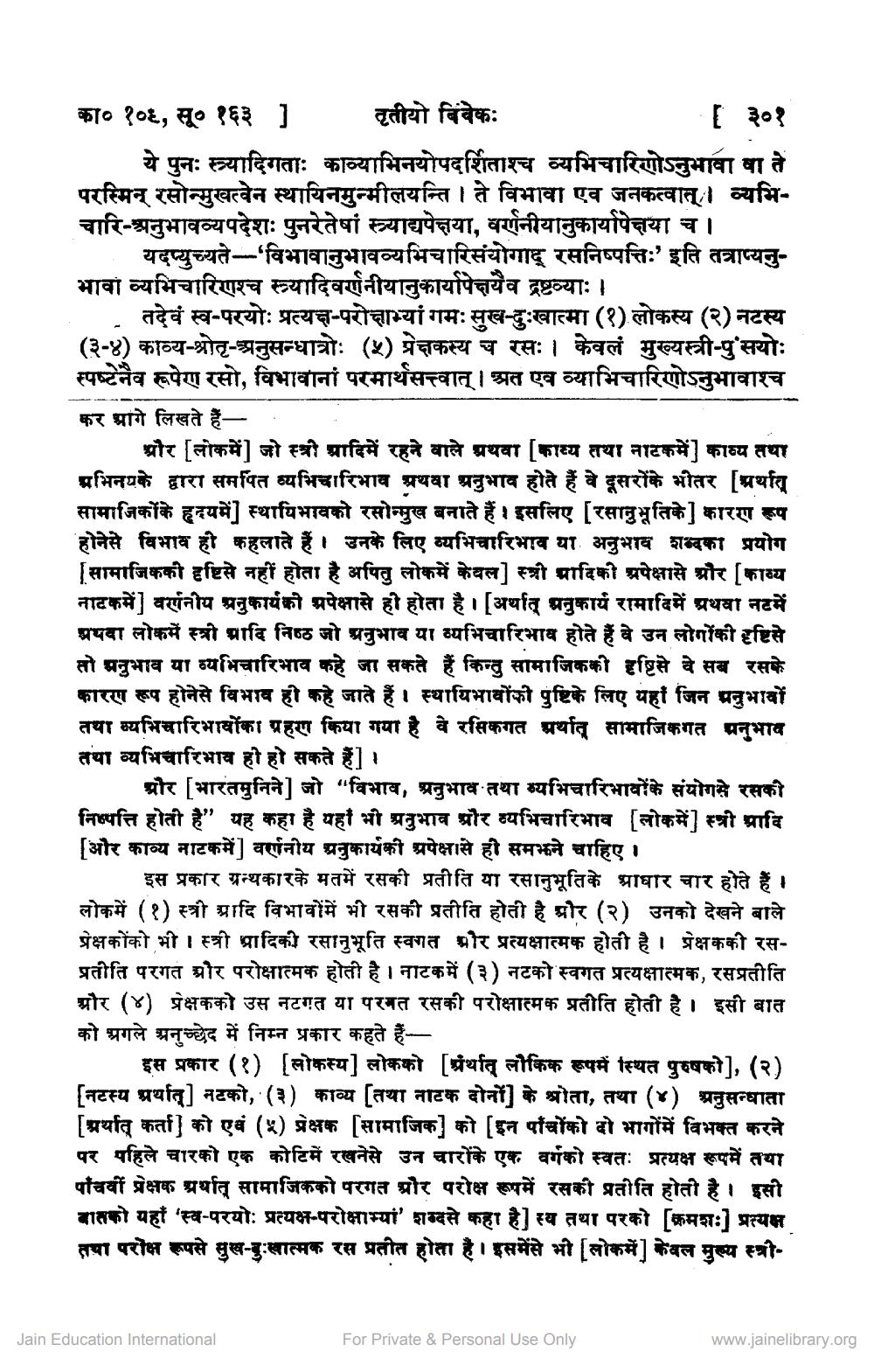________________
का० १०६, सू० १६३ ] तृतीयो विवेकः
[ ३०१ ये पुनः स्त्र्यादिगताः काव्याभिनयोपदर्शिताश्च व्यभिचारिणोऽनुभावा वा ते परस्मिन् रसोन्मुखत्वेन स्थायिनमुन्मीलयन्ति । ते विभावा एव जनकत्वात्। व्यमिचारि-अनुभावव्यपदेशः पुनरेतेषां स्त्याद्यपेक्षया, वर्णनीयानुकार्यापेक्षया च ।
. यदप्युच्यते-'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद् रसनिष्पत्तिः' इति तत्राप्यनुभावा व्यभिचारिणश्च त्यादिवर्णनीयानुकार्यापेक्षयैव द्रष्टव्याः।
.. तदेवं स्व-परयोः प्रत्यक्ष-परोक्षाभ्यांगमः सुख-दुःखात्मा (१) लोकस्य (२) नटस्य (३-४) काव्य-श्रोतृ-अनुसन्धात्रोः (५) प्रेक्षकस्य च रसः। केवलं मुख्यस्त्री-पुसयोः स्पष्टेनैव रूपेण रसो, विभावानां परमार्थसत्त्वात् । अत एव व्याभिचारिणोऽनुभावाश्च कर आगे लिखते हैं
और [लोकमें] जो स्त्री प्रादिमें रहने वाले अथवा [काव्य तथा नाटकमें] काव्य तथा अभिनयके द्वारा समर्पित व्यभिचारिभाव अथवा अनुभाव होते हैं वे दूसरोंके भीतर [अर्थात् सामाजिकोंके हृदयमें] स्थायिभावको रसोन्मुख बनाते हैं। इसलिए [रसानुभूतिके] कारण रूप होनेसे विभाव ही कहलाते हैं। उनके लिए व्यभिचारिभाव या अनुभाव शब्दका प्रयोग [सामाजिकको दृष्टिसे नहीं होता है अपितु लोकमें केवल स्त्री प्रादिको अपेक्षासे और [काव्य नाटकमें] वर्णनीय अनुकार्यको अपेक्षासे ही होता है । [अर्थात् अनुकार्य रामादिमें अथवा नटमें अथवा लोकमें स्त्री प्रादि निष्ठ जो अनुभाव या व्यभिचारिभाव होते हैं वे उन लोगोंकी दृष्टिसे तो अनुभाव या व्यभिचारिभाव कहे जा सकते हैं किन्तु सामाजिककी दृष्टिसे वे सब रसके कारण रूप होनेसे विभाव ही कहे जाते हैं। स्थायिभावोंकी पुष्टि के लिए यहां जिन अनुभावों तथा व्यभिचारिभावोंका ग्रहण किया गया है वे रसिकगत अर्थात् सामाजिकगत अनुभाव तथा व्यभिचारिभाव हो हो सकते हैं।
और [भारतमुनिने] जो "विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारिभावोंके संयोगसे रसकी निष्पत्ति होती है" यह कहा है यहाँ भी अनुभाव और व्यभिचारिभाव [लोकमें] स्त्री प्रादि [और काव्य नाटकमें] वर्णनीय अनुकार्यकी अपेक्षासे ही समझने चाहिए।
इस प्रकार ग्रन्थकारके मतमें रसकी प्रतीति या रसानुभूतिके आधार चार होते हैं । लोकमें (१) स्त्री आदि विभावोंमें भी रसकी प्रतीति होती है और (२) उनको देखने बाले प्रेक्षकोंको भी । स्त्री प्रादिकी रसानुभूति स्वगत और प्रत्यक्षात्मक होती है। प्रेक्षककी रसप्रतीति परगत और परोक्षात्मक होती है । नाटक में (३) नटको स्वगत प्रत्यक्षात्मक, रसप्रतीति और (४) प्रेक्षकको उस नटगत या परमत रसकी परोक्षात्मक प्रतीति होती है। इसी बात को अगले अनुच्छेद में निम्न प्रकार कहते हैं
इस प्रकार (१) [लोकस्य] लोकको [अंर्थात् लौकिक रूपमें स्थित पुरुषको], (२) [नटस्य अर्थात् नटको, (३) काव्य [तथा नाटक दोनों के श्रोता, तथा (४) अनुसन्धाता [अर्थात् कर्ता] को एवं (५) प्रेक्षक [सामाजिक को [इन पांचोंको दो भागोंमें विभक्त करने पर पहिले चारको एक कोटिमें रखनेसे उन चारोंके एक वर्गको स्वतः प्रत्यक्ष रूपमें तथा पांचवीं प्रेक्षक अर्थात् सामाजिकको परगत और परोक्ष रूपमें रसकी प्रतीति होती है। इसी बातको यहाँ 'स्व-परयोः प्रत्यक्ष-परोक्षाम्यां' शम्दसे कहा है] स्व तथा परको [क्रमशः] प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपसे सुख-दुःखात्मक रस प्रतीत होता है । इसमेंसे भी [लोकमें केवल मुख्य स्त्री
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org