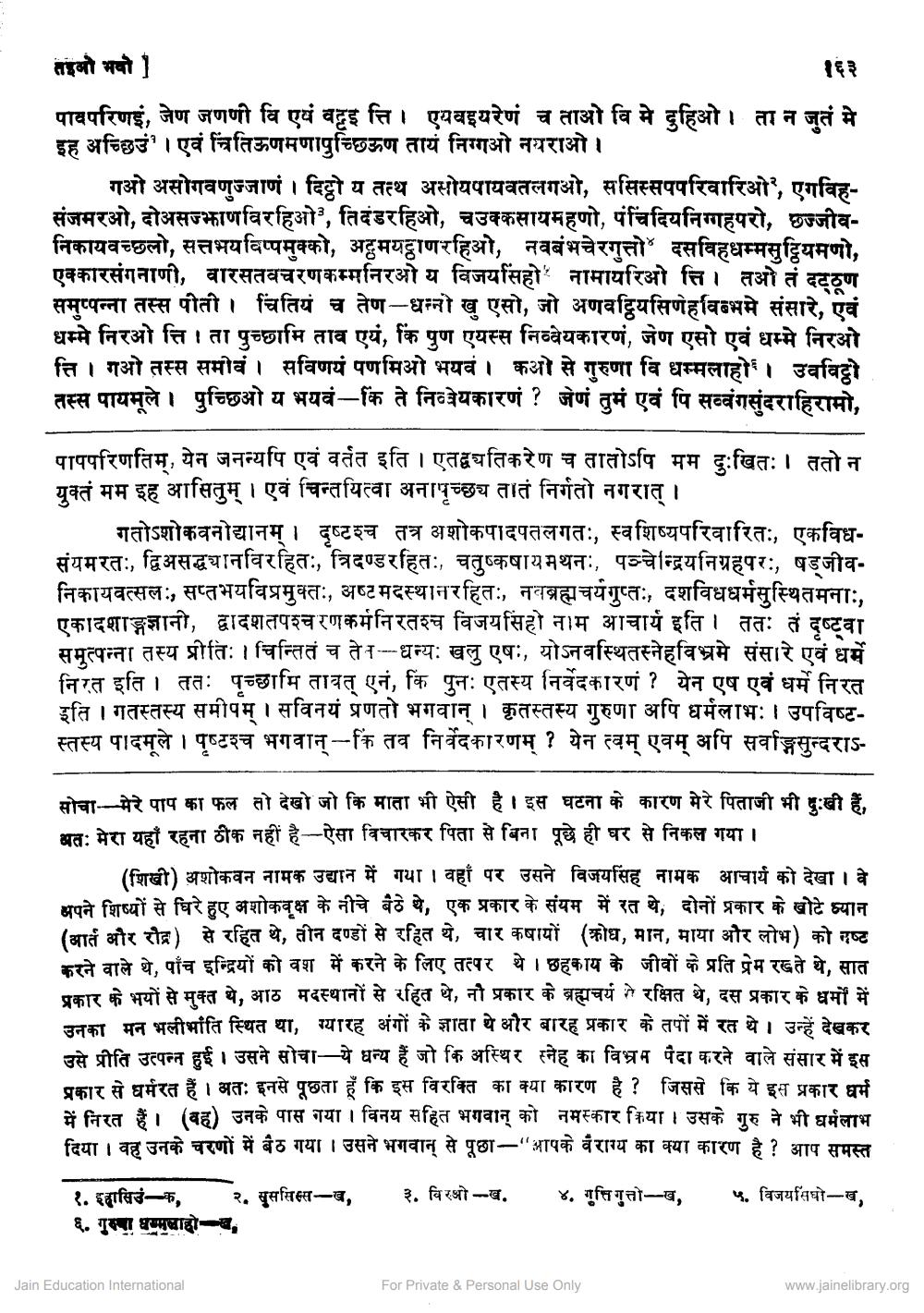________________
तमो भवो ]
१६३
पाव परिणई, जेण जणणी वि एवं वइति । एयवइयरेणं च ताओ वि मे दुहिओ । ता न जुतं मे इह अच्छिउं । एवं चितिऊणमणापुच्छिऊण तायं निग्गओ नयराओ ।
असोज्जा । दिट्ठो य तत्थ असोयपायवतलगओ, ससिस्सपपरिवारिओ, एगविहसंजमरओ, दोअसज्भाणविरहिओ', तिदंडरहिओ, चउक्कसाय महणो, पंचिदियनिग्गहपरो, छज्जीवनिकायवच्छलो, सत्तभयविष्पमुक्को, अट्टमयट्ठाणरहिओ, नवबंभचेरगुत्तो' दसविहधम्मसुट्टियमणो, एक्कारसंग नाणी, वारसतवचरणकम्मनिरओ य विजयसिंहो नामायरिओ त्ति । तओ तं दट्ठूण समुपपन्ना तस्स पीती । चितियं च तेण -धन्नो खु एसो, जो अणवट्टियसिणेहविभमे संसारे, एवं धम्मेरिओति । ता पुच्छामि ताव एयं किं पुण एयस्स निव्वेयकारणं, जेण एसो एवं धम्मे निरओ त्ति । गओ तस्स समोवं । सविणयं पणमिओ भयवं । कओ से गुरुणा वि धम्मलाहो । उवविट्ठो तस्स पायमूले । पुच्छिओ य भयवं - किं ते निव्वेयकारणं ? जेणं तुमं एवं पि सव्वंगसुंदरा हिरामो,
पापपरिणतिम्, येन जनन्यपि एवं वर्तत इति । एतद्वयतिकरेण च तातोऽपि मम दुःखितः । ततो न युक्तं मम इह आसितुम् । एवं चिन्तयित्वा अनापृच्छ्य तातं निर्गतो नगरात् ।
गतोऽशोकवनोद्यानम् । दृष्टश्च तत्र अशोकपादपतलगतः, स्वशिष्यपरिवारितः, एकविध - संयमरतः, द्विअसद्ध्यानविरहितः, त्रिदण्डरहितः, चतुष्कषायमथनः, पञ्चेन्द्रियनिग्रहपरः, षड्जीवनिकायवत्सलः, सप्तभयविप्रमुक्तः, अष्टमदस्थानरहितः, नवब्रह्मचर्यगुप्तः, दशविधधर्म सुस्थितमनाः, एकादशाङ्गज्ञानी, द्वादशतपश्च रणकर्मनिरतश्च विजयसिंहो नाम आचार्य इति । ततः तं दृष्ट्वा समुत्पन्ना तस्य प्रीतिः । चिन्तितं च तेन-धन्यः खलु एषः, योऽनवस्थितस्नेहविभ्रमे संसारे एवं धर्मे निरत इति । ततः पृच्छामि तावत् एनं किं पुनः एतस्य निर्वेदकारणं ? येन एष एवं धर्मे निरत इति । गतस्तस्य समीपम् । सविनयं प्रणतो भगवान् । कृतस्तस्य गुरुणा अपि धर्मलाभः । उपविष्टस्तस्य पादमूले । पृष्टश्च भगवान् - किं तव निर्वेदकारणम् ? येन त्वम् एवम् अपि सर्वाङ्गसुन्दराऽ
सोचा- मेरे पाप का फल तो देखो जो कि माता भी ऐसी है । इस घटना के कारण मेरे पिताजी भी दुःखी हैं, अतः मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है-ऐसा विचारकर पिता से बिना पूछे ही घर से निकल गया ।
(शिखी) अशोकवन नामक उद्यान में गया । वहाँ पर उसने विजयसिंह नामक आचार्य को देखा । वे अपने शिष्यों से घिरे हुए अशोकवृक्ष के नीचे बैठे थे, एक प्रकार के संयम में रत थे, दोनों प्रकार के खोटे ध्यान (आर्त और रौद्र) से रहित थे, तीन दण्डों से रहित थे, चार कषायों ( क्रोध, मान, माया और लोभ) को ग्रष्ट करने वाले थे, पाँच इन्द्रियों को वश में करने के लिए तत्पर थे। छहकाय के जीवों के प्रति प्रेम रखते थे, त प्रकार के भयों से मुक्त थे, आठ मदस्थानों से रहित थे, नौ प्रकार के ब्रह्मचर्य से रक्षित थे, दस प्रकार के धर्मों में उनका मन भलीभांति स्थित था, ग्यारह अंगों के ज्ञाता थे और बारह प्रकार के तपों में रत थे । उन्हें देखकर उसे प्रीति उत्पन्न हुई । उसने सोचा-ये धन्य हैं जो कि अस्थिर स्नेह का विभ्रम प्रकार से धर्मरत हैं । अतः इनसे पूछता हूँ कि इस विरक्ति का क्या कारण है ? जिससे कि ये इस प्रकार धर्म में निरत हैं । ( वह) उनके पास गया । विनय सहित भगवान् को नमस्कार किया। उसके गुरु ने भी धर्मलाभ दिया । वह उनके चरणों में बैठ गया । उसने भगवान् से पूछा - " आपके वैराग्य का क्या कारण है ? आप समस्त
पैदा करने वाले संसार में इस
२. सुससिस - ख
३. विस्श्रो -- ख.
४. गुप्तिगुत्तो-ख
५. विजयसिंघ - ख,
१. इहासिक, ६. गुरुचा धम्मलाहो'
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org