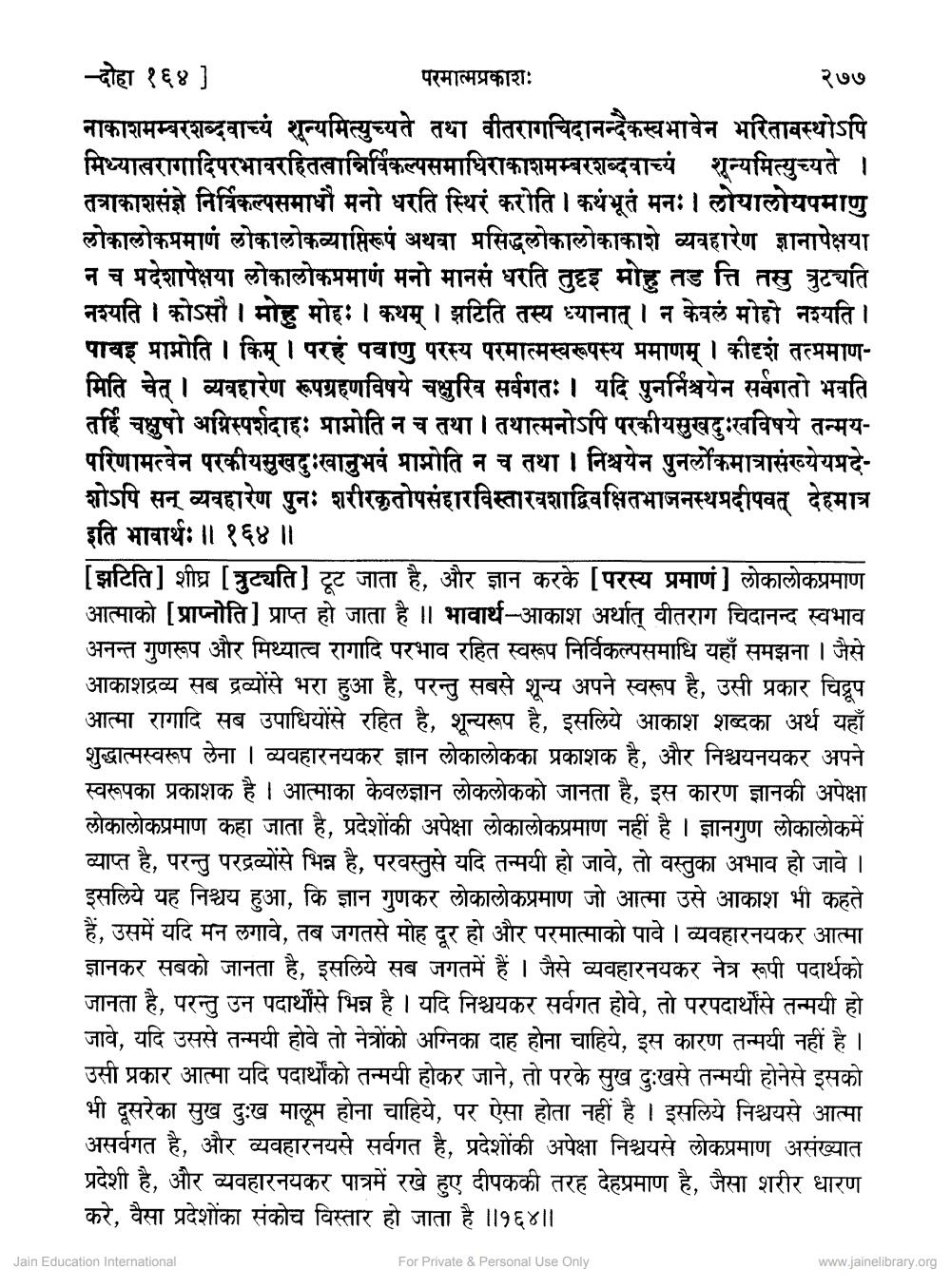________________
-दोहा १६४ ] परमात्मप्रकाशः
२७७ नाकाशमम्बरशब्दवाच्यं शून्यमित्युच्यते तथा वीतरागचिदानन्दैकस्वभावेन भरितावस्थोऽपि मिथ्यावरागादिपरभावरहितसानिर्विकल्पसमाधिराकाशमम्बरशब्दवाच्यं शून्यमित्युच्यते । तत्राकाशसंज्ञे निर्विकल्पसमाधौ मनो धरति स्थिरं करोति । कथंभूतं मनः । लोयालोयपमाणु लोकालोकप्रमाणं लोकालोकव्याप्तिरूपं अथवा प्रसिद्धलोकालोकाकाशे व्यवहारेण ज्ञानापेक्षया न च प्रदेशापेक्षया लोकालोकममाणं मनो मानसं धरति तुदृइ मोहु तड त्ति तसु त्रुटयति नश्यति । कोऽसौ । मोहु मोहः । कथम् । झटिति तस्य ध्यानात् । न केवलं मोहो नश्यति । पावइ प्रामोति । किम् । परहं पवाणु परस्य परमात्मस्वरूपस्य प्रमाणम् । कीदृशं तत्प्रमाणमिति चेत् । व्यवहारेण रूपग्रहणविषये चक्षुरिव सर्वगतः। यदि पुननिश्चयेन सर्वगतो भवति तर्हि चक्षुषो अग्निस्पर्शदाहः प्रामोति न च तथा । तथात्मनोऽपि परकीयसुखदुःखविषये तन्मयपरिणामत्वेन परकीयसुखदुःखानुभवं प्राप्नोति न च तथा । निश्चयेन पुनर्लोकमात्रासंख्येयप्रदेशोऽपि सन् व्यवहारेण पुनः शरीरकृतोपसंहारविस्तारवशाद्विवक्षितभाजनस्थप्रदीपवत् देहमात्र इति भावार्थः॥ १६४॥ [झटिति] शीघ्र [त्रुट्यति] टूट जाता है, और ज्ञान करके [परस्य प्रमाणं] लोकालोकप्रमाण आत्माको [प्राप्नोति] प्राप्त हो जाता है ।। भावार्थ-आकाश अर्थात् वीतराग चिदानन्द स्वभाव अनन्त गुणरूप और मिथ्यात्व रागादि परभाव रहित स्वरूप निर्विकल्पसमाधि यहाँ समझना । जैसे आकाशद्रव्य सब द्रव्योंसे भरा हुआ है, परन्तु सबसे शून्य अपने स्वरूप है, उसी प्रकार चिद्रूप आत्मा रागादि सब उपाधियोंसे रहित है, शून्यरूप है, इसलिये आकाश शब्दका अर्थ यहाँ शुद्धात्मस्वरूप लेना । व्यवहारनयकर ज्ञान लोकालोकका प्रकाशक है, और निश्चयनयकर अपने स्वरूपका प्रकाशक है । आत्माका केवलज्ञान लोकलोकको जानता है, इस कारण ज्ञानकी अपेक्षा लोकालोकप्रमाण कहा जाता है, प्रदेशोंकी अपेक्षा लोकालोकप्रमाण नहीं है । ज्ञानगुण लोकालोकमें व्याप्त है, परन्तु परद्रव्योंसे भिन्न है, परवस्तुसे यदि तन्मयी हो जावे, तो वस्तुका अभाव हो जावे । इसलिये यह निश्चय हुआ, कि ज्ञान गुणकर लोकालोकप्रमाण जो आत्मा उसे आकाश भी कहते हैं, उसमें यदि मन लगावे, तब जगतसे मोह दूर हो और परमात्माको पावे । व्यवहारनयकर आत्मा ज्ञानकर सबको जानता है, इसलिये सब जगतमें हैं । जैसे व्यवहारनयकर नेत्र रूपी पदार्थको जानता है, परन्तु उन पदार्थोंसे भिन्न है । यदि निश्चयकर सर्वगत होवे, तो परपदार्थोंसे तन्मयी हो जावे, यदि उससे तन्मयी होवे तो नेत्रोंको अग्निका दाह होना चाहिये, इस कारण तन्मयी नहीं है । उसी प्रकार आत्मा यदि पदार्थोंको तन्मयी होकर जाने, तो परके सुख दुःखसे तन्मयी होनेसे इसको भी दूसरेका सुख दुःख मालूम होना चाहिये, पर ऐसा होता नहीं है । इसलिये निश्चयसे आत्मा असर्वगत है, और व्यवहारनयसे सर्वगत है, प्रदेशोंकी अपेक्षा निश्चयसे लोकप्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, और व्यवहारनयकर पात्रमें रखे हुए दीपककी तरह देहप्रमाण है, जैसा शरीर धारण करे, वैसा प्रदेशोंका संकोच विस्तार हो जाता है ।।१६४।।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org