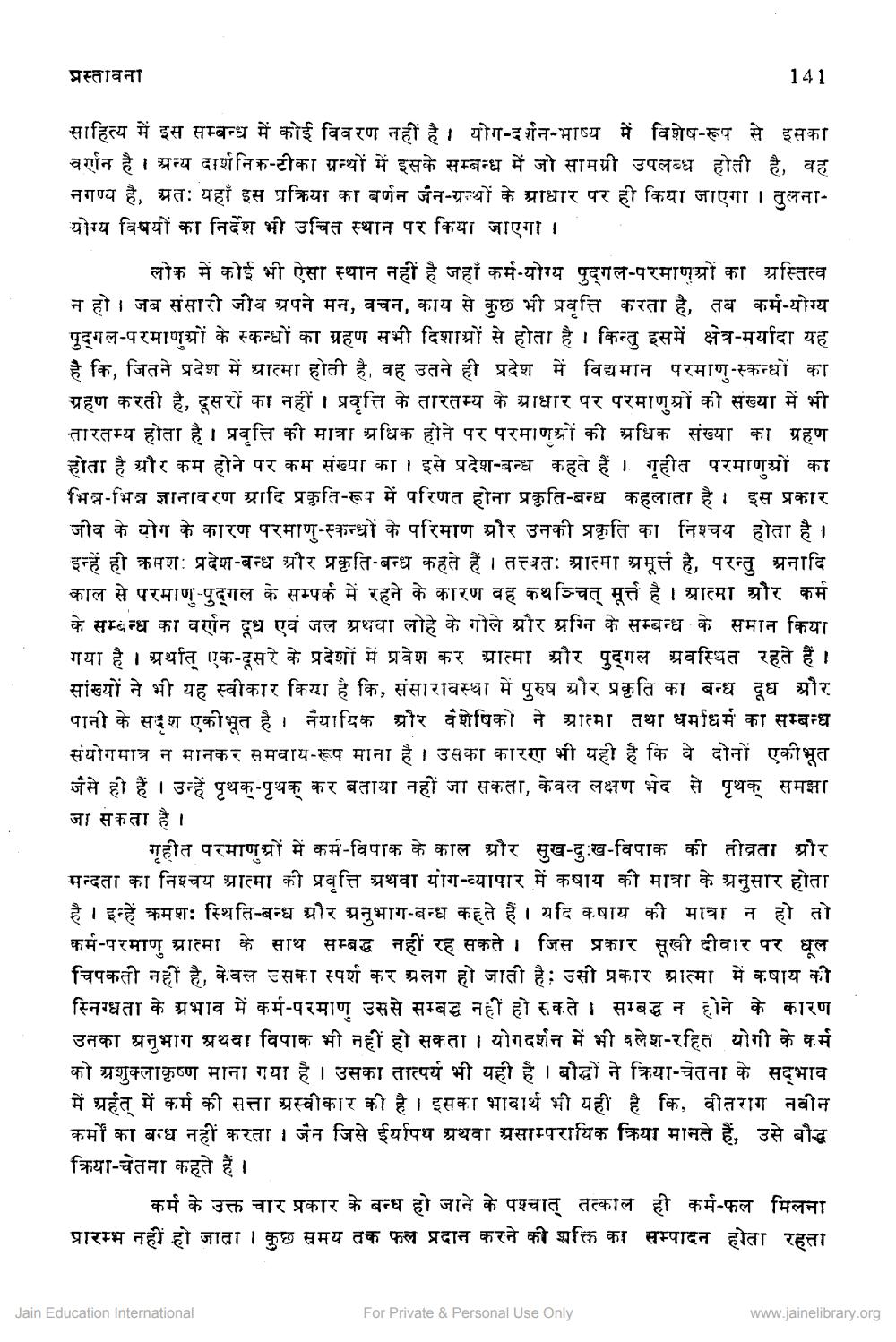________________
प्रस्तावना
141
साहित्य में इस सम्बन्ध में कोई विवरण नहीं है। योग-दर्शन-भाष्य में विशेष-रूप से इसका वर्णन है । अन्य दार्शनिक-टीका ग्रन्थों में इसके सम्बन्ध में जो सामग्री उपलब्ध होती है, वह नगण्य है, अतः यहाँ इस प्रक्रिया का वर्णन जन-ग्रन्थों के अाधार पर ही किया जाएगा । तुलनायोग्य विषयों का निर्देश भी उचित स्थान पर किया जाएगा।
लोक में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कर्म-योग्य पुद्गल-परमाणों का अस्तित्व न हो। जब संसारी जीव अपने मन, वचन, काय से कुछ भी प्रवृत्ति करता है, तब कर्म-योग्य पुदगल-परमाणों के स्कन्धों का ग्रहण सभी दिशानों से होता है। किन्तु इसमें क्षेत्र-मर्यादा यह है कि, जितने प्रदेश में प्रात्मा होती है, वह उतने ही प्रदेश में विद्यमान परमाणु-स्कन्धों का ग्रहण करती है, दूसरों का नहीं। प्रवत्ति के तारतम्य के प्राधार पर परमाणों की संख्या में भी तारतम्य होता है। प्रवृत्ति की मात्रा अधिक होने पर परमाणुओं की अधिक संख्या का ग्रहण होता है और कम होने पर कम संख्या का। इसे प्रदेश-बन्ध कहते हैं । गृहीत परमाणुओं का भिन्न-भिन्न ज्ञानावरण प्रादि प्रकृति-रूप में परिणत होना प्रकृति-बन्ध कहलाता है। इस प्रकार जीव के योग के कारण परमाणु-स्कन्धों के परिमाण और उनकी प्रकृति का निश्चय होता है । इन्हें ही क्रमशः प्रदेश-बन्ध और प्रकृति-बन्ध कहते हैं । तत्त्वतः आत्मा अमूर्त है, परन्तु अनादि काल से परमाणु-पुद्गल के सम्पर्क में रहने के कारण वह कथञ्चित् मूर्त है । आत्मा और कर्म के सम्बन्ध का वर्णन दूध एवं जल अथवा लोहे के गोले और अग्नि के सम्बन्ध के समान किया गया है । अर्थात् एक-दूसरे के प्रदेशों में प्रवेश कर आत्मा और पुद्गल अवस्थित रहते हैं। सांख्यों ने भी यह स्वीकार किया है कि, संसारावस्था में पुरुष और प्रकृति का बन्ध दूध और पानी के सदश एकीभूत है। नैयायिक और वैशेषिकों ने प्रात्मा तथा धर्माधर्म का सम्बन्ध संयोगमात्र न मानक र समवाय-रूप माना है। उसका कारण भी यही है कि वे दोनों एकीभूत जैसे ही हैं । उन्हें पृथक्-पृथक् कर बताया नहीं जा सकता, केवल लक्षण भेद से पृथक् समझा जा सकता है।
गृहीत परमाणुनों में कम-विपाक के काल और सुख-दुःख-विपाक की तीव्रता और मन्दता का निश्चय आत्मा की प्रवत्ति अथवा योग-व्यापार में कषाय की मात्रा के अनुसार होता है । इन्हें क्रमशः स्थिति-बन्ध और अनुभाग-बन्ध कहते हैं। यदि कषाय की मात्रा न हो तो कर्म-परमाणु आत्मा के साथ सम्बद्ध नहीं रह सकते । जिस प्रकार सूखी दीवार पर धूल चिपकती नहीं है, केवल उसका स्पर्श कर अलग हो जाती है : उसी प्रकार प्रात्मा में कषाय की स्निग्धता के अभाव में कर्म-परमाणु उससे सम्बद्ध नहीं हो सकते । सम्बद्ध न होने के कारण उनका अनुभाग अथवा विपाक भी नहीं हो सकता । योगदर्शन में भी क्लेश-रहित योगी के कर्म को अशुक्लाकृष्ण माना गया है । उसका तात्पर्य भी यही है । बौद्धों ने क्रिया-चेतना के सद्भाव में अर्हत् में कर्म की सत्ता अस्वीकार की है । इसका भावार्थ भी यही है कि, वीतराग नवीन कर्मों का बन्ध नहीं करता । जैन जिसे ईर्यापथ अथवा असाम्परायिक क्रिया मानते हैं, उसे बौद्ध क्रिया-चेतना कहते हैं।
___कर्म के उक्त चार प्रकार के बन्ध हो जाने के पश्चात् तत्काल ही कर्म-फल मिलना प्रारम्भ नहीं हो जाता। कुछ समय तक फल प्रदान करने की शक्ति का सम्पादन होता रहता
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org