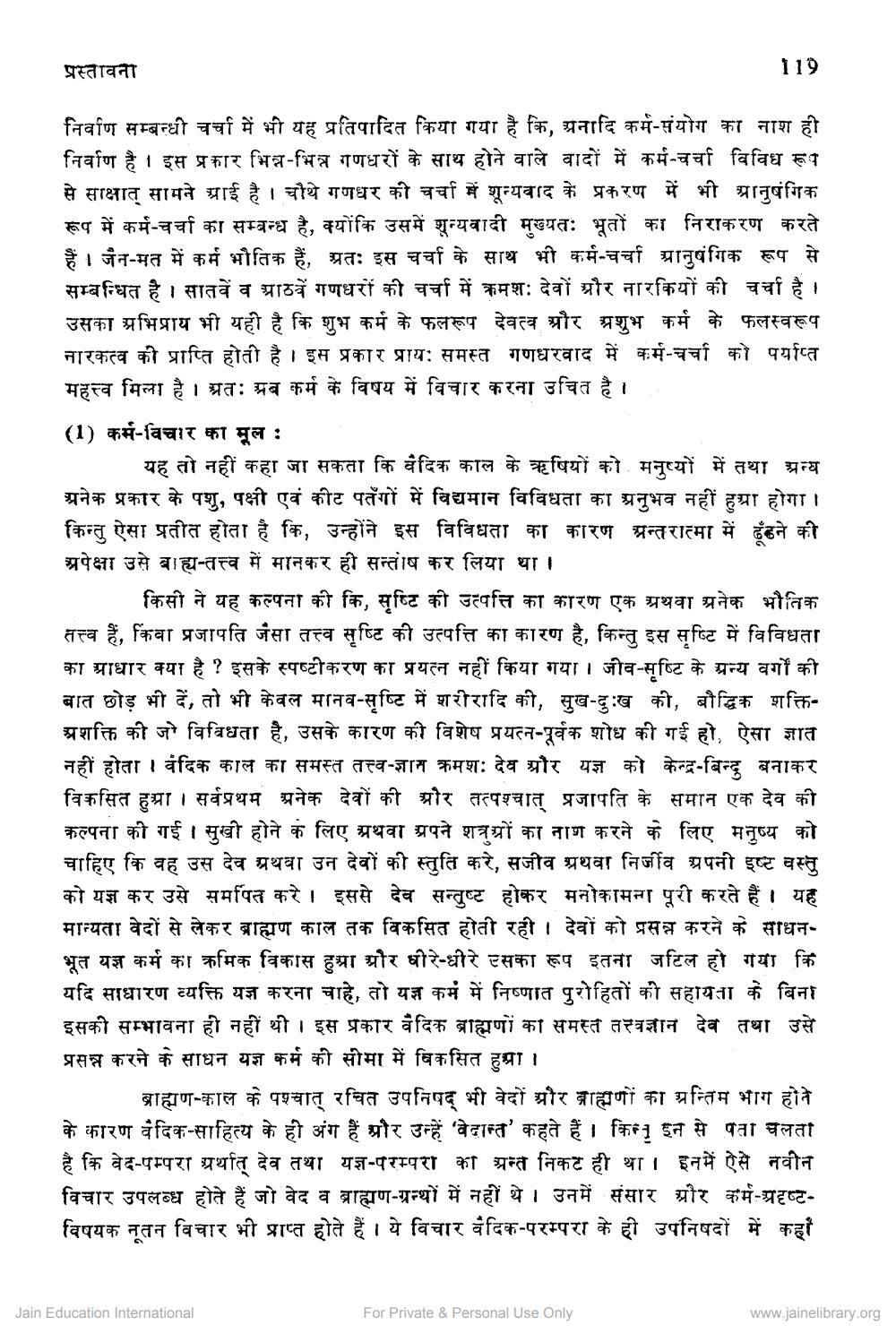________________
प्रस्तावना
119
निर्वाण सम्बन्धी चर्चा में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि, अनादि कर्म-संयोग का नाश ही निर्वाण है । इस प्रकार भिन्न-भिन्न गणधरों के साथ होने वाले वादों में कर्म-चर्चा विविध रूप से साक्षात् सामने आई है । चौथे गणधर की चर्चा में शून्यवाद के प्रकरण में भी आनुषंगिक रूप में कर्म-चर्चा का सम्बन्ध है, क्योंकि उसमें शून्यवादी मुख्यतः भूतों का निराकरण करते हैं । जैन-मत में कर्म भौतिक हैं, अतः इस चर्चा के साथ भी कर्म-चर्चा पानुषंगिक रूप से सम्बन्धित है । सातवें व आठवें गणधरों की चर्चा में क्रमश: देवों और नारकियों की चर्चा है । उसका अभिप्राय भी यही है कि शुभ कर्म के फलरूप देवत्व और अशुभ कर्म के फलस्वरूप नारकत्व की प्राप्ति होती है। इस प्रकार प्रायः समस्त गणधरवाद में कर्म-चर्चा को पर्याप्त महत्त्व मिला है। अतः अब कर्म के विषय में विचार करना उचित है। (1) कर्म-विचार का मूल :
___ यह तो नहीं कहा जा सकता कि वैदिक काल के ऋषियों को मनुष्यों में तथा अन्य अनेक प्रकार के पशु, पक्षी एवं कीट पतंगों में विद्यमान विविधता का अनुभव नहीं हुअा होगा। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि, उन्होंने इस विविधता का कारण अन्तरात्मा में ढूंढने की अपेक्षा उसे बाह्य-तत्त्व में मानकर ही सन्तोष कर लिया था।
किसी ने यह कल्पना की कि, सृष्टि की उत्पत्ति का कारण एक अथवा अनेक भौतिक तत्त्व हैं, किंवा प्रजापति जसा तत्त्व सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है, किन्तु इस सृष्टि में विविधता का आधार क्या है ? इसके स्पष्टीकरण का प्रयत्न नहीं किया गया। जीव-सष्टि के अन्य वर्गों की बात छोड़ भी दें, तो भी केवल मानव-सृष्टि में शरीरादि की, सुख-दुःख की, बौद्धिक शक्तिअशक्ति की जो विविधता है, उसके कारण की विशेष प्रयत्न-पूर्वक शोध की गई हो, ऐसा ज्ञात नहीं होता । वंदिक काल का समस्त तत्त्व-ज्ञान क्रमशः देव और यज्ञ को केन्द्रबिन्दु बनाकर विकसित हुआ । सर्वप्रथम अनेक देवों की और तत्पश्चात् प्रजापति के समान एक देव की कल्पना की
की गई। सुखी होने के लिए अथवा अपने शत्रों का नाश करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह उस देव अथवा उन देवों की स्तुति करे, सजीव अथवा निर्जीव अपनी इष्ट वस्तु को यज्ञ कर उसे समपित करे। इससे देव सन्तुष्ट होकर मनोकामना पूरी करते हैं। यह मान्यता वेदों से लेकर ब्राह्मण काल तक विकसित होती रही । देवों को प्रसन्न करने के साधनभूत यज्ञ कर्म का क्रमिक विकास हुआ और धीरे-धीरे उसका रूप इतना जटिल हो गया कि यदि साधारण व्यक्ति यज्ञ करना चाहे, तो यज्ञ कर्म में निष्णात पुरोहितों की सहायता के बिना इसकी सम्भावना ही नहीं थी। इस प्रकार वैदिक ब्राह्मणों का समस्त तत्त्वज्ञान देव तथा उसे प्रसन्न करने के साधन यज्ञ कर्म की सीमा में विकसित हुमा।
ब्राह्मण-काल के पश्चात् रचित उपनिषद् भी वेदों और ब्राह्मणों का अन्तिम भाग होने के कारण वैदिक-साहित्य के ही अंग हैं और उन्हें 'वेदान्त' कहते हैं। किन्तु इन से पता चलता है कि वेद-पम्परा अर्थात् देव तथा यज्ञ-परम्परा का अन्त निकट ही था। इनमें ऐसे नवीन विचार उपलब्ध होते हैं जो वेद व ब्राह्मण-ग्रन्थों में नहीं थे। उनमें संसार और कर्म-अदृष्टविषयक नूतन विचार भी प्राप्त होते हैं । ये विचार वैदिक-परम्परा के ही उपनिषदों में कहीं
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org