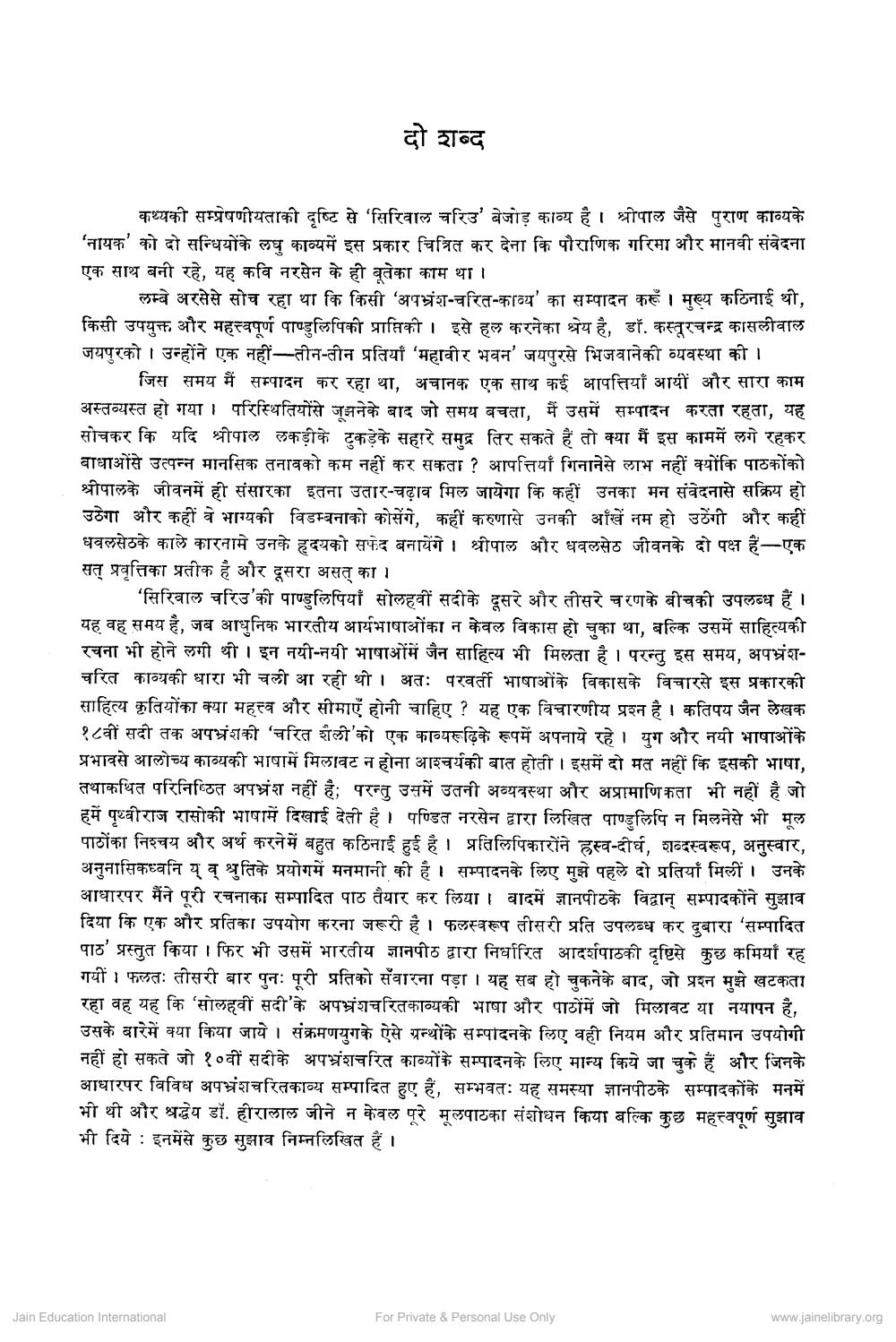________________
दो शब्द
कथ्यकी सम्प्रेषणीयताकी दृष्टि से 'सिरिवाल चरिउ' बेजोड़ काव्य है। श्रीपाल जैसे पुराण काव्यके 'नायक' को दो सन्धियोंके लघ काव्यमें इस प्रकार चित्रित कर देना कि पौराणिक गरिमा और मानवी संवेदना एक साथ बनी रहे, यह कवि नरसेन के ही बूतेका काम था।
लम्बे अरसेसे सोच रहा था कि किसी 'अपभ्रंश-चरित-काव्य' का सम्पादन करूँ । मुख्य कठिनाई थी, किसी उपयुक्त और महत्त्वपूर्ण पाण्डुलिपिकी प्राप्तिकी। इसे हल करनेका श्रेय है, डॉ. कस्तूरचन्द्र कासलीवाल जयपुरको। उन्होंने एक नहीं-तीन-तीन प्रतियाँ 'महावीर भवन' जयपुरसे भिजवाने की व्यवस्था की।
जिस समय मैं सम्पादन कर रहा था, अचानक एक साथ कई आपत्तियाँ आयीं और सारा काम अस्तव्यस्त हो गया। परिस्थितियोंसे जानेके बाद जो समय बचता. मैं उसमें सम्पादन करता रहता, यह सोचकर कि यदि श्रीपाल लकड़ीके टुकड़ेके सहारे समद्र तिर सकते हैं तो क्या मैं इस काममें लगे रहकर बाधाओंसे उत्पन्न मानसिक तनावको कम नहीं कर सकता? आपत्तियाँ गिनानेसे लाभ नहीं क्योंकि पाठकोंको श्रीपालके जीवनमें ही संसारका इतना उतार-चढ़ाव मिल जायेगा कि कहीं उनका मन संवेदनासे सक्रिय हो उठेगा और कहीं वे भाग्यकी विडम्बनाको कोसेंगे, कहीं करुणासे उनकी आँखें नम हो उठेगी और कहीं धवलसेठके काले कारनामे उनके हृदयको सफेद बनायेंगे। श्रीपाल और धवलसेठ जीवनके दो पक्ष हैं-एक सत् प्रवृत्तिका प्रतीक है और दूसरा असत् का।
_ 'सिरिवाल चरिउ'की पाण्डुलिपियाँ सोलहवीं सदीके दूसरे और तीसरे चरणके बीचकी उपलब्ध हैं । यह वह समय है, जब आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओंका न केवल विकास हो चुका था, बल्कि उसमें साहित्यकी रचना भी होने लगी थी। इन नयी-नयी भाषाओंमें जैन साहित्य भी मिलता है। परन्तु इस समय, अपभ्रंशचरित काव्यकी धारा भी चली आ रही थी। अतः परवर्ती भाषाओंके विकासके विचारसे इस प्रकारकी साहित्य कृतियोंका क्या महत्त्व और सीमाएँ होनी चाहिए? यह एक विचारणीय प्रश्न है । कतिपय जैन लेखक १८वीं सदी तक अपभ्रंशकी 'चरित शैली'को एक काव्यरूढिके रूपमें अपनाये रहे। युग और नयी भाषाओंके प्रभावसे आलोच्य काव्यकी भाषामें मिलावट न होना आश्चर्यकी बात होती । इसमें दो मत नहीं कि इसकी भाषा, तथाकथित परिनिष्ठित अपभ्रंश नहीं है। परन्तु उसमें उतनी अव्यवस्था और अप्रामाणिकता भी नहीं है जो हमें पृथ्वीराज रासोकी भाषामें दिखाई देती है। पण्डित नरसेन द्वारा लिखित पाण्डुलिपि न मिलनेसे भी मूल पाठोंका निश्चय और अर्थ करने में बहुत कठिनाई हुई है। प्रतिलिपिकारोंने ह्रस्व-दीर्घ, शब्दस्वरूप, अनुस्वार, अनुनासिकध्वनि य व श्रुतिके प्रयोगमें मनमानी की है। सम्पादनके लिए मुझे पहले दो प्रतियाँ मिलीं। उनके आधारपर मैंने पूरी रचनाका सम्पादित पाठ तैयार कर लिया। बादमें ज्ञानपीठके विद्वान् सम्पादकोंने सुझाव दिया कि एक और प्रतिका उपयोग करना जरूरी है। फलस्वरूप तीसरी प्रति उपलब्ध कर दुबारा 'सम्पादित पाठ' प्रस्तुत किया। फिर भी उसमें भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा निर्धारित आदर्शपाठकी दृष्टिसे कुछ कमियाँ रह गयीं। फलतः तीसरी बार पुनः पूरी प्रतिको सँवारना पड़ा । यह सब हो चुकनेके बाद, जो प्रश्न मुझे खटकता रहा वह यह कि 'सोलहवीं सदी के अपभ्रंशचरितकाव्यकी भाषा और पाठोंमें जो मिलावट या नयापन है, उसके बारेमें क्या किया जाये। संक्रमणयुगके ऐसे ग्रन्थोंके सम्पादनके लिए वही नियम और प्रतिमान उपयोगी नहीं हो सकते जो १०वीं सदीके अपभ्रंशचरित काव्योंके सम्पादनके लिए मान्य किये जा चुके हैं और जिनके आधारपर विविध अपभ्रंशचरितकाव्य सम्पादित हए हैं, सम्भवतः यह समस्या ज्ञानपीठके सम्पादकोंके मनमें भी थी और श्रद्धेय डॉ. हीरालाल जीने न केवल पूरे मूलपाठका संशोधन किया बल्कि कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव भी दिये : इनमेंसे कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org