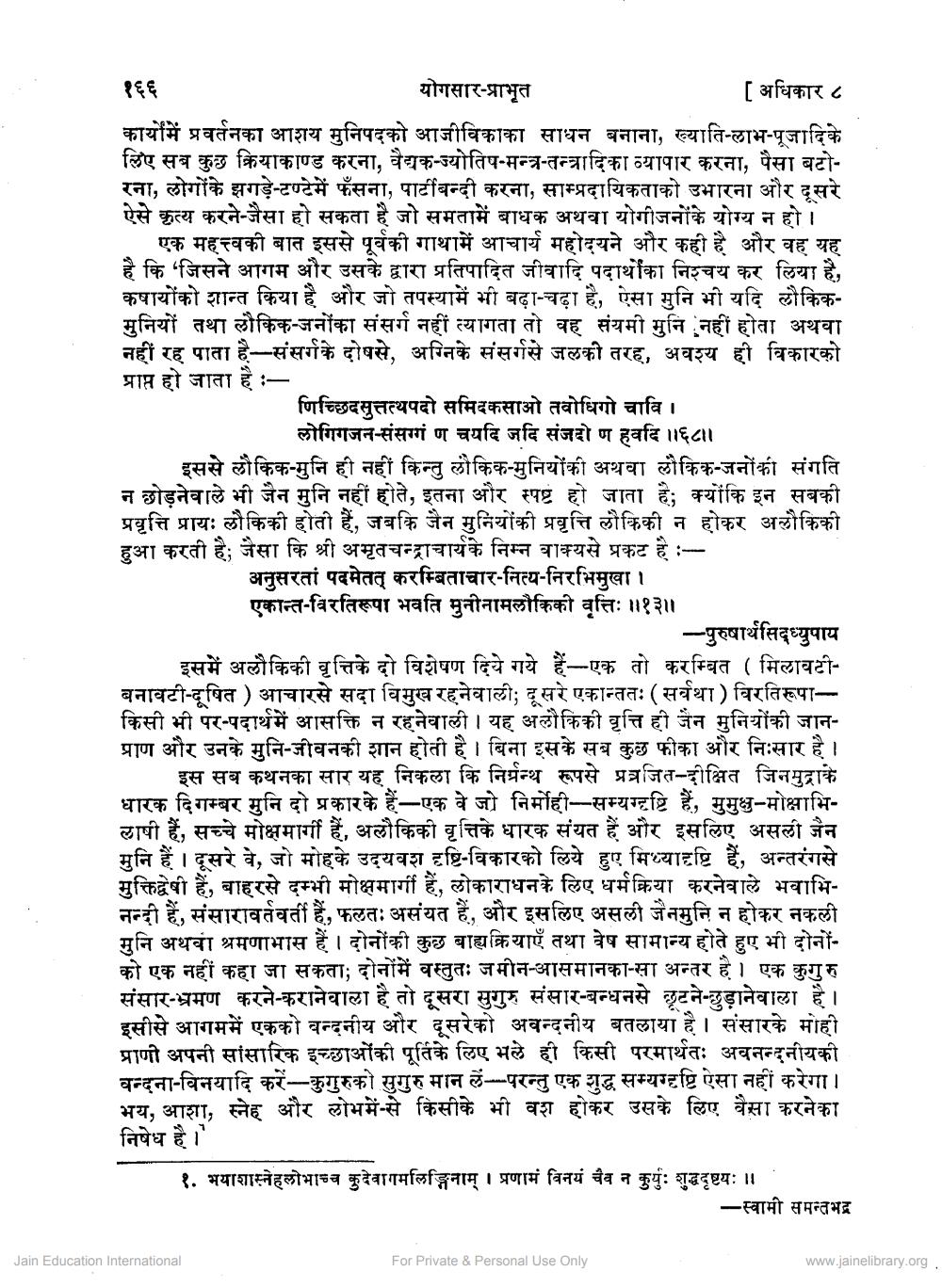________________
१६६ योगसार-प्राभृत
[ अधिकार ८ कार्यों में प्रवर्तनका आशय मुनिपदको आजीविकाका साधन बनाना, ख्याति-लाभ-पूजादिके लिए सब कुछ क्रियाकाण्ड करना, वैद्यक-ज्योतिष-मन्त्र-तन्त्रादिका व्यापार करना, पैसा बटोरना, लोगोंके झगड़े-टण्टेमें फँसना, पार्टीबन्दी करना, साम्प्रदायिकताको उभारना और दूसरे ऐसे कृत्य करने-जैसा हो सकता है जो समतामें बाधक अथवा योगीजनोंके योग्य न हो।
एक महत्त्वकी बात इससे पूर्वकी गाथामें आचार्य महोदयने और कही है और वह यह है कि 'जिसने आगम और उसके द्वारा प्रतिपादित जीवादि पदार्थोंका निश्चय कर लिया है, कषायोंको शान्त किया है और जो तपस्यामें भी बढ़ा-चढ़ा है, ऐसा मुनि भी यदि लौकिकमुनियों तथा लौकिक-जनोंका संसर्ग नहीं त्यागता तो वह संयमी मुनि नहीं होता अथवा नहीं रह पाता है-संसर्गके दोषसे, अग्निके संसर्गसे जलकी तरह, अवश्य ही विकारको प्राप्त हो जाता है :
णिच्छिदसुत्तत्थपदो समिदकसाओ तवोधिगो चावि ।
लोगिगजन-संसग्गं ण चयदि जदि संजदो ण हवदि ॥६८॥ इससे लौकिक-मुनि ही नहीं किन्तु लौकिक-मुनियोंकी अथवा लौकिक-जनोंकी संगति न छोड़नेवाले भी जैन मुनि नहीं होते, इतना और स्पष्ट हो जाता है; क्योंकि इन सबकी प्रवृत्ति प्रायः लौकिकी होती हैं, जबकि जैन मुनियोंकी प्रवृत्ति लौकिकी न होकर अलौकिकी हुआ करती हैजैसा कि श्री अमृतचन्द्राचार्य के निम्न वाक्यसे प्रकट है:
अनुसरतां पदमेतत् करम्बिताचार-नित्य-निरभिमुखा। एकान्त-विरतिरूपा भवति मुनीनामलौकिकी वृत्तिः ॥१३॥
-पुरुषार्थसिद्ध्युपाय इसमें अलौकिकी वृत्तिके दो विशेषण दिये गये हैं-एक तो करम्बित ( मिलावटीबनावटी-दूषित ) आचारसे सदा विमुख रहनेवाली; दूसरे एकान्ततः (सर्वथा) विरतिरूपाकिसी भी पर-पदार्थमें आसक्ति न रहनेवाली । यह अलौकिकी वृत्ति ही जैन मुनियोंकी जानप्राण और उनके मुनि-जीवनकी शान होती है। बिना इसके सब कुछ फीका और निःसार है।
इस सब कथनका सार यह निकला कि निर्ग्रन्थ रूपसे प्रत्रजित-दीक्षित जिन मुद्राके धारक दिगम्बर मुनि दो प्रकार के हैं-एक वे जो निर्मोही-सम्यग्दृष्टि हैं, मुमुक्षु-मोक्षाभिलाषी हैं, सच्चे मोक्षमार्गी हैं, अलौकिकी वृत्तिके धारक संयत हैं और इसलिए असली जैन मुनि हैं । दूसरे वे, जो मोहके उदयवश दृष्टि-विकारको लिये हुए मिथ्यादृष्टि हैं, अन्तरंगसे मुक्तिद्वेषी हैं, बाहरसे दम्भी मोक्षमार्गी हैं, लोकाराधनके लिए धर्म क्रिया करनेवाले भवाभिनन्दी हैं, संसारावर्तवर्ती हैं, फलतः असंयत हैं, और इसलिए असली जैनमुनि न होकर नकली मुनि अथवा श्रमणाभास हैं । दोनोंकी कुछ बाह्य क्रियाएँ तथा वेष सामान्य होते हुए भी दोनोंको एक नहीं कहा जा सकता; दोनोंमें वस्तुतः जमीन-आसमानका-सा अन्तर है। एक कुगुरु संसार-भ्रमण करने-करानेवाला है तो दूसरा सुगुरु संसार-बन्धनसे छूटने-छुड़ानेवाला है। इसीसे आगममें एकको बन्दनीय और दूसरेको अवन्दनीय बतलाया है । संसारके मोही प्राणी अपनी सांसारिक इच्छाओंकी पूर्तिके लिए भले ही किसी परमार्थतः अवनन्दनीयकी वन्दना-विनयादि करें-कुगुरुको सुगुरु मान लें-परन्तु एक शुद्ध सम्यग्दृष्टि ऐसा नहीं करेगा। भय, आशा, स्नेह और लोभमें-से किसीके भी वश होकर उसके लिए वैसा करनेका निषेध है।' १. भयाशास्नेहलोभाच्च कुदेवागमलिङ्गिनाम् । प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्धदृष्टयः ।।
-स्वामी समन्तभद्र
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org.