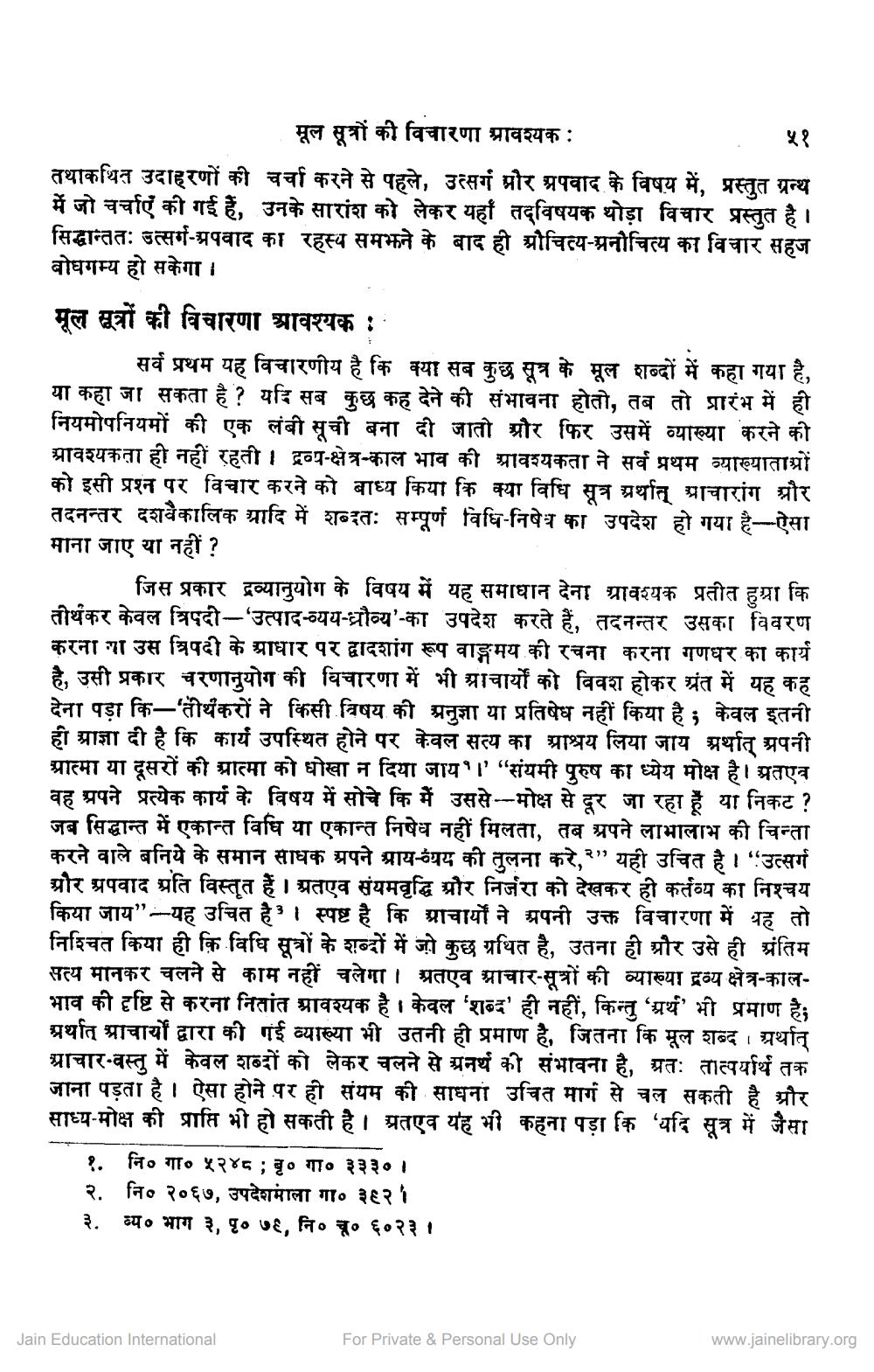________________
मूल सूत्रों की विचारणा श्रावश्यक :
५१
तथाकथित उदाहरणों की चर्चा करने से पहले, उत्सगं और अपवाद के विषय में, प्रस्तुत ग्रन्थ में जो चर्चाएँ की गई हैं, उनके सारांश को लेकर यहाँ तद्विषयक थोड़ा विचार प्रस्तुत है । सिद्धान्ततः उत्सर्ग - अपवाद का रहस्य समझने के बाद ही औचित्य - अनौचित्य का विचार सहज बोधगम्य हो सकेगा ।
मूल सूत्रों की विचारणा आवश्यक :
सर्व प्रथम यह विचारणीय है कि क्या सब कुछ सूत्र के मूल शब्दों में कहा गया है, या कहा जा सकता है ? यदि सब कुछ कह देने की संभावना होतो, तब तो प्रारंभ में ही नियमोपनियमों की एक लंबी सूची बना दी जातो और फिर उसमें व्याख्या करने की आवश्यकता ही नहीं रहती । द्रव्य-क्षेत्र काल भाव की प्रावश्यकता ने सर्व प्रथम व्याख्याताओं को इसी प्रश्न पर विचार करने को बाध्य किया कि क्या विधि सूत्र अर्थात् आचारांग और तदनन्तर दशवैकालिक ग्रादि में शब्दतः सम्पूर्ण विधि-निषेध का उपदेश हो गया है - ऐसा माना जाए या नहीं ?
जिस प्रकार द्रव्यानुयोग के विषय में यह समाधान देना ग्रावश्यक प्रतीत हुग्रा कि तीर्थंकर केवल त्रिपदी - 'उत्पाद व्यय - ध्रौव्य' - का उपदेश करते हैं, तदनन्तर उसका विवरण करना या उस त्रिपदी के आधार पर द्वादशांग रूप वाङ्गमय की रचना करना गणधर का कार्य है, उसी प्रकार चरणानुयोग की विचारणा में भी प्राचार्यों को विवश होकर अंत में यह कह देना पड़ा कि - 'तीर्थंकरों ने किसी विषय की अनुज्ञा या प्रतिषेध नहीं किया है; केवल इतनी ही आज्ञा दी है कि कार्यं उपस्थित होने पर केवल सत्य का आश्रय लिया जाय अर्थात् अपनी आत्मा या दूसरों की प्रात्मा को धोखा न दिया जाय ।" "संयमी पुरुष का ध्येय मोक्ष है । प्रतएव वह अपने प्रत्येक कार्य के विषय में सोचे कि में उससे - मोक्ष से दूर जा रहा हूँ या निकट ? जब सिद्धान्त में एकान्त विधि या एकान्त निषेध नहीं मिलता, तब अपने लाभालाभ की चिन्ता करने वाले बनिये के समान साधक अपने प्राय-व्यय की तुलना करे, ” यही उचित है । “उत्सर्ग और अपवाद प्रति विस्तृत हैं । अतएव संयमवृद्धि और निर्जरा को देखकर ही कर्तव्य का निश्चय किया जाय " - यह उचित है। स्पष्ट है कि आचार्यों ने अपनी उक्त विचारणा में वह तो निश्चित किया ही कि विधि सूत्रों के शब्दों में जो कुछ ग्रथित है, उतना ही और उसे ही अंतिम सत्य मानकर चलने से काम नहीं चलेगा । श्रतएव प्रचार सूत्रों की व्याख्या द्रव्य क्षेत्र - कालभाव की दृष्टि से करना नितांत आवश्यक है । केवल 'शब्द' ही नहीं, किन्तु 'अर्थ' भी प्रमाण है; अर्थात् प्राचार्यों द्वारा की गई व्याख्या भी उतनी ही प्रमाण है, जितना कि मूल शब्द अर्थात् आचार-वस्तु में केवल शब्दों को लेकर चलने से अनर्थ की संभावना है, अतः तात्पर्यार्थ तक जाना पड़ता है । ऐसा होने पर ही संयम की साधना उचित मार्ग से चल सकती है और साध्य- मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है । प्रतएव यह भी कहना पड़ा कि 'यदि सूत्र में जैसा
२१
[
१.
२.
३.
नि० गा० ५२४८ ; बृ० गा० ३३३० । नि० २०६७, उपदेशमाला गा० ३६२ ।
व्य० भाग ३, पृ० ७६, नि० ० ६०२३ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org