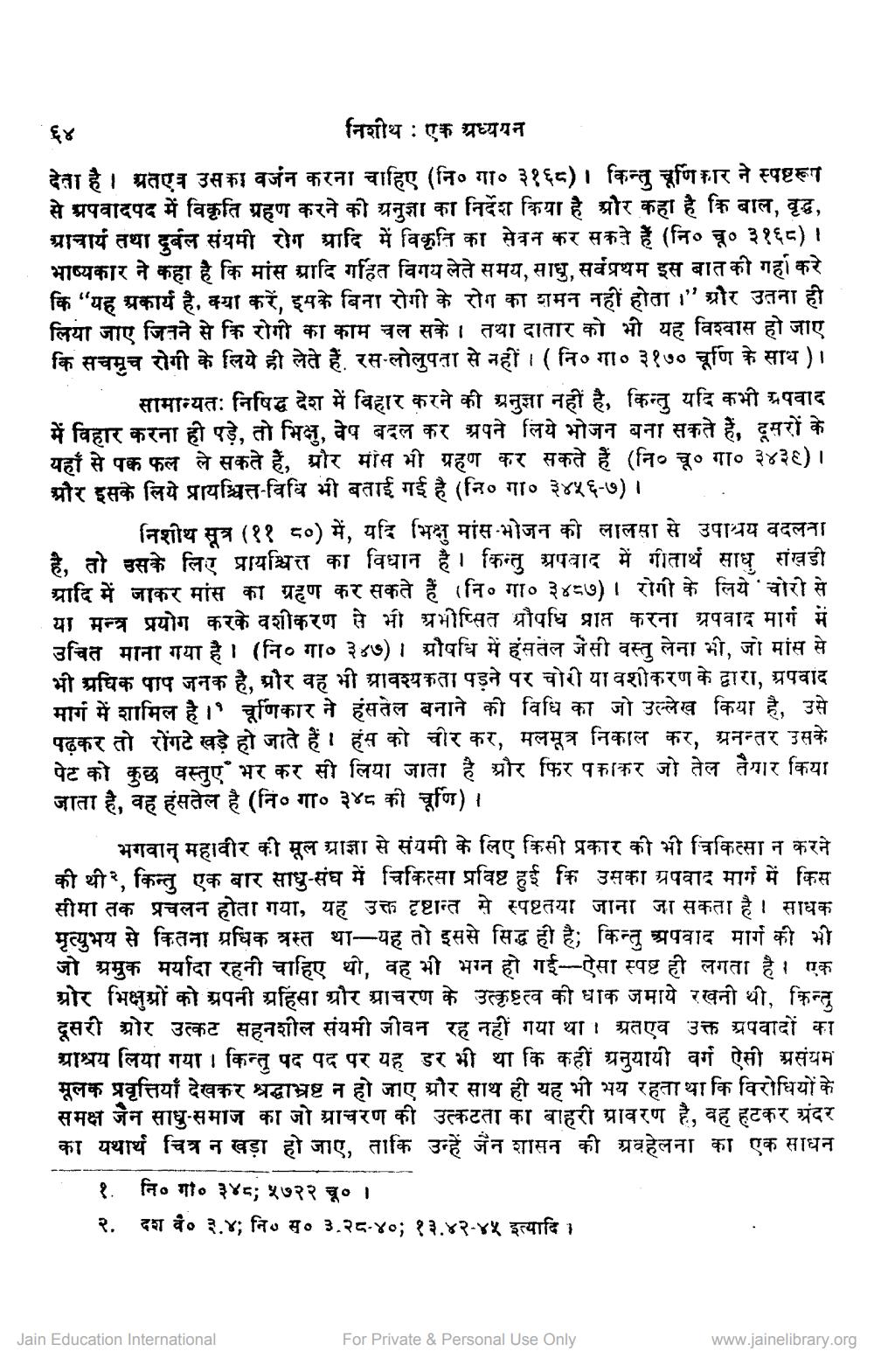________________
६४
निशीथ : एक अध्ययन देता है। अतएव उसका वजन करना चाहिए (नि० गा० ३१६८)। किन्तु चूर्णिकार ने स्पष्टरूप से अपवादपद में विकृति ग्रहण करने की अनुज्ञा का निर्देश किया है और कहा है कि बाल, वृद्ध, प्राचार्य तथा दुर्बल संयमी रोग प्रादि में विकृति का सेवन कर सकते हैं (नि० चू० ३१६८) । भाष्यकार ने कहा है कि मांस आदि गहित विगय लेते समय, साधु,सर्वप्रथम इस बात की गहां करे कि "यह अकार्य है, क्या करें, इसके बिना रोगी के रोग का शमन नहीं होता।" और उतना ही लिया जाए जितने से कि रोगी का काम चल सके । तथा दातार को भी यह विश्वास हो जाए कि सचमुच रोगी के लिये ही लेते हैं. रस-लोलुपता से नहीं। (नि० गा० ३१७० चूणि के साथ )।
सामान्यतः निषिद्ध देश में विहार करने की अनुज्ञा नहीं है, किन्तु यदि कभी अपवाद में विहार करना ही पड़े, तो भिक्षु, वेष बदल कर अपने लिये भोजन बना सकते हैं, दूसरों के यहाँ से पक फल ले सकते हैं, और मांस भी ग्रहण कर सकते हैं (नि० चू० गा० ३४३६) । और इसके लिये प्रायश्चित्त-विवि भी बताई गई है (नि० गा० ३४५६-७)। .
निशीथ सूत्र (११ ८०) में, यदि भिक्षु मांस भोजन को लालसा से उपायय बदलता है, तो उसके लिए प्रायश्चित्त का विधान है। किन्तु अपवाद में गीतार्थ साध संखडी ग्रादि में जाकर मांस का ग्रहण कर सकते हैं (नि० गा० ३४८७)। रोगी के लिये चोरी से या मन्त्र प्रयोग करके वशीकरण से भी अभीप्सित प्रौपधि प्रात करना अपवाद मार्ग में उचित माना गया है। (नि० गा० ३४७)। औषधि में हंसतेल जेसी वस्तु लेना भी, जो मांस से भी अधिक पाप जनक है, और वह भी आवश्यकता पड़ने पर चोरी या वशीकरण के द्वारा, अपवाद मार्ग में शामिल है।' चूर्णिकार ने हंसतेल बनाने की विधि का जो उल्लेख किया है, उसे पढ़कर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हंस को चीर कर, मलमूत्र निकाल कर, अनन्तर उसके पेट को कुछ वस्तुएं भर कर सी लिया जाता है और फिर पकाकर जो तेल तैयार किया जाता है, वह हंसतेल है (नि० गा० ३४८ की चूणि)।
भगवान् महावीर की मूल ग्राज्ञा से संयमी के लिए किसी प्रकार की भी चिकित्सा न करने की थी, किन्तु एक बार साधु-संघ में चिकित्सा प्रविष्ट हुई कि उसका अपवाद मार्ग में किस सीमा तक प्रचलन होता गया, यह उक्त दृष्टान्त से स्पष्टतया जाना जा सकता है। साधक मृत्युभय से कितना अधिक त्रस्त था-यह तो इससे सिद्ध ही है; किन्तु अपवाद मार्ग की भी जो अमुक मर्यादा रहनी चाहिए थी, वह भी भग्न हो गई-ऐसा स्पष्ट ही लगता है। एक पोर भिक्षुओं को अपनी अहिंसा और आचरण के उत्कृष्टत्व की धाक जमाये रखनी थी, किन्तु दूसरी ओर उत्कट सहनशील संयमी जीवन रह नहीं गया था। अतएव उक्त अपवादों का प्राश्रय लिया गया। किन्तु पद पद पर यह डर भी था कि कहीं अनुयायी वर्ग ऐसी असंयम मूलक प्रवृत्तियाँ देखकर श्रद्धाभ्रष्ट न हो जाए और साथ ही यह भी भय रहता था कि विरोधियों के समक्ष जैन साधु-समाज का जो पाचरण की उत्कटता का बाहरी प्रावरण है, वह हटकर अंदर का यथार्थ चित्र न खड़ा हो जाए, ताकि उन्हें जैन शासन की अवहेलना का एक साधन
१. नि० गा० ३४८; ५७२२ चू० । २. दश वै० ३.४; नि० स० ३.२८.४०; १३.४२-४५ इत्यादि ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org