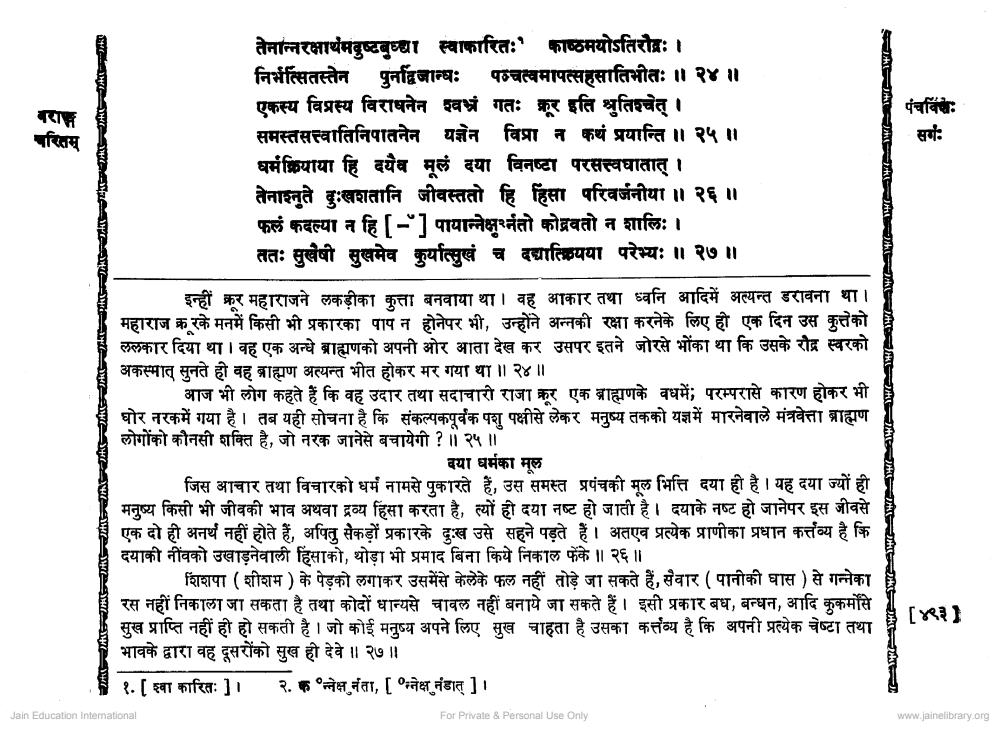________________
बराङ्ग चरितम्
तेनान्नरक्षार्थमवुष्टबुध्धा स्वाकारितः काष्ठमयोऽतिरौद्रः । निर्भत्सतस्तेन पुनद्वजान्धः पञ्चत्वमापत्सहसातिभीतः ॥ २४ ॥ एकस्य विप्रस्य विराधनेन श्वभ्रं गतः क्रूर इति श्रुतिश्चेत् । समस्तसत्वातिनिपातनेन यज्ञेन विप्रा न कथं प्रयान्ति ॥ २५ ॥ धर्मक्रियाया हि दयैव मूलं दया विनष्टा परसस्त्वघातात् । तेनाश्नुते दुःखशतानि जीवस्ततो हि हिंसा परिवर्जनीया ॥ २६ ॥ फलं कल्यान हि [ - ] पायान्नेक्षुर्नतो कोद्रवतो न शालि: । ततः सुखेषी सुखमेव कुर्यात्सुखं च दद्यात्क्रियया परेभ्यः ॥ २७ ॥
इन्हीं क्रूर महाराजने लकड़ीका कुत्ता बनवाया था। वह आकार तथा ध्वनि आदिमें अत्यन्त डरावना था । महाराज करके मनमें किसी भी प्रकारका पाप न होनेपर भी, उन्होंने अन्नकी रक्षा करनेके लिए ही एक दिन उस कुत्ते को ललकार दिया था। वह एक अन्धे ब्राह्मणको अपनी ओर आता देख कर उसपर इतने जोरसे भोंका था कि उसके रौद्र स्वरको अकस्मात् सुनते ही वह ब्राह्मण अत्यन्त भीत होकर मर गया था ॥ २४ ॥
आज भी लोग कहते हैं कि वह उदार तथा सदाचारी राजा क्रूर एक ब्राह्मणके वधमें; परम्परासे कारण होकर भी घोर नरकमें गया है । तब यही सोचना है कि संकल्पकपूर्वक पशु पक्षीसे लेकर मनुष्य तकको यज्ञ में मारनेवाले मंत्रवेत्ता ब्राह्मण लोगोंको कौनसी शक्ति है, जो नरक जानेसे बचायेगी ? ॥ २५ ॥
या धर्मका मूल
जिस आचार तथा विचारको धर्मं नामसे पुकारते हैं, उस समस्त प्रपंचकी मूल भित्ति दया ही है। यह दया ज्यों ही मनुष्य किसी भी जीवकी भाव अथवा द्रव्य हिंसा करता है, त्यों ही दया नष्ट हो जाती है । दयाके नष्ट हो जानेपर इस जीवसे एक दो ही अनर्थं नहीं होते हैं, अपितु सैकड़ों प्रकारके दुःख उसे सहने पड़ते हैं । अतएव प्रत्येक प्राणीका प्रधान कर्त्तव्य है कि दयाकी नींवको उखाड़नेवाली हिंसाको, थोड़ा भी प्रमाद बिना किये निकाल फेंके ॥ २६ ॥
शिशपा ( शीशम ) के पेड़को लगाकर उसमेंसे केलेके फल नहीं तोड़े जा सकते हैं, सेवार ( पानीकी घास) से गन्नेका रस नहीं निकाला जा सकता है तथा कोदों धान्यसे चावल नहीं बनाये जा सकते हैं। इसी प्रकार बध, बन्धन, आदि कुकर्मों से सुख प्राप्ति नहीं ही हो सकती है। जो कोई मनुष्य अपने लिए सुख चाहता है उसका कर्त्तव्य है कि अपनी प्रत्येक चेष्टा तथा भावके द्वारा वह दूसरोंको सुख ही देवे ॥ २७ ॥
१. [ श्वा कारितः ] ।
२. कनेक्षनंता, [ नेक्ष नंडात् ] ।
Jain Education International
For Private
Personal Use Only
पंचविशे: सर्गः
[ ४९३]
www.jainelibrary.org