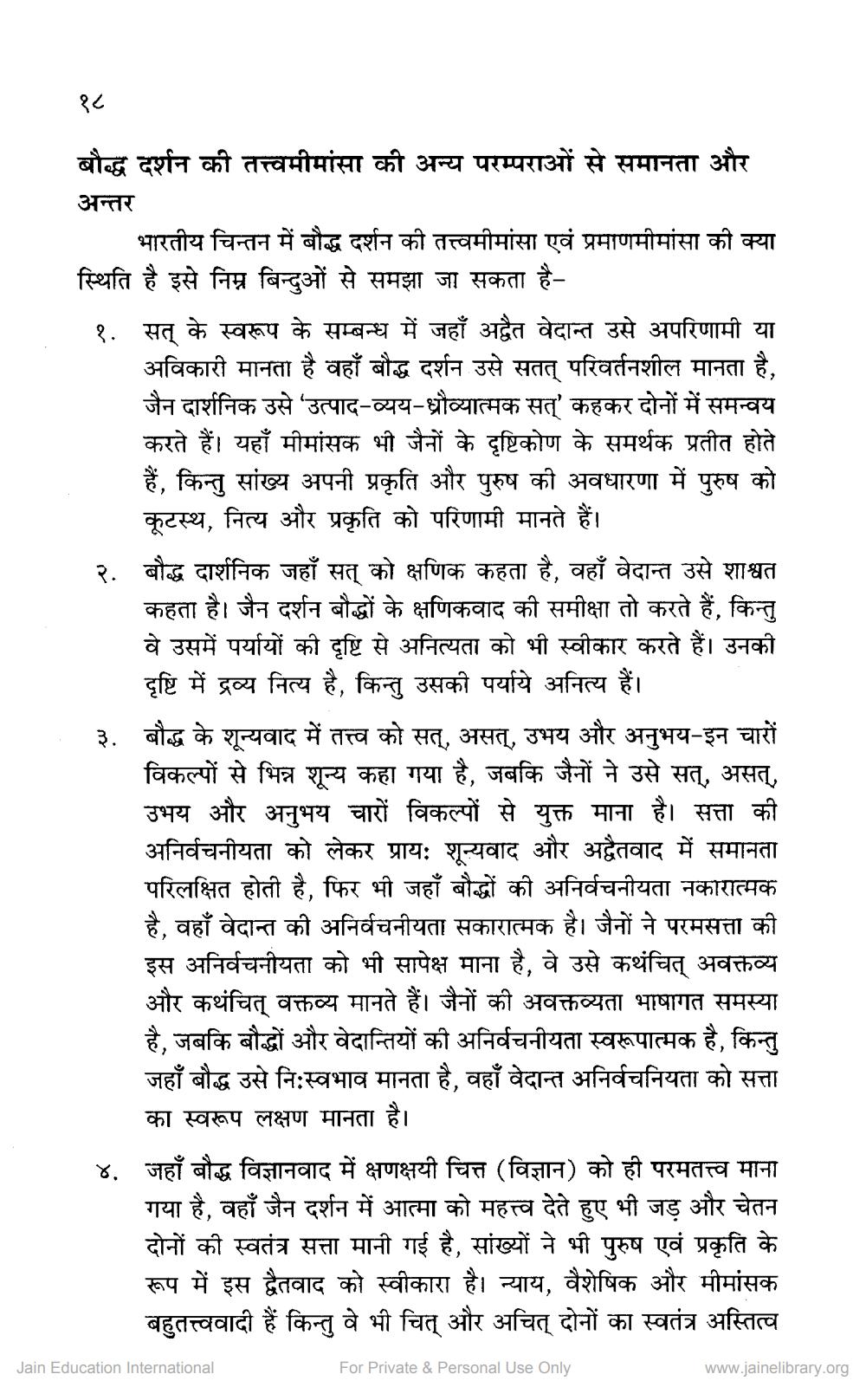________________
बौद्ध दर्शन की तत्त्वमीमांसा की अन्य परम्पराओं से समानता और अन्तर
भारतीय चिन्तन में बौद्ध दर्शन की तत्त्वमीमांसा एवं प्रमाणमीमांसा की क्या स्थिति है इसे निम्न बिन्दुओं से समझा जा सकता है१. सत् के स्वरूप के सम्बन्ध में जहाँ अद्वैत वेदान्त उसे अपरिणामी या
अविकारी मानता है वहाँ बौद्ध दर्शन उसे सतत् परिवर्तनशील मानता है, जैन दार्शनिक उसे 'उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक सत्' कहकर दोनों में समन्वय करते हैं। यहाँ मीमांसक भी जैनों के दृष्टिकोण के समर्थक प्रतीत होते हैं, किन्तु सांख्य अपनी प्रकृति और पुरुष की अवधारणा में पुरुष को
कूटस्थ, नित्य और प्रकृति को परिणामी मानते हैं। २. बौद्ध दार्शनिक जहाँ सत् को क्षणिक कहता है, वहाँ वेदान्त उसे शाश्वत
कहता है। जैन दर्शन बौद्धों के क्षणिकवाद की समीक्षा तो करते हैं, किन्तु वे उसमें पर्यायों की दृष्टि से अनित्यता को भी स्वीकार करते हैं। उनकी
दृष्टि में द्रव्य नित्य है, किन्तु उसकी पर्याये अनित्य हैं। ३. बौद्ध के शून्यवाद में तत्त्व को सत, असत्, उभय और अनुभय-इन चारों
विकल्पों से भिन्न शून्य कहा गया है, जबकि जैनों ने उसे सत, असत, उभय और अनुभय चारों विकल्पों से युक्त माना है। सत्ता की अनिर्वचनीयता को लेकर प्रायः शून्यवाद और अद्वैतवाद में समानता परिलक्षित होती है, फिर भी जहाँ बौद्धों की अनिर्वचनीयता नकारात्मक है, वहाँ वेदान्त की अनिर्वचनीयता सकारात्मक है। जैनों ने परमसत्ता की इस अनिर्वचनीयता को भी सापेक्ष माना है, वे उसे कथंचित् अवक्तव्य
और कथंचित् वक्तव्य मानते हैं। जैनों की अवक्तव्यता भाषागत समस्या है. जबकि बौद्धों और वेदान्तियों की अनिर्वचनीयता स्वरूपात्मक है, किन्तु जहाँ बौद्ध उसे नि:स्वभाव मानता है, वहाँ वेदान्त अनिर्वचनियता को सत्ता
का स्वरूप लक्षण मानता है। ४. जहाँ बौद्ध विज्ञानवाद में क्षणक्षयी चित्त (विज्ञान) को ही परमतत्त्व माना
गया है, वहाँ जैन दर्शन में आत्मा को महत्त्व देते हुए भी जड़ और चेतन दोनों की स्वतंत्र सत्ता मानी गई है, सांख्यों ने भी पुरुष एवं प्रकृति के रूप में इस द्वैतवाद को स्वीकारा है। न्याय, वैशेषिक और मीमांसक बहुतत्त्ववादी हैं किन्तु वे भी चित् और अचित् दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org
Jain Education International