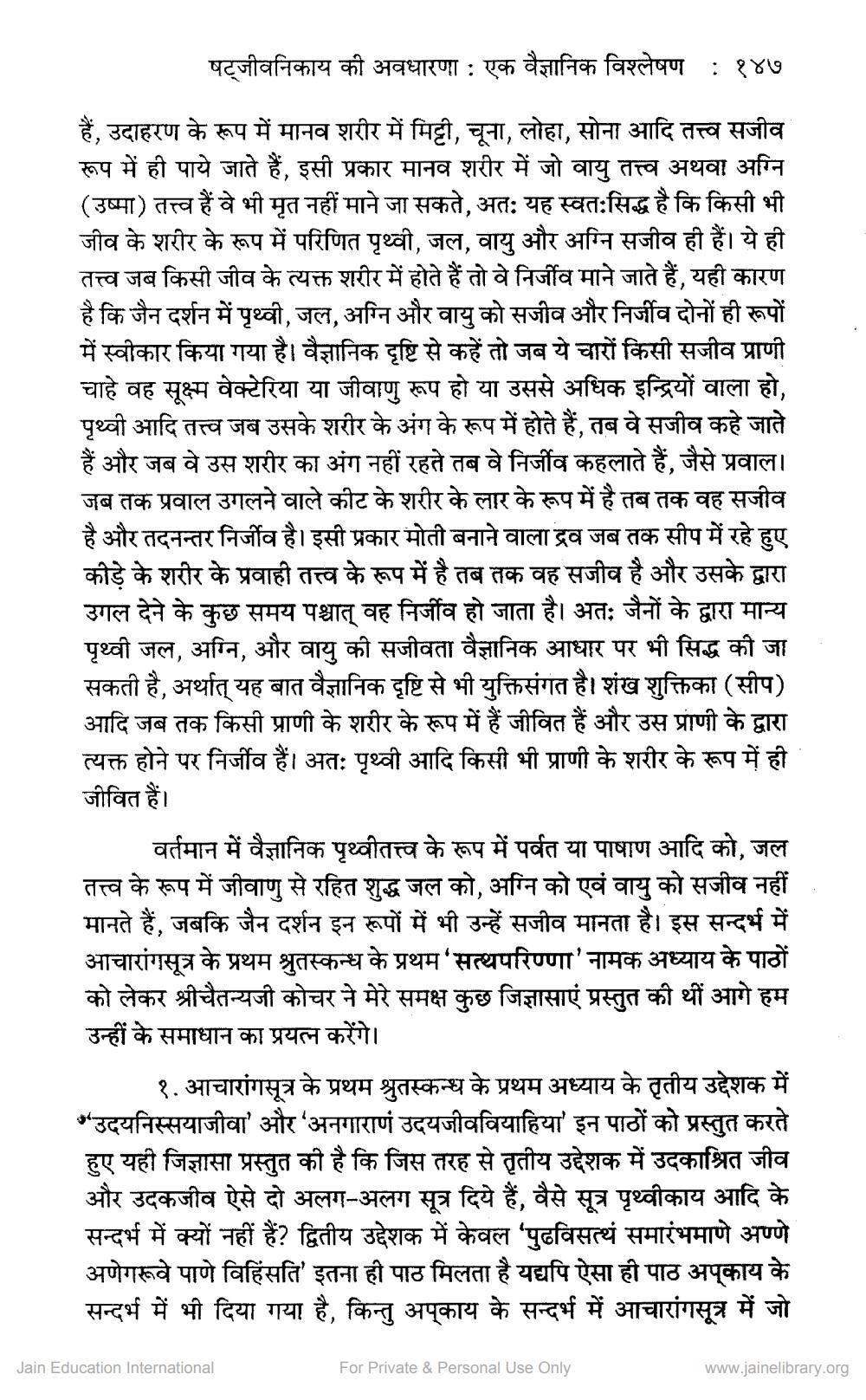________________
षट्जीवनिकाय की अवधारणा : एक वैज्ञानिक विश्लेषण : १४७
हैं, उदाहरण के रूप में मानव शरीर में मिट्टी, चूना, लोहा, सोना आदि तत्त्व सजीव रूप में ही पाये जाते हैं, इसी प्रकार मानव शरीर में जो वायु तत्त्व अथवा अग्नि (उष्मा) तत्त्व हैं वे भी मृत नहीं माने जा सकते, अतः यह स्वतः सिद्ध है कि किसी भी जीव के शरीर के रूप में परिणित पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि सजीव ही हैं। ये ही तत्त्व जब किसी जीव के त्यक्त शरीर में होते हैं तो वे निर्जीव माने जाते हैं, यही कारण है कि जैन दर्शन में पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को सजीव और निर्जीव दोनों ही रूपों में स्वीकार किया गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से कहें तो जब ये चारों किसी सजीव प्राणी चाहे वह सूक्ष्म वेक्टेरिया या जीवाणु रूप हो या उससे अधिक इन्द्रियों वाला हो, पृथ्वी आदि तत्त्व जब उसके शरीर के अंग के रूप में होते हैं, तब वे सजीव कहे जाते हैं और जब वे उस शरीर का अंग नहीं रहते तब वे निर्जीव कहलाते हैं, जैसे प्रवाल । जब तक प्रवाल उगलने वाले कीट के शरीर के लार के रूप में है तब तक वह सजीव है और तदनन्तर निर्जीव है। इसी प्रकार मोती बनाने वाला द्रव जब तक सीप में रहे हुए कीड़े के शरीर के प्रवाही तत्त्व के रूप में है तब तक वह सजीव है और उसके द्वारा उगल देने के कुछ समय पश्चात् वह निर्जीव हो जाता है। अतः जैनों के द्वारा मान्य पृथ्वी जल, अग्नि, और वायु की सजीवता वैज्ञानिक आधार पर भी सिद्ध की जा सकती है, अर्थात् यह बात वैज्ञानिक दृष्टि से भी युक्तिसंगत है। शंख शुक्तिका (सीप) आदि जब तक किसी प्राणी के शरीर के रूप में हैं जीवित हैं और उस प्राणी के द्वारा त्यक्त होने पर निर्जीव हैं। अतः पृथ्वी आदि किसी भी प्राणी के शरीर के रूप में ही जीवित हैं।
वर्तमान में वैज्ञानिक पृथ्वीतत्त्व के रूप में पर्वत या पाषाण आदि को, जल तत्त्व के रूप में जीवाणु से रहित शुद्ध जल को, अग्नि को एवं वायु को सजीव नहीं मानते हैं, जबकि जैन दर्शन इन रूपों में भी उन्हें सजीव मानता है। इस सन्दर्भ में आचारांगसूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध के प्रथम 'सत्थपरिण्णा' नामक अध्याय के पाठों को लेकर श्रीचैतन्यजी कोचर ने मेरे समक्ष कुछ जिज्ञासाएं प्रस्तुत की थीं आगे हम उन्हीं के समाधान का प्रयत्न करेंगे।
१. आचारांगसूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध के प्रथम अध्याय के तृतीय उद्देशक में 'उदयनिस्सयाजीवा' और 'अनगाराणं उदयजीववियाहिया' इन पाठों को प्रस्तुत करते हुए यही जिज्ञासा प्रस्तुत की है कि जिस तरह से तृतीय उद्देशक में उदकाश्रित जीव और उदकजीव ऐसे दो अलग-अलग सूत्र दिये हैं, वैसे सूत्र पृथ्वीकाय आदि के सन्दर्भ में क्यों नहीं हैं? द्वितीय उद्देशक में केवल 'पुढविसत्थं समारंभमाणे अण्णे अणेगरूवे पाणे विहिंसति' इतना ही पाठ मिलता है यद्यपि ऐसा ही पाठ अप्काय के सन्दर्भ में भी दिया गया है, किन्तु अप्काय के सन्दर्भ में आचारांगसूत्र में जो
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org