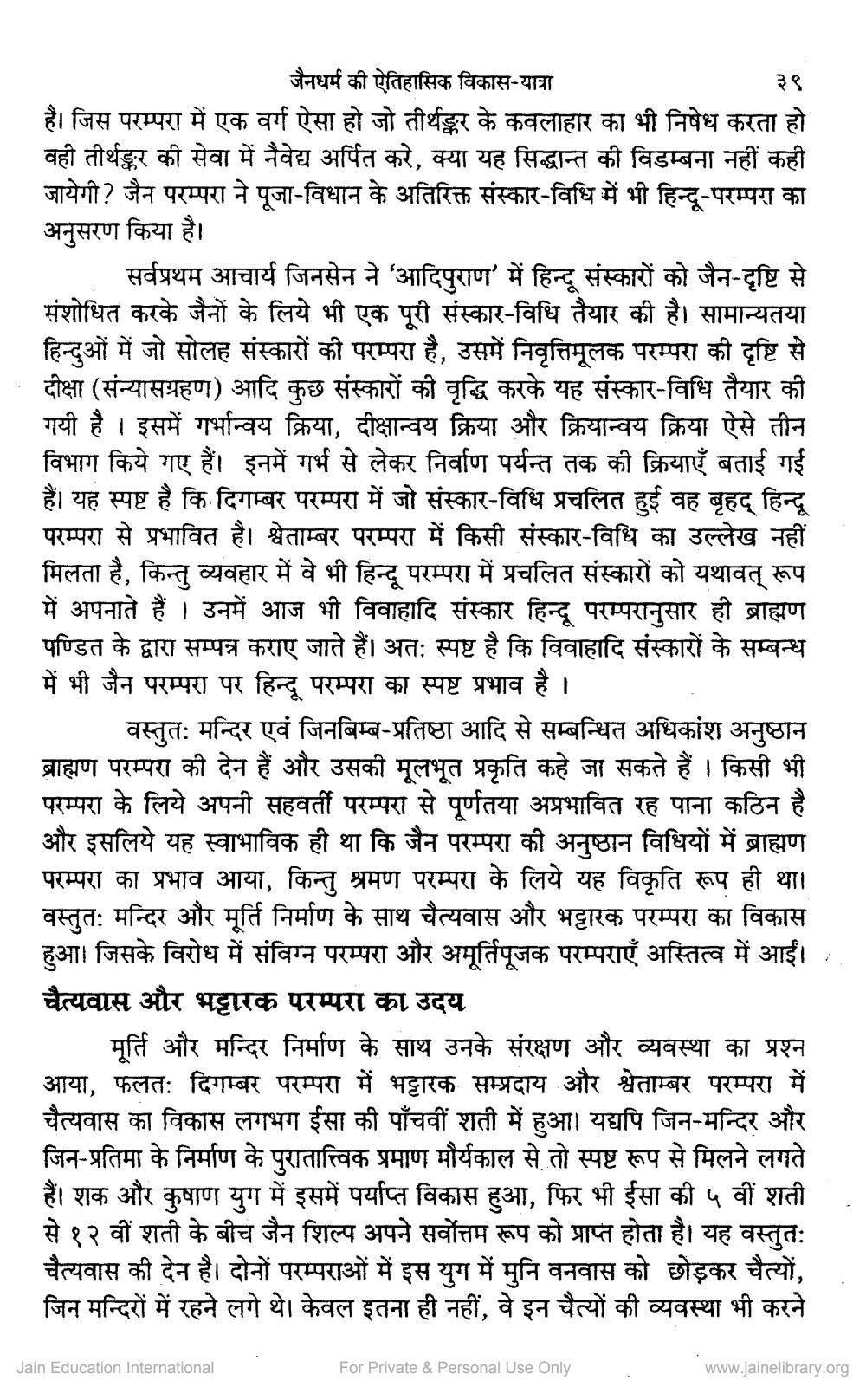________________
३९
जैनधर्म की ऐतिहासिक विकास-यात्रा है। जिस परम्परा में एक वर्ग ऐसा हो जो तीर्थङ्कर के कवलाहार का भी निषेध करता हो वही तीर्थङ्कर की सेवा में नैवेद्य अर्पित करे, क्या यह सिद्धान्त की विडम्बना नहीं कही जायेगी? जैन परम्परा ने पूजा-विधान के अतिरिक्त संस्कार-विधि में भी हिन्दू-परम्परा का अनुसरण किया है।
सर्वप्रथम आचार्य जिनसेन ने 'आदिपुराण' में हिन्दू संस्कारों को जैन-दृष्टि से संशोधित करके जैनों के लिये भी एक पूरी संस्कार-विधि तैयार की है। सामान्यतया हिन्दुओं में जो सोलह संस्कारों की परम्परा है, उसमें निवृत्तिमूलक परम्परा की दृष्टि से दीक्षा (संन्यासग्रहण) आदि कुछ संस्कारों की वृद्धि करके यह संस्कार-विधि तैयार की गयी है । इसमें गर्भान्वय क्रिया, दीक्षान्वय क्रिया और क्रियान्वय क्रिया ऐसे तीन विभाग किये गए हैं। इनमें गर्भ से लेकर निर्वाण पर्यन्त तक की क्रियाएँ बताई गई हैं। यह स्पष्ट है कि दिगम्बर परम्परा में जो संस्कार-विधि प्रचलित हुई वह बृहद् हिन्दू परम्परा से प्रभावित है। श्वेताम्बर परम्परा में किसी संस्कार-विधि का उल्लेख नहीं मिलता है, किन्तु व्यवहार में वे भी हिन्दू परम्परा में प्रचलित संस्कारों को यथावत् रूप में अपनाते हैं । उनमें आज भी विवाहादि संस्कार हिन्दू परम्परानुसार ही ब्राह्मण पण्डित के द्वारा सम्पन्न कराए जाते हैं। अत: स्पष्ट है कि विवाहादि संस्कारों के सम्बन्ध में भी जैन परम्परा पर हिन्दू परम्परा का स्पष्ट प्रभाव है ।
वस्तुत: मन्दिर एवं जिनबिम्ब-प्रतिष्ठा आदि से सम्बन्धित अधिकांश अनुष्ठान ब्राह्मण परम्परा की देन हैं और उसकी मूलभूत प्रकृति कहे जा सकते हैं । किसी भी परम्परा के लिये अपनी सहवर्ती परम्परा से पूर्णतया अप्रभावित रह पाना कठिन है और इसलिये यह स्वाभाविक ही था कि जैन परम्परा की अनुष्ठान विधियों में ब्राह्मण परम्परा का प्रभाव आया, किन्तु श्रमण परम्परा के लिये यह विकृति रूप ही था। वस्तुत: मन्दिर और मूर्ति निर्माण के साथ चैत्यवास और भट्टारक परम्परा का विकास हुआ। जिसके विरोध में संविग्न परम्परा और अमूर्तिपूजक परम्पराएँ अस्तित्व में आईं। । चैत्यवास और भट्टारक परम्परा का उदय
मूर्ति और मन्दिर निर्माण के साथ उनके संरक्षण और व्यवस्था का प्रश्न आया, फलत: दिगम्बर परम्परा में भट्टारक सम्प्रदाय और श्वेताम्बर परम्परा में चैत्यवास का विकास लगभग ईसा की पाँचवीं शती में हुआ। यद्यपि जिन-मन्दिर और जिन-प्रतिमा के निर्माण के पुरातात्त्विक प्रमाण मौर्यकाल से तो स्पष्ट रूप से मिलने लगते हैं। शक और कुषाण युग में इसमें पर्याप्त विकास हुआ, फिर भी ईसा की ५ वीं शती से १२ वीं शती के बीच जैन शिल्प अपने सर्वोत्तम रूप को प्राप्त होता है। यह वस्तुतः चैत्यवास की देन है। दोनों परम्पराओं में इस युग में मुनि वनवास को छोड़कर चैत्यों, जिन मन्दिरों में रहने लगे थे। केवल इतना ही नहीं, वे इन चैत्यों की व्यवस्था भी करने
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org