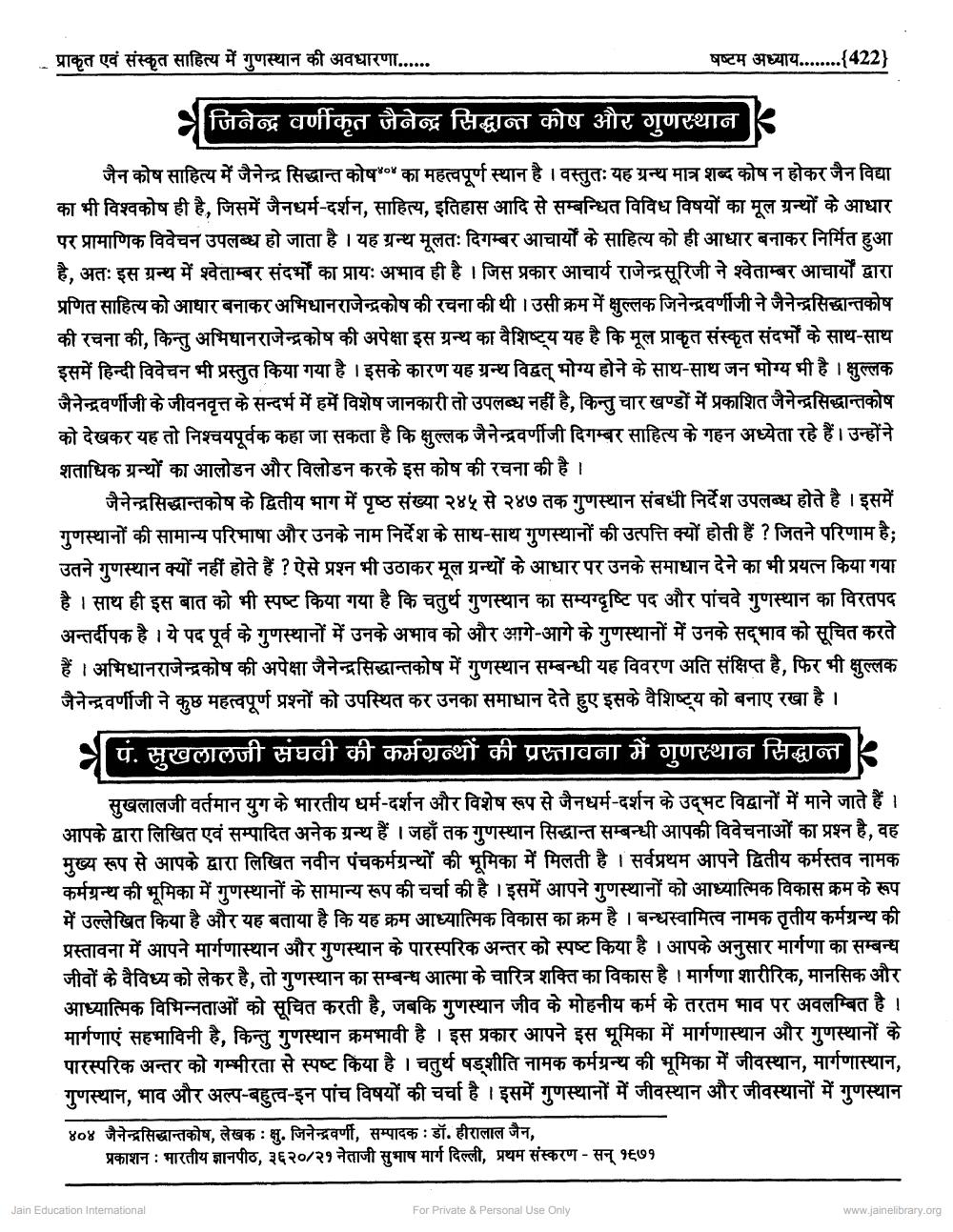________________
- प्राकृत एवं संस्कृत साहित्य में गुणस्थान की अवधारणा....
षष्टम अध्याय........{422}
जिनेन्द्र वर्गीकृत जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष और गुणस्थान k जैन कोष साहित्य में जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष का महत्वपूर्ण स्थान है । वस्तुतः यह ग्रन्थ मात्र शब्द कोष न होकर जैन विद्या का भी विश्वकोष ही है, जिसमें जैनधर्म-दर्शन, साहित्य, इतिहास आदि से सम्बन्धित विविध विषयों का मूल ग्रन्थों के आधार पर प्रामाणिक विवेचन उपलब्ध हो जाता है । यह ग्रन्थ मूलतः दिगम्बर आचार्यों के साहित्य को ही आधार बनाकर निर्मित हुआ है, अतः इस ग्रन्थ में श्वेताम्बर संदर्भो का प्रायः अभाव ही है । जिस प्रकार आचार्य राजेन्द्रसूरिजी ने श्वेताम्बर आचार्यों द्वारा प्रणित साहित्य को आधार बनाकर अभिधानराजेन्द्रकोष की रचना की थी। उसी क्रम में क्षुल्लक जिनेन्द्रवर्णीजी ने जैनेन्द्रसिद्धान्तकोष की रचना की, किन्तु अभिधानराजेन्द्रकोष की अपेक्षा इस ग्रन्थ का वैशिष्ट्य यह है कि मूल प्राकृत संस्कृत संदर्भो के साथ-साथ इसमें हिन्दी विवेचन भी प्रस्तुत किया गया है । इसके कारण यह ग्रन्थ विद्वत् भोग्य होने के साथ-साथ जन भोग्य भी है । क्षुल्लक जैनेन्द्रवर्णीजी के जीवनवृत्त के सन्दर्भ में हमें विशेष जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, किन्तु चार खण्डों में प्रकाशित जैनेन्द्रसिद्धान्तकोष को देखकर यह तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि क्षुल्लक जैनेन्द्रवर्णीजी दिगम्बर साहित्य के गहन अध्येता रहे हैं। उन्होंने शताधिक ग्रन्थों का आलोडन और विलोडन करके इस कोष की रचना की है।
जैनेन्द्रसिद्धान्तकोष के द्वितीय भाग में पृष्ठ संख्या २४५ से २४७ तक गुणस्थान संबधी निर्देश उपलब्ध होते है । इसमें गुणस्थानों की सामान्य परिभाषा और उनके नाम निर्देश के साथ-साथ गुणस्थानों की उत्पत्ति क्यों होती हैं ? जितने परिणाम है; उतने गुणस्थान क्यों नहीं होते हैं ? ऐसे प्रश्न भी उठाकर मूल ग्रन्थों के आधार पर उनके समाधान देने का भी प्रयत्न किया गया है । साथ ही इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि चतुर्थ गुणस्थान का सम्यग्दृष्टि पद और पांचवे गुणस्थान का विरतपद अन्तर्दीपक है । ये पद पूर्व के गुणस्थानों में उनके अभाव को और आगे-आगे के गुणस्थानों में उनके सद्भाव को सूचित करते हैं । अभिधानराजेन्द्रकोष की अपेक्षा जैनेन्द्रसिद्धान्तकोष में गुणस्थान सम्बन्धी यह विवरण अति संक्षिप्त है, फिर भी क्षुल्लक जैनेन्द्रवर्णीजी ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को उपस्थित कर उनका समाधान देते हुए इसके वैशिष्ट्य को बनाए रखा है । त्रपं. सुखलालजी संघवी की कर्मग्रन्थों की प्रस्तावना में गुणस्थान सिद्धान्त
सुखलालजी वर्तमान युग के भारतीय धर्म-दर्शन और विशेष रूप से जैनधर्म-दर्शन के उभट विद्वानों में माने जाते हैं। आपके द्वारा लिखित एवं सम्पादित अनेक ग्रन्थ हैं । जहाँ तक गुणस्थान सिद्धान्त सम्बन्धी आपकी विवेचनाओं का प्रश्न है, वह मुख्य रूप से आपके द्वारा लिखित नवीन पंचकर्मग्रन्थों की भूमिका में मिलती है । सर्वप्रथम आपने द्वितीय कर्मस्तव नामक कर्मग्रन्थ की भूमिका में गुणस्थानों के सामान्य रूप की चर्चा की है। इसमें आपने गुणस्थानों को आध्यात्मिक विकास क्रम के रूप में उल्लेखित किया है और यह बताया है कि यह क्रम आध्यात्मिक विकास का क्रम है । बन्धस्वामित्व नामक तृतीय कर्मग्रन्थ की प्रस्तावना में आपने मार्गणास्थान और गुणस्थान के पारस्परिक अन्तर को स्पष्ट किया है । आपके अनुसार मार्गणा का सम्बन्ध जीवों के वैविध्य को लेकर है, तो गुणस्थान का सम्बन्ध आत्मा के चारित्र शक्ति का विकास है । मार्गणा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विभिन्नताओं को सूचित करती है, जबकि गुणस्थान जीव के मोहनीय कर्म के तरतम भाव पर अवलम्बित है। मार्गणाएं सहभाविनी है, किन्तु गुणस्थान क्रमभावी है । इस प्रकार आपने इस भूमिका में मार्गणास्थान और गुणस्थानों के पारस्परिक अन्तर को गम्भीरता से स्पष्ट किया है । चतुर्थ षड्शीति नामक कर्मग्रन्थ की भूमिका में जीवस्थान, मार्गणास्थान, गुणस्थान, भाव और अल्प-बहुत्व-इन पांच विषयों की चर्चा है । इसमें गुणस्थानों में जीवस्थान और जीवस्थानों में गुणस्थान ४०४ जैनेन्द्रसिद्धान्तकोष, लेखक : क्षु. जिनेन्द्रवर्णी, सम्पादक : डॉ. हीरालाल जैन,
प्रकाशन : भारतीय ज्ञानपीठ, ३६२०/२१ नेताजी सुभाष मार्ग दिल्ली, प्रथम संस्करण - सन् १९७१
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org