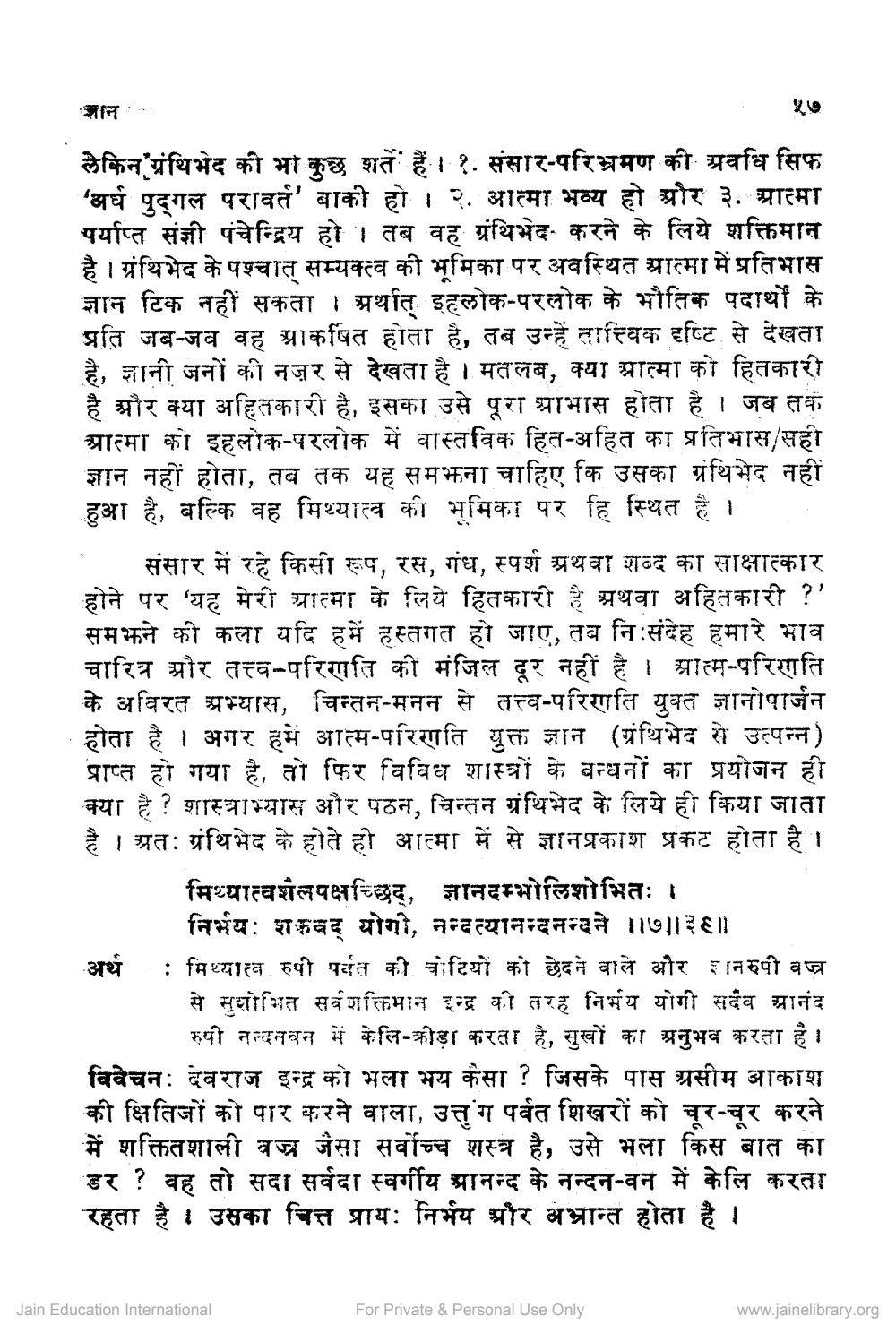________________
ज्ञान
૭
लेकिन ग्रंथिभेद की भी कुछ शर्तें हैं । १. संसार - परिभ्रमण की अवधि सिफ 'अर्ध पुद्गल परावर्त' बाकी हो । २. आत्मा भव्य हो और ३. आत्मा पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय हो । तब वह ग्रंथिभेद करने के लिये शक्तिमान है । ग्रंथिभेद के पश्चात् सम्यक्त्व की भूमिका पर अवस्थित आत्मा में प्रतिभास ज्ञान टिक नहीं सकता । अर्थात् इहलोक - परलोक के भौतिक पदार्थों के प्रति जब-जब वह प्राकर्षित होता है, तब उन्हें तात्त्विक दृष्टि से देखता है, ज्ञानी जनों की नज़र से देखता है। मतलब, क्या श्रात्मा को हितकारी है और क्या अहितकारी है, इसका उसे पूरा आभास होता है । जब तक आत्मा को इहलोक - परलोक में वास्तविक हित-अहित का प्रतिभास / सही ज्ञान नहीं होता, तब तक यह समझना चाहिए कि उसका ग्रंथिभेद नहीं हुआ है, बल्कि वह मिथ्यात्व की भूमिका पर हि स्थित है ।
संसार में रहे किसी रूप, रस, गंध, स्पर्श अथवा शब्द का साक्षात्कार होने पर 'यह मेरी आत्मा के लिये हितकारी है अथवा अहितकारी ?" समझने की कला यदि हमें हस्तगत हो जाए, तब नि:संदेह हमारे भाव चारित्र और तत्त्व-परिणति की मंजिल दूर नहीं है । आत्म-परिणति के अविरत अभ्यास, चिन्तन-मनन से तत्त्व-परिणति युक्त ज्ञानोपार्जन होता है । अगर हमें आत्म-परिणति युक्त ज्ञान (ग्रंथिभेद से उत्पन्न ) प्राप्त हो गया है, तो फिर विविध शास्त्रों के बन्धनों का प्रयोजन ही क्या है ? शास्त्राभ्यास और पठन, चिन्तन ग्रंथिभेद के लिये ही किया जाता है । अतः ग्रंथिभेद के होते ही आत्मा में से ज्ञानप्रकाश प्रकट होता है । ज्ञानदम्भोलिशोभितः । निर्भय: शक्रवद् योगी, नन्दत्यानन्दनन्दने ||७||३६||
मिथ्यात्वशैलपक्षच्छिद्
अर्थ
: मिथ्यात्व रुपी पर्वत की चोटियों को छेदने वाले और ज्ञानरुपी वज्र से सुशोभित सर्वशक्तिमान इन्द्र की तरह निर्भय योगी सदैव प्रानंद रुपी नन्दनवन में केलि-क्रीड़ा करता है, सुखों का अनुभव करता है । विवेचन: देवराज इन्द्र को भला भय कैसा ? जिसके पास असीम आकाश की क्षितिजों को पार करने वाला, उत्तुंग पर्वत शिखरों को चूर-चूर करने में शक्तितशाली वज्र जैसा सर्वोच्च शस्त्र है, उसे भला किस बात का डर ? वह तो सदा सर्वदा स्वर्गीय आनन्द के नन्दन-वन में केलि करता रहता है । उसका चित्त प्रायः निर्भय और अभ्रान्त होता है ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org