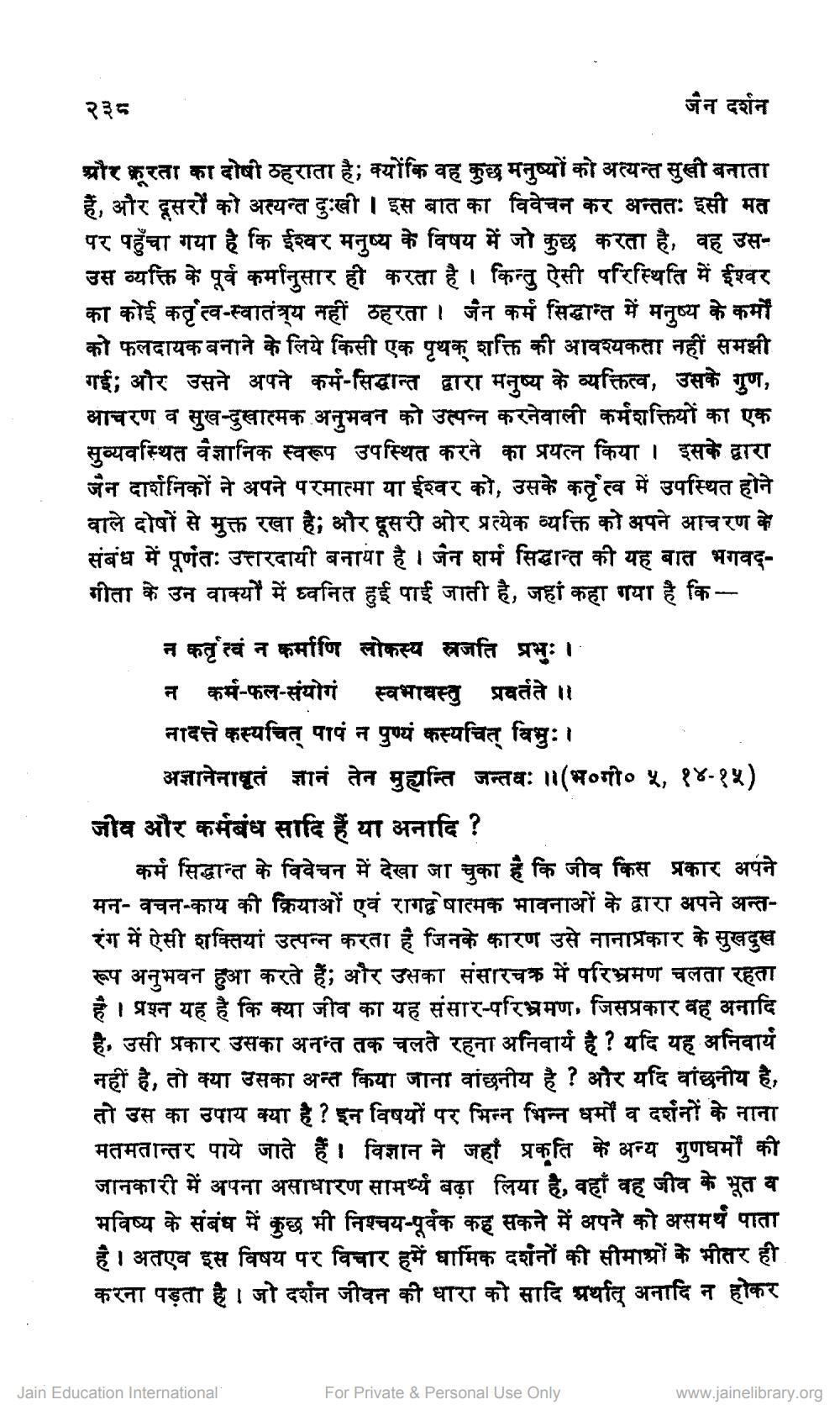________________
२३८
जैन दर्शन
और क्रूरता का दोषी ठहराता है; क्योंकि वह कुछ मनुष्यों को अत्यन्त सुखी बनाता हैं, और दूसरों को अत्यन्त दुःखी । इस बात का विवेचन कर अन्ततः इसी मत पर पहुँचा गया है कि ईश्वर मनुष्य के विषय में जो कुछ करता है, वह उसउस व्यक्ति के पूर्व कर्मानुसार ही करता है। किन्तु ऐसी परिस्थिति में ईश्वर का कोई कर्तृत्व-स्वातंत्र्य नहीं ठहरता। जैन कर्म सिद्धान्त में मनुष्य के कर्मों को फलदायक बनाने के लिये किसी एक पृथक् शक्ति की आवश्यकता नहीं समझी गई; और उसने अपने कर्म-सिद्धान्त द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व, उसके गुण, आचरण व सुख-दुखात्मक अनुभवन को उत्पन्न करनेवाली कर्मशक्तियों का एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक स्वरूप उपस्थित करने का प्रयत्न किया। इसके द्वारा जैन दार्शनिकों ने अपने परमात्मा या ईश्वर को, उसके कर्तृत्व में उपस्थित होने वाले दोषों से मुक्त रखा है; और दूसरी ओर प्रत्येक व्यक्ति को अपने आचरण के संबंध में पूर्णतः उत्तरदायी बनाया है। जैन शर्म सिद्धान्त की यह बात भगवद्गीता के उन वाक्यों में ध्वनित हुई पाई जाती है, जहां कहा गया है कि
न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य स्रजति प्रभुः। न कर्म-फल-संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ।। नादत्ते कस्यचित् पापं न पुण्यं कस्यचित् विभुः।
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥(भ०गी० ५, १४-१५) जीव और कर्मबंध सादि हैं या अनादि ?
कर्म सिद्धान्त के विवेचन में देखा जा चुका है कि जीव किस प्रकार अपने मन-वचन-काय की क्रियाओं एवं रागद्वेषात्मक भावनाओं के द्वारा अपने अन्तरंग में ऐसी शक्तियां उत्पन्न करता है जिनके कारण उसे नानाप्रकार के सुखदुख रूप अनुभवन हुआ करते हैं; और उसका संसारचक्र में परिभ्रमण चलता रहता है । प्रश्न यह है कि क्या जीव का यह संसार-परिभ्रमण, जिसप्रकार वह अनादि है, उसी प्रकार उसका अनन्त तक चलते रहना अनिवार्य है ? यदि यह अनिवार्य नहीं है, तो क्या उसका अन्त किया जाना वांछनीय है ? और यदि वांछनीय है, तो उस का उपाय क्या है ? इन विषयों पर भिन्न भिन्न धर्मों व दर्शनों के नाना मतमतान्तर पाये जाते हैं। विज्ञान ने जहाँ प्रकति के अन्य गुणधर्मों की जानकारी में अपना असाधारण सामर्थ्य बढ़ा लिया है, वहाँ वह जीव के भूत व भविष्य के संबंध में कुछ भी निश्चय-पूर्वक कह सकने में अपने को असमर्थ पाता है। अतएव इस विषय पर विचार हमें धार्मिक दर्शनों की सीमाओं के भीतर ही करना पड़ता है । जो दर्शन जीवन की धारा को सादि अर्थात् अनादि न होकर
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org