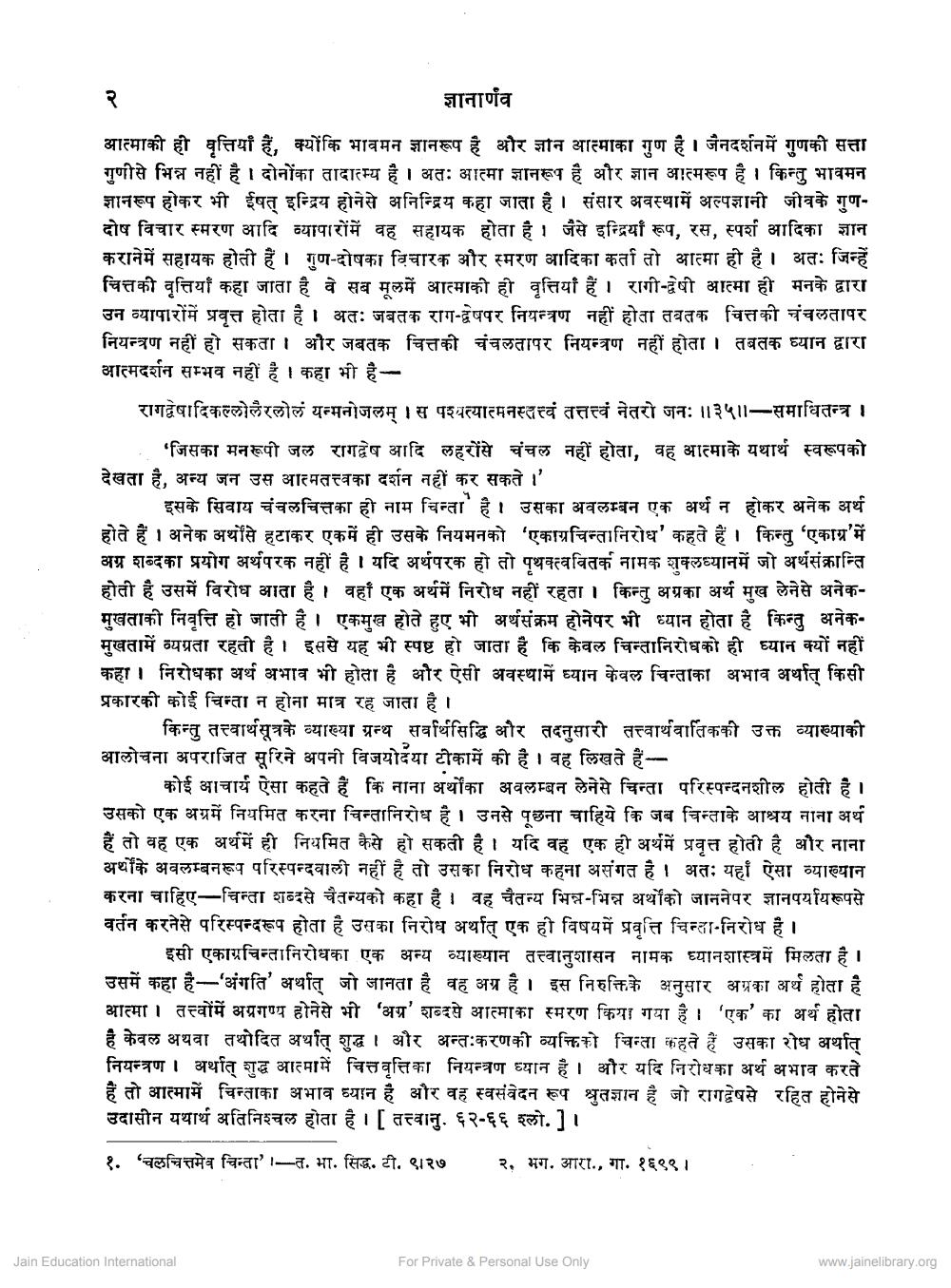________________
२
ज्ञानार्णव
आत्माकी हो वृत्तियाँ हैं, क्योंकि भावमन ज्ञानरूप है और ज्ञान आत्माका गुण है । जैनदर्शन में गुणकी सत्ता गुणीसे भिन्न नहीं है । दोनोंका तादात्म्य है । अतः आत्मा ज्ञानरूप है और ज्ञान आत्मरूप है । किन्तु भावमन ज्ञानरूप होकर भी ईषत् इन्द्रिय होनेसे अनिन्द्रिय कहा जाता है। संसार अवस्था में अल्पज्ञानी जीवके गुणदोष विचार स्मरण आदि व्यापारोंमें वह सहायक होता है। जैसे इन्द्रियाँ रूप, रस, स्पर्श आदिका ज्ञान कराने में सहायक होती हैं। गुण-दोषका विचारक और स्मरण आदिका कर्ता तो आत्मा ही है। अतः जिन्हें चित्तको वृत्तियाँ कहा जाता है वे सब मूलमें आत्माकी हो वृत्तियाँ हैं। रागी-द्वेषी आत्मा ही मनके द्वारा उन व्यापारोंमें प्रवृत्त होता है । अतः जबतक राग-द्वेषपर नियन्त्रण नहीं होता तबतक चित्त की चंचलतापर नियन्त्रण नहीं हो सकता। और जबतक चित्तकी चंचलतापर नियन्त्रण नहीं होता तबतक ध्यान द्वारा आत्मदर्शन सम्भव नहीं है। कहा भी है
रागद्वेषादिकल्लोलोलं यन्मनोजलम् । स पश्यत्यात्मनस्तत्वं तत्तत्वं नेतरो जनः ॥ ३५ ॥ - समाधितन्त्र
'जिसका मनरूपी जल रागद्वेष आदि लहरोंसे चंचल नहीं होता, वह आत्माके यथार्थ स्वरूपको देखता है, अन्य जन उस आत्मतत्त्वका दर्शन नहीं कर सकते ।'
इसके सिवाय चंचलचित्तका ही नाम चिन्ता' है। उसका अवलम्बन एक अर्थ न होकर अनेक अर्थ होते हैं । अनेक अर्थोंसे हटाकर एक में ही उसके नियमनको 'एकाग्रचिन्ता निरोध' कहते हैं । किन्तु 'एकाग्र ' में अग्रशब्दका प्रयोग अर्थपरक नहीं है। यदि अर्थपरक हो तो पृथक्त्ववितर्क नामक शुक्लध्यानमें जो अर्थसंक्रान्ति होती है उसमें विरोध आता है। वहीं एक अर्थमें निशेष नहीं रहता । किन्तु अग्रका अर्थ मुख लेनेसे अनेक। मुखताकी निवृत्ति हो जाती है। एकमुख होते हुए भी अर्थसंक्रम होनेपर भी ध्यान होता है किन्तु अनेकमुखतामें व्यग्रता रहती है । इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि केवल चिन्तानिरोधको ही ध्यान क्यों नहीं कहा। निरोधका अर्थ अभाव भी होता है और ऐसी अवस्था में ध्यान केवल चिन्ताका अभाव अर्थात् किसी प्रकारकी कोई चिन्ता न होना मात्र रह जाता है ।
किन्तु तत्त्वार्थ सूत्र के व्याख्या ग्रन्थ सर्वार्थसिद्धि और तदनुसारी तत्त्वार्थवार्तिकको उक्त व्याख्याको आलोचना अपराजित सूरिने अपनी विजयोदया टोकामें की है। वह लिखते हैं
कोई आचार्य ऐसा कहते हैं कि नाना अर्थोंका अवलम्बन लेनेसे चिन्ता परिस्पन्दनशील होती है । उसको एक अग्रमें नियमित करना चिन्तानिरोध है। उनसे पूछना चाहिये कि जब चिन्ताके आश्रय नाना अर्थ हैं तो वह एक अर्थ में ही नियमित कैसे हो सकती है । यदि वह एक ही अर्थ में प्रवृत्त होती है और नाना अर्थोके अवलम्बनरूप परिस्पन्दवाली नहीं है तो उसका निरोध कहना असंगत है। अतः यहाँ ऐसा व्याख्यान करना चाहिए - चिन्ता शब्दसे चैतन्यको कहा है। वह चैतन्य भिन्न-भिन्न अर्थोंको जानने पर ज्ञानपर्यायरूपसे वर्तन करनेसे परिस्पन्दरूप होता है उसका निरोध अर्थात् एक ही विषय में प्रवृत्ति चिन्हा निरोष है। इसी एकाग्रचिन्ता निरोधका एक अन्य व्याख्यान तत्त्वानुशासन नामक ध्यानशास्त्रमें मिलता है। उसमें कहा है- 'अंगति' अर्थात् जो जानता है वह अग्र है । इस निरुक्ति के अनुसार अग्रका अर्थ होता है आत्मा । तत्त्वोंमें अग्रगण्य होनेसे भी 'अग्र' शब्दसे आत्माका स्मरण किया गया है । 'एक' का अर्थ होता है केवल अथवा तयोदित अर्थात् शुद्ध और अन्तःकरणकी व्यक्तिको चिन्ता कहते हैं उसका रोष अर्थात् नियन्त्रण अर्थात् आत्मायें चित्तवृत्तिका नियन्त्रण ध्यान है और यदि निरोधका अर्थ अभाव करते हैं तो आत्मामें चिन्ताका अभाव ध्यान है और वह स्वसंवेदन रूप श्रुतज्ञान है जो रागद्वेषसे रहित होने से उदासीन यथार्थ अतिनिश्चल होता है । [ तत्त्वानु. ६२-६६ श्लो. ] 1
१. 'चलचित्तमेव चिन्ता' । त. भा. सिद्ध. टी. ९१२७ २. भग. आरा., गा. १६९९ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org