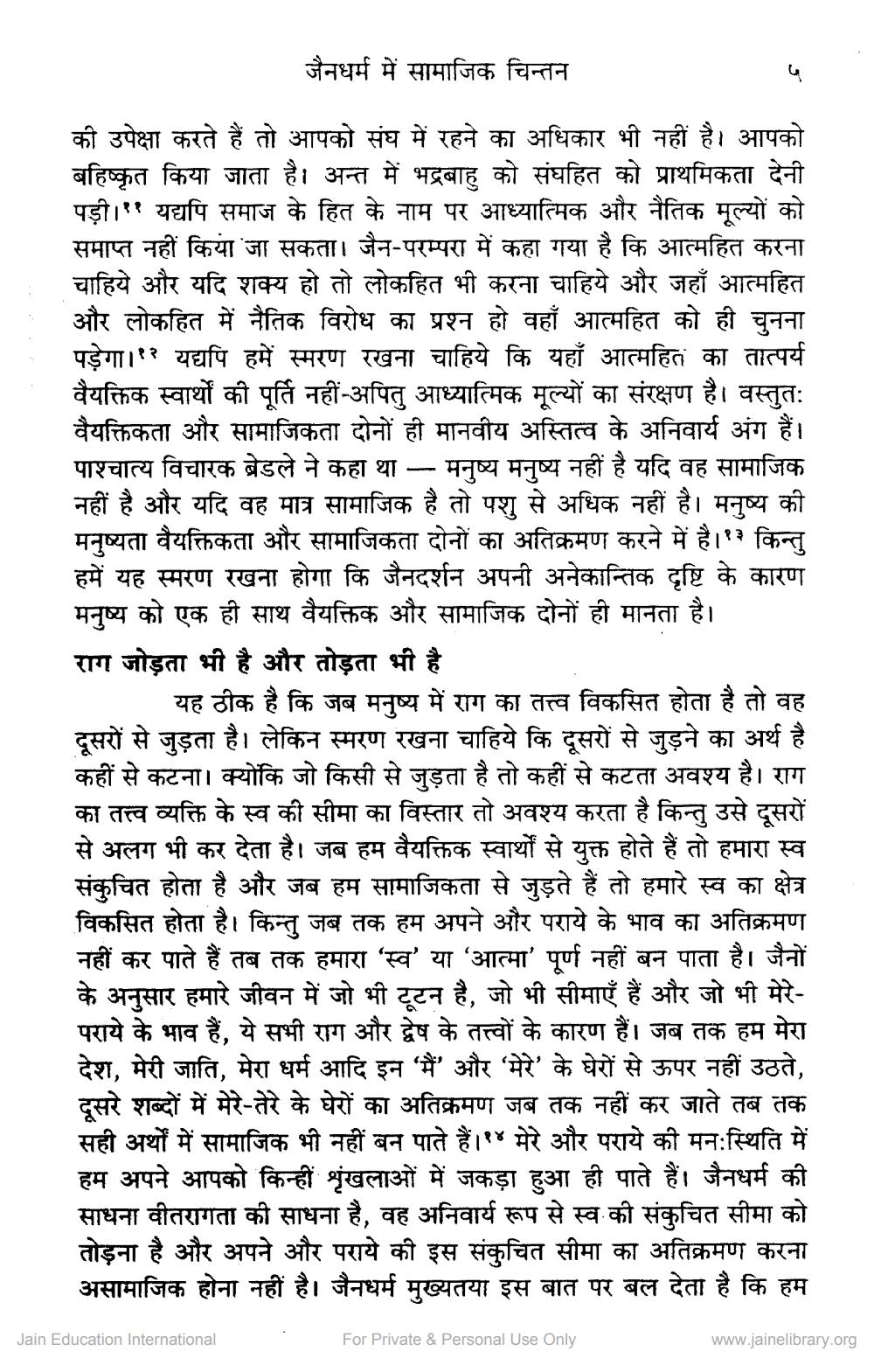________________
जैनधर्म में सामाजिक चिन्तन
की उपेक्षा करते हैं तो आपको संघ में रहने का अधिकार भी नहीं है। आपको बहिष्कृत किया जाता है। अन्त में भद्रबाह को संघहित को प्राथमिकता देनी पड़ी। यद्यपि समाज के हित के नाम पर आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को समाप्त नहीं किया जा सकता। जैन-परम्परा में कहा गया है कि आत्महित करना चाहिये और यदि शक्य हो तो लोकहित भी करना चाहिये और जहाँ आत्महित
और लोकहित में नैतिक विरोध का प्रश्न हो वहाँ आत्महित को ही चुनना पड़ेगा।१२ यद्यपि हमें स्मरण रखना चाहिये कि यहाँ आत्महित का तात्पर्य वैयक्तिक स्वार्थों की पूर्ति नहीं अपितु आध्यात्मिक मूल्यों का संरक्षण है। वस्तुत: वैयक्तिकता और सामाजिकता दोनों ही मानवीय अस्तित्व के अनिवार्य अंग हैं। पाश्चात्य विचारक ब्रेडले ने कहा था - मनुष्य मनुष्य नहीं है यदि वह सामाजिक नहीं है और यदि वह मात्र सामाजिक है तो पशु से अधिक नहीं है। मनुष्य की मनुष्यता वैयक्तिकता और सामाजिकता दोनों का अतिक्रमण करने में है। १३ किन्तु हमें यह स्मरण रखना होगा कि जैनदर्शन अपनी अनेकान्तिक दृष्टि के कारण मनुष्य को एक ही साथ वैयक्तिक और सामाजिक दोनों ही मानता है। राग जोड़ता भी है और तोड़ता भी है
यह ठीक है कि जब मनुष्य में राग का तत्त्व विकसित होता है तो वह दूसरों से जुड़ता है। लेकिन स्मरण रखना चाहिये कि दूसरों से जुड़ने का अर्थ है कहीं से कटना। क्योंकि जो किसी से जुड़ता है तो कहीं से कटता अवश्य है। राग का तत्त्व व्यक्ति के स्व की सीमा का विस्तार तो अवश्य करता है किन्तु उसे दूसरों से अलग भी कर देता है। जब हम वैयक्तिक स्वार्थों से युक्त होते हैं तो हमारा स्व संकुचित होता है और जब हम सामाजिकता से जुड़ते हैं तो हमारे स्व का क्षेत्र विकसित होता है। किन्तु जब तक हम अपने और पराये के भाव का अतिक्रमण नहीं कर पाते हैं तब तक हमारा 'स्व' या 'आत्मा' पूर्ण नहीं बन पाता है। जैनों के अनुसार हमारे जीवन में जो भी टूटन है, जो भी सीमाएँ हैं और जो भी मेरेपराये के भाव हैं, ये सभी राग और द्वेष के तत्त्वों के कारण हैं। जब तक हम मेरा देश, मेरी जाति, मेरा धर्म आदि इन 'मैं' और 'मेरे' के घेरों से ऊपर नहीं उठते, दूसरे शब्दों में मेरे-तेरे के घेरों का अतिक्रमण जब तक नहीं कर जाते तब तक सही अर्थों में सामाजिक भी नहीं बन पाते हैं।१४ मेरे और पराये की मन:स्थिति में हम अपने आपको किन्हीं श्रृंखलाओं में जकड़ा हुआ ही पाते हैं। जैनधर्म की साधना वीतरागता की साधना है, वह अनिवार्य रूप से स्व की संकुचित सीमा को तोड़ना है और अपने और पराये की इस संकुचित सीमा का अतिक्रमण करना असामाजिक होना नहीं है। जैनधर्म मुख्यतया इस बात पर बल देता है कि हम
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org