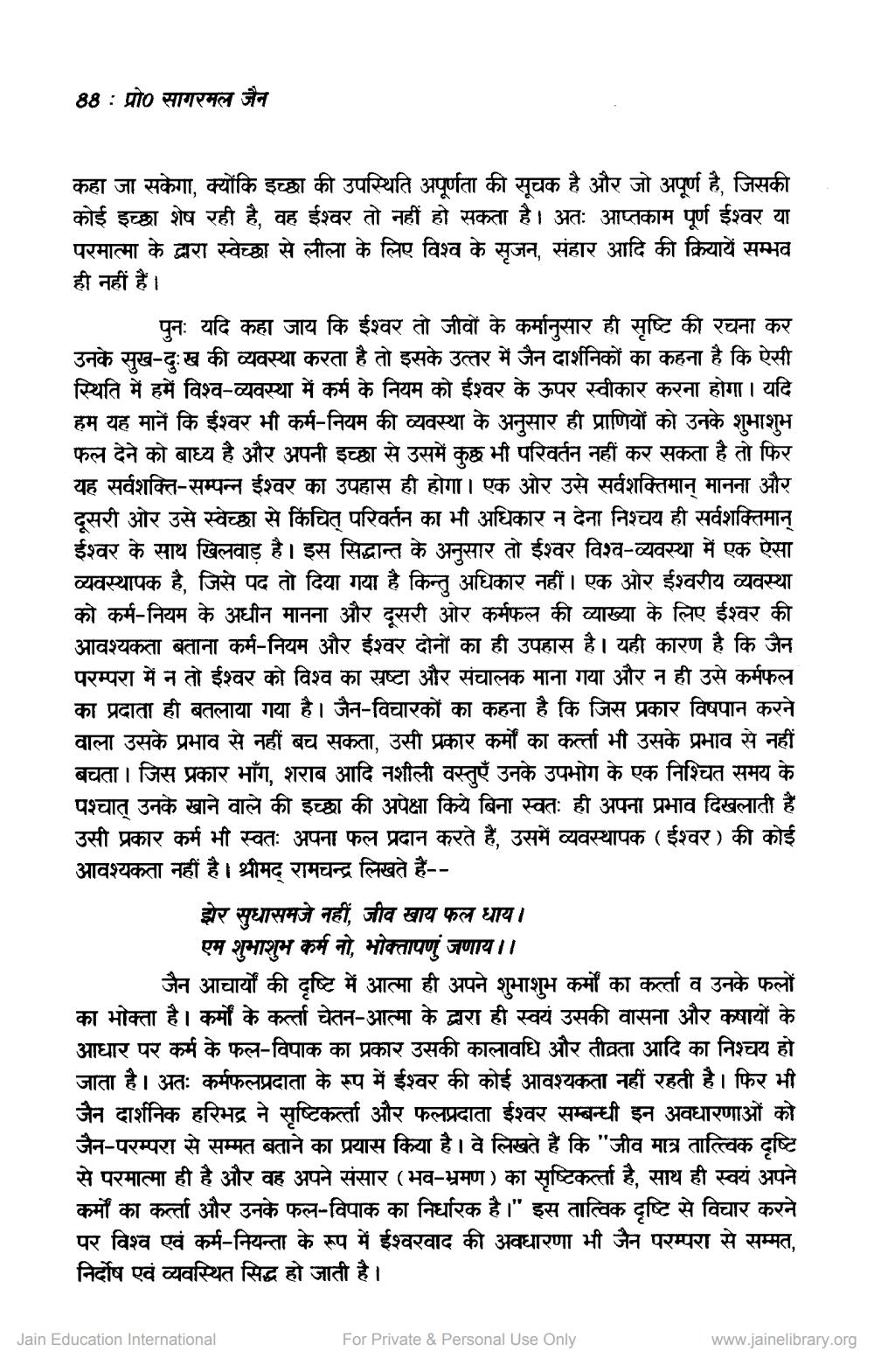________________
88 : प्रो० सागरमल जैन
कहा जा सकेगा, क्योंकि इच्छा की उपस्थिति अपूर्णता की सूचक है और जो अपूर्ण है, जिसकी कोई इच्छा शेष रही है, वह ईश्वर तो नहीं हो सकता है। अतः आप्तकाम पूर्ण ईश्वर या परमात्मा के द्वारा स्वेच्छा से लीला के लिए विश्व के सृजन, संहार आदि की क्रियायें सम्भव ही नहीं हैं।
पुनः यदि कहा जाय कि ईश्वर तो जीवों के कर्मानुसार ही सृष्टि की रचना कर उनके सुख-दुःख की व्यवस्था करता है तो इसके उत्तर में जैन दार्शनिकों का कहना है कि ऐसी स्थिति में हमें विश्व-व्यवस्था में कर्म के नियम को ईश्वर के ऊपर स्वीकार करना होगा। यदि हम यह मानें कि ईश्वर भी कर्म-नियम की व्यवस्था के अनुसार ही प्राणियों को उनके शुभाशुभ फल देने को बाध्य है और अपनी इच्छा से उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता है तो फिर यह सर्वशक्ति-सम्पन्न ईश्वर का उपहास ही होगा। एक ओर उसे सर्वशक्तिमान् मानना और दूसरी ओर उसे स्वेच्छा से किंचित् परिवर्तन का भी अधिकार न देना निश्चय ही सर्वशक्तिमान् ईश्वर के साथ खिलवाड़ है। इस सिद्धान्त के अनुसार तो ईश्वर विश्व-व्यवस्था में एक ऐसा व्यवस्थापक है, जिसे पद तो दिया गया है किन्तु अधिकार नहीं। एक ओर ईश्वरीय व्यवस्था को कर्म-नियम के अधीन मानना और दूसरी ओर कर्मफल की व्याख्या के लिए ईश्वर की आवश्यकता बताना कर्म-नियम और ईश्वर दोनों का ही उपहास है। यही कारण है कि जैन परम्परा में न तो ईश्वर को विश्व का स्रष्टा और संचालक माना गया और न ही उसे कर्मफल का प्रदाता ही बतलाया गया है। जैन-विचारकों का कहना है कि जिस प्रकार विषपान करने वाला उसके प्रभाव से नहीं बच सकता, उसी प्रकार कर्मों का कर्ता भी उसके प्रभाव से नहीं बचता। जिस प्रकार भाँग, शराब आदि नशीली वस्तुएँ उनके उपभोग के एक निश्चित समय के पश्चात् उनके खाने वाले की इच्छा की अपेक्षा किये बिना स्वतः ही अपना प्रभाव दिखलाती है उसी प्रकार कर्म भी स्वतः अपना फल प्रदान करते हैं, उसमें व्यवस्थापक (ईश्वर) की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् रामचन्द्र लिखते हैं--
झेर सुधासमजे नहीं, जीव खाय फल धाय। एम शुभाशुभ कर्म नो, भोक्तापणुंजणाय।।
जैन आचार्यों की दृष्टि में आत्मा ही अपने शुभाशुभ कर्मों का कर्ता व उनके फलों का भोक्ता है। कर्मों के कर्ता चेतन-आत्मा के द्वारा ही स्वयं उसकी वासना और कषायों के आधार पर कर्म के फल-विपाक का प्रकार उसकी कालावधि और तीव्रता आदि का निश्चय हो जाता है। अतः कर्मफलप्रदाता के रूप में ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। फिर भी जैन दार्शनिक हरिभद्र ने सृष्टिकर्ता और फलप्रदाता ईश्वर सम्बन्धी इन अवधारणाओं को जैन-परम्परा से सम्मत बताने का प्रयास किया है। वे लिखते हैं कि "जीव मात्र तात्त्विक दृष्टि से परमात्मा ही है और वह अपने संसार (भव-भ्रमण) का सृष्टिकर्ता है, साथ ही स्वयं अपने कर्मों का कर्ता और उनके फल-विपाक का निर्धारक है।" इस तात्विक दष्टि से विचार करने पर विश्व एवं कर्म-नियन्ता के रूप में ईश्वरवाद की अवधारणा भी जैन परम्परा से सम्मत, निर्दोष एवं व्यवस्थित सिद्ध हो जाती है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org