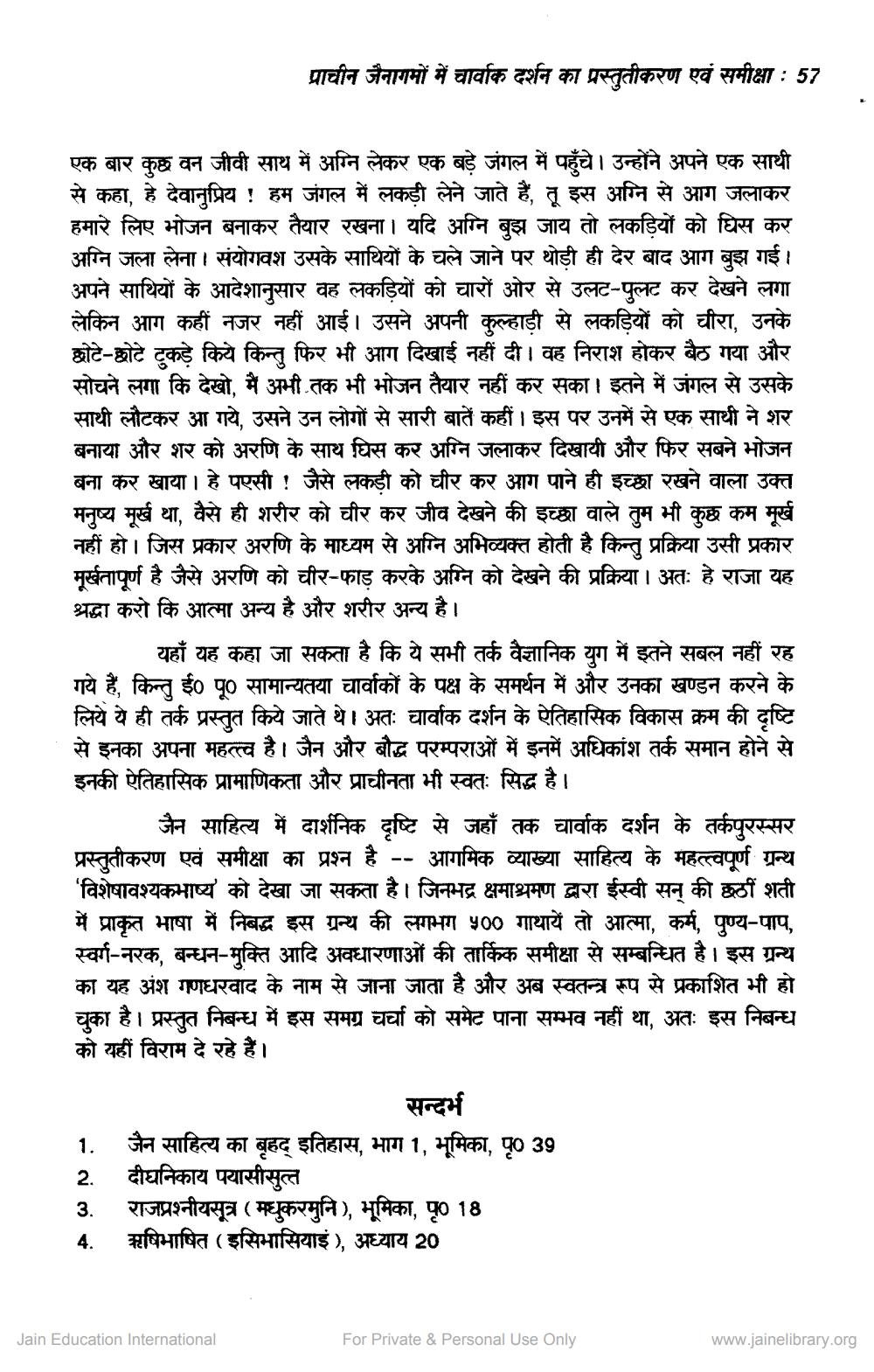________________
प्राचीन जैनागमों में चार्वाक दर्शन का प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा : 57
एक बार कुछ वन जीवी साथ में अग्नि लेकर एक बड़े जंगल में पहुंचे। उन्होंने अपने एक साथी से कहा, हे देवानुप्रिय ! हम जंगल में लकड़ी लेने जाते हैं, तू इस अग्नि से आग जलाकर हमारे लिए भोजन बनाकर तैयार रखना। यदि अग्नि बुझ जाय तो लकड़ियों को घिस कर अग्नि जला लेना। संयोगवश उसके साथियों के चले जाने पर थोड़ी ही देर बाद आग बझ गई। अपने साथियों के आदेशानुसार वह लकड़ियों को चारों ओर से उलट-पुलट कर देखने लगा लेकिन आग कहीं नजर नहीं आई। उसने अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियों को चीरा, उनके छोटे-छोटे टुकड़े किये किन्तु फिर भी आग दिखाई नहीं दी। वह निराश होकर बैठ गया और सोचने लगा कि देखो, मैं अभी तक भी भोजन तैयार नहीं कर सका। इतने में जंगल से उसके साथी लौटकर आ गये, उसने उन लोगों से सारी बातें कहीं। इस पर उनमें से एक साथी ने शर बनाया और शर को अरणि के साथ घिस कर अग्नि जलाकर दिखायी और फिर सबने भोजन बना कर खाया। हे पएसी ! जैसे लकडी को चीर कर आग पाने ही इच्छा रखने वाला उक्त मनुष्य मूर्ख था, वैसे ही शरीर को चीर कर जीव देखने की इच्छा वाले तुम भी कुछ कम मूर्ख नहीं हो। जिस प्रकार अरणि के माध्यम से अग्नि अभिव्यक्त होती है किन्तु प्रक्रिया उसी प्रकार मूर्खतापूर्ण है जैसे अरणि को चीर-फाड़ करके अग्नि को देखने की प्रक्रिया। अतः हे राजा यह श्रद्धा करो कि आत्मा अन्य है और शरीर अन्य है।
यहाँ यह कहा जा सकता है कि ये सभी तर्क वैज्ञानिक युग में इतने सबल नहीं रह गये हैं, किन्तु ई0 पू0 सामान्यतया चार्वाकों के पक्ष के समर्थन में और उनका खण्डन करने के लिये ये ही तर्क प्रस्तुत किये जाते थे। अतः चार्वाक दर्शन के ऐतिहासिक विकास क्रम की दृष्टि से इनका अपना महत्त्व है। जैन और बौद्ध परम्पराओं में इनमें अधिकांश तर्क समान होने से इनकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता और प्राचीनता भी स्वतः सिद्ध है।
जैन साहित्य में दार्शनिक दृष्टि से जहाँ तक चार्वाक दर्शन के तर्कपुरस्सर प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा का प्रश्न है -- आगमिक व्याख्या साहित्य के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'विशेषावश्यकभाष्य को देखा जा सकता है। जिनभद्र क्षमाश्रमण द्वारा ईस्वी सन् की छठीं शती में प्राकृत भाषा में निबद्ध इस ग्रन्थ की लगभग ५०० गाथायें तो आत्मा, कर्म, पुण्य-पाप, स्वर्ग-नरक, बन्धन-मुक्ति आदि अवधारणाओं की तार्किक समीक्षा से सम्बन्धित है। इस ग्रन्थ का यह अंश गणधरवाद के नाम से जाना जाता है और अब स्वतन्त्र रूप से प्रकाशित भी हो चुका है। प्रस्तुत निबन्ध में इस समग्र चर्चा को समेट पाना सम्भव नहीं था, अतः इस निबन्ध को यहीं विराम दे रहे हैं।
सन्दर्भ
1. जैन साहित्य का बृहद् इतिहास, भाग 1, भूमिका, पृ0 39 2. दीघनिकाय पयासीसुत्त 3. राजप्रश्नीयसूत्र (मधुकरमुनि), भूमिका, पृ0 18 4. ऋषिभाषित (इसिभासियाइं), अध्याय 20
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org