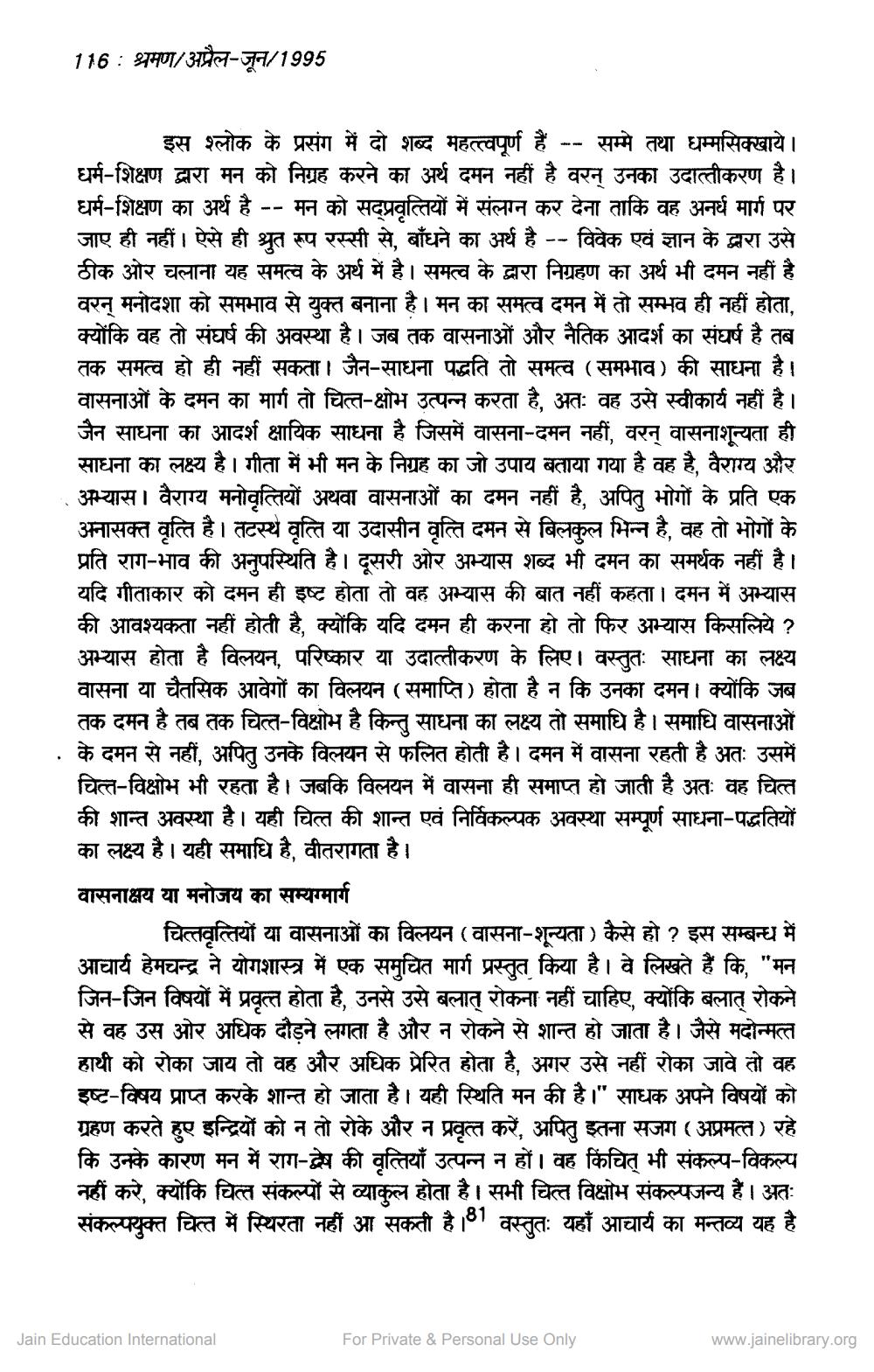________________
116 : श्रमण/अप्रैल-जून/1995
इस श्लोक के प्रसंग में दो शब्द महत्त्वपूर्ण हैं -- सम्मे तथा धम्मसिक्खाये। धर्म-शिक्षण द्वारा मन को निग्रह करने का अर्थ दमन नहीं है वरन् उनका उदात्तीकरण है। धर्म-शिक्षण का अर्थ है -- मन को सद्प्रवृत्तियों में संलग्न कर देना ताकि वह अनर्थ मार्ग पर जाए ही नहीं। ऐसे ही श्रुत रूप रस्सी से, बाँधने का अर्थ है -- विवेक एवं ज्ञान के द्वारा उसे ठीक ओर चलाना यह समत्व के अर्थ में है। समत्व के द्वारा निग्रहण का अर्थ भी दमन नहीं है वरन् मनोदशा को समभाव से युक्त बनाना है। मन का समत्व दमन में तो सम्भव ही नहीं होता, क्योंकि वह तो संघर्ष की अवस्था है। जब तक वासनाओं और नैतिक आदर्श का संघर्ष है तब तक समत्व हो ही नहीं सकता। जैन-साधना पद्धति तो समत्व (समभाव) की साधना है। वासनाओं के दमन का मार्ग तो चित्त-क्षोभ उत्पन्न करता है, अतः वह उसे स्वीकार्य नहीं है। जैन साधना का आदर्श क्षायिक साधना है जिसमें वासना-दमन नहीं, वरन् वासनाशून्यता ही साधना का लक्ष्य है। गीता में भी मन के निग्रह का जो उपाय बताया गया है वह है, वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य मनोवृत्तियों अथवा वासनाओं का दमन नहीं है, अपितु भोगों के प्रति एक अनासक्त वृत्ति है। तटस्थ वृत्ति या उदासीन वृत्ति दमन से बिलकुल भिन्न है, वह तो भोगों के प्रति राग-भाव की अनुपस्थिति है। दूसरी ओर अभ्यास शब्द भी दमन का समर्थक नहीं है। यदि गीताकार को दमन ही इष्ट होता तो वह अभ्यास की बात नहीं कहता। दमन में अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यदि दमन ही करना हो तो फिर अभ्यास किसलिये ? अभ्यास होता है विलयन, परिष्कार या उदात्तीकरण के लिए। वस्तुतः साधना का लक्ष्य वासना या चैतसिक आवेगों का विलयन (समाप्ति) होता है न कि उनका दमन। क्योंकि जब तक दमन है तब तक चित्त-विक्षोभ है किन्तु साधना का लक्ष्य तो समाधि है। समाधि वासनाओं के दमन से नहीं, अपितु उनके विलयन से फलित होती है। दमन में वासना रहती है अतः उसमें चित्त-विक्षोभ भी रहता है। जबकि विलयन में वासना ही समाप्त हो जाती है अतः वह चित्त की शान्त अवस्था है। यही चित्त की शान्त एवं निर्विकल्पक अवस्था सम्पूर्ण साधना-पद्धतियों का लक्ष्य है। यही समाधि है, वीतरागता है। वासनाक्षय या मनोजय का सम्यग्मार्ग
चित्तवृत्तियों या वासनाओं का विलयन (वासना-शून्यता) कैसे हो? इस सम्बन्ध में आचार्य हेमचन्द्र ने योगशास्त्र में एक समुचित मार्ग प्रस्तुत किया है। वे लिखते हैं कि, "मन जिन-जिन विषयों में प्रवृत्त होता है, उनसे उसे बलात् रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि बलात् रोकने से वह उस ओर अधिक दौड़ने लगता है और न रोकने से शान्त हो जाता है। जैसे मदोन्मत्त हाथी को रोका जाय तो वह और अधिक प्रेरित होता है, अगर उसे नहीं रोका जावे तो वह इष्ट-विषय प्राप्त करके शान्त हो जाता है। यही स्थिति मन की है।" साधक अपने विषयों को ग्रहण करते हुए इन्द्रियों को न तो रोके और न प्रवृत्त करें, अपितु इतना सजग (अप्रमत्त) रहे कि उनके कारण मन में राग-द्वेष की वृत्तियाँ उत्पन्न न हों। वह किंचित् भी संकल्प-विकल्प नहीं करे, क्योंकि चित्त संकल्पों से व्याकुल होता है। सभी चित्त विक्षोभ संकल्पजन्य है। अतः संकल्पयुक्त चित्त में स्थिरता नहीं आ सकती है।81 वस्तुतः यहाँ आचार्य का मन्तव्य यह है
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org