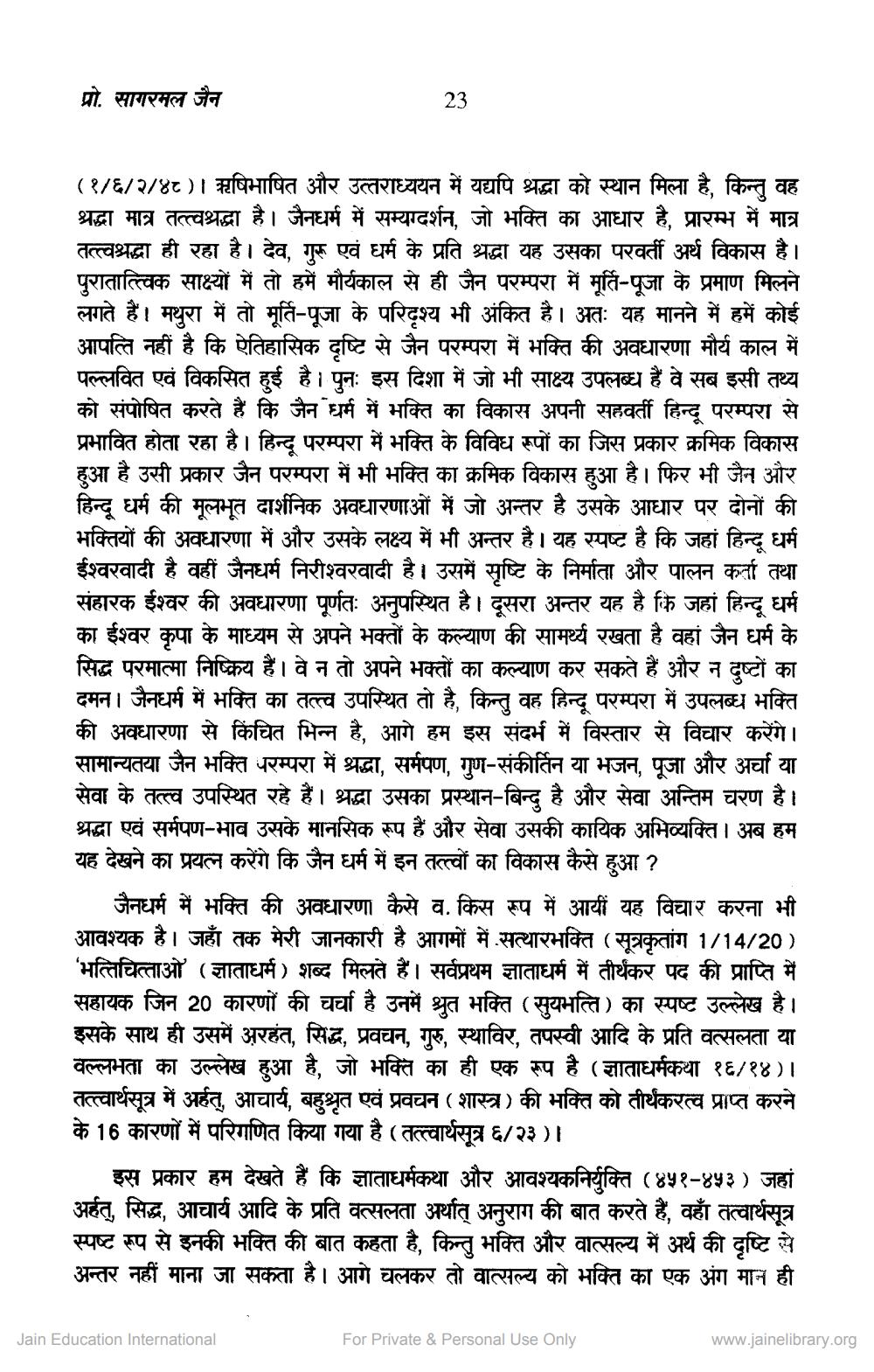________________
प्रो. सागरमल जैन
23
(१/६/२/४८ ) । ऋषिभाषित और उत्तराध्ययन में यद्यपि श्रद्धा को स्थान मिला है, किन्तु वह श्रद्धा मात्र तत्त्वश्रद्धा है। जैनधर्म में सम्यग्दर्शन, जो भक्ति का आधार है, प्रारम्भ में मात्र तत्त्वश्रद्धा ही रहा है। देव, गुरू एवं धर्म के प्रति श्रद्धा यह उसका परवर्ती अर्थ विकास है। पुरातात्त्विक साक्ष्यों में तो हमें मौर्यकाल से ही जैन परम्परा में मूर्ति-पूजा के प्रमाण मिलने लगते हैं। मथुरा में तो मूर्ति-पूजा के परिदृश्य भी अंकित है। अतः यह मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है कि ऐतिहासिक दृष्टि से जैन परम्परा में भक्ति की अवधारणा मौर्य काल में पल्लवित एवं विकसित हुई है। पुनः इस दिशा में जो भी साक्ष्य उपलब्ध हैं वे सब इसी तथ्य को संपोषित करते हैं कि जैन धर्म में भक्ति का विकास अपनी सहवर्ती हिन्दू परम्परा से प्रभावित होता रहा है। हिन्दू परम्परा में भक्ति के विविध रूपों का जिस प्रकार क्रमिक विकास हुआ है उसी प्रकार जैन परम्परा में भी भक्ति का क्रमिक विकास हुआ है। फिर भी जैन और हिन्दू धर्म की मूलभूत दार्शनिक अवधारणाओं में जो अन्तर है उसके आधार पर दोनों की भक्तियों की अवधारणा में और उसके लक्ष्य में भी अन्तर है । यह स्पष्ट है कि जहां हिन्दू धर्म ईश्वरवादी है वहीं जैनधर्म निरीश्वरवादी है । उसमें सृष्टि के निर्माता और पालन कर्ता तथा संहारक ईश्वर की अवधारणा पूर्णतः अनुपस्थित है। दूसरा अन्तर यह है कि जहां हिन्दू धर्म का ईश्वर कृपा के माध्यम से अपने भक्तों के कल्याण की सामर्थ्य रखता है वहां जैन धर्म के सिद्ध परमात्मा निष्क्रिय हैं। वे न तो अपने भक्तों का कल्याण कर सकते हैं और न दुष्टों का दमन । जैनधर्म में भक्ति का तत्त्व उपस्थित तो है, किन्तु वह हिन्दू परम्परा में उपलब्ध भक्ति की अवधारणा से किंचित भिन्न है, आगे हम इस संदर्भ में विस्तार से विचार करेंगे । सामान्यतया जैन भक्ति परम्परा में श्रद्धा, सर्मपण, गुण-संकीर्तिन या भजन, पूजा और अर्चा या सेवा के तत्त्व उपस्थित रहे हैं। श्रद्धा उसका प्रस्थान - बिन्दु है और सेवा अन्तिम चरण है । श्रद्धा एवं सर्मपण-भाव उसके मानसिक रूप हैं और सेवा उसकी कायिक अभिव्यक्ति । अब हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि जैन धर्म में इन तत्त्वों का विकास कैसे हुआ ?
जैनधर्म में भक्ति की अवधारणा कैसे व किस रूप में आयीं यह विचार करना भी आवश्यक है। जहाँ तक मेरी जानकारी है आगमों में सत्थारभक्ति (सूत्रकृतांग 1 / 14 / 20 ) 'भत्तिचित्ताओं' (ज्ञाताधर्म) शब्द मिलते हैं। सर्वप्रथम ज्ञाताधर्म में तीर्थंकर पद की प्राप्ति में सहायक जिन 20 कारणों की चर्चा है उनमें श्रुत भक्ति (सुयभत्ति) का स्पष्ट उल्लेख है । इसके साथ ही उसमें अरहंत, सिद्ध, प्रवचन, गुरु, स्थाविर, तपस्वी आदि के प्रति वत्सलता या वल्लभता का उल्लेख हुआ है, जो भक्ति का ही एक रूप है ( ज्ञाताधर्मकथा १६ / १४ ) । तत्त्वार्थसूत्र में अर्हत, आचार्य, बहुश्रुत एवं प्रवचन (शास्त्र) की भक्ति को तीर्थंकरत्व प्राप्त करने के 16 कारणों में परिगणित किया गया है (तत्त्वार्थसूत्र ६ / २३ ) ।
इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञाताधर्मकथा और आवश्यकनिर्युक्ति ( ४५१ - ४५३ ) जहां अर्हतु, सिद्ध, आचार्य आदि के प्रति वत्सलता अर्थात् अनुराग की बात करते हैं, वहाँ तत्वार्थसूत्र स्पष्ट रूप से इनकी भक्ति की बात कहता है, किन्तु भक्ति और वात्सल्य में अर्थ की दृष्टि से अन्तर नहीं माना जा सकता है। आगे चलकर तो वात्सल्य को भक्ति का एक अंग मान ही
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org