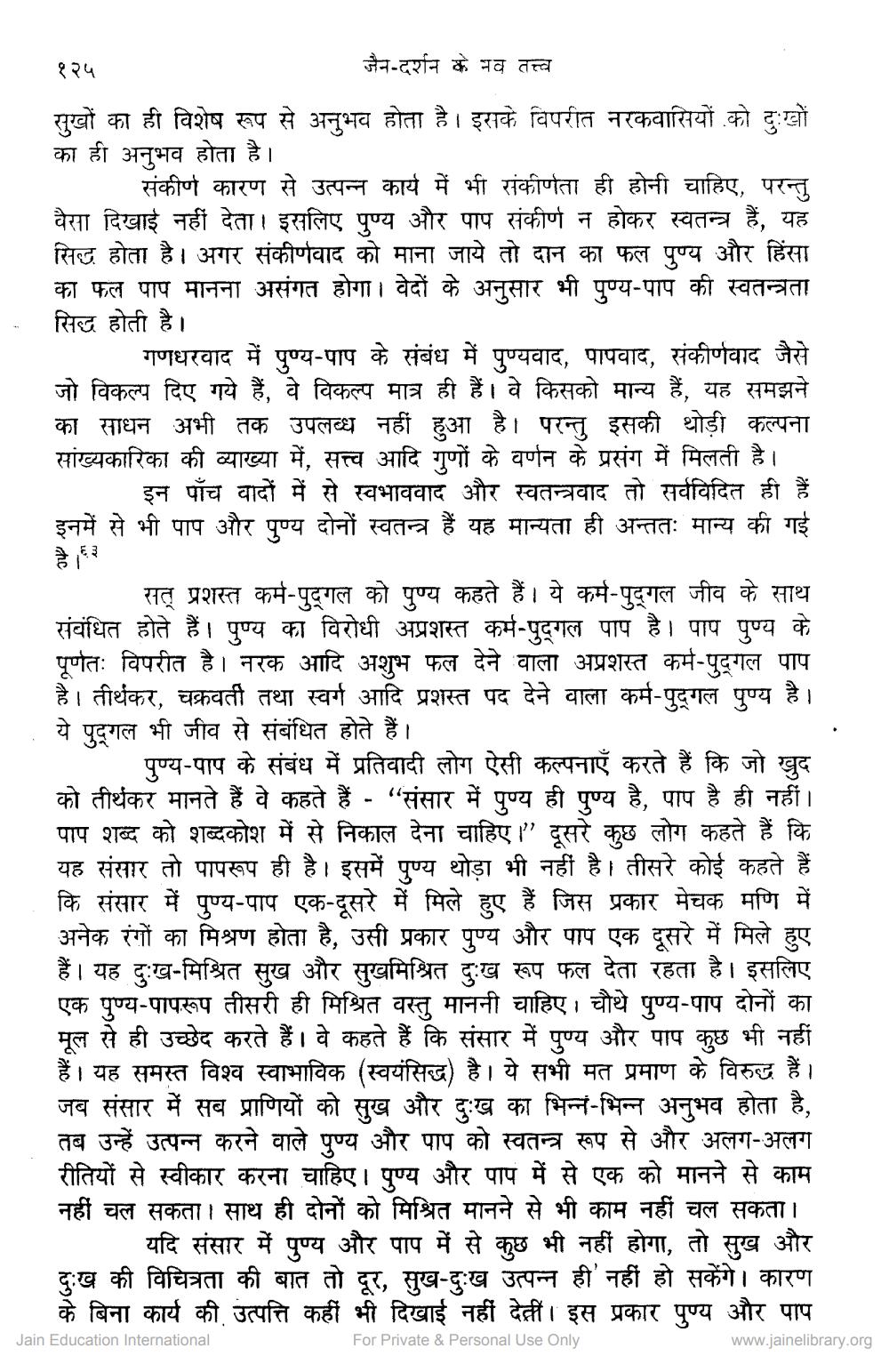________________
१२५
जैन-दर्शन के नव तत्त्व सुखों का ही विशेष रूप से अनुभव होता है। इसके विपरीत नरकवासियों को दुःखों का ही अनुभव होता है।
संकीर्ण कारण से उत्पन्न कार्य में भी संकीर्णता ही होनी चाहिए, परन्तु वैसा दिखाई नहीं देता। इसलिए पुण्य और पाप संकीर्ण न होकर स्वतन्त्र हैं, यह सिद्ध होता है। अगर संकीर्णवाद को माना जाये तो दान का फल पुण्य और हिंसा
का फल पाप मानना असंगत होगा। वेदों के अनुसार भी पुण्य-पाप की स्वतन्त्रता सिद्ध होती है।
गणधरवाद में पुण्य-पाप के संबंध में पुण्यवाद, पापवाद, संकीर्णवाद जैसे जो विकल्प दिए गये हैं, वे विकल्प मात्र ही हैं। वे किसको मान्य हैं, यह समझने का साधन अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। परन्तु इसकी थोड़ी कल्पना सांख्यकारिका की व्याख्या में, सत्त्व आदि गुणों के वर्णन के प्रसंग में मिलती है।
इन पाँच वादों में से स्वभाववाद और स्वतन्त्रवाद तो सर्वविदित ही हैं इनमें से भी पाप और पुण्य दोनों स्वतन्त्र हैं यह मान्यता ही अन्ततः मान्य की गई
सत् प्रशस्त कर्म-पुद्गल को पुण्य कहते हैं। ये कर्म-पुद्गल जीव के साथ संबंधित होते हैं। पुण्य का विरोधी अप्रशस्त कर्म-पुद्गल पाप है। पाप पुण्य के पूर्णतः विपरीत है। नरक आदि अशुभ फल देने वाला अप्रशस्त कर्म-पुद्गल पाप है। तीर्थकर, चक्रवर्ती तथा स्वर्ग आदि प्रशस्त पद देने वाला कर्म-पुद्गल पुण्य है। ये पुद्गल भी जीव से संबंधित होते हैं।
___ पुण्य-पाप के संबंध में प्रतिवादी लोग ऐसी कल्पनाएँ करते हैं कि जो खुद को तीर्थकर मानते हैं वे कहते हैं - “संसार में पुण्य ही पुण्य है, पाप है ही नहीं। पाप शब्द को शब्दकोश में से निकाल देना चाहिए।" दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार तो पापरूप ही है। इसमें पुण्य थोड़ा भी नहीं है। तीसरे कोई कहते हैं कि संसार में पुण्य-पाप एक-दूसरे में मिले हुए हैं जिस प्रकार मेचक मणि में अनेक रंगों का मिश्रण होता है, उसी प्रकार पुण्य और पाप एक दूसरे में मिले हुए हैं। यह दुःख-मिश्रित सुख और सुखमिश्रित दुःख रूप फल देता रहता है। इसलिए एक पुण्य-पापरूप तीसरी ही मिश्रित वस्तु माननी चाहिए। चौथे पुण्य-पाप दोनों का मूल से ही उच्छेद करते हैं। वे कहते हैं कि संसार में पुण्य और पाप कुछ भी नहीं हैं। यह समस्त विश्व स्वाभाविक (स्वयंसिद्ध) है। ये सभी मत प्रमाण के विरुद्ध हैं। जब संसार में सब प्राणियों को सुख और दुःख का भिन्न-भिन्न अनुभव होता है, तब उन्हें उत्पन्न करने वाले पुण्य और पाप को स्वतन्त्र रूप से और अलग-अलग रीतियों से स्वीकार करना चाहिए। पुण्य और पाप में से एक को मानने से काम नहीं चल सकता। साथ ही दोनों को मिश्रित मानने से भी काम नहीं चल सकता।
यदि संसार में पुण्य और पाप में से कुछ भी नहीं होगा, तो सुख और दुःख की विचित्रता की बात तो दूर, सुख-दुःख उत्पन्न ही नहीं हो सकेंगे। कारण
के बिना कार्य की उत्पत्ति कहीं भी दिखाई नहीं देतीं। इस प्रकार पुण्य और पाप Jain Education International For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org