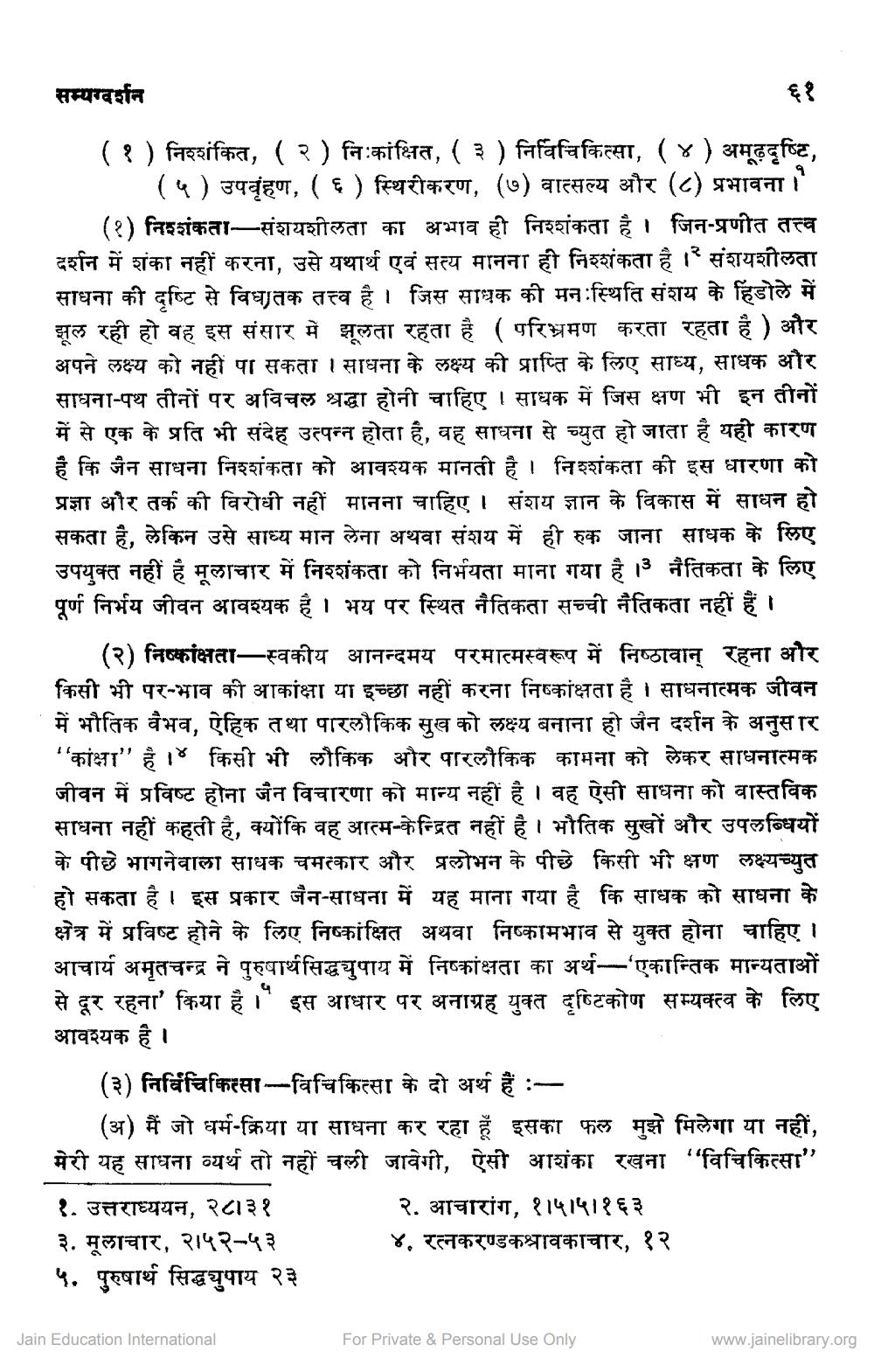________________
सम्यग्दर्शन
( १ ) निरशंकित, ( २ ) नि:कांक्षित, ( ३ ) निर्विचिकित्सा, ( ४ ) अमूढदृष्टि, (५) उपबृंहण, ( ६ ) स्थिरीकरण, (७) वात्सल्य और (८) प्रभावना i
(१) निश्शंकता - संशयशीलता का अभाव ही निश्शंकता है । जिन प्रणीत तत्त्व दर्शन में शंका नहीं करना, उसे यथार्थ एवं सत्य मानना हो निश्शंकता है । संशयशीलता साधना की दृष्टि से विधातक तत्त्व है । जिस साधक की मनःस्थिति संशय के हिंडोले में झूल रही हो वह इस संसार में झूलता रहता है ( परिभ्रमण करता रहता है ) और अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता । साधना के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साध्य, साधक और साधना-पथ तीनों पर अविचल श्रद्धा होनी चाहिए । साधक में जिस क्षण भी इन तीनों में से एक के प्रति भी संदेह उत्पन्न होता है, वह साधना से च्युत हो जाता है यही कारण है कि जैन साधना निश्शंकता को आवश्यक मानती है । निश्शंकता की इस धारणा को प्रज्ञा और तर्क की विरोधी नहीं मानना चाहिए । संशय ज्ञान के विकास में साधन हो सकता है, लेकिन उसे साध्य मान लेना अथवा संशय में ही रुक जाना साधक के लिए उपयुक्त नहीं है मूलाचार में निश्शंकता को निर्भयता माना गया है । 3 नैतिकता के लिए पूर्ण निर्भय जीवन आवश्यक है । भय पर स्थित नैतिकता सच्ची नैतिकता नहीं हैं ।
(२) निष्कांक्षता - स्वकीय आनन्दमय परमात्मस्वरूप में निष्ठावान् रहना और किसी भी पर-भाव की आकांक्षा या इच्छा नहीं करना निष्कांक्षता है । साधनात्मक जीवन में भौतिक वैभव, ऐहिक तथा पारलौकिक सुख को लक्ष्य बनाना हो जैन दर्शन के अनुसार "कांक्षा" है । किसी भी लौकिक और पारलौकिक कामना को लेकर साधनात्मक जीवन में प्रविष्ट होना जैन विचारणा को मान्य नहीं है । वह ऐसी साधना को वास्तविक साधना नहीं कहती है, क्योंकि वह आत्म- केन्द्रित नहीं है । भौतिक सुखों और उपलब्धियों के पीछे भागनेवाला साधक चमत्कार और प्रलोभन के पीछे किसी भी क्षण लक्ष्यच्युत हो सकता है । इस प्रकार जैन-साधना में यह माना गया है कि साधक को साधना के क्षेत्र में प्रविष्ट होने के लिए निष्कांक्षित अथवा निष्कामभाव से युक्त होना चाहिए । आचार्य अमृतचन्द्र ने पुरुषार्थसिद्धयुपाय में निष्कांक्षता का अर्थ - 'एकान्तिक मान्यताओं से दूर रहना' किया है ।" इस आधार पर अनाग्रह युक्त दृष्टिकोण सम्यक्त्व के लिए आवश्यक है ।
(३) निर्विचिकित्सा - विचिकित्सा के दो अर्थ हैं
१. उत्तराध्ययन, २८३१ ३. मूलाचार, २।५२-५३ ५. पुरुषार्थ सिद्धयुपाय २३
६१
:--
( अ ) मैं जो धर्म - क्रिया या साधना कर रहा हूँ इसका फल मुझे मिलेगा या नहीं, मेरी यह साधना व्यर्थ तो नहीं चली जावेगी, ऐसी आशंका रखना “विचिकित्सा "
Jain Education International
२. आचारांग १।५।५।१६३
४. रत्नकरण्ड श्रावकाचार, १२
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org