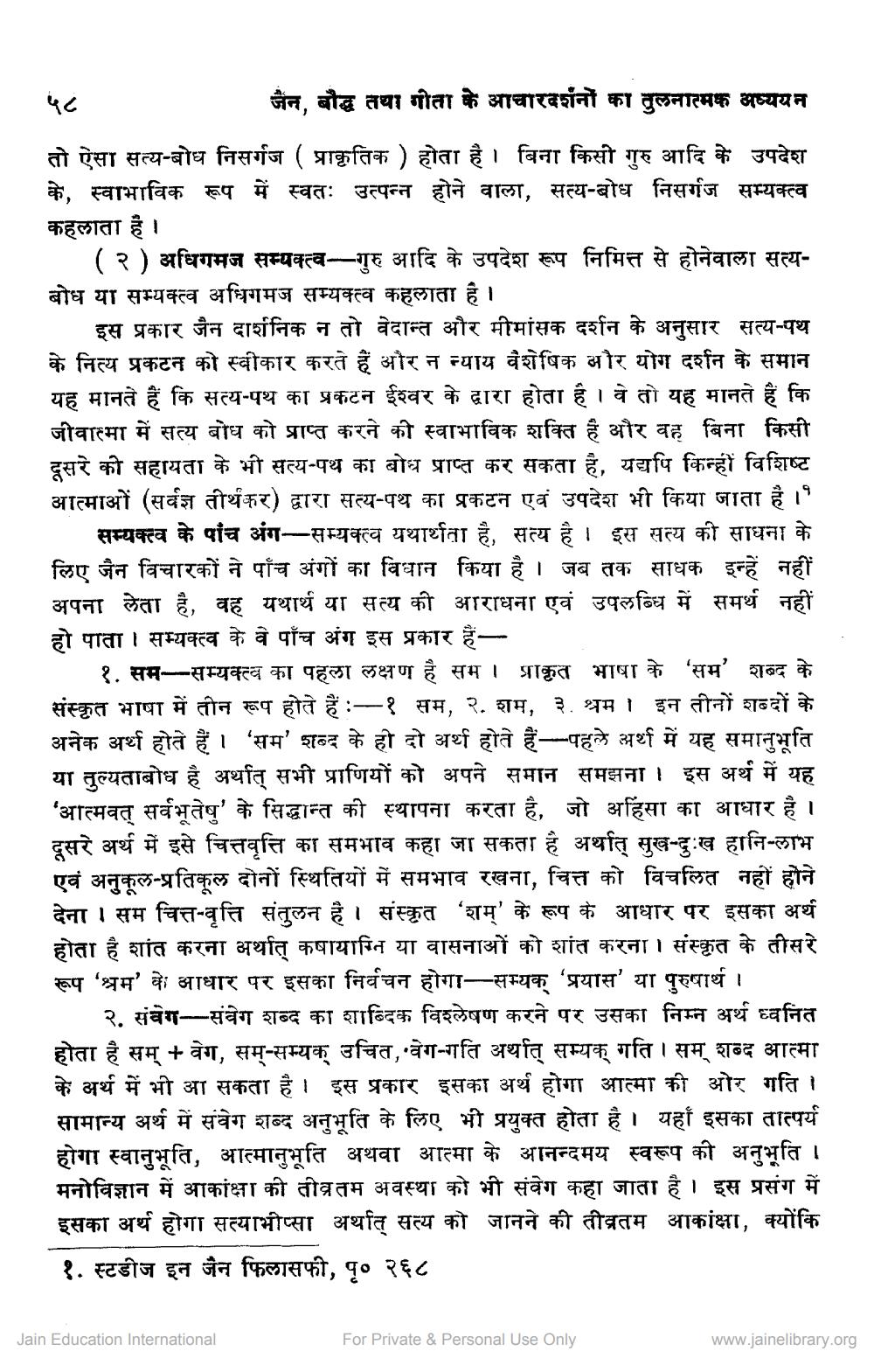________________
५८
जैन, बौद्ध तथा गीता के आचारवशनों का तुलनात्मक अध्ययन तो ऐसा सत्य-बोध निसर्गज ( प्राकृतिक ) होता है। बिना किसी गुरु आदि के उपदेश के, स्वाभाविक रूप में स्वतः उत्पन्न होने वाला, सत्य-बोध निसर्गज सम्यक्त्व कहलाता है।
(२) अधिगमज सम्यक्त्व-गुरु आदि के उपदेश रूप निमित्त से होनेवाला सत्यबोध या सम्यक्त्व अधिगमज सम्यक्त्व कहलाता है।
इस प्रकार जैन दार्शनिक न तो वेदान्त और मीमांसक दर्शन के अनुसार सत्य-पथ के नित्य प्रकटन को स्वीकार करते हैं और न न्याय वैशेषिक और योग दर्शन के समान यह मानते हैं कि सत्य-पथ का प्रकटन ईश्वर के द्वारा होता है । वे तो यह मानते हैं कि जीवात्मा में सत्य बोध को प्राप्त करने की स्वाभाविक शक्ति है और वह बिना किसी दूसरे की सहायता के भी सत्य-पथ का बोध प्राप्त कर सकता है, यद्यपि किन्हीं विशिष्ट आत्माओं (सर्वज्ञ तीर्थंकर) द्वारा सत्य-पथ का प्रकटन एवं उपदेश भी किया जाता है।'
सम्यक्त्व के पांच अंग-सम्यक्त्व यथार्थता है, सत्य है । इस सत्य की साधना के लिए जैन विचारकों ने पाँच अंगों का विधान किया है । जब तक साधक इन्हें नहीं अपना लेता है, वह यथार्थ या सत्य की आराधना एवं उपलब्धि में समर्थ नहीं हो पाता । सम्यक्त्व के वे पाँच अंग इस प्रकार हैं
१. सम-सम्यक्त्व का पहला लक्षण है सम । प्राकृत भाषा के 'सम' शब्द के संस्कृत भाषा में तीन रूप होते हैं :-१ सम, २. शम, ३. श्रम । इन तीनों शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं । 'सम' शब्द के ही दो अर्थ होते हैं--पहले अर्थ में यह समानुभूति या तुल्यताबोध है अर्थात् सभी प्राणियों को अपने समान समझना। इस अर्थ में यह 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' के सिद्धान्त की स्थापना करता है, जो अहिंसा का आधार है । दूसरे अर्थ में इसे चित्तवृत्ति का समभाव कहा जा सकता है अर्थात् सुख-दुःख हानि-लाभ एवं अनुकूल-प्रतिकूल दोनों स्थितियों में समभाव रखना, चित्त को विचलित नहीं होने देना । सम चित्त-वृत्ति संतुलन है। संस्कृत 'शम्' के रूप के आधार पर इसका अर्थ होता है शांत करना अर्थात् कषायाग्नि या वासनाओं को शांत करना। संस्कृत के तीसरे रूप 'श्रम' के आधार पर इसका निर्वचन होगा-सम्यक् 'प्रयास' या पुरुषार्थ ।
२. संवेग-संवेग शब्द का शाब्दिक विश्लेषण करने पर उसका निम्न अर्थ ध्वनित होता है सम् + वेग, सम्-सम्यक् उचित, वेग-गति अर्थात् सम्यक् गति । सम शब्द आत्मा के अर्थ में भी आ सकता है। इस प्रकार इसका अर्थ होगा आत्मा की ओर गति । सामान्य अर्थ में संवेग शब्द अनुभूति के लिए भी प्रयुक्त होता है। यहाँ इसका तात्पर्य होगा स्वानुभूति, आत्मानुभूति अथवा आत्मा के आनन्दमय स्वरूप की अनुभूति । मनोविज्ञान में आकांक्षा की तीव्रतम अवस्था को भी संवेग कहा जाता है। इस प्रसंग में इसका अर्थ होगा सत्याभीप्सा अर्थात् सत्य को जानने की तीव्रतम आकांक्षा, क्योंकि १. स्टडीज इन जैन फिलासफी, पृ० २६८
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org