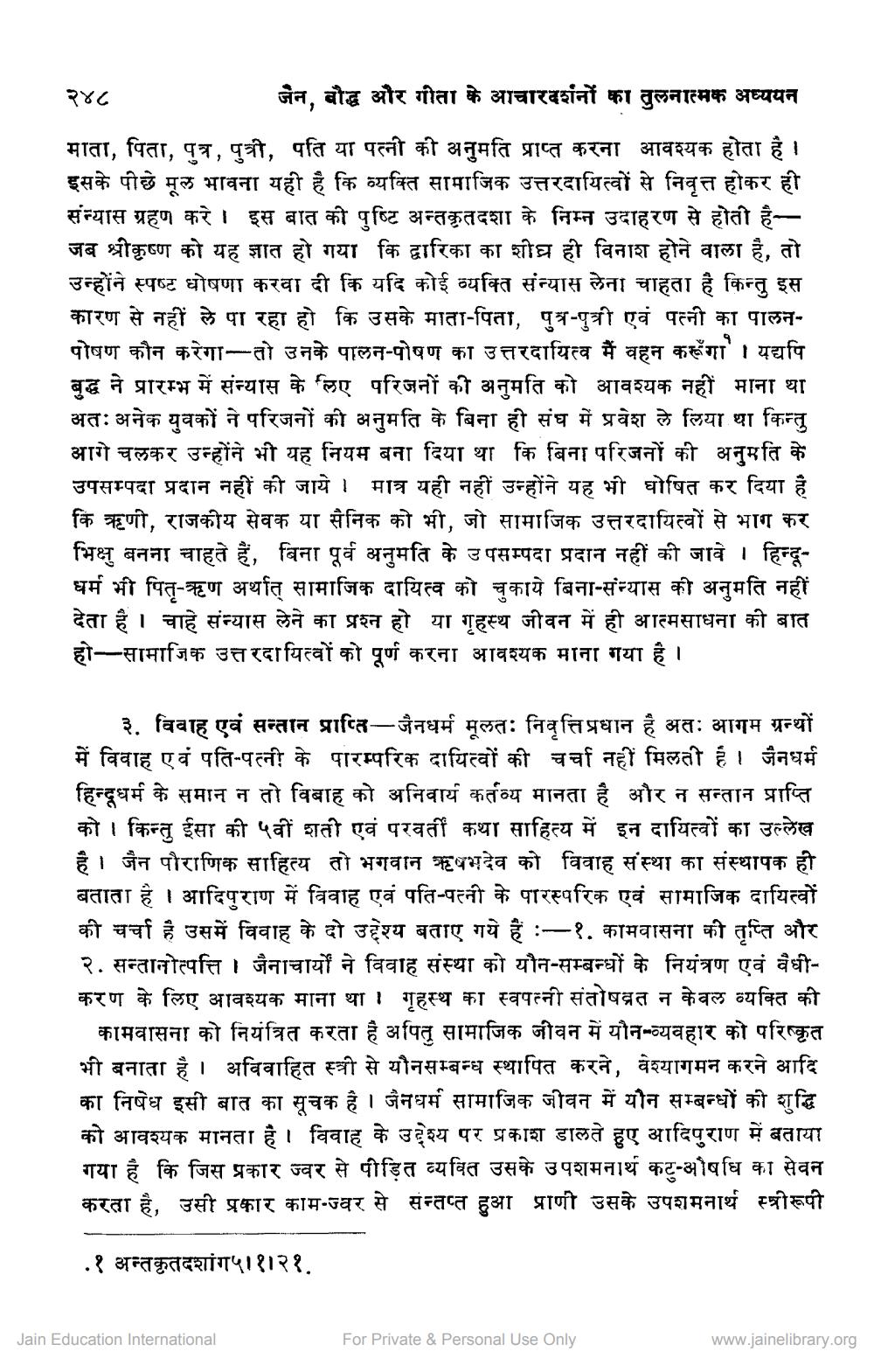________________
२४८
जैन, बौद्ध और गीता के आचारदर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन
माता, पिता, पुत्र, पुत्री, पति या पत्नी की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है । इसके पीछे मूल भावना यही है कि व्यक्ति सामाजिक उत्तरदायित्वों से निवृत्त होकर ही संन्यास ग्रहण करे | इस बात की पुष्टि अन्तकृतदशा के निम्न उदाहरण से होती हैजब श्रीकृष्ण को यह ज्ञात हो गया कि द्वारिका का शीघ्र ही विनाश होने वाला है, तो उन्होंने स्पष्ट घोषणा करवा दी कि यदि कोई व्यक्ति संन्यास लेना चाहता है किन्तु इस कारण से नहीं ले पा रहा हो कि उसके माता-पिता, पुत्र-पुत्री एवं पत्नी का पालनपोषण कौन करेगा -तो उनके पालन-पोषण का उत्तरदायित्व मैं वहन करूँगा । यद्यपि
-
बुद्ध ने प्रारम्भ में संन्यास के लिए परिजनों की अनुमति को आवश्यक नहीं माना था अतः अनेक युवकों ने परिजनों की अनुमति के बिना ही संघ में प्रवेश ले लिया था किन्तु आगे चलकर उन्होंने भी यह नियम बना दिया था कि बिना परिजनों की अनुमति के उपसम्पदा प्रदान नहीं की जाये । मात्र यही नहीं उन्होंने यह भी घोषित कर दिया है। कि ऋणी, राजकीय सेवक या सैनिक को भी, जो सामाजिक उत्तरदायित्वों से भाग कर भिक्षु बनना चाहते हैं, बिना पूर्व अनुमति के उपसम्पदा प्रदान नहीं की जावे । हिन्दूधर्म भी पितृ ऋण अर्थात् सामाजिक दायित्व को चुकाये बिना संन्यास की अनुमति नहीं देता है | चाहे संन्यास लेने का प्रश्न हो या गृहस्थ जीवन में ही आत्मसाधना की बात हो - सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूर्ण करना आवश्यक माना गया है ।
३. विवाह एवं सन्तान प्राप्ति - जैनधर्म मूलतः निवृत्तिप्रधान है अतः आगम ग्रन्थों में विवाह एवं पति-पत्नी के पारम्परिक दायित्वों की चर्चा नहीं मिलती है । जैनधर्म हिन्दूधर्म के समान न तो विबाह को अनिवार्य कर्तव्य मानता है और न सन्तान प्राप्ति को । किन्तु ईसा की ५वीं शती एवं परवर्ती कथा साहित्य में इन दायित्वों का उल्लेख है । जैन पौराणिक साहित्य तो भगवान ऋषभदेव को विवाह संस्था का संस्थापक ही बताता है । आदिपुराण में विवाह एवं पति-पत्नी के पारस्परिक एवं सामाजिक दायित्वों की चर्चा है उसमें विवाह के दो उद्देश्य बताए गये हैं। :- - १. कामवासना की तृप्ति और २. सन्तानोत्पत्ति | जैनाचार्यों ने विवाह संस्था को यौन सम्बन्धों के नियंत्रण एवं वैधीकरण के लिए आवश्यक माना था । गृहस्थ का स्वपत्नी संतोषव्रत न केवल व्यक्ति की
कामवासना को नियंत्रित करता है अपितु सामाजिक जीवन में यौन व्यवहार को परिष्कृत भी बनाता है । अविवाहित स्त्री से यौनसम्बन्ध स्थापित करने, वेश्यागमन करने आदि का निषेध इसी बात का सूचक है । जैनधर्म सामाजिक जीवन में यौन सम्बन्धों की शुद्धि को आवश्यक मानता है । विवाह के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए आदिपुराण में बताया गया है कि जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित व्यक्ति उसके उपशमनार्थ कटु औषधि का सेवन करता है, उसी प्रकार काम ज्वर से सन्तप्त हुआ प्राणी उसके उपशमनार्थ स्त्रीरूपी
. १ अन्तकृतदशांग५।१।२१.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org